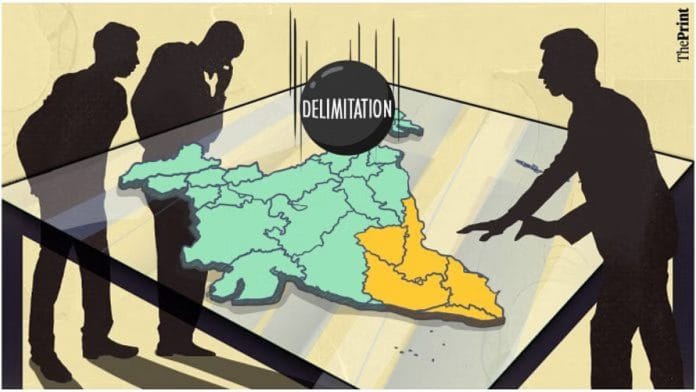भूगोल और जनसंख्या संघीय या परिसंघीय ढांचे के साफ-सुथरे खानों में पूरी तरह फिट नहीं बैठते. यही वजह है कि जनगणना से जुड़ी चर्चाओं में प्रतिनिधित्व और अनुपात का मुद्दा केंद्र में रहता है.
कितनी सीमा तक और कितने समय तक राजनीतिक प्रतिनिधित्व को आबादी के हिस्से से जोड़ा जाना चाहिए? निष्पक्ष प्रतिनिधित्व ज़रूरी है, लेकिन लोकतांत्रिक समाजों को अल्पसंख्यक आबादी और दूर-दराज़ इलाकों में रहने वाले लोगों के अधिकारों का भी संतुलन बनाना होता है.
शायद हम यूरोपीय संघ में अपनाए जाने वाले डिग्रेसिव प्रपोर्शनैलिटी (डीपी) के सिद्धांत से सीख ले सकते हैं. यूरोपीय संघ में सदस्य देशों की आबादी में बड़ा अंतर है—जर्मनी की आबादी 83.6 मिलियन है, जबकि लक्ज़मबर्ग और माल्टा की आबादी करीब पांच लाख है. यूरोपीय संघ के अनुच्छेद 14(2) में शामिल DP सिद्धांत यह सुनिश्चित करता है कि बड़े सदस्य देश यूरोपीय संसद (MEPs) में छोटे देशों की तुलना में ज्यादा प्रतिनिधि चुनें, लेकिन छोटे देशों में प्रति आबादी प्रतिनिधियों की संख्या बड़े देशों से ज्यादा हो. यह पूर्ण अनुपातिकता (जहां वोट की ताकत बराबर होती है) और पूरी समानता (जहां सबको तय संख्या में वोट मिलते हैं) के बीच का एक अच्छा रास्ता है.
भारतीय संदर्भ में, यह रवि के मिश्रा के सुझाव जैसा है: लोकसभा की कुल सीटों की संख्या इस तरह बढ़ाई जाए कि हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश (लक्षद्वीप और लद्दाख जैसे सबसे छोटे इलाकों को छोड़कर) को उसकी मौजूदा आबादी के आधार पर अनुपातिक प्रतिनिधित्व मिले और किसी भी राज्य की वर्तमान सीटों में एक भी सीट कम न हो. यह ‘एक व्यक्ति, एक वोट, एक मूल्य’ के सिद्धांत के सबसे करीब होगा. इससे सभी राज्यों में निर्वाचन क्षेत्रों की औसत आबादी भी कम होगी.
2011 की जनगणना के आंकड़ों के आधार पर गणना करते हुए, मिश्रा का तर्क है कि “राज्यों में आबादी और राजनीतिक प्रतिनिधित्व के बीच सामान्य संतुलन बनाए रखने के लिए हमें 728 लोकसभा सांसद होने चाहिए (एनएसए के तहत महिला सांसदों को जोड़ने के बिना). केरल और हिमाचल को छोड़कर सभी राज्यों को एक अतिरिक्त सांसद मिलेगा, लेकिन यूपी, बिहार और राजस्थान में क्रमशः 31, 22 और 19 सीटों की बढ़ोतरी होगी.”
इससे निश्चित तौर पर यूपी की राजनीतिक ताकत बढ़ेगी—भारत के सभी प्रधानमंत्री, मोरारजी देसाई (1977-79), नरसिंह राव (1991-96), एचडी देवगौड़ा (1996-97), आईके गुजराल (1997-98) और मनमोहन सिंह (2004-2014) को छोड़कर, या तो यूपी से रहे हैं या वहीं से चुने गए हैं.
LS की सीटों को ‘अनफ्रीज़’ करना और RS की सीटें बरकरार रखना
दक्षिणी राज्यों में ‘नुकसान’ की भावना को कम करने का एक और व्यावहारिक तरीका यह हो सकता है कि कम से कम 2047—भारत की आज़ादी के 100वें वर्ष—तक राज्यसभा की सीटों को बिना बदले रखा जाए. इससे यह सुनिश्चित होगा कि जहां लोकसभा मतदाता वर्ग की राजनीतिक ताकत को दर्शाएगी, वहीं राज्यसभा राज्यों के हितों को सामने रखती रहेगी. यह सही है कि धन विधेयकों और सामान्य निर्णयों में इसकी शक्तियां सीमित हैं, लेकिन संविधान संशोधन के मामलों में इसके पास समान अधिकार होते हैं और नए अखिल भारतीय सेवाओं के गठन के समय इसकी भूमिका बेहद अहम होती है.
यहां यह भी बताना ज़रूरी है कि कई संघीय व्यवस्थाओं में (अमेरिका सहित), ऊपरी सदन में हर घटक इकाई को समान महत्व दिया जाता है.
बड़े राज्यों का पुनर्गठन
2027 की जनगणना के बाद होने वाले परिसीमन में एक ऐसी स्थिति से भी निपटना होगा, जहां डिग्रेसिव प्रपोर्शनैलिटी के बावजूद छोटे राज्यों—सिक्किम, मिजोरम, नागालैंड और यूपी, राजस्थान, बिहार, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र जैसे बड़े राज्यों के बीच असमानता दूर नहीं हो पाएगी. इसलिए दो संभावित विकल्प सामने आते हैं: बड़े राज्यों का पुनर्गठन, ताकि नए राज्यों की मांग करने वालों—विदर्भ, पूर्वांचल, मिथिला, उत्तर आंध्र प्रदेश, बुंदेलखंड और मारवाड़, को ज्यादा आवाज़ मिल सके; साथ ही गोरखालैंड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन की तर्ज पर क्षेत्रीय स्वायत्तता और भाषाई परिषदों व मातृभाषा में शिक्षा के लिए राज्य का समर्थन.
रिकॉर्ड के लिए, नवंबर 2011 में यूपी विधानसभा द्वारा पारित प्रस्ताव में यूपी को बुंदेलखंड, पूर्वांचल, अवध प्रदेश और पश्चिम प्रदेश में पुनर्गठित करने पर विचार किया गया था. हालांकि, इन तीनों के विपरीत, बुंदेलखंड एक अंतर-राज्यीय पुनर्गठन का मामला बनता है. झांसी, चित्रकूट, बांदा, जालौन, हमीरपुर, महोबा और ललितपुर के सात जिलों के अलावा, पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश के सागर, छतरपुर, टीकमगढ़, दमोह और दतिया व पन्ना जिलों में भी बुंदेला पहचान मानी जाती है.
राज्यों का नए सिरे से (De novo) पुनर्गठन
एक और, इससे भी ज्यादा बड़े बदलाव का सुझाव गौतम देसीराजू ने दिया है (किताबों के लेखक— Bharat: India 2.0 और Delimitation and States Reorganization: For a Better Democracy in Bharat).
वह देश की राजनीतिक सीमाओं का नए सिरे से पुनर्गठन करने का सुझाव देते हैं—करीब समान जनसंख्या वाले 75 राज्यों में, जहां क्षेत्र की सांस्कृतिक, भाषाई, आर्थिक और राजनीतिक आकांक्षाएं पूरी तरह मेल खाती हों. उनका तर्क है कि यह व्यवस्था भारत की राजनीतिक सोच के ज्यादा अनुकूल है, बजाय उन प्रशासनिक प्रांतों के, जो ब्रिटिश राज की विरासत हैं. महाभारत के समय में भी भारत (आज के अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश के इलाकों को छोड़कर) में लगभग इतनी ही संख्या में राजनीतिक इकाइयां थीं—राज्य, गणराज्य और अर्ध-स्वायत्त क्षेत्र, जो अपने-अपने स्तर पर स्वतंत्र थीं, लेकिन भारत की पवित्र और राजनीतिक भू-रचना का हिस्सा थीं. उनका मानना है कि राज्यों के पुनर्गठन आयोग द्वारा अपनाया गया ढांचा वास्तव में साइमन कमीशन की सिफारिशों और 1935 के भारत सरकार अधिनियम की ही निरंतरता था.
वह ऐसे पुनर्गठन का सुझाव देने वाले पहले व्यक्ति नहीं हैं. सत्तर के दशक में सांसद, राजनीतिक वैज्ञानिक और कांग्रेस सांसद रशीदुद्दीन खान ने देश के सांस्कृतिक और कृषि-जलवायु क्षेत्रों के अनुरूप 56 इकाइयों वाला एक संघीय भारत प्रस्तावित किया था.
शक्ति संतुलन
यह सच है कि पिछले सात दशकों में शक्ति संतुलन राज्यों से केंद्र की ओर खिसक गया है. यह इस बात से भी दिखता है कि केंद्रीय बजट—करीब 56 लाख करोड़ रुपये—सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के कुल बजट—करीब 50 लाख करोड़ रुपये, से काफी ज्यादा है.
इसके अलावा, जैसे-जैसे अर्थव्यवस्था एकीकृत होती जा रही है, स्वास्थ्य से लेकर शिक्षा और कौशल विकास तक के कल्याण कार्यक्रम नीति और फंडिंग—दोनों के लिए, केंद्र सरकार पर ज्यादा निर्भर होते जा रहे हैं. जीएसटी राजस्व संग्रह का मुख्य स्रोत बन गया है और राज्यों का ध्यान सेवाओं की डिलीवरी और तेज़ी से क्रियान्वयन पर केंद्रित हो गया है. संघीय नीति के नज़रिये से देखें तो राज्यों को नुकसान हुआ है—राजनीतिक और आर्थिक ताकत दोनों में, लेकिन नागरिक सेवाओं के मामले में राज्यों की भूमिका ज्यादा सीधी और तात्कालिक हो गई है.
अगर ऐसा है, तो छोटे राज्यों का विचार ज्यादा तार्किक लगता है.
फायदे और नुकसान
ऊपर दिए गए किसी भी विकल्प में सिर्फ फायदे ही नहीं हैं, नुकसान भी हैं. वास्तव में, जनगणना के तुरंत बाद और परिसीमन आयोग के गठन की घोषणा के साथ ही—हर एक निर्वाचन क्षेत्र, नए राज्यों के गठन, क्षेत्रों के शामिल या बाहर किए जाने, को लेकर प्रस्तुतियों की संख्या काफी बढ़ जाएगी.
जहां शिक्षाविदों और विश्लेषकों की आवाज़ें अभी भी संतुलित रह सकती हैं, वहीं राजनीतिक टकराव काफी तीखा होगा. दिलचस्प गठजोड़ देखने को मिलेंगे—जैसे टीडीपी और द्रविड़ दल, जो यथास्थिति बनाए रखने की बात करेंगे; जबकि आरजेडी और सपा यूपी और बिहार के लिए ज्यादा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना चाहेंगे; टीएमसी और शिवसेना पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र के पुनर्गठन का विरोध करेंगे और बीजेपी के लिए केंद्र और राज्यों—दोनों में अपनी पकड़ चाहने वाली अपनी सभी इकाइयों के हितों में संतुलन बनाना बेहद कठिन होगा.
एक बार अगर यह ‘भीड़ का छत्ता’ छेड़ा गया, तो इससे क्या नतीजे निकलेंगे—कहना मुश्किल है.
(यह भारत में जनगणना पर चार-पार्ट की सीरीज़ का आखिरी लेख है, जो NUJS कोलकाता में वार्षिक न्यायिक सम्मेलन में दिए गए की-नोट भाषण पर आधारित है.)
संजीव चोपड़ा एक पूर्व आईएएस अधिकारी हैं और वैली ऑफ वर्ड्स साहित्य महोत्सव के निदेशक हैं. हाल तक वे LBSNAA के निदेशक रहे हैं और लाल बहादुर शास्त्री मेमोरियल (एलबीएस म्यूज़ियम) के ट्रस्टी भी हैं. वे सेंटर फॉर कंटेम्पररी स्टडीज़, पीएमएमएल के सीनियर फेलो हैं. उनका एक्स हैंडल @ChopraSanjeev है. यह लेख लेखक के निजी विचार हैं.
(इस लेख को अंग्रेज़ी में पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)
यह भी पढ़ें: जनगणना 2027 में प्रवासी मज़दूर कहां गिने जाएंगे—जन्मभूमि या कर्मभूमि?