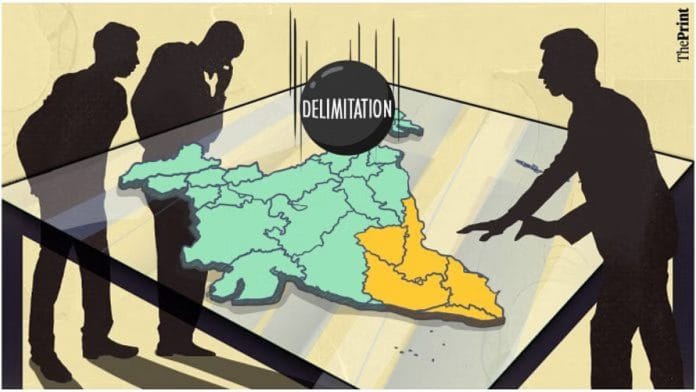कहा जाता है कि समय पर लगाया गया एक टांका 99 और टांके लगाने से बचाता है, लेकिन वक्त जब पांच दशक जितना लंबा हो तो खुद कपड़ा ही तार-तार होने के कगार पर पहुंच जाता है.
संसदीय चुनाव क्षेत्रों के परिसीमन (डिलिमिटेशन) की कवायद को 50 साल से जिस तरह ठंडे बस्ते में डाल कर रखा गया उसके चलते उत्तर और दक्षिण भारत के बीच कड़वा विवाद छिड़ गया है. इसकी अंतिम कवायद 25 वर्ष की अवधि के लिए इमरजेंसी के दौरान 1976 में शुरू की गई थी. रवि के. मिश्र की किताब ‘डेमोग्राफी, रिप्रेजेंटेशन ऐंड डिलिमिटेशन’ बताती है कि आज जो बहस छिड़ी हुई है उसमें अप्रामाणिक बातों ने तथ्यों को धूमिल कर दिया है.
इस बहस में, लोकसभा सांसदों की संख्या के मामले में राज्यों के बीच संतुलन से लेकर वित्त आयोग द्वारा आबादी आधारित फंड वितरण जैसे कई मसले गड्डमड्ड हो गए हैं. इस वजह से इस विवादास्पद मसले पर आम सहमति बना पाना काफी चुनौतीपूर्ण हो गया है.
परिसीमन क्या है और क्या कहते हैं अनुच्छेद 81-82
पहले हम यह समझ लें कि परिसीमन का मतलब क्या है. इसका शाब्दिक अर्थ यह है कि यह विधायिका नाम की संस्था वाले देश में चुनाव क्षेत्रों की भौगोलिक सीमा तय करने की प्रक्रिया. भारत यह काम ‘परिसीमन आयोग’ (या सीमा आयोग) नामक उच्च अधिकार-प्राप्त संस्था को सौंपा जाता है जिसके आदेश को कानून के बराबर माना जाता है और उसे किसी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती. ऐसे आयोग का गठन चार बार किया गया है — 1952 में (परिसीमन आयोग अधिनियम, 1952 के तहत); 1962 में (1962 के अधिनियम के तहत); 1972 में (1972 के अधिनियम के तहत); और 2002 में (2002 के अधिनियम के तहत). इस संदर्भ में हमें यह ज़रूर समझना चाहिए कि संविधान के अनुच्छेद 81 और 82 क्या हैं, जिन्हें समय-समय पर संशोधित किया जाता रहा है.
अनुच्छेद-81 का ताल्लुक लोकसभा की संरचना से है, जबकि अनुच्छेद-82 आदेश देता है कि हर एक जनगणना के बाद सीटों का समायोजन ज़रूर किया जाना चाहिए. यह अनुच्छेद यह भी कहता है कि सीमाओं को पुनः परिभाषित किया जाना चाहिए. संविधान जब पहली बार लागू किया गया था तब लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 500 तय की गई थी और 494 सांसद चुने गए थे; हर एक सांसद करीब 7.5 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहा था. बेशक कुछ भिन्नताएं भी थीं. मतदाताओं की संख्या और चुनाव क्षेत्र का आकार जनसंख्या के स्वरूप, भूगोल और इतिहास के जटिल मिश्रण से भी तय होता है. इसके दस साल बाद, आबादी में बढ़ोतरी और राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर राज्यों के पुनर्गठन के बाद सांसदों की संख्या 1963 में 525 और 1973 में 542 कर दी गई. कर्नाटक और केरल जैसे राज्यों से लोकसभा सांसदों की संख्या में एक की वृद्धि की गई जबकि मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र को तीन-तीन ज्यादा संसद मिले.
आज स्थिति यह है कि अनुच्छेद 81(2) ने लोकसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या 550 तय कर दी है, जिनमें 530 सदस्य राज्यों से और 20 सदस्य आठ केंद्रशासित प्रदेशों से होंगे. परिच्छेद 81(2)(ए) कहता है कि आबादी और सीट का अनुपात सभी राज्यों में यथासंभव समान होना चाहिए. परिच्छेद 81(2)(बी) कहता है कि हर एक राज्य को भौगोलिक चुनाव क्षेत्रों में इस तरह बांटा जाना चाहिए कि हर एक चुनाव क्षेत्र में आबादी और आवंटित सीटों की संख्या का अनुपात पूरे राज्य में लगभग एक समान हो.
यह भी पढ़ें: तीसरी और पांचवीं लोकसभा चुनाव के बीच भारतीय लोकतंत्र कैसे बदला?
1976 तक तो हर दस साल पर होने वाली जनगणना के बाद लोकसभा, राज्यसभा और राज्यों की विधानसभाओं की सीटों की संख्या इस तरह तय की जाती रही ताकि आबादी के प्रतिनिधित्व का समान अनुपात बना रहे, लेकिन इमरजेंसी के दौरान 42वें संविधान संशोधन ने संसद और विधानसभाओं में सीटों की संख्या 2001 की जनगणना के आधार पर स्थिर कर दी. इस फैसले को आगे बढ़ाने में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की प्रमुख भूमिका निभाई. उन्होंने इसे विभिन्न राज्यों में परिवार नियोजन के मामले में असमान प्रगति का हवाला देकर सही ठहराया. इसके पीछे सोच यह था कि दो दशकों के अंदर भारत के सभी राज्य समान सकल प्रजनन दर (टीएफआर) हासिल कर लेंगे.
लेकिन वैश्विक रुझानों के विपरीत भारत ने आर्थिक-जनसांख्यीकीय विरोधाभास को उजागर किया. आर्थिक उत्पादन करने वाले क्षेत्र प्रवासियों के आगमन के कारण आबादी में तेज़ वृद्धि दर्ज करते हैं, लेकिन भारत में राज्यों के बीच प्रवासियों की पहली लहर में केवल पुरुष ही थे जो उत्पादन और निर्माण के क्षेत्रों में रोज़गार ढूंढने निकले थे. महिलाएं खेतीबाड़ी संभालने के लिए रुक गई थीं. कुछ समय बाद पूरा परिवार ही शहरों में जाने लगा और अक्सर दूसरे राज्यों में जाने लगा. यह कहानी कितनी सच्ची है यह अगली जनगणना से ही पता चल पाएगा.
आबादी के हिसाब से संतुलन बिताने के लिए 2001 में चुनाव क्षेत्रों की सीमाओं का पुनर्निर्धारण किया गया, लेकिन हर एक राज्य में लोकसभा और विधानसभा की सीटों की संख्या में परिवर्तन नहीं किया गया. यह 84वें संविधान संशोधन के कारण हुआ, जिसने उनकी संख्या में 2026 तक परिवर्तन करने से रोक लगा दी थी, लेकिन इसके विरोध में कुछ आवाज़ें उठी थीं. पूर्व लोकसभा अध्यक्ष शिवराज पाटील और सोमनाथ चटर्जी ने चेतावनी दी थी की इस तरह की रोक के कारण जनप्रतिनिधित्व में असमानता पैदा हो रही है क्योंकि कुछ सांसद पांच लाख से कम मतदाताओं का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं जबकि कुछ सांसद 30 लाख से ज्यादा की आबादी वाले चुनाव क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं. इस परिप्रेक्ष्य से देखें तो पता चलेगा कि उत्तर भारत ने अपने मतदाताओं को उतना समानुपातिक राजनीतिक वजन नहीं दिया.
यह भी पढ़ें: भारत में लोकसभा चुनाव कराने की रणनीति कितनी चौंका देने वाली है? पहली से 18 तारीख तक
परिसीमन मसले पर एकजुट हुआ दक्षिण
लेकिन पूरी दक्षिण भारतीय राजनीतिक जमात, जिसमें सभी पार्टियां शामिल हैं, परिसीमन की अगली प्रक्रिया को एक सुर में भारत के संघीय ढांचे के लिए खतरा बता रही है. सभी विचारधारा के नेता एक तरह के तर्क दे रहे हैं. उदाहरण के लिए कांग्रेस के शशि थरूर ने कहा कि “इस तर्क में कुछ दम तो है कि लोकतंत्र में सभी नागरिकों को समान माना जाना चाहिए, चाहे वह एक प्रगतिशील राज्य में रहता हो या ऐसे राज्य में जिसने अपनी महिलाओं को इतना सक्षम नहीं बनाया कि प्रजनन दर में कमी ला सके और अपनी आबादी को बेहिसाब बढ़ने दिया, लेकिन कोई संघीय लोकतंत्र इस धारणा को लेकर चल नहीं सकता कि कोई राज्य अगर अपना अच्छा विकास करता है तो उसका राजनीतिक वजन घट सकता है जबकि दूसरे राज्यों को अपनी नाकामी के लिए संसद में ज्यादा सीटों का इनाम मिल सकता है.” ज़ाहिर तौर पर वे केरल और बिहार जैसे राज्यों की ओर इशारा कर रहे हैं.
यह विचार टीडीपी के चंद्रबाबू नायडू, डीएमके के एम.के. स्टालिन, या सीपीएम के एम.ए. बेबी के विचार से भिन्न नहीं है. वास्तव में, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री नायडू और तमिलनाडु के स्टालिन ने तो अपने मतदाताओं से यह मज़ाकिया अपील तक की है कि भविष्य में जनसंख्या का लाभ उठाने के लिए वह ज्यादा बच्चे पैदा करें. पूर्व कैबिनेट सेक्रेटरी के.एम. चंद्रशेखर ने भी चेताया है कि “दक्षिण के सभी राज्यों का राजनीतिक प्रभाव उत्तर के राज्यों के मुकाबले कम हो जाएगा”. सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश के.एम. जोसफ ने तो और आगे बढ़कर यह कहा कि “इस तरह का परिसीमन होगा तो केरल और तमिलनाडु जैसे राज्यों में चुनाव क्षेत्रों की संख्या कम हो जाएगी और अपनी आबादी पर काबू न कर पाने वाले बिहार और उत्तर प्रदेश में चुनाव क्षेत्रों की संख्या बढ़ जाएगी. तब भारत में संघीय व्यवस्था का क्या होगा? भारतीय संघ की जो अवधारणा थी उसका क्या होगा?”
इतिहासकार रामचंद्र गुहा ने भी पत्रिका ‘फॉरेन अफेयर्स’ में लिखा है कि “भारतीय संघीय व्यवस्था पर जो दबाव पड़ रहा है वह 2026 में उबाल पर आ सकता है…उत्तर और दक्षिण भारत के बीच आज जो हल्की दरार है वह तब असली खाई में बदल सकती है”. दबाव बेशक वास्तविक हैं, लेकिन भारतीय राजनीतिक व्यवस्था ने भाषायी आधार पर राज्यों के पुनर्गठन जैसे जटिल मसले और विकास संबंधी मांगों का जिस तरह समाधान किया उसके मद्देनज़र सतर्क आशावाद की गुंजाइश बनती है. अपेक्षाओं और दावों के बीच अंततः किसी तरह का तालमेल उभर जाएगा. भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए और कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूपीए गठबंधनों के सहयोगी पूरे देश मैं फैले हैं, वह ज़ोर-शोर से विधानसभाओं के चुनाव लड़ते हैं और जिला परिषद से लेकर नगरपालिकाओं आदि तक हर स्तर पर शासन पर अपनी छाप छोड़ते हैं.
विपरीत तथ्य क्या हैं
विपरीत तथ्य जानना भी महत्वपूर्ण है. वह यह कि संविधान निर्माताओं ने अनुच्छेद 82 को जिस मकसद से दर्ज किया था अगर वह उसी मकसद के साथ लागू होता तो क्या होता? सीटों के आवंटन में परिवर्तन धीरे-धीरे और शायद कम विवादास्पद तरीके से किया जाता. लोकसभा में प्रतिनिधित्व में कमी की भरपाई के लिए वैकल्पिक व्यवस्था लागू की जाती जिसके तहत, राज्यों के सरोकारों का समाधान करने के लिए फंड के वितरण का अलग फॉर्मूला अपनाया जाता या अंतर्राज्यीय परिषदों को अधिक मजबूत बनाया जाता, लेकिन इसकी जगह मसले को लंबे समय तक ठंडे बस्ते में डाले रखने से एक ऐसा राजनीतिक टाइम बम तैयार हो गया है जिसे भारतीय लोकतंत्र को बड़ी सावधानी, आम सहमति और संवैधानिक दूरदर्शिता के साथ बेअसर करना ही होगा.
(भारत के परिसीमन विवाद पर दो-पार्ट की सीरीज़ का यह पहला लेख है.)
(संजीव चोपड़ा पूर्व आईएएस अधिकारी हैं और वैली ऑफ वर्ड्स के फेस्टिवल के निदेशक रहे हैं. हाल तक वे लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी के निदेशक थे. उनका एक्स हैंडल @ChopraSanjeev हैं. व्यक्त किए गए विचार निजी हैं.)
(इस लेख को अंग्रेज़ी में पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें.)
यह भी पढ़ें: आपातकाल की विरासत? 1977-1989 के लोकसभा चुनावों ने भारत के राजनीतिक परिदृश्य को कैसे बदला