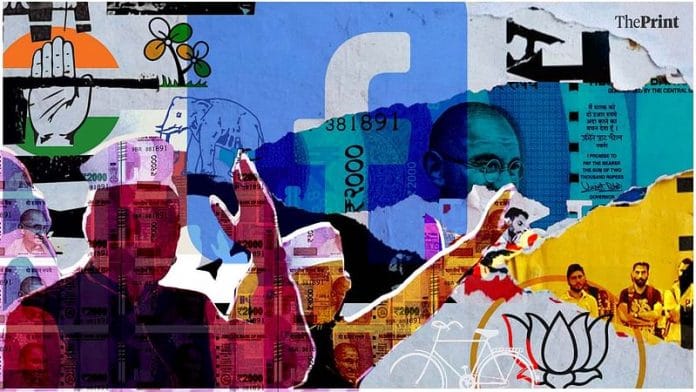बिहार में लोकतांत्रिक प्रक्रिया को झटका दिया गया है. भारतीय चुनाव आयोग (ईसीआई) ने घोषणा कर दी है कि जो लोग अपनी नागरिकता साबित करेंगे उन्हें ही राज्य के अगले विधानसभा चुनाव में वोट देने दिया जाएगा.
जो नागरिक हैं वे ही मतदान कर सकते हैं, इस सुज्ञात संवैधानिक सिद्धांत की याद दिलाना कोई गलत बात नहीं है. लेकिन नागरिकता साबित करने का जो तरीका अपनाया जा रहा है, और इसके लिए जरूरी दस्तावेजों की जो सूची जारी की गई है उन सबसे सभी नागरिकों को वोट देने का अधिकार सुनिश्चित नहीं होता. बल्कि उन्हें खासकर नागरिकों के वंचित तबकों को मताधिकार से वंचित करने की स्थिति पैदा होती है. सिद्धांततः जो एक समावेशी विचार है, जिसका नाम नागरिकता है वह व्यवहार में बहिष्कार का साधन बन सकता है.
बिहार में लोकतांत्रिक प्रक्रिया को जो झटका दिया गया है उसके महत्व को समझने में इतिहास और तुलना मददगार हो सकती है.
नागरिक और प्रजा
आधुनिक राजनीतिशास्त्र में, ‘प्रजा’ और ‘नागरिक’ में काफी अंतर किया जाता रहा है. आधुनिक काल से पहले की राजनीतिक व्यवस्थाओं में लोग प्रजा हुआ करते थे. यह व्यवस्था आधुनिक काल में भी रिस कर आ गई. राजाओं की प्रजा हुआ करती थी जिसके अधिकार और हक़ राजा की कृपा पर निर्भर होते थे.
इसके विपरीत, नागरिकता मूलतः एक आधुनिक अवधारणा है जिसका जन्म 18वीं सदी के अंत में हुआ अमेरिकी और फ्रांसीसी क्रांतियों के साथ हुआ. सिद्धांततः, नागरिकता का अर्थ है किसी राजनीतिक समुदाय की सदस्यता और इसके कारण मिलने वाले अधिकार. नागरिकता से जुड़े अधिकार शाही मर्जी पर निर्भर नहीं होते. नागरिकता समावेशी और समतामूलक होती है, जबकि प्रजा की अवधारणा बहिष्कारी है क्योंकि इसमें विभिन्न वर्गों को विभिन्न तरह के अधिकार दिए जाते हैं.
बीसवीं सदी में, जब ज्यादा से ज्यादा (सभी नहीं) आधुनिक राजनीतिक व्यवस्थाएं लोकतांत्रिक होती गईं तब मताधिकार नागरिकता से जुड़े अधिकारों में शामिल होता गया जिसमें वर्ग, जाति या लिंग के आधार पर भेद नहीं किया जाता. दूसरे विश्वयुद्ध के बाद, सार्वभौमिक मताधिकार लोकतांत्रिक नागरिकता की जीवनी-शक्ति बन गया.
इतिहास में ऐसे उदाहरण मिलते हैं जब नागरिकता के समावेशी स्वरूप को बहुत कमजोर किया गया. चुनाव आयोग बिहार में जो कुछ करने की कोशिश कर रहा है उसके नतीजों के बारे में विचार करते हुए हमें अतीत के ऐसे उदाहरणों को ध्यान में रखना होगा.
नागरिकता में कटौती का सबसे चर्चित और क्रूर मामला 1880 के दशक से लेकर 1960 के दशक तक अमेरिका के दक्षिणी भाग का है. 1865 में, मुख्यतः रिपब्लिकनों के नेतृत्व वाले उत्तरी अमेरिका और डेमोक्रेटों के नेतृत्व वाले दक्षिणी अमेरिका के बीच गृहयुद्ध (जिसमें उत्तर की जीत हुई थी) की समाप्ति के बाद अमेरिकी संविधान में 13वें संशोधन के जरिए दास प्रथा को खत्म किया गया, 14वें संशोधन के जरिए अश्वेत अमेरिकियों को पहली बार नागरिकता प्रदान की गई, और 15वें संशोधन ने वयस्क अश्वेत पुरुषों को मताधिकार प्रदान किया. 1873-74 तक दक्षिण के 80-85 फीसदी अश्वेतों ने वोट देने के लिए अपना नाम दर्ज करा लिया था. 1876 के बाद डेमोक्रेट दक्षिण के राज्यों में सत्ता हासिल करने लगे. उनका एक सबसे बड़ा राजनीतिक लक्ष्य था— अश्वेतों को मताधिकार से वंचित करना.
ऐसा उन्होंने किस तरह किया? साक्षरता को कसौटी बनाकर, वोट टैक्स लगाकर, और तमाम तरह के दस्तावेजों की मांग करके. अश्वेत अमेरिकियों में साक्षरता दर काफी नीची थी, और उनकी आमदनी इतनी कम थी कि वे मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए वोट टैक्स नहीं दे सकते थे. इन वजहों से दक्षिण के अश्वेतों के विशाल बहुमत ने अपना मताधिकार खो दिया. 1870 के दशक के मध्य में 84-85 फीसदी अश्वेत वोट दे रहे थे, तो 1904-05 में महज 4-5 फीसदी अश्वेत ही मताधिकार का प्रयोग कर रहे थे. 1965 में जाकर अमेरिका में सार्वभामिक मताधिकार लागू हुआ. यानी मताधिकार में कटौती सात-आठ दशक तक जारी रही.
बिहार का भी वही हाल
बिहार के लिए चुनाव आयोग की योजना भी अमेरिकी उदाहरण के समान है. बुनियादी समानता, और बड़ा आश्चर्य यह है कि अमेरिका की तरह बिहार में भी खुद को मतदाता के रूप में दर्ज करवाने का ज़िम्मेदारी नागरिकों के ऊपर डाल दी गई है, जबकि हमेशा से यह सरकार की ज़िम्मेदारी रही. अब वोट देने के लिए लोगों को सबूत देना होगा कि वे नागरिक हैं. भारत के निर्माताओं ने सोचा था कि गरीब नागरिक इतने साक्षर नहीं होंगे कि वे मतदाता के रूप में अपना नाम दर्ज करवाने के लिए आगे आ सकें. इसलिए सरकार ही अपने विशाल संसाधनों का इस्तेमाल करते हुए उन तक पहुंचेगी और उनका नाम मतदाता सूची में दर्ज करेगी.
दूसरी समानता साक्षरता के मामले में है. पिछली जनगणना (2011) के मुताबिक बिहार में साक्षरता दर मात्र 61.8 फीसदी थी (जबकि भारत की 73 फीसदी थी). अनपढ़ नागरिकों के पास वे दस्तावेज़ (जन्म प्रमाणपत्र, पासपोर्ट, मैट्रिक का सर्टिफिकेट आदि) होने की संभावना कम ही होती है, जिनकी मांग चुनाव आयोग नागरिकता के सबूत के तौर पर कर रहा है.
जो लोग अस्थायी तौर पर बिहार से बाहर रह रहे हैं और जिनके पास बिहार में दर्ज दस्तावेज़ हैं या नहीं हैं उनसे कहा गया है कि वे किसी कंप्यूटर से उस आवेदनपत्र की प्रति हासिल करें, उसे भरें और चुनाव आयोग की वेबसाइट या उसके एप पर अपलोड करें. दिल्ली, मुंबई, बंगलूरू, चेन्नै आदि में दरबान, गार्ड, मजदूर के रूप में काम कर रहे लाखों प्रवासी बिहारियों के लिए यह शर्त पूरी करना असंभव ही है.
नागरिकता की तलवार
समस्या इसलिए भी गंभीर हो गई है कि भारत सरकार नागरिकता का कोई एक दस्तावेज़ नहीं जारी करती. पढ़े-लिखे लोगों समेत कम ही लोगों के पास जन्म प्रमाणपत्र या पासपोर्ट होगा. नागरिकता का दावा कई तरह के दस्तावेजों के आधार पर किया जाता है. पुरानी प्रथा यही चल रही है कि जो भी खुद को नागरिक बताता है और वोट देना चाहता है उसे नागरिक या मतदाता मान लिया जाता है, बशर्ते उसके दावे को कोई चुनौती नहीं दे और उसके खिलाफ अधिसूचना न जारी हुई हो.
अयोग्य मतदाता की समस्या को दस्तावेज़ के आधार पर हल करने की प्रक्रिया, जिसमें पूरी ज़िम्मेदारी नागरिकों के ऊपर डाल दी गई है, उन्हें बहिष्कृत करने वाली प्रक्रिया ही है. समाज विज्ञान संबंधी अनुसंधान से जुड़े सब लोगों को मालूम है कि दस्तावेज़ की पर्याप्तता का विचार गरीबों और अनपढ़ों (जिस स्थिति को उन्होंने चुना नहीं है बल्कि जिसके वे भुक्तभोगी हैं) के हक के खिलाफ जाता है.
इस उपक्रम के कारण कौन-से समुदाय मताधिकार से वंचित होंगे? बिहार के अधिकतर गरीबों में दलित, मुस्लिम, और निम्न वर्गीय ओबीसी (बिहार में आदिवासी समुदाय काफी छोटा है) शामिल हैं. मतदाताओं में ऊंची जातियां और उच्चवर्गीय ओबीसी असमान अनुपात में होंगे. मतदान के आंकड़े बताते हैं कि ऐसे समुदाय भी हैं जो भाजपा को जम कर वोट देते हैं. अब यह साबित करना मुमकिन हो या नहीं कि चुनाव आयोग यह चाहता है या नहीं, मगर यह जो नयी प्रक्रिया चलाई जा रही है उससे भाजपा का ही पलड़ा भारी होने जा रहा है.
निष्पक्ष और समावेशी चुनाव भारतीय लोकतंत्र की पहचान रही है. भारत को इसे फिर से हासिल करना है. संस्थागत आदेश के जरिए मताधिकार से वंचित करना बिलकुल अलोकतांत्रिक कदम है. नागरिकता सिद्धांततः तो एक समावेशी राजनीतिक विचार है, लेकिन व्यवहार में उसे नागरिकों को बहिष्कृत करने के हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है.
आशुतोष वार्ष्णेय इंटरनेशनल स्टडीज़ और सोशल साइंसेज़ के सोल गोल्डमैन प्रोफेसर और ब्राउन यूनिवर्सिटी में पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर हैं. व्यक्त विचार निजी हैं.
(इस लेख को अंग्रेज़ी में पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)
यह भी पढ़ें: रणवीर इलाहाबादिया के साथ सरकार को क्या करना चाहिए? जवाब है: कुछ नहीं