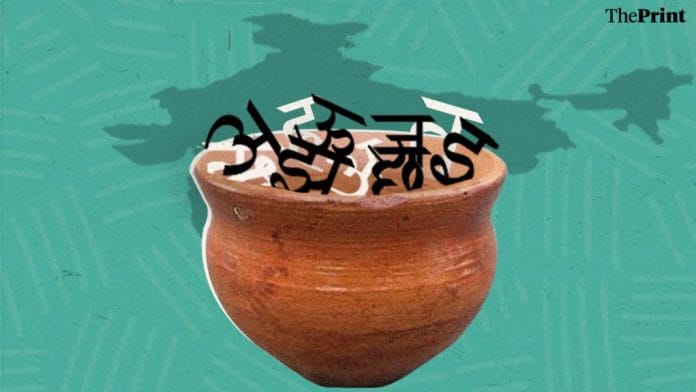जून, 1996 की बात है. कर्नाटक निवासी अहिन्दी भाषी जनता दल नेता हरदनहल्ली डोडेगौड़ा देवगौड़ा देश के ग्यारहवें प्रधानमंत्री बने तो कई प्रेक्षकों ने उनकी सबसे बड़ी कमजोरी यह बताई कि उन्हें हिन्दी तो आती ही नहीं. सवाल उठाये जाने लगे कि इस कमजोरी के रहते वे इस विशाल हिन्दी भाषी देश के प्रधानमंत्रित्व के दायित्व को भला कैसे निभायेंगे?
एक पत्रकार ने तो खचाखच भरे संवाददाता सम्मेलन में भी उनसे यह सवाल पूछने में संकोच नहीं किया. लेकिन अविचलित देवगौड़ा का बेहद संयत-सा उत्तर था, ‘चिंता मत कीजिए. तकलीफों की भाषा दुनिया भर में एक ही है और मैं उस भाषा को अच्छी तरह जानता-समझता हूं !’ सवाल पूछने वाले पत्रकार को आगे कोई और सवाल नहीं सूझा और बात वहीं खत्म हो गई.
अलबत्ता, देवगौड़ा ने खासी तेजी से हिन्दी सीखकर जल्दी ही अपनी ‘विकलांगता’ दूर कर ली थी. उन दिनों होश संभाल चुके लोगों को अभी भी याद होगा, थोड़े ही दिनों बाद राजनीतिक कारणों से उन्हें पद त्यागना पड़ा तो उन्होंने देश के नाम अपना विदाई संदेश हिन्दी में ही दिया था. उनकी विदाई के इतने सालों बाद यह देखकर संतोष होता है कि भले ही उनके बाद के देश के हिन्दी भाषी प्रधानमंत्रियों ने भी हिन्दी को उसकी उचित जगह देकर उसे ‘तकलीफों की भाषा’ बनाने या बनाये रखने को लेकर ज्यादा गंभीरता प्रदर्शित नहीं की, हिन्दी ने जहां तक संभव हुआ, न स्वतंत्रता संघर्ष के वक्त से चली आ रही अपनी प्रतिरोध की परंपरा को कमजोर पड़ने दिया है, न ही तकलीफजदा तबकों का साथ छोड़ा है.
अपने कुछ संस्तरों के हवा का रुख देखकर ‘समय के प्रवाह’ में बह जाने के बावजूद हिन्दी हर किसी को उसकी पुरानी पहचान से अलग करने के इस कठिन दौर से गुजरकर भी ‘गुलामों, गंवारों और जाहिलों’ की भाषा बनी रही है, साथ ही उसने उनके प्रति अपनी संवेदनाओं को मरने नहीं दिया है, तो यह कोई छोटी बात नहीं है. खासकर जब हम ऐसे समय में जा पहुंचे हैं, जिसमें भारत हर हाल में ‘इंडिया’ (अब तो न्यू इंडिया भी) होकर ही बचने को अभिशप्त है और लोकतंत्र ऐसी व्यवस्था में बदल या ढलकर, जिसमें कुछ लोगों को उसकी सारी उपलब्धियों को ऊपर-ऊपर रोक लेने की आजादी है और ढेर सारे लोगों को वोट देने, तालियां बजाने व जयकारे लगाने की!
यह भी पढ़ें: हिंदी की बात छिड़ी तो नेहरू ने क्यों कहा था, ‘अच्छा काम, गलत वक्त पर बुरा काम हो जाता है’
हिन्दी का संघर्ष
बताने की बात नहीं कि हिंदी को अपनी इस संवेदना, साथ ही चेतना को बचाने के लिए अलगाव, उद्वेलन, घृणा, पुरातनपंथ, पोंगापंथ, संकीर्णताओं व क्षुद्रताओं के कितने हमले झेलने पड़े हैं. साथ ही विज्ञापन, व्यापार व मनोरंजन के क्षेत्रों तक सीमित कर दिये जाने की कितनी साजिशों से गुजरना पड़ा है.
‘वोट मांगने’ की इस भाषा को सत्ता व शासन, चिंतन-मनन, ज्ञान-विज्ञान व विचार-विमर्श के दायरों में फिट करना अभी भी किसे अभीष्ट है? अच्छी बात है कि ऐसे में हिन्दी ने, खासकर उसके निचले कहे जाने वाले संस्तरों ने, समझा है कि उनके लिए अपना पक्ष बदलना अपने अस्तित्व से खेलना होगा.
इसी चेतना के तहत हिन्दी के इन संस्तरों ने डिजिटल होकर या ‘बच’ कर शीर्ष पर पहुंच जाने की राह चुनने के बजाय प्रतिकार और प्रतिरोध की आवाजों को बेदम होने से बचाने में शक्ति लगाये रखी है. भले ही साहित्य और पत्रकारिता की दुनिया के शीर्ष पर अवस्थित कई महानुभाव अभिव्यक्ति के सारे खतरे उठाने के बजाय नाना सत्ता रूपों और उच्च मध्य वर्गों की विलासलीला के बखान में ही अपनी सार्थकता तलाश रहे हैं.
यकीनन, समय के अंधेरों से जूझने वालों को हिन्दी से ऐसे उजाले की ओर ले जाने वाली भूमिका की ही दरकार है, जो भविष्य की इबारतें पढ़ने में उनकी मदद करे और बुरे समय में भी सच्ची अस्मिता व संस्कृति से जोड़े रखे. इसलिए आज हिन्दी दिवस पर हमें कामना करनी चाहिए कि हिन्दी कभी इतनी कमजोर न पड़े कि उसे अपनी इस भूमिका पर पुनर्विचार करना पड़े.
यह भी पढ़ें: हिंदी दिवस: क्या बाज़ार ने हिंदी की संवेदना, रचनाशीलता, रचनात्मकता को कम किया है
हिन्दी की सेवा नहीं कर पा रही नई पीढ़ी
यहां याद करना चाहिए कि वर्ष 2015 में 10-12 सितंबर को भोपाल में संपन्न हुए दसवें विश्व हिन्दी सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस सिलसिले में एक सौ टके की बात कही थी.
उन्होंने कहा था, ‘भाषा तो हवा का बहता हुआ झोंका होती है. ऐसा झोंका, जो बगीचे से गुजरे तो उसकी सुगंध और ड्रेनेज से गुजरे तो उसकी दुर्गंध बटोर लेता है. उन्होंने यह भी कहा था कि वर्तमान विश्व की छह हजार में से नब्बे प्रतिशत से ज्यादा भाषाएं सदी के अंत तक अस्तित्व संकट में फंस जायेंगी. अलबत्ता, जो तीन उसके पार जाकर बचेंगी, अच्छी बात यह है कि उनमें अंग्रेज़ी व चीनी के साथ हिन्दी भी होगी.’
प्रधानमंत्री के इस कथन के सहारे बात को आगे ले जायें तो आज हिन्दी की राह की सबसे बड़ी मुश्किल यह है कि देश में ड्रेनेज बढ़ते और बगीचे घटते जा रहे हैं.
यही कारण है कि अपनी मातृभाषा व राष्ट्रभाषा से ही नहीं, जमीन व विरासत तक से कटाव को अभिशप्त हमारी नई पीढ़ी का एक बड़ा हिस्सा भले ही दुनिया मुट्ठी में करने को आतुर हो और इसके लिए पंख फैलाकर उड़ रहा हो, यह पीढ़ी हिन्दी की उतनी भी सेवा नहीं कर पा रही, जितनी गुलामी के दौर में गिरमिटिये मजदूरों ने की थी.
यह भी पढ़ें: हिंदी के वर्चस्व को छोड़िए, असल मुद्दा भाषा की ताकत और ताकत की भाषा के बीच है
अवांछनीय होती हिन्दी
देश की गुलामी के दौरान सात समुंदर पार गये वे मजदूर उस गुलामी व लाचारी में भी अपनी भाषा व संस्कृति को लेकर स्वाभिमान से भरे हुए थे, जबकि यह नयी पीढ़ी उन्हें लेकर कतई इमोशनल नहीं है. हो भी कैसे, जब इस धारणा की शिकार है कि हिन्दी पढ़ने या उसमें लिखने से मिलता क्या है?
इसी धारणा के चलते हिन्दी भाषी अंचलों के दूरदराज के गांवों तक में चमकते-दमकते इंग्लिश मीडियम स्कूल अपने हाल पर रोने को मजबूर हिन्दी माध्यम स्कूलों को ऐसी हिकारत की निगाह से देखते हैं, जैसे हिंदी क्षेत्रों में भी अंग्रेजी के बजाय हिंदी ही अवांछनीय हो गयी हो.
सवाल है कि हिंदी इस स्थिति से कैसे निजात पायेगी? उसका भविष्य इस सवाल के जवाब पर ही निर्भर करेगा. इस पर भी कि वह इस बात को ठीक से समझती है या नहीं कि कहीं उसने अपने बचने के लिए तकलीफजदा लोगों की भाषा होने से बचने और अपनी पहचान बदलने की कोशिश की तो ‘बच’ जाये तो भी समय के अंधेरों से जूझने वालों को बचा पाने में कोई भूमिका न निभा पाने के कारण व्यर्थ होकर रह जायेगी, जो उससे नये मार्ग प्रशस्त करने में भूमिका निभाने की अपेक्षा रखती है, न कि तथाकथित रौशनी से चौंधियाकर आंखों को अंधी कर देने में लग जाने की.
याद कीजिए, स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान हिन्दी ने कितनी कुशलता से देशवासियों का मार्गदर्शन किया था. इतिहास गवाह है कि उसी दौर के संघर्षों में तपकर उसने सबसे ज्यादा मंज़िलें तय कीं.
उन दिनों के उलट क्षुद्रताओं के पैरोकार उस पर कब्ज़ा करने की अपनी साज़िशें सफल कर लें, उसे विज्ञापन, व्यापार व मनोरंजन के क्षेत्रों तक सीमित कर दें, वोट मांगने की भाषा ही बनाये रखें, सत्ता व शासन की भाषा न बनने दें, चिंतन-मनन, ज्ञान-विज्ञान व विचार-विमर्श के दायरों से बाहर बैठा दें और दलितों, स्त्रियों व अल्पसंख्यकों समेत हर पीड़ित समुदाय की अस्मिताओं व चेतनाओं को मुंह चिढ़़ाने के लिए प्रयोग करें, तो उसके होने का क्या अर्थ?
आज की तारीख में जो भी खुद को ‘हिन्दी’ या ‘हिन्दीसेवी’ कहते हैं, उन्हें इस सवाल का सामना करना और साथ ही समझना चाहिए कि कर्णधारों का हिन्दी के प्रति दिखावे की भावुकता प्रदर्शित करने वाला चेहरा भी न सिर्फ हिन्दी बल्कि उसकी पहचान का कितना विरोधी और कितना वीभत्स है.
(लेखक जनमोर्चा अख़बार के स्थानीय संपादक हैं. व्यक्त विचार निजी हैं)
यह भी पढ़ें: हिंदी अब ज्ञान की भाषा नहीं रही, स्तरहीनता के साम्राज्य ने इसकी आत्मा को कुचल दिया है