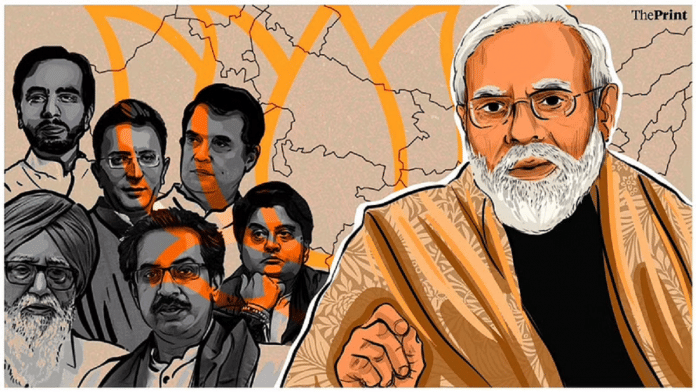यह एक मज़ाक ही था. पिछले महीने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बता रहे थे कि इमरजेंसी में अभिव्यक्ति की आज़ादी पर किस तरह रोक लगा दी गई थी, जबकि उनकी पुलिस और उनके राजनीतिक सहयोगी उस इमरजेंसी की भावना को नया जीवन देने में जुटे थे.
इंदिरा गांधी की इमरजेंसी (जून 1975 से मार्च 1977 तक) के दौरान कई भयानक चीजें हुईं. सरकार ने पूरे विपक्ष को जेल में बंद कर दिया, संविधान के साथ खिलवाड़ किया, युवकों की जबरन नसबंदी कर दी, कई लोगों को यातनाएं देकर मार डाला गया. लेकिन आम आदमी को सबसे ज्यादा तकलीफ बोलने की आज़ादी छीने जाने से पहुंची.
प्रेस सेंसरशिप के बारे में हम सब जानते हैं, लेकिन युवाओं को याद नहीं होगा (या वे इसके बारे में जानते भी नहीं होंगे) कि पूरे नागरिक समुदाय पर भय का माहौल हावी हो गया था. ऐसी नौबत आ गई थी कि लोग सरकार की कोई आलोचना करने से डरने लगे थे. इमरजेंसी के विलन माने गए संजय गांधी के बारे में कोई कड़वी बात कहने से पहले लोग अगल-बगल झांक लिया करते थे कि कोई सुन तो नहीं रहा है. सरकार के बारे में सार्वजनिक स्थान पर कोई मज़ाक करने का अर्थ था मुकदमे को न्योता देना.
वही दौर लौट आया
मैं यह नहीं कहता कि इमरजेंसी फिर लागू हो गई है. लेकिन इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि आज हम ऐसे समाज में जी रहे हैं जहां स्वतंत्र अभिव्यक्ति पर हमले हो रहे हैं और नेता लोग कानून का उन लोगों के खिलाफ गलत इस्तेमाल कर सकते हैं जो उनके खिलाफ बोलते हों.
सीधी-सी बात यह है कि केवल केंद्र की भाजपा सरकार ही अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को नहीं दबा रही है. लगभग हरेक राज्य में लगभग हर पार्टी असहमति या आलोचना को कुचलने के लिए कानून और पुलिस का इस्तेमाल कर रही हैं. इससे भी बुरी बात यह है कि इसका दमदार विरोध कोई नहीं कर रहा है- न मीडिया और न ही न्यायपालिका.
अमेरिका जैसे कुछ देशों में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी दी गई है. कई यूरोपीय देशों समेत दूसरे देशों में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तो दी गई है मगर नफरत उगलने वाले, नस्लवादी आदि भाषण की आज़ादी नहीं दी गई है. भारत में हमें कानून की उपनिवेशवादी व्यवस्था विरासत में मिली जिसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को तरजीह नहीं दी गई थी.
आज़ाद भारत के पुराने नेता देश के बंटवारे के कारण पीड़ा में थे और भविष्य में अलगाववादी आंदोलनों को लेकर आशंकित थे. उन्हें डर था कि भारत एकजुट रह पाएगा भी या नहीं. इसलिए उन्होंने कई दमनकारी कानूनों को किताब में दर्ज किए रखा. इमरजेंसी भी पूरी तरह से वैधानिक थी, मौलिक अधिकारों में कटौती करने का संविधान में प्रावधान किया गया है.
भारत निर्माताओं का मानना था कि उनके बाद जो नेता लोग बागडोर संभालेंगे वे ईमानदार होंगे और कानूनों का दुरुपयोग नहीं करेंगे. वे गलत थे. इमरजेंसी ने यह साबित कर दिया. और आज के हमारे नेता लोग तो इसे हर दिन, बार-बार साबित कर रहे हैं.
यह भी पढ़ें: विधायक अब राजनीतिक उद्यमी बन गए हैं, महाराष्ट्र इसकी ताजा मिसाल है
जमीन पर क्या हो रहा है
एक क्षण के लिए आज के बड़े मामले को भूल जाएं— ट्विटर अपने प्लेटफॉर्म पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की कटौती करने के खिलाफ सरकार से कर्नाटक हाइकोर्ट में लड़ाई लड़ रही है. खुद ट्वीटर ने सरकार से दोस्ती करने के लिए पिछले कुछ वर्षों में जो चाल चली उसके कारण मेरे मन में उसके लिए खास सम्मान का भाव नहीं है (हालांकि उसकी चाल फेसबुक और व्हाट्सअप जितनी धूर्ततापूर्ण नहीं थी). इसलिए उस मामले में हम नहीं पड़ते.
हम यह भी भूल जाएं भारत में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के प्रति सम्मान की कमी को लेकर दुनियाभर में उसकी क्या आलोचना हुई है, क्योंकि यह आंतरिक मामला है और हमें इसकी परवाह नहीं करनी चाहिए कि विदेशी लोग क्या कह रहे हैं.
लेकिन हम जमीन से मिल रहे असली उदाहरणों पर ही गौर करें.
‘आल्ट न्यूज़’ के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर की गिरफ्तारी के बारे में क्या कहा जाए? उनके खिलाफ दायर मामला एक मज़ाक ही है. यह एक पुराने ट्वीट पर आधारित है जिसमें हृषिकेश मुखर्जी की दशकों पुरानी फिल्म का हवाला दिया गया है. चूंकि अधिकारियों को मालूम है कि अंततः यह मामला अपने आप खारिज हो जाएगा इसलिए उन्होंने नये, असंबद्ध आरोपों को जोड़ दिया और उत्तर प्रदेश पुलिस को भी साथ ले लिया है. एक मामला खारिज होगा तो दूसरा चलता रहेगा. ईडी को भी शामिल कर लिया जाएगा. इस तरह सिलसिला जारी रखा जाएगा.
इसके अलावा, छत्तीसगढ़ पुलिस ने राहुल गांधी का एक तोड़ा-मरोड़ा वीडियो प्रसारित करने के मामले में ज़ी न्यूज़ के एंकर रोहित रंजन को गिरफ्तार करने की जो कोशिश हाल में की उस पर भी विचार किया जा सकता है. कोई नहीं कह रहा है कि वीडियो को प्रसारित किया जाना चाहिए था. लेकिन ज़ी न्यूज़ ने माफी मांग ली है, और कानून में ऐसी धाराएं हैं जिनका इस्तेमाल रंजन के खिलाफ किया जा सकता है. तो कांग्रेस शासित छत्तीसगढ़ पुलिस दल एंकर को गिरफ्तार करने के लिए उत्तर प्रदेश क्यों आ गया? इससे भी बुरी बात यह कि रंजन छत्तीसगढ़ पुलिस की गिरफ्त में आने से इसलिए बच गए क्योंकि यूपी पुलिस उनकी मदद के लिए आगे आई और उन्हें एक ऐसे मामूली आरोप में हिरासत में ले लिया जिससे उन्हें अगले दिन रिहा कर दी गया.
हम आज किस तरह के समाज में रह रहे हैं कि पत्रकारों को खबर देने पर गिरफ्तार होने का खतरा पैदा हो गया है और जहां उन्हें अपनी सुरक्षा के लिए अनुकूल राज्य सरकार और उसकी पुलिस पर निर्भर होना पड़ता है?
या मराठी अभिनेत्री केतकी चितले का मामला लीजिए. महाराष्ट्र पुलिस ने उन्हें इस फेसबुक पोस्ट के लिए गिरफ्तार कर लिया गया जिसमें कहा गया था कि राज्य सरकार पिछली महाराष्ट्र सरकार के ‘गॉडफादर’ शरद पवार की विरोधी है. चितले के खिलाफ कोई वास्तविक मामला नहीं है लेकिन उन्हें एक महीने से ज्यादा जेल में रहना पड़ा क्योंकि उनके खिलाफ 22 एफआइआर दायर कर दिए गए थे. इसलिए उन्हें जमानत लेने में देर हुई.
ऐसे कई उदाहरण मैं दे सकता हूं. बात केवल मीडिया पर दबाव की नहीं है, जो प्रायः सरकार की लाइन पर चल कर संतुष्ट हो जाता है, जैसा कि 1975 और 1976 में हुआ था. अभिव्यक्ति की आज़ादी पर हमले का खतरनाक और चिंताजनक पहलू यह है कि इमरजेंसी के दौर में सार्वजनिक स्थान पर गपशप का जो रूप आज फेसबुक या ट्वीटर के पोस्ट ने लिया है उस पर भी हमला हो रहा है.
क्या न्यायपालिका भी?
मैं ऐसे किसी दूसरे देश की कल्पना नहीं कर सकता जो खुद को उदार लोकतंत्र कहता है और अभिव्यक्ति की आज़ादी का सम्मान करने का दावा करता है लेकिन जहां व्यक्ति के अधिकारों का मनमाना उल्लंघन होता है.
मुख्यधारा का अधिकांश मीडिया इस सबका विरोध करने से डरता है. लेकिन न्यायपालिका को क्या हुआ है? भारत के जजों ने दिखाया है कि वे कुछ मामलों में बड़ी तेजी से निर्णायक फैसला दे देते हैं. जैसे अर्णब गोस्वामी और ताजिंदर बग्गा के मामले याद आते हैं. लेकिन अधिकांश मामलों में वे अदालती प्रक्रिया को ही सज़ा बनाकर संतुष्ट हो जाते हैं. निचली अदालत पुलिस की सुनती है और जमानत देने से माना कर देती है. चाहे आरोप कितने भी बेमानी क्यों न हों. पुलिस जब कहती है कि उन्हें और ज्यादा कस्टडी नहीं चाहिए, तब भी जज उन लोगों की न्यायिक हिरासत बढ़ा देते हैं जिनके खिलाफ कोई वास्तविक आरोप नहीं होता है.
इसके बावजूद ऊंची अदालतें कुछ नहीं करतीं. हम सुप्रीम कोर्ट से प्रार्थना करते रहे हैं कि वे जजों को इस पुराने मुहावरे पर अमल करने के लिए कहे कि जमानत ही नियम होना चाहिए और जेल अपवाद.
क्या जज लहरें पैदा करने को राजी नहीं होते? क्या वे उस तरह के संगठित हमले से डरते हैं जैसा हमला हाल में दो जजों को नूपुर शर्मा मामले में झेलना पड़ा?
मैं नहीं कह सकता, लेकिन सच यही है कि जब पुलिस नेताओं के आदेश पर मनमानी पर उतर आए तो समझ लीजिए कि हम पुलिसिया राज की तरफ बढ़ रहे हैं. न्यायपालिका का यह कर्तव्य है कि वह इस पतन को रोके.
अगर हम अभिव्यक्ति की आज़ादी की रक्षा के लिए खड़े नहीं होते तो हमें इसे हमेशा के लिए अलविदा कहने को तैयार हो जाना चाहिए.
(वीर सांघवी भारतीय प्रिंट और टीवी पत्रकार, लेखक और टॉक शो होस्ट हैं. उनका ट्विटर हैंडल @virsanghvi है. व्यक्त विचार निजी हैं)
(इस लेख को अंग्रेजी में पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)
यह भी पढ़ें: योगी के दाहिने हाथ पर रसातल है, सो मोदी भाजपाई कट्टरपंथियों पर कसें लगाम