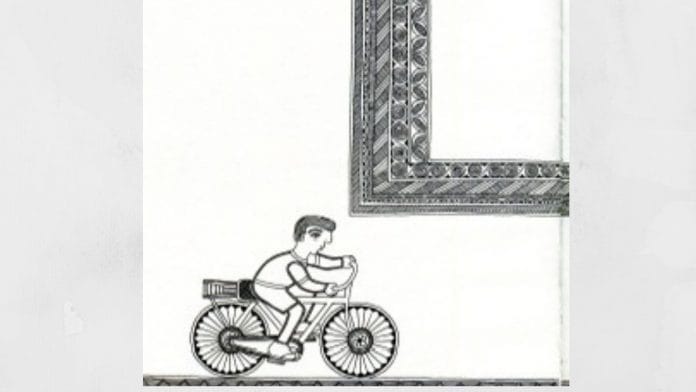उन्मादी धार्मिकता, थोथे बयानात, ओछी छींटाकशी व मानवता को कलंकित करते कृत्यों की ख़बरों के मध्य साहित्य का कोना मानो कादे में कमल या बंद कोठरी में उजालदान. किंतु इधर के दशक में हिंदी के नामचीन अखबारों के यहां साहित्य, विशेषतः हिंदी साहित्य के लिए स्थान कम से कमतर होता जा रहा है. कहानियों की शब्द संख्या सिमटते-सिमटते इतनी रह गयी है कि चुटकुले उन पर हावी हो जाएं. कविताएं इनको यों नागवार जैसे शाकाहारी को परोसे में चिकन-करी. पुस्तक समीक्षा, रचनाकारों से साक्षात्कार की उम्मीद ऐसे अख़बारों से करना बेमानी है, जिनको साहित्य की मुकर्रर जगह पर साप्ताहिक भविष्यफल देने से गुरेज़ नहीं.
वैसे हिंदी के प्रति ऐसा सौतेला व्यवहार अनपेक्षित भी नहीं माना जाना चाहिए. दरअसल यह एक लम्बी तैयारी और जुदा मानसिकता का नतीजा है. बल्कि यदि षड़यंत्र ही कहूं तो बेजा न होगा. षड़यंत्र जिसका खुलासा मुझ पर आकाशवाणी से नियमित प्रसारित ‘ज्ञानवाणी’ कार्यक्रम सुनते हुए हुआ. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू) के पत्रकारिता के छात्रों के लिए आयोजित एक साक्षात्कार का सीधा प्रसारण चल रहा था. मुद्दा था- अख़बार में स्तम्भ लेखन कैसे किया जाए?
विशेषज्ञ महोदय का नामचीन पत्रकार कह परिचय करवाया गया था, जो पंद्रह से अधिक बरसों से अंग्रेज़ी और हिंदी अख़बारों में निरंतर स्तम्भ लेखन कर रहे थे. कैसे सुनिश्चित करें कि लिखा छपे, इस सवाल पर उनका दिया गुरु मन्त्र आंखे खोलता है -‘विषय और शैली चयन के पूर्व यह निर्धारित करना चाहिए कि स्तम्भ किस भाषा के अख़बार हेतु लिखना चाहते हैं. यह छपने की, सम्पादक को पसंद आने की ओर जाती सीढ़ी की प्रथम और सबसे महत्वपूर्ण पेढ़ी है. मैं यह मानकर लिखता हूं कि अंग्रेज़ी का पाठक कम से कम स्नातक होता है, जबकि हिन्दी अख़बार का पाठक अधिकतर दसवीं पास. अतएव विषय, भाषा और शैली का चयन करते हुए यह तथ्य नज़रअंदाज़ नहीं किया जाना चाहिए… आदि..आदि.’ गोया कि लिखने की कुछ कहने की बेकली सब बेमानी, किसी भी कीमत पर कैसे छपना यह भर सीख लो.
ऐसे विकट दौर में जब हिंदी के अख़बारनवीस हमें कमपढ़-मंदमति माने बैठे हों किसी अंग्रेज़ी अख़बार में हिंदी किताब पर लंबी चर्चा देख दिल जुड़ जाता है. राजकुमारी की पुस्तक ‘बिक्सू’ पर केंद्रित ऐसी ही लम्बी चर्चा जब ‘द हिन्दू’ में पढ़ी तो मन में मानो सावन की घटाएं झूम उठीं. मुरझाए-मुसमुसे पंख खुल गए, अर्से से मायूस-गुमसुम बैठा मन-मयूर नृत्य कर उठा. व्यग्र हो गया वो जल्द से जल्दी ‘बिक्सू’ हासिल करने हेतु. चुनांचे बंदा निकल पड़ा किताबों की दुकानों की ओर. वैसे किताब, वो भी भारतीय भाषा की किताब, बेचने वाली पेढ़ियां इंदौर में बची ही कितनी हैं? दो-चार. सब की सब रुग्ण, अंतिम सांसे गिनतीं. जानता हूं वहां मायूसी मिलेगी, फिर भी जाता हूं एक ज़िम्मेदारी सी लगती है, इनको जिलाये रखने की. जिम्मेदारी यूं कि इन दुकानों का महती योगदान है मुझमें साहित्य अनुराग पैदा करने में. अधिक पुरानी बात नहीं, कुछ दस-पंद्रह बरस पहले तक इनकी पेढ़ी चढ़ते ही गर्मजोशी से स्वागत हुआ करता था. ‘मधुशाला’ अथवा ‘भारत- भारती’ की तलाश करो तो दुकानदार या वहां के कर्मचारी ‘कामायनी’ और ‘साकेत’ भी पढ़ने को कहते और ‘गुनाहों का देवता’ मांगो तो ‘अंधा युग’ भी आगे बढ़ाते.
बहरहाल, आप सर पर उठाई ज़िम्मेदारी के तहत नियम से जाता हूं किताब की दुकानों पर. हिंदी की किताबें भली-भांति नुमाया न करने पर बहस करता हूं फ़ेहरिस्त थमा किताबें मंगवाने की गुज़ारिश करता हूं. एक आस जो न दबती है न मरती. ले जाती है बार-बार सौदागरों की दहलीज़ पर कि पिछली बार जो समझाईश-मनौव्वल-गुज़ारिश के दौर चले थे. उनका कुछ असर दिखेगा कि इस बार दुकानों में किताबें बिखरी नहीं होंगी और नहीं होंगी काउंटर के पीछे से झांकती उम्मीद से खाली निगाहें ही कि एक बार फिर मुझे देख उन नयनों में नागफनी नहीं राबिते के बिरवे उग आएंगे.
यह भी पढ़ें : प्योर हिन्दी बोल नहीं पाता, व्हाट शुड आई डू सर? युवाओं के बीच हिंदी की दुर्दशा
परन्तु ‘बिक्सू’ की तलाश में जो कुछ गुज़रा, जो हासिल हुआ उसका बयां करते हुए दिल दरकता है. हिन्दी साहित्य पर एकाग्र दुकानों में पसरी मिली मसानी-नीरवता. एक भाई ने तो पुस्तकों को हटा शोकेस में ‘सेल-सेल फिफ्टी परसेंट तक डिस्काउंट’ की तख़्ती तले बाकायदा चादरें रख छोड़ी थीं. लगा जैसे दुष्यंत कुमार का आधा शेर परे सरका भाई लोगों ने बिछाने-ओढ़ने वाली सामग्री का धंधा ही अपना लिया हो. बहुभाषी पुस्तकें मुहैया करवाने वाले दो पुराने संस्थानों में से एक अब सिर्फ़ धार्मिक और सेल्फ-हेल्प साहित्य बेचने में जुटा था. दूसरे के यहां ख़ूब भीड़ थी, ख़ूब किताबें भी. पर सब की सब अंग्रेज़ी. हर कहीं लोग किताब पलट रहे थे. हर संभावित ख़रीददार से एक सेल्समेन चिपका फिर रहा था. उनमें से एक से हिंदी-किताब की अलमारी का पता दरियाफ़्त किया.

‘क्या चाहिए?’ उधर से प्रश्न उछला.
‘बिक्सू- राजकुमारी द्वारा लिखी किताब, बिक्सू!
‘यह कौन सी किताब है, हमने तो नाम नहीं सुना’, फिर मेरे लटकते चेहरे को देख उसने जोड़ा,’ उधर चले जाएं, वहां कुछ हिंदी की किताबें रखी हैं, खुद तलाश लीजिये.’
‘भाई जिस किताब के बारे में ‘दी हिन्दू’ ने एक पूरा पन्ना भर लिक्खा है, उसका नाम तक नहीं सुना आपने?’
‘अच्छा हिन्दू ने लिखा है? कब? मुझे तो ध्यान नहीं. आप उधर देख लें, जो नहीं मिले तो प्रकाशक का नाम काउंटर पर लिखा दीजियेगा, जब आएगी आपको फोन कर देंगे’, वो दूकान के भीतरी कोने की तरफ़ इशारा करते हुए बोला.
लापरवाही के शिकार उस कोने में पुस्तक नहीं मिलनी थी सो नहीं मिली. काउंटर पर तमाम मालूमात नोंद करने के बावज़ूद भले मानुष ने न तो किताब बुलवाई न फ़ोन ही करवाया. झक मार अमेज़न पर तलाशा. नतीजा सिफ़र. अमेज़न भी तो दूकान ही ठहरी, मनोकांक्षा पूरी करने वाला चिराग़ तो नहीं. यहां भी वही मिलता है जो बेचने वाले बेचा करे हैं. हिन्दी की किताबों की तलाश में अंतर्जाल-नगरी में बहुधा इधर-उधर भटकना पड़ता है. भटका. अंततः इकतारा प्रकाशन से संपर्क साधा. लम्बी जद्दोजहद के बाद आख़िरकार अभीष्ट पुस्तक हाथ में आयी. और क्या ख़ूब आयी!
बारह बरस के विकास कुमार विद्यार्थी उर्फ़ ‘बिक्सू’ के विद्यार्थी जीवन का एक सौ तेरह पन्नों का रोज़नामचा. मेरे जाने हिन्दी में ऐसा अभिनव प्रयोग शायद ही पहले कभी हुआ हो. सुना तो बहुत था कलाओं के मध्य आवाजाही के बारे में. परन्तु साहित्य में कलाओं के ऐसे सघन, सार्थक तथा सफ़ल सफ़र का दूसरा उदाहरण कदाचित ही कहीं देखने मिले. बिक्सू के जीवन के तमाम अंतरंगपल , सारी घटनाएं राजकुमारी जी ने मधुबनी शैली में बने चित्रों के माध्यम से प्रस्तुत की हैं. तीखी-तीखी नाकेँ, बड़ी-बड़ी आंखें, भरे-भरे मांडणें इनके यहां साधारण कार्टूनों की तरह किसी भी पात्र का चित्रण सीधा सपाट नहीं. गाय है तो शरीर पर फूल टंगें हैं.साइकिल है तो पहियों पर झालर वाली. इसमें शुमार स्वप्न दृश्य तो देखते ही बनता है. भाषा भी सीधी सपाट हिन्दी नहीं, झारखंड के छोटा नागपुर में बोली जाने वाली हिंदी. जिसका हर हर्फ़ रस से लबरेज़. जो इबारत पर पोर फिराओ और चाटते जाओ तो ब्लड शुगर चार सौ पार जाना तय! मेरी मानें तो बच्चों के मान से लिखी यह किताब न सिर्फ़ हर घर में होना चाहिए बल्कि सब बड़ों को पढ़ना चाहिए. क्योंकि बच्चों का मानस, उनकी चाहत समझने का इससे बेहतर और आसान ज़रिया दूजा नहीं मिलेगा.
यह भी पढ़ें : क्या आप हिंदी की सबसे ज्यादा बिकने वाली किताब के लेखक को जानते हैं?
किताब से एक ही बैठक में आद्योपांत गुज़रने के बाद ठीक वही अनुभूति हुई जो किसी बेहतरीन कला-उत्सव के पूर्ण होने पर होती है. सोचता हूं जब हमारे पास ऐसा अकूत शब्द भण्डार है, इतना भाषिक वैविध्य है, ऐसे प्रयोगधर्मी रचनाकार-प्रकाशक हैं तो फिर किस बिना पर हिंदी को कमपढ़ लोगों की भाषा के रूप में चरितार्थ किया जा रहा है? क्यों हिंदी के अख़बार साहित्य को हफ़्ते में एक पूरा पन्ना देने से भी परहेज़ करते हैं? क्यों ‘बुक-स्टोर’ हिन्दी की किताब ‘स्टोर’ करने से बिदकते हैं? क्यों हिंदी का पाठक सम्पादकों-दूकानदारों के समक्ष सीना-ठोक कभी विरोध दर्ज़ नहीं करता?
सनद रहे कि भाषिक संस्कार कोसने भर से नहीं मरते. अलबत्ता तिरस्कार से घबरा कुंठित हो जाने पर मृत्यु को प्राप्त होते हैं. भारतीय भाषाओं को अंग्रेज़ी से ख़तरा नहीं वरन भीतराघातियों से धड़का है. यह तो सर्वज्ञात है कि पुख़्ता दरख़्त भी दीमक लगने पर धराशायी हो जाता है. अपनी मातृभाषा से अटूट नेह ही दीमक दूर रखने का कारगर उपाय है. हिंदी की किताब अपने शहर-कस्बे की दुकानों पर जा बार-बार किताब मांगना, उन पर बहस करना, भाषा सहेजने का मेरा अपना तरीका है. अकेला सही पर मैं यह जारी रखूंगा ! कभी तो पत्थर पिघलेगा, कभी तो असर निकलेगा !
(अजय सोडानी लेखक है और पेशे से न्यूरो फिज़िशियन हैं.यह लेख लेखक का निजी विचार है.)