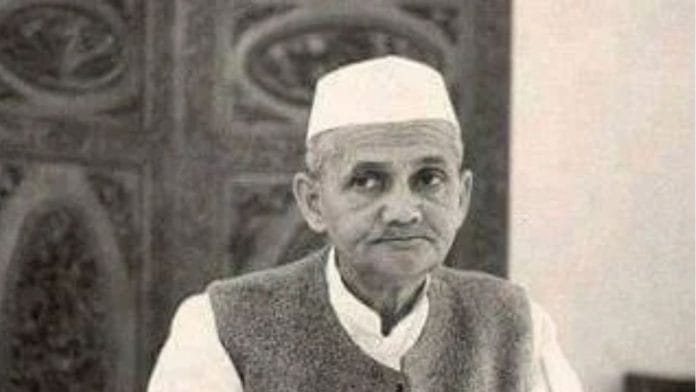लाल बहादुर शास्त्री ने अपने छोटे, लेकिन बेहद अहम प्रधानमंत्री कार्यकाल में जो अंतिम और दूरगामी फैसलों में से एक लिया था, वह था 1 दिसंबर 1965 को सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) की स्थापना. इसे बनाने का तात्कालिक कारण भारत और पाकिस्तान के बीच जनवरी से अप्रैल 1965 तक रण ऑफ कच्छ क्षेत्र में हुई सीमा झड़पें थीं.
पंजाब और बंगाल में सीमा निर्धारण (और आबादी के आदान-प्रदान) को रेडक्लिफ अवॉर्ड के तहत औपचारिक रूप दिया गया था, लेकिन रण ऑफ कच्छ के लिए ऐसा कोई विचार नहीं हुआ क्योंकि यह साफ तौर पर वेस्टर्न इंडियन स्टेट्स एजेंसी (जिसे बाद में सौराष्ट्र यूनियन कहा गया) का हिस्सा था. इस स्थिति की पुष्टि सिंध प्रांत की गज़ेटियर, बॉम्बे प्रेसीडेंसी और सर्वे ऑफ़ इंडिया के नक्शों ने भी की थी.
हालांकि, बीएसएफ की जड़ें शास्त्री के गृहमंत्री कार्यकाल (अप्रैल 1961 से अगस्त 1963) से जुड़ी मानी जाती हैं. उस समय, 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत बने ज़ोनल काउंसिल्स की बैठकों में उन्होंने प्रस्ताव दिया था कि एक ‘रिज़र्व पुलिस फोर्स’ बनाई जाए, जिसे ज़रूरत पड़ने पर विभिन्न ज़ोन में इस्तेमाल किया जा सके.
भारतीय सिविल सेवा (आईसीएस) के अधिकारी और बाद में भारत के सबसे लंबे समय तक गृह सचिव रहे एल.पी. सिंह (1964-1970) ने अपनी किताब Portrait of Lal Bahadur Shastri: A Quintessential Gandhian में इसका ज़िक्र किया.
सिंह ने लिखा, “यह एक व्यावहारिक विचार था क्योंकि किसी ज़ोन के हर राज्य को एक साथ अतिरिक्त बल की ज़रूरत नहीं पड़ती…यह व्यवस्था न सिर्फ राज्यों का कुछ खर्च बचा सकती थी, बल्कि उनके बीच सहयोग और आपसी तालमेल भी बढ़ा सकती थी.” हालांकि, यह प्रस्ताव लागू नहीं हो पाया क्योंकि राज्य सरकारें अपने ‘राज्य सूची’ के अधिकार केंद्र को देने के लिए तैयार नहीं थीं.
सिंह ने आगे लिखा, “अगर शास्त्री लंबे समय तक गृहमंत्री रहते या प्रधानमंत्री बनने के बाद ज़्यादा जीवित रहते, तो शायद राज्यों के बीच सहमति बना लेते.”
1962 के चीन युद्ध के बाद गृह मंत्रालय ने मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की राज्य सशस्त्र पुलिस (एसएपी, पीएसी) की बटालियनें असम भेजनी शुरू कीं और पंजाब आर्म्ड पुलिस को जम्मू-कश्मीर की सीमा सुरक्षा में लगाया गया. 1965 की शुरुआत में रण ऑफ कच्छ में हुई झड़पों ने शास्त्री को विश्वास दिला दिया कि भारत को सीमा सुरक्षा के लिए एक संगठित बल की ज़रूरत है.
पाकिस्तान ने यह ज़िम्मेदारी 1958 से वेस्ट पाकिस्तान रेंजर्स को सौंपी हुई थी और उन्हें रक्षा मंत्रालय के अधीन रखा गया था.
यह भी पढ़ें: पिंजरे का तोता या बेखौफ बाज़? भारत को ‘शास्त्री फॉर्मूला’ आज़माना चाहिए
एक नौकरशाही कवायद
अप्रैल 1965 में, गृह मंत्रालय ने सेना उप प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल पी.पी. कुमारमंगलम की अध्यक्षता में एक समिति बनाई, जिसका उद्देश्य था “पूरे भारत-पाकिस्तान सीमा को सबसे प्रभावी ढंग से कैसे संभाला जाए, इसकी जांच और सिफारिश करना.”
उनकी रिपोर्ट का अध्ययन एल.पी. सिंह और थलसेना प्रमुख (सीओएएस) जनरल जे.एन. चौधरी ने किया. दोनों ने प्रधानमंत्री को जानकारी दी. इसके बाद शास्त्री ने अपने मंत्रिमंडल सहयोगियों रक्षा मंत्री वाई.बी. चव्हाण, गृह मंत्री गुलजारीलाल नंदा और विदेश मंत्री स्वर्ण सिंह से विचार-विमर्श किया. उन्होंने विपक्ष के नेताओं से भी परामर्श बढ़ाया, जिनमें स्वतंत्र पार्टी के एन.जी. रंगा, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के सुरेंद्रनाथ द्विवेदी, सीपीआई के हिरेंद्रनाथ मुखर्जी और भूपेश गुप्ता, जनसंघ के अटल बिहारी वाजपेयी और यू.एम. त्रिवेदी, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के मनी राम बागड़ी, डीएमके के के. मनोहरन, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के बी.पी. मौर्य और निर्दलीय सदस्य प्रकाशवीर शास्त्री, इंदुलाल याज्ञिक, एन.सी. चटर्जी और फ्रैंक एंथनी शामिल थे.
जैसे-जैसे चर्चा आगे बढ़ी, यह स्पष्ट हुआ कि सीमा बल का गठन केवल तत्काल खतरों से निपटने के लिए नहीं बल्कि एक व्यापक रणनीति का हिस्सा था सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के बीच विश्वास पैदा करना, सोने की तस्करी और मानव तस्करी पर रोक लगाना और देश की क्षेत्रीय अखंडता सुनिश्चित करना.
22 अप्रैल 1965 को, थलसेना प्रमुख ने ‘आवर मिलिट्री कॉरेस्पॉन्डेंट’ नामक छद्म नाम से एक लेख लिखा, जिसमें उन्होंने एमएचए के तहत एक संघीय सीमा-रक्षक बल की वकालत की. यह लेख द स्टेट्समैन अखबार में छपा, जो उस समय बेहद प्रभावशाली माना जाता था.
इसके तुरंत बाद, मई के पहले हफ्ते में गृह मंत्रियों और राज्यों के पुलिस महानिरीक्षकों की बैठक बुलाई गई, ताकि “सीमा बल की संभावना और आवश्यकता” पर चर्चा हो सके.
प्रधानमंत्री शास्त्री ने बैठक को संबोधित किया और गुजरात सीमा पर पाकिस्तानी सैनिकों की हलचल पर प्रकाश डाला. चूंकि, आधारभूत काम पहले से हो चुका था, इस मुद्दे पर आम सहमति बन गई. दिलचस्प विडंबना यह थी कि के.एफ. रुस्तमजी, जो आगे चलकर बीएसएफ के पहले महानिदेशक बने, ने मध्य प्रदेश सरकार की ओर से आपत्ति दर्ज की. उस समय रुस्तमजी मध्य प्रदेश के पुलिस महानिरीक्षक थे. उन्हें ऐसा करने का निर्देश उनके मुख्यमंत्री डी.पी. मिश्र ने दिया था, जो कभी शास्त्री के आगे पिछड़ने को पचा नहीं पाए थे.
एक “सैद्धांतिक” निर्णय लिया गया कि एक नया सीमा बल बनाया जाए, जिसे एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के अधीन रखा जाए. यह बल “मुख्यतः पुलिस संबंधी कार्य” करेगा, लेकिन “युद्ध की स्थिति में सेना के कमांड में काम करने की उम्मीद” रखी जाएगी. 17 मई 1965 को एल.पी. सिंह ने थलसेना प्रमुख चौधरी और रक्षा सचिव ए.डी. पंडित के साथ बैठक की. बैठक के बाद उन्होंने कार्यवृत्त गृह मंत्री और प्रधानमंत्री के अनुमोदन के लिए भेज दिया.
रुस्तमजी को बीएसएफ का पहला महानिदेशक नियुक्त किया गया, जिनका पदभार भारतीय सेना के लेफ्टिनेंट जनरल के समकक्ष रखा गया. उन्हें चुनने का एक बड़ा कारण यह था कि उनका जनरल चौधरी से बेहतरीन तालमेल था. रुस्तमजी ने ऑपरेशन पोलो (हैदराबाद के निज़ाम को संघ में शामिल करने के लिए की गई पुलिस कार्रवाई) में चौधरी के अधीन काम किया था.
हालांकि, रुस्तमजी गृह मंत्रालय को रिपोर्ट करते थे, लेकिन उनकी सेवाओं का उपयोग पाकिस्तान सीमा पर विभिन्न पुलिस बलों के बीच समन्वय के लिए किया गया. बीएसएफ का वास्तविक गठन भारत-पाक युद्ध समाप्त होने के बाद हुआ, जब 25 राज्य सशस्त्र पुलिस बटालियनों को नए बल में मिला दिया गया.
यह भी पढ़ें: जय जवान, जय किसान से लेकर CVC तक—शास्त्री ने जो कहा, वही किया, लेकिन भ्रष्टाचार मिटाना आसान नहीं था
बीएसएफ अब
तब से लेकर अब तक बीएसएफ का विस्तार कई गुना हो चुका है. यह अब दुनिया की सबसे बड़ी सीमा सुरक्षा बल है, जिसमें 200 बटालियन और 2,70,000 से अधिक जवान हैं. इसकी गतिशीलता और लॉजिस्टिक्स को बल के अपने विमान, जलपोत और प्रशिक्षित घोड़े व ऊंट संभालते हैं. इसका डॉग स्क्वॉड बारूदी सुरंगों का पता लगाने और मादक पदार्थ विरोधी अभियानों में बड़ी भूमिका निभाता रहा है. अब यह अपना पहला समर्पित ड्रोन स्क्वॉड्रन तैयार कर रहा है, ताकि भारत-पाक सीमा पर निगरानी और हमले की क्षमता को और मजबूत किया जा सके.
फिर भी इस बल को चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, खासकर पूर्वी सेक्टर में, जहां भूमि अधिग्रहण की धीमी प्रक्रिया की वजह से बॉर्डर फेंसिंग का काम रुका हुआ है, विशेषकर पश्चिम बंगाल में. ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस सरकार, बांग्लादेश से आने वाले अवैध प्रवासियों की ‘पुशबैक’ कार्रवाई में बीएसएफ की भूमिका की आलोचना करती रही है.
यूपीएससी द्वारा आयोजित सीएपीएफ परीक्षा से सीधे बीएसएफ में भर्ती हुए अधिकारी भी, उच्च स्तर पर आईपीएस अधिकारियों के वर्चस्व से नाराज़ रहते हैं — खासकर आईजी, एडीजी और डीजी जैसे पदों पर. हालांकि, इन छोटी-मोटी दिक्कतों के बावजूद, शास्त्री द्वारा स्थापित यह बल अब देश की वर्दीधारी सेनाओं में गौरव का स्थान रखता है.
सबसे अहम बात यह है कि बीएसएफ की स्थापना ने पंजाब के पुनर्गठन का रास्ता खोल दिया. राज्य पुनर्गठन आयोग (1956) ने पंजाबी सूबा की मांग यह कहकर ठुकरा दी थी कि अंतरराष्ट्रीय सीमा वाले राज्यों को प्रशासनिक दृष्टि से बड़ा और आर्थिक रूप से सक्षम होना चाहिए ताकि वे सीमा सुरक्षा के लिए सशस्त्र पुलिस बनाए रख सकें, लेकिन बीएसएफ बनने के बाद यह तर्क निरर्थक हो गया, और ग्यारह महीने बाद, 1 नवंबर 1966 को पंजाब का पुनर्गठन लागू हो गया.
पंजाबी सूबा, हरियाणा और (तब के) केंद्र शासित प्रदेश हिमाचल प्रदेश के गठन का श्रेय शास्त्री के उत्तराधिकारी इंदिरा गांधी को मिल गया, क्योंकि इस बीच शास्त्री का जीवन और उनकी उपलब्धियां पीछे चली गईं.
(यह लेख लाल बहादुर शास्त्री और उनके द्वारा स्थापित संस्थाओं पर आधारित सीरीज़ का अंतिम हिस्सा है)
(संजीव चोपड़ा एक पूर्व आईएएस अधिकारी हैं और वैली ऑफ वर्ड्स साहित्य महोत्सव के निदेशक हैं. हाल तक वे लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी के निदेशक भी रहे हैं. उनका एक्स हैंडल @ChopraSanjeev है. यह लेख लेखक के निजी विचार हैं.)
स्पष्टीकरण: लेखक लाल बहादुर शास्त्री मेमोरियल (एलबीएस म्यूज़ियम) के ट्रस्टी भी हैं.
(इस लेख को अंग्रेज़ी में पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)
यह भी पढ़ें: शास्त्री के दौर में खाद्य संकट के लिए MSP लागू हुई मगर अब उस पर पुनर्विचार की ज़रूरत