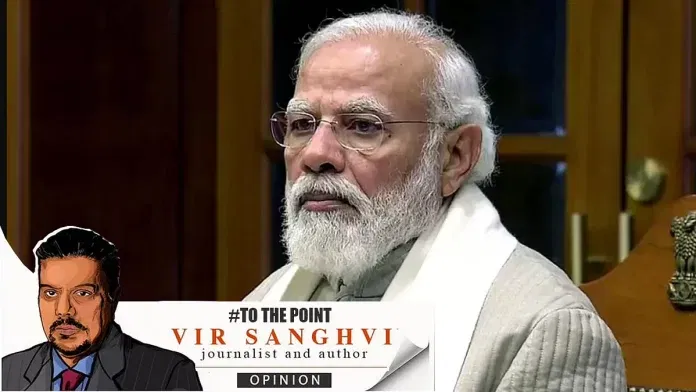इस सप्ताह रुपये की कीमत ने जब ‘ऐतिहासिक गिरावट’ दर्ज की, तो कह नहीं सकता कि कितने लोगों ने मुझे श्री श्री रवि शंकर के उस ख्यात ट्वीट की याद दिलाई जिसमें उन्होंने लिखा था कि नरेंद्र मोदी सत्ता में आएंगे तब एक डॉलर की कीमत मात्र 40 रुपये रह जाएगी. वास्तव में, आज एक डॉलर की कीमत 77 रुपये है और यह बताता है कि श्री श्री का अनुमान किस तरह दोगुना गलत था. इसके अलावा, श्रीलंका में फैली अराजकता से तुलना की जाती है. मैंने यह टिप्पणी भी सुनी है कि हम भी उसी ओर बढ़ रहे हैं क्योंकि ‘अर्थव्यवस्था सचमुच बदहाल है और मीडिया है कि लीपापोती में लगा है.’
भारतीय अर्थव्यवस्था की हालत पर मुझे छह नेत्रहीन और एक हाथी वाली कहानी याद आती है जिसमें हरेक नेत्रहीन उसके अलग-अलग अंग को छूकर बताता है कि हाथी कैसा होगा. लगता है कि अर्थव्यवस्था के बारे में भी यही हो रहा है, अलग-अलग लोग इसे अलग-अलग रूप में देख रहे हैं. कयामत की चेतावनियों के अलावा ऐसे लोग भी कई हैं जो दूसरे संकेतकों की ओर इशारा करके कह रहे हैं कि हालत इतनी बुरी भी नहीं है.
मैं कोई अर्थशास्त्री नहीं हूं लेकिन मुझे यह विश्वास करने में मुश्किल होती है कि हम दूसरा श्रीलंका बनने जा रहे हैं. हां, हम समस्याओं से घिरे हैं- रुपया कमजोर है, मुद्रास्फीति है, विदेशी मुद्रा का भंडार छोटा हो रहा है, आदि-आदि. लेकिन हमारी अर्थव्यवस्था का जो आकार है उसकी तुलना आप श्रीलंका से नहीं कर सकते.
अर्थव्यवस्था से लेकर मीडिया तक उदाहरण मौजूद हैं
कयामत की चेतावनी आज के भारत में ध्रुवीकरण के लक्षण हैं. इस ध्रुवीकरण के केंद्र में नरेंद्र मोदी की शख्सियत है. जिस तरह प्रधानमंत्री के अपने प्रशंसक हैं जो यह मानते हैं कि वे गलती कर ही नहीं सकते, उसी तरह ऐसे लोग भी हैं जो यह मानते हैं उनका सत्ता में आना इतने दशकों में भारत के लिए सबसे बुरी बात हुई है. जब आप मोदी के घोर विरोधियों से बात करते हैं तो वे अपनी चिंताओं की कई वजहें गिनाते हैं. पहली वजह है अर्थव्यवस्था की हालत, जिसके बारे में हम देख चुके हैं कि अतिशयोक्ति की जा सकती है. जब सरकार ने नोटबंदी जैसी बेवकूफाना स्कीम को खारिज कर दिया उसके बाद से ऐसा कोई संकेत नहीं मिलता कि मोदी ने अर्थव्यवस्था के मामले में ऐसा कोई कदम उठाया है जो भारत के भविष्य को ही खतरे में डालता हो.
कई लोगों की शिकायत है कि प्रधानमंत्री की शैली तानाशाही वाली है. यह वाजिब शिकायत हो सकती है लेकिन भारत में प्रायः यही माना जाता है कि अगर आप अकेले अपने बूते अपनी पार्टी को चुनाव जितवाते हैं तो आप अपने साथियों की परवाह किए बिना अपनी मर्जी से जो चाहे कर सकते हैं. इंदिरा गांधी के मामले में ऐसा ही था. और अब यह मोदी के मामले में हो रहा है.
शिकायत यह भी है कि सरकार ने देश में डर का माहौल बना दिया है. सरकारी एजेंसियों का राजनीतिक मकसद से इस्तेमाल किया जा रहा है, मीडिया को आतंकित करके झुका दिया गया है.
ये सारी आलोचनाएं वाजिब हैं लेकिन ऐसा नहीं है कि यह सब पहले नहीं हुआ था. पहले की सरकारों ने भी सरकारी एजेंसियों का राजनीतिक मकसद से इस्तेमाल किया. हवाला मामले की याद तो होगी ही, जिसमें लालकृष्ण आडवाणी पर आरोप लगाया गया था? यहां तक कि एच.डी. देवेगौड़ा ने अपने राजनीतिक विरोधियों को निशाना बनाने और रेसकोर्स रोड के बंगले में ज्यादा समय तक टिके रहने के लिए एजेंसियों को हथियार के रूप में इस्तेमाल किया था.
जहां तक मीडिया की बात है, तो उसमें समस्याएं हैं. मुख्यधारा वाला प्रेस सरकार को नाखुश करने से इस कदर डरा हुआ है कि तमाम संपादक और मालिकान, जो यूपीए-2 के दौर में बब्बर शेर बने नज़र आते थे, आज भीगी बिल्ली बने दिख रहे हैं.
लेकिन मीडिया के साथ इस तरह का सुलूक करने वाली यह कोई पहली सरकार नहीं है. अटल बिहारी वाजपेयी के दौर में सरकार की आलोचना करने वाले प्रकाशनों के दफ्तरों पर छापे मारे गए थे. राजीव गांधी ने ‘इंडियन एक्सप्रेस’ के खिलाफ कई मामले दायर किए थे, और इंदिरा गांधी ने तो प्रेस सेंसरशिप ही लगा दी थी. मीडिया की आज जो हालत है उससे शायद ही कोई खुश होगा. लेकिन पहले भी ऐसा हो चुका है, केवल ‘डिग्री’ का अंतर हो सकता है.
जब आप प्रधानमंत्री के आलोचकों से बात करेंगे तो पाएंगे कि उनकी प्रायः सभी चिंताएं प्रायः वाजिब तो हैं लेकिन उनमें जितनी दहशत है उसे ये चिंताएं उचित नहीं ठहरातीं. जब तक आप अर्थव्यवस्था, चीन के साथ संबंधों, सरकारी एजेंसियों के दुरुपयोग जैसे मुद्दों से आगे नहीं बढ़ते तब तक आप मूल मसले तक नहीं पहुंचते.
प्रधानमंत्री अगर ध्रुवीकरण के केंद्र बने हैं तो इसकी असली वजह वह सब नहीं है जो उनके बारे में टीवी चैनलों पर होने वाली बहसों या प्रेस में कहा जा रहा है. इसकी वजह यह है कि नरेंद्र मोदी की सरकार उस आम सहमति को उलट देने में जुटी है, जो भारत का आधार रही है.
यह भी पढ़ें : ट्विटर एक शोरशराबे वाले मंच से ज्यादा कुछ नहीं, बीजेपी ये अच्छे से जानती है लेकिन पत्रकार नहीं
हिंदू दक्षिणपंथ की अनकही मंशा
देश के आज़ाद होने से पहले और उसके ठीक बाद कुछ समय तक आरएसएस के नेताओं और ‘चिंतकों’ ने जो कुछ कहा था उस पर अगर आप गौर करेंगे तो आप ऐसे भी बयान पाएंगे (मसलन हिटलर और नाज़ियों की तारीफ के) कि आरएसएस को भी शर्म आएगी. लेकिन उनके ऐसे विचार भी सामने आएंगे जो भविष्य के भारत के बारे में गांधी, नेहरू, पटेल और आंबेडकर के विचारों के पूरी तरह विपरीत हैं. इन दोनों नजरियों में जो फर्क है उसे एक जुमले में समेटा जा सकता है और वह है— ‘हिंदू-मुस्लिम’.
हमारे संविधान निर्माताओं ने उस भारत की कल्पना की थी जिस पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आदि सबका बराबर का हक होगा, लेकिन आरएसएस हिंदू राष्ट्र चाहता है.
सच कहा जाए तो आज जो प्रचार फैलाया जा रहा है उसके विपरीत, आरएसएस यह नहीं चाहता कि मुसलमानों का संहार किया जाए. वह सिर्फ यह चाहता है कि मुसलमान यह कबूल करें कि वे एक हिंदू देश में रह रहे हैं. मुसलमानों को आक्रमणकारियों का वंशज मानने वाले आरएसएस प्रमुख एम.एस. गोलवलकर के इस बयान को देखिए— ‘विदेशी नस्ल वालों को अपनी अलग पहचान खत्म करके हिंदू नस्ल की पहचान में मिला देना चाहिए, या वे इस देश में हिंदू राष्ट्र के पूरी तरह अधीन होकर ही रह सकते हैं और वे किसी विशेष अधिकार के हकदार नहीं होंगे, उन्हें कोई प्राथमिकता नहीं दी जाएगी, न ही नागरिक अधिकार दिए जाएंगे.’ इसी तरह की कई और बातें की गई हैं.
यह कोई संयोग नहीं है कि हिंदू दक्षिणपंथियों ने ऐसी लफ्फाजी केवल मुगलों को लेकर ही की है. उस दौर में हिंदू बहुसंख्यक थे और अपना कामकाज शांति से चलाते थे. लेकिन शासन बेशक मुसलमानों का था और हिंदुओं को अक्सर अपने अधिकारों से वंचित किया जाता था और धर्म के आधार पर उनसे टैक्स वसूला जाता था.
हिंदू दक्षिणपंथियों के लिए आदर्श स्थिति यह होती कि आज भूमिकाएं उलट जातीं. मुसलमानों को एहसास कराया जाता कि वे हिंदुओं के शासन के अधीन हैं और अब हिंदू तौर-तरीके ही चलेंगे. उनका कहना है कि हिंदू जब मुगलों के अधीन उस तरह रह सकते थे तो आज के भारत में मुसलमान उस तरह क्यों नहीं रह सकते?
इसे आप एक बार समझ लें, तो हिंदू दक्षिणपंथियों (जुनूनियों से लेकर नेताओं तक) की हर बात इसी तर्क से उभरती नज़र आएगी. इसीलिए कोई भी सड़क मुगलों के नाम पर नहीं होनी चाहिए (दिल्ली भाजपा अकबर रोड और हुमायूं रोड के नाम बदलना चाहती है). इसीलिए किसी शहर का नाम मुस्लिम नाम पर न हो (इलाहाबाद को प्रयागराज कहा जाए, आदि-आदि). इसीलिए मुसलमानों को गोमांस खाने की छूट न हो; वे हिंदू तौर-तरीकों को अपनाएं. इसीलिए हिंदू त्योहारों में मांस की दुकानें बंद की जाएं. इसीलिए इस्लामी स्मारकों की या तो उपेक्षा की जाए या उनके मूल पर सवाल खड़ा किया जाए. उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार के अनुसार महान स्मारकों की सूची में ताजमहल को ऊंचा स्थान नहीं दिया जाएगा. और हिंदू दक्षिणपंथी इसे हिंदू महल घोषित करेंगे.
भारत की इस तरह की छवि बनाए जाने को लोग अक्सर हिंदू-मुस्लिम टकराव के रूप में लेते हैं. हमेशा ऐसा नहीं होता. तनाव हमेशा से रहा है. भारत बंटवारे के दंगों और हिंदू-मुस्लिम हिंसा में से ही बना है. अफसोस कि यह हमारे देश की एक सच्चाई है. खाइयों को कभी पाटा नहीं गया और सभी दलों के नेता उनका फायदा ही उठाने की कोशिश करते रहे.
लेकिन आज जो कुछ हो रहा है वह इससे भी आगे की बात है. यह उस आम सहमति को उलटने के लिए राज्यसत्ता का इस्तेमाल करने की कोशिश है, जिसके आधार पर आधुनिक भारत की इमारत खड़ी करने की कोशिश की गई थी.
मोदी को ध्रुवीकरण का केंद्र बनने से परहेज नहीं
यह स्पष्ट नहीं है कि भाजपा को यह सब करने का जनादेश मिला है या नहीं. प्रधानमंत्री ने कभी यह कबूल नहीं किया है कि वे ऐसा करना चाहते हैं. उनके भाषणों में सांप्रदायिकता के सवालों को शायद ही कभी उठाया गया है. और उनके समर्थक जब हद पार करते हैं (मसलन गाय के मामले में लिंचिंग आदि) तब वे कुछ समय तक चुप्पी ओढ़े रहते हैं और बाद में इन कार्रवाइयों के खिलाफ कभीकभार अपनी चुप्पी तोड़ते हैं.
यह कहना मुश्किल है कि भाजपा और मोदी अगर वास्तव में यह घोषित कर दें कि यह उनका एजेंडा है तो उन्हें व्यापक समर्थन हासिल होगा ही. प्रशांत किशोर कहते रहे हैं कि भाजपा की बड़ी जीत होती है तब भी उसे भारतीयों और हिंदुओं तक के बहुमत का समर्थन शायद ही हासिल होता है. आप 40 फीसदी वोट लेकर भारत में राष्ट्रीय चुनाव जीत सकते हैं, आपको जबरदस्त जीत हासिल हो सकती है लेकिन तब भी यह नहीं माना जाएगा कि आपको बहुमत का समर्थन मिल गया है, उस एजेंडा के लिए तो कतई नहीं जो अघोषित है.
जब आप प्रधानमंत्री के आलोचकों से बात करते हैं तब आर्थिक स्थिति, विदेश नीति आदि के बारे में तमाम बातें करने के बाद यही मुद्दा होता है जो मोदी की भाजपा के खिलाफ विरोध को परिभाषित करता है. यही वजह है कि प्रधानमंत्री इतने गहरे ध्रुवीकरण के केंद्र बनते हैं.
ध्रुवीकरण का केंद्र बनना अपने आपमें कोई बुरी बात नहीं है. फ्रैंकलिन डी. रूज़वेल्ट ने अमेरिका में ध्रुवीकरण कर दिया था, डोनाल्ड ट्रंप ने भी किया. मारग्रेट थैचर ने ब्रिटेन को दो खेमों में बांट दिया था. इसलिए मुझे लगता है कि मोदी अपने आलोचकों की बातों की शायद ही परवाह करते हैं.
लेकिन यह हमें तीन बड़े सवालों के सामने ला खड़ा करता है.
पहला : प्रधानमंत्री मोदी यह सब क्यों कर रहे हैं? एक संभावना यह है कि वे राजनीतिक फायदे के लिए ऐसा कर रहे होंगे. इसमें वे विश्वास करते हैं. भारत के बारे में उनकी कल्पना यही है.
दूसरा : अगर आप हिंदू-मुस्लिम मसले को परे कर देते हैं तो मोदी की भाजपा को और व्यापक समर्थन मिल सकता है. हम देख चुके हैं कि प्रधानमंत्री के खिलाफ लोगों की दूसरी शिकायतें उतनी बड़ी नहीं हैं. और विपक्ष जिस कदर अक्षम दिखता है उसके कारण मोदी लोकसभा चुनाव फिर जीत सकते हैं. इसलिए क्यों माथापच्ची की जाए?
तीसरा और अंतिम सवाल : अगर वे इसी रास्ते पर चलते रहे तो क्या भारत आगे खुशहाल बन पाएगा? क्या सारी दुनिया हमारे खिलाफ नहीं हो जाएगी? क्या अल्पसंख्यक खुद को हाशिये पर डाला जाना चुपचाप कबूल कर लेंगे?
इन सवालों के जो जवाब आपके मन में उभर रहे हैं वे मेरे मन में भी उभर रहे हैं. लेकिन इन पर गंभीरता से सोचने की जरूरत है.
(वीर सांघवी भारतीय प्रिंट और टीवी पत्रकार, लेखक और टॉक शो होस्ट हैं. उनका ट्विटर हैंडल @virsanghvi है. व्यक्त विचार निजी हैं)
(इस लेख को अंग्रेजी में पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)
यह भी पढ़ें : अगर भाजपा क्षेत्रीय पार्टी बनना चाहती है तो फिर वो देश में हिंदी को जरूर थोपे