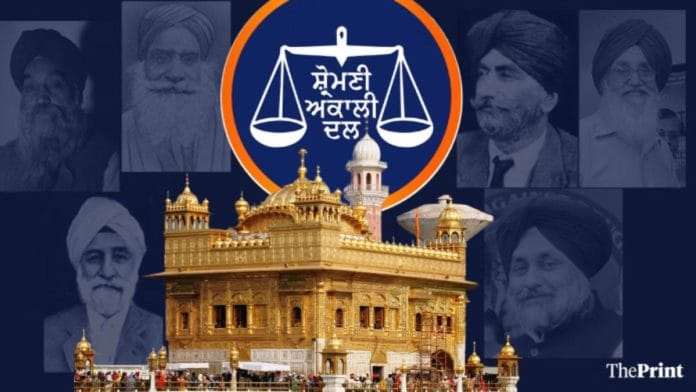चंडीगढ़: शिरोमणि अकाली दल (शिअद) पिछले हफ्ते एक और फाड़ का गवाह बना—इस बार नए गुट ने खुद को “असली” अकाली दल बताया है. ज्ञानी हरप्रीत सिंह की अगुवाई वाला यह नया गुट 2017 में सत्ता खोने के बाद पार्टी में बढ़ते बिखराव का ही एक और उदाहरण है.
पंजाब यूनिवर्सिटी, चंडीगढ़ के इतिहास विभाग के प्रमुख प्रोफेसर जसबीर सिंह ने दिप्रिंट से कहा, “2017 के बाद जो भी फाड़ें हुईं, वह उन लोगों की अगुवाई में थीं जो सत्ता में रहते हुए फायदे उठाते रहे. चुनावी हार के बाद उन्होंने बादल परिवार को दोष दिया और पार्टी छोड़कर अपने अलग-अलग गुट बना लिए, लेकिन इसमें कुछ नया नहीं है.”
उन्होंने आगे कहा, “सौ साल से भी ज्यादा के इतिहास में अकाली दल के नेता एकजुट कम और बंटे हुए ज़्यादा रहे हैं, फिर भी यह पार्टी पंजाब की राजनीति में हमेशा एक बड़ी ताकत बनी रही.”
दिसंबर 1920 में स्थापना के बाद से ही अकाली दल कई बार बिखरा है. कई मौकों पर एक ही समय पर आधा दर्जन गुट मौजूद रहे.
डीएवी कॉलेज, अंबाला के राजनीति विज्ञान विभाग से जुड़े प्रोफेसर भूपिंदर सिंह अपने एक शोध पत्र में लिखते हैं कि आमतौर पर, “जब अकाली सत्ता से बाहर होते हैं तो आपस में लड़ते हैं, और जब सत्ता में होते हैं तो दूसरों से.”
यह भी पढ़ें: SGPC अध्यक्ष के इस्तीफे ने धार्मिक संस्था और अकाल तख्त को परेशानी में क्यों डाल दिया है
अकाली दल की शुरुआती टूट: 1925, 1928
गुरुद्वारा सुधार आंदोलन के दौरान नवंबर 1920 में शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (एसजीपीसी) का गठन हुआ ताकि सिख गुरुद्वारों को स्वतंत्र बनाया जा सके. एक महीने बाद, शिरोमणि अकाली दल बनाया गया, जिसे पहले गुरुद्वारा सेवक दल कहा जाता था. यह एसजीपीसी का टास्क फोर्स था.
इतिहासकार अमरजीत सिंह नारंग अपनी किताब Region, Religion, and Politics: 100 Years of Shiromani Akali Dal में लिखते हैं कि शिअद का गठन उन स्वयंसेवकों यानी अकालियों के प्रयासों को समन्वित करने के लिए किया गया था, जो स्थानीय नेताओं का अनुसरण करते थे. इससे पहले, 1919 में सेंट्रल सिख लीग नामक राजनीतिक पार्टी बनी थी, जिसके नेता एसजीपीसी और शिअद दोनों में समान थे. इसके संस्थापकों में बाबा खरक सिंह भी शामिल थे.
इतिहासकार मोहिंदर सिंह लिखते हैं कि जब 1925 में सिख गुरुद्वारे और श्राइन बिल पास हुआ, जिसने एसजीपीसी को अधिकार दिए, तभी एसजीपीसी के नेताओं में फूट पड़ गई. एक ओर मध्यमार्गी नेता सरदार बहादुर मेहताब सिंह और ज्ञानी शेर सिंह थे, तो दूसरी ओर कट्टरपंथी बाबा खरक सिंह और मास्टर तारा सिंह. ये सभी अक्टूबर 1923 से लाहौर जेल में बंद थे क्योंकि ब्रिटिश प्रशासन ने एसजीपीसी को गैर-कानूनी संगठन घोषित कर दिया था. कट्टरपंथी नेताओं ने मध्यमार्गी नेताओं की आलोचना की क्योंकि उन्होंने ब्रिटिश हुकूमत से अपनी रिहाई के लिए बातचीत की थी.
बाद में अकाल तख्त ने हस्तक्षेप करके सेंट्रल सिख लीग (जिसमें बाबा खरक सिंह और मास्टर तारा सिंह थे) और एसजीपीसी का वह धड़ा जिसे सरदार बहादुर पार्टी कहा जाता था (जिसमें मेहताब सिंह और ज्ञानी शेर सिंह थे), दोनों को एक करने की कोशिश की.
लेकिन इतिहासकार मोहिंदर सिंह लिखते हैं— “असल एकता फिर कभी हासिल नहीं हो पाई.”
1928 में अकाली दल में एक और शुरुआती टूट हुई. यह मतभेद मोतीलाल नेहरू समिति रिपोर्ट पर अलग-अलग विचारों के कारण हुआ. इस रिपोर्ट ने अलग-अलग धार्मिक प्रतिनिधित्व खत्म करने और साझा निर्वाचन प्रणाली लागू करने की सिफारिश की थी.
प्रोफेसर कंवलप्रीत कौर (राजनीति विज्ञान विभाग, डीएवी कॉलेज, सेक्टर-10, चंडीगढ़) ने दिप्रिंट को बताया, “लेकिन रिपोर्ट में पंजाब और बंगाल में किसी भी समुदाय के लिए सीटों के आरक्षण का ज़िक्र नहीं था. इसी कारण अकाली दल तीन हिस्सों में बंट गया: एक धड़ा बाबा खरक सिंह के नेतृत्व में, दूसरा मंगल सिंह गिल के नेतृत्व में और तीसरा मास्टर तारा सिंह के नेतृत्व में.”
मंगल सिंह गिल नेहरू समिति में शामिल थे और रिपोर्ट का समर्थन कर रहे थे. नेहरू रिपोर्ट के खिलाफ प्रतिक्रिया में बाबा खरक सिंह ने 1929 के लाहौर कांग्रेस अधिवेशन के बहिष्कार का आह्वान किया. मास्टर तारा सिंह भी नेहरू रिपोर्ट के विरोधी थे, लेकिन कांग्रेस अधिवेशन के बहिष्कार से सहमत नहीं थे.
दोनों नेताओं— बाबा खरक सिंह और मास्टर तारा सिंह में 1930 के सविनय अवज्ञा आंदोलन में शामिल होने को लेकर भी मतभेद थे. उस वक्त एसजीपीसी के अध्यक्ष बाबा खरक सिंह इस आंदोलन में शामिल होने के खिलाफ थे क्योंकि राष्ट्रीय ध्वज में अब तक केसरिया रंग नहीं था, जो सिख समुदाय का प्रतीक माना जाता है. वहीं मास्टर तारा सिंह आंदोलन का सीधा विरोध नहीं करना चाहते थे.
अकाली दल बनाम सेंट्रल अकाली दल
इतिहासकार अमरजीत सिंह नारंग लिखते हैं, “अब अकाली दल में सीधा-सीधा बड़ा फूट पड़ गया था. बाबा खरक सिंह ने शिरोमणि अकाली दल पर कांग्रेस के आगे ‘समर्पण’ का आरोप लगाया और एसजीपीसी और सेंट्रल सिख लीग के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देकर कुछ अन्य नेताओं के साथ शिअद को छोड़ दिया. मास्टर तारा सिंह ने शिअद और एसजीपीसी दोनों के अध्यक्ष पद संभाल लिए और अगले तीन दशकों तक शीर्ष नेतृत्व में बने रहे.”
वे आगे लिखते हैं, “बाबा खरक सिंह ने बाद में मार्च 1934 में एक नई पार्टी बनाई, जिसे शुरुआत में ‘सिख नेशनल लीग’ कहा गया और फिर नाम बदलकर ‘सेंट्रल अकाली दल’ कर दिया गया. ‘सेंट्रल अकाली दल’, जो 1947 तक सक्रिय रहा, कभी जनसमर्थन हासिल नहीं कर सका और शिअद ही सिख मुख्यधारा का प्रतिनिधि बना रहा.”
मास्टर तारा सिंह के नेतृत्व वाले अकाली दल और बाबा खरक सिंह व ज्ञानी शेर सिंह के नेतृत्व वाले सेंट्रल अकाली दल के बीच मतभेद कई सालों तक चलते रहे. ये मतभेद 1940 के शुरुआती दशक में फिर उभरकर सामने आए, जब सेंट्रल अकाली दल ने मास्टर तारा सिंह के आज़ाद पंजाब अभियान का विरोध किया. इस अभियान का मकसद पंजाब की सीमाओं का पुनर्निर्धारण करना था, ताकि हिंदू या सिख बहुल इलाकों को मुस्लिम लीग के पाकिस्तान के खाके से अलग किया जा सके.
यह भी पढ़ें: सुखबीर सिंह बादल ने हमलावर को तो चकमा दे दिया, लेकिन असली खतरा अकाल तख्त का फैसला है
तारा सिंह बनाम फतेह सिंह
पंजाबी सूबा आंदोलन, जो 1947 में शुरू हुआ, के दौरान अकालियों ने पंजाबी सूबा (यानी पंजाबी बोलने वालों के लिए राज्य) की मांग को लेकर अभियान चलाया.
करीब डेढ़ दशक बाद, 1962 में पार्टी दो हिस्सों में बंट गई—एक गुट मास्टर तारा सिंह के नेतृत्व में और दूसरा संत फतेह सिंह के नेतृत्व में. बाद में, उम्रदराज़ हो चुके मास्टर तारा सिंह ने 1965 में संत फतेह सिंह का विरोध छोड़ दिया. इसके बाद 1966 में पंजाब का पुनर्गठन हुआ और यह एकभाषी (पंजाबी) राज्य बना.
जे.एस. ग्रेवाल अपनी किताब The Akalis, A Short History में लिखते हैं कि 1967 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को बहुमत नहीं मिला और दूसरी पार्टियां संत फतेह सिंह गुट के अकालियों के साथ मिलकर सरकार बनाने को तैयार हो गईं.
मार्च 1967 में जस्टिस गुरनाम सिंह ने पहली ग़ैर-कांग्रेसी सरकार बनाई, जिसे पीपुल्स यूनाइटेड फ्रंट सरकार कहा गया.
हालांकि, नवंबर 1967 में यह सरकार गिर गई क्योंकि कांग्रेस ने एक अन्य अकाली नेता, लछमन सिंह गिल को समर्थन दे दिया, जो गुरनाम सिंह की जगह मुख्यमंत्री बनना चाहते थे. 22 नवंबर 1967 को लछमन सिंह गिल मुख्यमंत्री बने, उसी दिन मास्टर तारा सिंह का निधन हुआ, लेकिन गिल की सरकार भी ज़्यादा नहीं चली और अगस्त 1968 में गिर गई. इसके बाद पंजाब राष्ट्रपति शासन के अधीन आ गया—यह सब “संयुक्त पंजाब” (पंजाब और हरियाणा) के पुनर्गठन के मुश्किल से दो साल बाद हुआ.
तोहरा-तलवंडी बनाम बादल
मास्टर तारा सिंह की मौत के बाद, 1968 में विधानसभा के मध्यावधि चुनावों से कुछ महीने पहले दोनों अकाली गुट फिर से एकजुट हो गए. 1969 में हुए चुनाव में अकालियों ने कांग्रेस को हराया. जनसंघ के सहयोग से गुरनाम सिंह फिर मुख्यमंत्री बने, लेकिन राज्यसभा में उम्मीदवार के चयन को लेकर संत फतेह सिंह और गुरनाम सिंह में मतभेद हो गए.
जनसंघ विधायकों के अलग होने के बाद, 1970 में संत फतेह सिंह गुट ने प्रकाश सिंह बादल को मुख्यमंत्री बनाया. मगर 1971 में उनकी सरकार भी गिर गई और राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया.
गुरनाम सिंह ने अपना अलग अकाली गुट बना लिया, जिसने 1972 के चुनाव में अकाली दल के खिलाफ चुनाव लड़ा.
1975 में इंदिरा गांधी द्वारा आपातकाल लगाने के बाद शिरोमणि अकाली दल में और दरारें गहरी हो गईं. प्रकाश सिंह बादल ने आपातकाल का विरोध किया, लेकिन गुरचरण सिंह तोहरा और जगदेव सिंह तलवंडी शुरू में उनके खिलाफ थे. बाद में दोनों ने अपना रुख बदल दिया.
जून 1977 में बादल ने जनता पार्टी के साथ मिलकर सरकार बनाई और मुख्यमंत्री बने. कुछ समय बाद उनके शिक्षा मंत्री सुखजिंदर सिंह पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे. बादल उन्हें हटाना चाहते थे, लेकिन तब के एसजीपीसी प्रमुख तोहरा और अकाली दल प्रमुख तलवंडी सुखजिंदर सिंह के साथ खड़े रहे.
कुलदीप कौर अपनी किताब Akali Dal in Punjab politics: Splits and mergers में लिखती हैं कि बादल, तोहरा और तलवंडी के बीच मतभेदों से अकाली दल में संगठनात्मक और धार्मिक नेतृत्व की खींचतान पैदा हो गई.
सितंबर 1979 में अकाली दल की कार्यकारिणी चुनावों से पहले तोहरा और तलवंडी ने अकाल तख्त के जत्थेदार को चिट्ठी लिखी और आरोप लगाया कि प्रकाश सिंह बादल और एसजीपीसी उपाध्यक्ष हरचंद सिंह लोंगोवाल सिख हितों के खिलाफ काम कर रहे हैं.
चारों नेताओं को अकाल तख्त बुलाया गया. जत्थेदार साधू सिंह भौरा ने सभी को एकजुट करने की कोशिश की, लेकिन असफल रहे. उसी साल बादल सरकार को बर्खास्त कर दिया गया और पंजाब में दोबारा राष्ट्रपति शासन लग गया.
फिर कांग्रेस नेता दरबारा सिंह मुख्यमंत्री बने.
अगस्त 1980 में बादल गुट ने अकाली दल से जगदेव सिंह तलवंडी को हटा दिया. जवाब में तलवंडी ने, जो तब तक अपने गुट को मज़बूत कर चुके थे, बादल को ही अपनी पार्टी से निकाल दिया.
हालांकि, तलवंडी ने खुद को अपने गुट का प्रमुख घोषित किया, लेकिन बादल गुट ने अकाली दल का नेतृत्व हरचंद सिंह लोंगोवाल को सौंप दिया, जिन्हें एसजीपीसी प्रमुख तोहरा का समर्थन मिला. इस तरह बादल ने बाज़ी अपने पक्ष में पलट दी, भले ही अस्थायी रूप से.
सत्ता से बाहर होने के बाद, बादल और तलवंडी गुट पंथक राजनीति में एक-दूसरे से प्रतिस्पर्धा करने लगे. अगस्त 1982 में लोंगोवाल ने आनंदपुर साहिब प्रस्ताव को लागू करने के लिए धरम युद्ध मोर्चा शुरू किया. इसमें उन्होंने सिख धर्म को एक स्वतंत्र और अलग धर्म के रूप में स्थापित करने की बात रखी—हिंदू धर्म से अलग. इससे कुछ महीने पहले ही तलवंडी गुट ने इसी तरह का कार्यक्रम घोषित किया था.
इसके बाद गुटबाज़ी और बढ़ी. भगवंत सिंह दानेवालिया, जो अब तक तलवंडी का साथ दे रहे थे, अलग हो गए और उन्होंने फेडरल शिरोमणि अकाली दल नाम से अपना गुट बना लिया.
यह भी पढ़ें: ‘तनखैया’ घोषित किए जाने के बाद, बादल के अकाली दल के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के क्या हैं मायने
लौंगोवाल–तलवंडी–बादल–बर्नाला
1984 के ऑपरेशन ब्लू स्टार और जरनैल सिंह भिंडरांवाले की मौत के बाद, उनके पिता बाबा जोगिंदर सिंह को तलवंडी ने अकाली दल की कमान संभालने के लिए कहा, ताकि सभी गुट एक साथ आ जाएं. 1985 में जोगिंदर सिंह ने यह ऐलान किया कि अकाली दल का विलय होगा और उन्होंने 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या की साजिश के आरोप में गिरफ्तार सिमरनजीत सिंह मान को दल का संयोजक बना दिया, लेकिन लौंगोवाल इसमें शामिल नहीं हुए.
उसी साल लौंगोवाल ने प्रधानमंत्री राजीव गांधी से शांति वार्ता की, जबकि बादल और तोहरा इसके खिलाफ थे. सुरजीत सिंह बर्नाला के समर्थन से हरचंद सिंह लौंगोवाल ने राजीव गांधी के साथ शांति समझौते पर दस्तखत कर दिए. इसका उन्हें बड़ा खामियाज़ा भुगतना पड़ा. अगस्त 1985 में उग्रवादियों ने उनकी हत्या कर दी. इसके बाद बर्नाला ने उनके गुट की कमान संभाली. तोहरा और बादल ने भी बर्नाला का साथ दिया.
अकाली दल ने 1985 का विधानसभा चुनाव जीता और बर्नाला मुख्यमंत्री बने, लेकिन अप्रैल 1986 में जब उन्होंने स्वर्ण मंदिर से उग्रवादियों को बाहर निकालने के लिए ऑपरेशन चलाया, तो बादल 27 विधायकों के साथ अलग हो गए और अपनी अकाली दल की अलग पार्टी बना ली.
बर्नाला सरकार में मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी इसका विरोध करते हुए इस्तीफा दे दिया और अकाली दल (बादल) के अध्यक्ष बन गए.
फरवरी 1987 में अकाल तख्त के जत्थेदार दर्शन सिंह ने सभी गुटों को भंग करते हुए एक संयुक्त अकाली दल (यूएडी) बनाने का एलान किया और इसकी कमान मान को दी, जो उस समय जेल में थे.
जत्थेदार के आदेश मानते हुए कैप्टन अमरिंदर और जोगिंदर सिंह ने अपने-अपने गुटों की अध्यक्षता से इस्तीफा दे दिया. जोगिंदर सिंह के समर्थन से मान ने अकाली दल (बादल), अकाली दल (तलवंडी), ऑल इंडिया सिख स्टूडेंट्स फेडरेशन (AISSF) और दामदमी टकसाल का विलय कर दिया, लेकिन सुरजीत बर्नाला इससे अलग रहे.
दोनों अकाली गुटों ने अपने-अपने एसजीपीसी अध्यक्ष चुने.
कुछ महीनों बाद बर्नाला सरकार बर्खास्त कर दी गई और एक बार फिर पंजाब राष्ट्रपति शासन के अधीन आ गया.
अकाली दल का बिखराव
फरवरी 1992 में पंजाब में चुनाव होने वाले थे. प्रोफेसर कंवलप्रीत ने दिप्रिंट को बताया कि उस साल के चुनाव से पहले अकाली दल सबसे ज़्यादा गुटों में बंट गया था.
20 दिसंबर 1991 को अकाली दल (लोंगोवाल) और अकाली दल (पंथिक) ने राज्य चुनाव लड़ने के लिए गठबंधन करके आपस में विलय कर लिया, लेकिन प्रोफेसर के अनुसार, एआईएसएसएफ, अकाली दल (बादल), अकाली दल (मान), अकाली दल (बाबा) और अकाली दल (बब्बर) ने तब तक चुनाव बहिष्कार का ऐलान कर दिया जब तक पंजाब समस्या का स्थायी हल नहीं निकल जाता.
इसके बाद, अकाली दल (लोंगोवाल) के सदस्य काबुल सिंह ने अपनी पार्टी के चुनाव लड़ने के फैसले का विरोध किया और अकाली दल (काबुल) नाम का अलग गुट बना लिया. वहीं, अकाली दल (बादल) के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुखजिंदर सिंह ने चुनाव न लड़ने के फैसले का विरोध किया और अकाली दल (सुखजिंदर) बना लिया.
इसके अलावा, वरिष्ठ अकाली नेता जीवन सिंह उमरानांगल ने तरुणा निहंग दल के प्रमुख बाबा अजीत सिंह निहंग के साथ मिलकर शिरोमणि जगत अकाली दल (शिअद) बनाया. इनका भी मकसद चुनाव लड़ना था.
अकाली दल (फेरुमन) ने चुनाव न लड़ने का फैसला किया. तलवंडी का अकाली दल-टी भी चुनाव का बहिष्कार करने पर अड़ा रहा. इसी दौरान एआईएसएसएफ से एक नया गुट निकला, जिसका नाम पड़ा अकाली दल (मंजीत).
आखिरकार 1992 के चुनाव कांग्रेस ने जीत लिए और बेअंत सिंह मुख्यमंत्री बने. 1994 में अकाल तख्त ने फिर से सभी गुटों को एक करने की कोशिश की. मई में सिमरनजीत मान की अगुवाई में शिरोमणि अकाली दल (अमृतसर) का गठन हुआ.
हालांकि, बादल ने इसका विरोध किया और इसमें शामिल होने से साफ इनकार कर दिया.
यह भी पढ़ें: SGPC कैसे कराती है चुनाव और पंजाब की राजनीति से इसका क्या है संबंध
बादल बनाम तोहरा
1995 तक ज़्यादातर अकाली धड़े प्रकाश सिंह बादल के समूह में शामिल हो गए थे, जिसने पंजाब में एक धर्मनिरपेक्ष विकल्प पेश किया. वहीं, मान के नेतृत्व वाला अकाली दल (अमृतसर) और कैप्टन अमरिंदर का अकाली दल (पंथिक) बादल से अलग ही रहे.
1999 में, उस समय की गठबंधन सरकार के मुखिया बादल ने खालसा पंथ की स्थापना के 300 साल पूरे होने का जश्न मनाने का फैसला किया, लेकिन एसजीपीसी (शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी) के प्रमुख तोहरा नाराज़ हो गए क्योंकि बादल ने उनके धड़े को इस कार्यक्रम में शामिल नहीं किया.
तोहरा ने बादल की आलोचना की और उनसे अकाली दल प्रमुख का पद छोड़ने को कहा. इसके बाद मुख्यमंत्री बादल ने तोहरा को एसजीपीसी प्रमुख पद से हटाकर उनकी जगह बीबी जगीर कौर को नियुक्त कर दिया. बीबी जगीर कौर अब सुखबीर बादल का विरोध करने वाले हरप्रीत सिंह के नेतृत्व वाले बागी समूह में हैं.
1999 लोकसभा चुनाव से पहले तोहरा ने सरब हिंद शिरोमणि अकाली दल बनाया और चुनाव लड़ा. 2002 का पंजाब विधानसभा चुनाव प्रकाश सिंह बादल सरकार और अकाली दल के लिए बुरी तरह असफल रहा.
इसके बाद कांग्रेस टिकट पर पंजाब के मुख्यमंत्री बने कैप्टन अमरिंदर सिंह. उसी समय अकाल तख्त जत्थेदार जोगिंदर सिंह वेदांती ने तोहरा और बादल को फिर से एक किया. 2003 में, जगदेव तोहरा को दोबारा एसजीपीसी प्रमुख बनाया गया.
2007 में अकाली दल-बीजेपी गठबंधन ने फिर से पंजाब में सत्ता हासिल की और बादल चौथी बार मुख्यमंत्री बने.
अक्टूबर 2010 में बादल के भतीजे और तब पंजाब के वित्त मंत्री मनप्रीत बादल ने पार्टी से अलग होकर पीपल्स पार्टी ऑफ पंजाब बनाई. उस समय मौजूदा पंजाब सीएम भगवंत मान भी उनके साथ थे और पार्टी के महासचिव बने.
2012 के पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले मनप्रीत बादल ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीआई), माकपा (सीपीआई-एम) और शिरोमणि अकाली दल (लोंगोवाल) को साथ लाकर साझा मोर्चा (सांझा मोर्चा) बनाया. इस मोर्चे को 6% वोट मिले लेकिन एक भी सीट नहीं मिली.
2017 के पंजाब विधानसभा चुनाव से एक साल पहले, बागी अकाली नेता—भाई बलविंदर सिंह बैंस और सिमरजीत सिंह बैंस ने मिलकर लोक इंसाफ पार्टी बनाई. इस पार्टी ने आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन करके 5 सीटों पर चुनाव लड़ा. दोनों भाइयों ने अपनी-अपनी सीट जीतीं.
2017 के बाद की बगावतें
2017 पंजाब विधानसभा चुनाव में अकाली दल की करारी हार के बाद पार्टी के पुराने और ताकतवर ‘टकसाली नेता’—रंजीत सिंह ब्रह्मपुरा, सुखदेव सिंह ढींडसा, रत्तन सिंह अजनाला और सेवा सिंह सेखवां ने पार्टी छोड़ दी. इन नेताओं ने इस हार के लिए सीधे बादलों को जिम्मेदार ठहराया. खासतौर पर प्रकाश सिंह बादल पर आरोप लगा कि उन्होंने पार्टी को अपने परिवार की जागीर बना दिया है.
इसके बाद अजनाला, ब्रह्मपुरा और सेखवां ने मिलकर अकाली दल (टकसाली) बनाया और ढींडसाओं ने अकाली दल (डेमोक्रेटिक) खड़ा किया.
फरवरी 2019 में, अकाली दल (टकसाली) ने आप के बागी नेता सुखपाल सिंह खैरा और डॉ. धर्मवीर गांधी के साथ हाथ मिलाकर पंजाब डेमोक्रेटिक अलायंस (पीडीए) बनाया और लोकसभा चुनाव लड़ा, लेकिन इसका खास असर नहीं पड़ा.
अप्रैल 2021 में विधानसभा चुनाव से एक साल पहले, अकाली दल (टकसाली) और अकाली दल (डेमोक्रेटिक) ने घोषणा की कि वे मिलकर एक संयुक्त पार्टी के रूप में चुनाव लड़ेंगे. फिर भी 2022 के पंजाब विधानसभा चुनाव में अकाली दल को एक और शर्मनाक हार झेलनी पड़ी.
2023 में प्रकाश सिंह बादल की मौत के बाद पार्टी की स्थिति और कमज़ोर हो गई. हालांकि, सुखबीर बादल की सुलह की कोशिशों से कुछ पुराने नेता वापस लौट आए, लेकिन ढींडसा गुट लगातार अकाली दल को तोड़ने की हर कोशिश का समर्थन करता रहा.
2024 के लोकसभा चुनाव में करारी हार के बाद, पार्टी के 50 नेताओं ने जिनका नेतृत्व जगीर कौर, प्रेम सिंह चंदूमाजरा और परमिंदर ढींडसा कर रहे थे, सुखबीर बादल के खिलाफ बगावत कर दी. जून में नतीजे आने के बाद इन नेताओं ने सुखबीर के इस्तीफे की मांग की, जिससे पार्टी में मौजूदा और चल रहा संकट खड़ा हो गया.
(इस रिपोर्ट को अंग्रेज़ी में पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)
यह भी पढ़ें: जानिए कौन हैं पंजाब के शक्तिशाली डेरा ब्यास के नए आध्यात्मिक प्रमुख जसदीप सिंह गिल