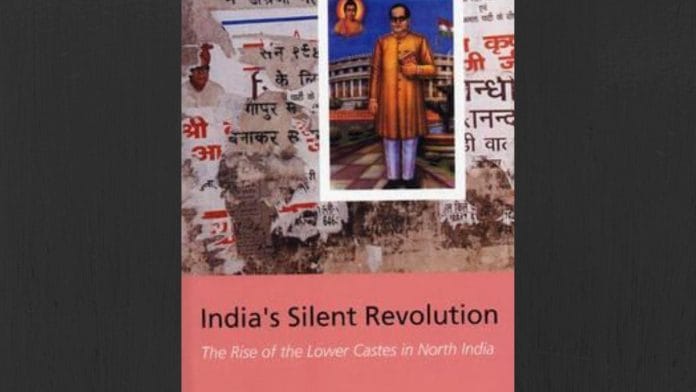भारत के सत्ता केंद्रों में सिर्फ राजनीतिक संस्थाएं ही ऐसी हैं, जहां भारत की सामाजिक विविधता को कुछ हद तक देखा जा सकता है. बाकी सत्ता केंद्रों जैसे न्यायपालिका, उच्च नौकरशाही, कॉरपोरेट जगत, मीडिया, मनोरंजन और कला इंडस्ट्री, धार्मिक संस्थाओं, उच्च शिक्षा संस्थानों में शिक्षक पदों आदि में विविधता का सख्त अभाव है.
अब ये चिंता जताई जा रही है कि राजनीति में भी सामाजिक विविधता घटने की प्रक्रिया शुरू हो गई है. वर्तमान लोकसभा में खासकर उत्तर भारत से आने वाले सांसदों में सवर्णों की हिस्सेदारी बढ़ी है. बीजेपी के 45 प्रतिशत सांसद सवर्ण हैं.
इसका असर नीतियों पर पड़ने लगा है. हाल में जिस तरह से आरक्षित वर्गों का कटऑफ कई राज्यों में ओपन कटेगरी से ऊपर चला गया या जिस तरह से सवर्णों को गरीबी के नाम पर आरक्षण दिया गया और इन मुद्दों पर राजनीतिक परिदृश्य में जिस तरह की खामोशी देखी गई, उससे ये लगता है कि सामाजिक न्याय और विविधता अब राजनीतिक मुद्दा नहीं रहे.
प्रस्तुत लेख का उद्देश्य उस राजनीति पर गौर करना है, जिसमें संविधान और नैतिकता को ताक पर रख कर कोई राजनीति पार्टी सत्ता में होने का फायदा उठाती है और अपने खास समर्थक वर्गों-जातियों का हित सुनिश्चित करने के लिए किसी भी हद तक जाती है. साथ ही ये जानने की कोशिश भी की जाएगी कि भारत में सामाजिक न्याय की राजनीति ढलान पर क्यों है.
सामाजिक न्याय की हार और भाजपा के साहसिक फैसले
भाजपा ने अपने कोर-समर्थकों की उम्मीदों और दीर्घकालिक ‘सामाजिक जरूरतों’ को पूरा करने के लिए जो कदम उठाए हैं, वे बेहद साहसिक हैं. ऐसा करते समय पार्टी ने किसी भी आलोचना की परवाह नहीं की. जिस गति से यह प्रक्रिया चल रही है, उसके नतीजे में आने वाले कई दशकों या उससे भी लंबे दौर तक के लिए दलित-पिछड़ी जातियों की इंसाफ की लड़ाई बाधित हो सकती है. साथ ही वंचित जातियों ने लोकतंत्र और संविधान के कारण अब तक जो उपलब्धियां हासिल की हैं, वे अब खतरे में हैं.
सवाल है कि क्या यह स्थिति अचानक और रातोरात आई है? क्या बीजेपी किसी जादू से सत्ता में आ गई और क्या सामाजिक न्याय की शक्तियां अचानक लापता हो गईं? क्या सामाजिक न्याय के मुद्दे अचानक लापता हो गए?
दरअसल, किसी भी विचारधारा की राजनीति अगर उस विचारधारा के लिए अनुकूल समाज नहीं बनाती है, तो उसका लंबे समय तक जिंदा रह पाना मुश्किल है. नब्बे के दशक में कुछ राज्यों में बहुजन तबकों के हाथ में सत्ता आई. भारत ही नहीं, दुनिया के प्रमुख राजनीति विज्ञानियों और समाजशास्त्रियों ने इस प्रक्रिया को लोकतंत्र का विस्तार माना. क्रिस्टोफ जैफोरले ने तो इसे साइलेंट रिवोल्यूशन की संज्ञा दी और ये सिद्धांत पेश किया कि नीचे की जातियों के लोकतंत्र में विश्वास के कारण ही भारत में लोकतंत्र टिक पाया है. जैफोरले ये देख रहे थे कि सिर्फ दक्षिण एशिया नहीं, दुनिया के कई विकासशील देशों में लोकतंत्र आया और फिर चला गया. इनमें से कई देशों में वहां की सत्ता को गरीबों और आम लोगों के विद्रोह का सामना करना पड़ा. लेकिन, भारत में ये नहीं हुआ.
परिवर्तन की शक्तियों को मौका मिला, फिर क्या हुआ?
1967 के बाद से भारत में कई राज्यों में निम्न और मध्यवर्ती जातियों के हाथ में सत्ता तो आई लेकिन उन्होंने सत्ता संरचना में बुनियादी बदलाव करने और समाज को अनुकूलित करने को अपना कार्यभार नहीं माना. उन्हें भी आमतौर पर एक यथास्थितिवादी ढांचे को ही निबाह देना भर जरूरी लगा. कुछ ढांचागत विकास को छोड़ दें, तो सामाजिक चेतना और अधिकारों के सवाल पर इस दौरान कोई काम नहीं हुआ. सांस्कृतिक मोर्चे पर समतामूलक विचारों को आगे बढ़ाने पर किसी ने ध्यान नहीं दिया, न ही पाठ्यपुस्तकों में इसके लिए बदलाव किए गए.
यह भी पढ़ें : आरक्षण नहीं, ये हैं भारतीय उच्च शिक्षा संस्थानों की दुर्गति की वजहें
लंबे समय तक कुछ राज्यों में सामाजिक न्याय की बात करने वाली ताकतों और कम्युनिस्ट पार्टियों की सत्ता कायम रही, लेकिन, सामाजिक वंचना के सवाल उनके एजेंडे में नहीं आए. जबकि समाज में पसरे अन्याय की सबसे बड़ी वजह बिल्कुल स्पष्ट थी. कुछ खास जातियों को छोड़ कर बाकी सब को शिक्षा से लेकर तंत्र के लगभग सभी हिस्सों में हाशिये के बाहर रखने की व्यवस्था चल रही थी. सामाजिक न्याय की राजनीति का दावा करके राजनीतिक सत्ता हासिल करने वाली पार्टियों के लिए यह सबसे बड़ी चुनौती और जिम्मेदारी थी कि वे शिक्षा और रोजगार के मोर्चे पर उम्मीद से ज्यादा सक्रियता दिखाते, स्कूल-अस्पताल का संजाल खड़ा कर देते, दलित-पिछड़ी जातियों, आदिवासियों और महिलाओं की ज्यादा से ज्यादा भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए हर संभव और सख्त फैसले लेते.
पुराने ढांचे पर निर्भर रही नई राजनीति
किसी समाज के वंचित तबकों के हक की लड़ाई के क्रम में अगर राजनीतिक सत्ता हासिल कर भी ली जाए तो वह तब तक बेमानी है, जब तक कि सत्ता तंत्र और संरचनाओं में इसकी भागीदारी और साफ असर न दिखे. मगर विडंबना यह रही कि सत्ता हासिल कर लेने के बाद सब कुछ ठीक हुआ मान लिया गया और बाकी मोर्चों पर कायम सामाजिक और जातिगत यथास्थिति को तोड़ने के लिए जरूरी फैसले नहीं लिए गए. नतीजतन, न शिक्षा, सेहत और रोजगार की तस्वीर में दलित-पिछड़ी जातियों और आदिवासियों के हक में कोई बदलाव आया, न इसकी बुनियाद पर कोई नई राजनीति खड़ी हो सकी. इन जाति-वर्गों के बीच चेतना-निर्माण और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के विकास की ऐतिहासिक जिम्मेदारी को कोई काम ही नहीं समझा गया कि कोई नया राजनीतिक विकल्प खड़ा हो पाता.
प्रचार तंत्र की अहमियत समझने में चूक
यही नहीं, जब मीडिया के एक हिस्से ने बिहार और उत्तर प्रदेश में यादव जाति के लोगों की बेलगाम भर्तियों की ‘खबर’ प्रचारित और प्रसारित की, तब सच इसके उलट होने के बावजूद, इसका उचित जवाब नहीं दिया गया. जबकि उस समय सरकार को सारी भर्तियों के आंकड़े सार्वजनिक कर देने थे. कायदे से समूचे तंत्र में सामाजिक विविधता के लिए ठोस पहलकदमी होनी चाहिए थी और ‘मुख्यधारा’ को अप्रिय लगने के बावजूद सख्त फैसले लिए जाने चाहिए थे! ऐसे में वर्चस्वशाली जातियों वाले तंत्र से विरोध उभर सकता था (उभरा भी!), लेकिन उसी तंत्र को दुरुस्त करना था! वंचित जातियों के बीच अंतर्विरोधों को भी मीडिया ने इस दौरान खूब हवा दी और इसका असर जातियों के बीच परस्पर अविश्वास की शक्ल में हुआ.
यह भी पढ़ें : सवर्ण करें दलित-पिछड़ों के महापुरुषों का सम्मान वरना बढ़ेंगी दूरियां
सवाल है कि जिन सामाजिक तबकों के सपने जमीन पर उतार लाने के वादे के साथ राजनीतिक सत्ता हासिल की गई थी, उन्हें क्या मिला! आखिर आज भी केंद्र और राज्यों की कुल नौकरियों में दलित-पिछड़ी जातियों की भागीदारी का अनुपात शर्मनाक निचले स्तर पर कायम क्यों है? इसमें सामाजिक न्याय और कम्युनिस्ट धारा की राजनीतिक पार्टियों ने क्या दखल दिया? एक राजनीतिक उम्मीद लेकर उभरे इन समूहों ने समाज को उसके हाल में कायम रहने के लिए क्यों छोड़ दिया?
यह बेवजह नहीं है कि लक्ष्य और अवसर से वंचित दलित-पिछड़ी जातियों के एक बड़े हिस्से को एक प्रतिगामी राजनीति की ओर खींच लेने में भाजपा को आसानी हुई. बीजेपी की सुविधा ये भी रही कि उसकी सांस्कृतिक विचारधारा को चुनौती देने वाली कोई धारा इस समय मौजूद ही नहीं है या फिर बेहद कमजोर स्थितियों में है.
कुल मिलाकर, जब तक जमीनी स्तर पर चेतना के सवालों पर संघर्ष नहीं होगा, तब तक सामाजिक यथास्थिति में कोई बदलाव नहीं आएगा और राजनीति की दिशा भी वही होगी! इसके बरक्स जिन्हें लगता है कि केवल सत्ता से ही सामाजिक सत्ता ‘संतुलन’ बदल जाएगा, उनके वहम का कोई इलाज नहीं है!
(लेखक वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक हैं और यह इनके निजी विचार हैं)