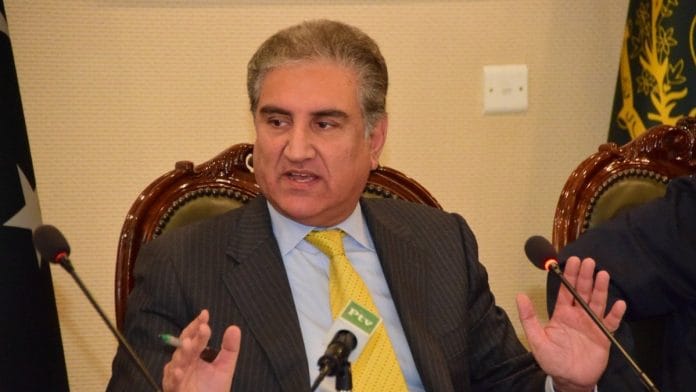भारत-चीन के बीच हालिया झड़प को बेचैनी और उत्तरी पड़ोसी की हरकत को विश्वासघात की भावना से देखने वाले लोगों के लिए एक सबसे नागवार पहलू था. पाकिस्तानियों का वह अनापेक्षित उल्लास जो उन्होंने अपने सबसे बड़े दुश्मन और अपने सर्वकालिक मित्र के बीच झगड़े के दौरान दिखाया. यहां तक कि जब भारत एक संभावित युद्ध के लिए कमर कस रहा था, पाकिस्तान के विदेश मंत्री अपने चीनी समकक्ष से फोन पर बात करके भरोसा दे रहे थे कि ‘मूलभूत हित’ में दोनों एक साथ खड़े होंगे.
लेकिन बहुत से लोग यह भूल गए होंगे कि कैसे चीन ने उस इलाके को हड़पना शुरू किया था, जिसे पाकिस्तान अपना बताता है, वो भी अक्साई चीन और लद्दाख पर बीजिंग की घेरेबंदी शुरू होने से बहुत पहले. यहां तक कि आज भी चीन अपना विस्तार जारी रखे है, बस तरीका थोड़ा-सा बदल गया है.
पाकिस्तानी क्षेत्र में चीन का सतत विस्तार शुरू तो पूरी तरह से कुछ घटनाओं के काल्पनिक आधार पर हुआ. लेकिन समय के साथ-साथ इसके मानचित्रों और दावों का श्रेणी में आ गया. यह ऐसी कहानी है जिसके सबक अच्छी तरह याद रखने की जरूरत है, क्योंकि बीजिंग ने गलवान घाटी के अलावा पूर्वी भूटान में नए दावे जताए हैं.
एक असामान्य ‘दोस्ती’
चीन की गिद्ध दृष्टि सबसे पहले हुंजा पर पड़ी थी, जो अब पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर का हिस्सा है. लेकिन एक समय यह रियासत रणनीतिक तौर पर अफगानिस्तान, पामीर, रूसी मध्य एशिया और दक्षिण शिनजियांग के साथ शक्सगाम हिल जो शिनजियांग सीमा पर स्थित है, का प्रवेश द्वार हुआ करती थी.
उस समय ही चीन ने पहली बार ‘दोस्ती’ का हाथ बढ़ाया. लेकिन हुंजा के मीर भी विस्तारवादी दृष्टिकोण रखते थे, इस तरह उन्होंने रक्सम घाटी और शिनजियांग के रणनीतिक नखलिस्तान ताशकोरगन, जो दोनों मौजूदा समय में चीन का हिस्सा हैं, पर दावेदारी जता दी. चूंकि एक नई ‘दोस्ती’ आकार ले रही थी, मीर के दावों ने चिंग कमांडरों को 1847 के आस-पास यारकंद और ताशकोरगन के बीच का इलाका हुंजा को ‘उपहार’ में देने से नहीं रोका.
बाद में, हुंजा रियासत कश्मीर के महाराजा गुलाब सिंह के आधिपत्य में आ जाने के बावजूद, चिंग लड़ाकों ने मीर को हथियार मुहैया कराए, राज्य में पहली बार अपने प्रतिनिधि भी भेजे.
उधर, अलग ही बड़े खेल में लगे ब्रितानियों ने चिंग को कश्मीर में दखलंदाजी के प्रति आगाह किया. अपने नामित व्यक्ति को सिंहासन पर बैठाया और अपना प्रभुत्व दर्शाने की कोशिश में चीनियों को समारोह में आमंत्रित किया. एक अधिकारी ने इसमें हिस्सा लिया. यद्यपि पीकिंग की तरफ से इसे हुंजा के एक ‘सहायक’ राज्य होने के संकेत के तौर पर प्रदर्शित किया गया.
यह भी पढ़ें : सीपेक चीन-पाकिस्तान का भ्रष्टाचार गलियारा है, यह भारतीय सुरक्षा को नए तरीके से चुनौतियां दे रहा है
इस बीच, हुंजाकुट्स ने व्यापारिक मार्गों पर लूटपाट जारी रखी, और शिनजियांग को भी कुछ हिस्सा भेजते रहे. इससे परस्पर सहमति वाली एक नई व्यवस्था बन गई, जिसमें मीर चीन में चारागाह वाली भूमि के इस्तेमाल के बदले भुगतान करते थे. यह क्रम 1930 के दशक तक चलता रहा, जिसके बाद यह चीनी अनुश्रुतियों का हिस्सा बन गया कि हुंजा उसकी जागीरदारी वाली रियासत थी.
हालांकि, शिनजियांग के कुछ हिस्सों में चीनी लोगों की तुलना में मीर का अधिक सम्मान हासिल था. जब भारत के विभाजन खतरा सामने आया तब च्यांग काई शेक की तत्कालीन सरकार ने तो उसे चीन में शामिल कराने की कोशिश भी की थी. लेकिन वह प्रस्ताव ठुकरा दिया गया और तब तक पाकिस्तान ने खुद को क्षेत्र में स्थापित भी कर लिया था.
आजादी के बाद, दोस्तों के बीच नए सौदे पर करार
आजादी के बाद, हुंजा पर पाकिस्तानी नियंत्रण काफी हद तक अस्थिर रहा. 1950 के दशक में इसने अपनी सीमांत पुलिस को जल्दबाजी में वापस बुला लिया, क्योंकि यह डर था कि इससे उसका बड़ा पड़ोसी नाराज हो सकता है, जिसके नागरिकों को सीमा के पास रहते देखा जा सकता था. 1959 में, चीनियों ने एक मानचित्र जारी कर हुंजा और गिलगित के 6,000 वर्ग मील इलाके पर दावा जताते हुए इसे अपना क्षेत्र बताया. भारत-चीन के बीच मौजूदा झड़पों की तरह ही इन दावों के साथ क्षेत्र में नियमित तौर पर सैन्य घुसपैठ होती रही.
सशंकित, पाकिस्तान ने चीन को यह समझाने के लिए आक्रामक कूटनीति अपनाई कि अमेरिकी गठबंधन प्रणाली सीटो (दक्षिण पूर्व एशिया संधि संगठन) में उसका शामिल होना केवल भारत से रक्षा के लिए था, इस संदर्भ में संसद में बयान दिए गए कि अगर इस वादे पर अमल नहीं हुआ तो पाकिस्तान यह गठबंधन छोड़ देगा.
इस बीच, चीन भारत के सामने सकारात्मक रूप से अस्पष्ट रुख अपनाए रहा, यहां तक कि चाऊ एन लाई इससे इनकार कर रहे थे कि वह ‘अब तक’ पाकिस्तान के साथ ‘सीमा समझौते’ की कोई रूपरेखा बना रहा है. इस तथ्य के बावजूद कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री मंजूर कादिर सीमांकन पर वार्ता कर रहे थे. जाहिर है, चीनी भारत से रियायतें चाहते थे. जब कुछ कारगर होता नहीं दिखा तो चीन ने भारत के साथ काराकोरम दर्रे से आगे किसी भी क्षेत्र पर चर्चा से इनकार कर दिया. 3 मई 1962 को, चीन ने पाकिस्तान-चीन सीमा पर एक अस्थायी समझौता कर लिया, इस प्रकार पूरब में अपना दावा सुनिश्चित कर लिया. अक्टूबर 1962 तक, चीन भारत के साथ युद्ध छेड़ चुका था.
अंतत: 1963 में पाकिस्तान-चीन सीमा समझौते को अंतिम रूप दिया गया, जिससे घोषित तौर पर हुंजा का 2500 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा इलाका चीन के पास चला गया, इसमें संभवत: उसकी पारंपरिक सीमाएं शामिल नहीं थी जो काराकोरम दर्रे के पास शक्सगाम घाटी तक फैली थीं.
भारत की अपनी स्थिति यह है कि कुल 5,120 किलोमीटर का इलाका पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) में चला गया था. 1987 में आकर हुए इस क्षेत्र के सर्वेक्षण से यह संभावना ज्यादा है कि खुद पाकिस्तान को ही इसका कोई अंदाजा नहीं है कि उसने कितनी जमीन चीन को सौंप दी है.
यह भी पढ़ें :एलएसी संघर्ष को ‘खुफिया विफलता’ कहना गलत है यह भारत की वास्तविक समस्या को नजरअंदाज करता है
1963 की संधि का एक और अजीबो-गरीब पहलू भी है. संधि के अनुच्छेद 6 में यद्यपि यह माना गया है कि कश्मीर पर फैसले के बाद इसे नए सिरे से आबाद करने की जरूरत होगी, लेकिन साथ ही हुंजा और उसके आसपास के क्षेत्र को विवादित हिस्सा कहा गया है, इस रुख से पाकिस्तान पूरी तरह पीछे हट चुका है. वह केवल ‘आजाद कश्मीर’ के एक छोटे से हिस्से पर बात कर रहा है. अक्टूबर 1967 में, चीन और पाकिस्तान के बीच एक अप्रकाशित समझौते से इन मामलों की ‘रणनीतिक’ अहमियत का पता चलता है. इसमें मिंटाका दर्रे से होते हुए सीधे हुंजा तक एक ऑल वेदर रोड पर सहमति जताई गई है. लगता है कि इसी में सुधार करके सीधे गिलगित तक संपर्क मार्ग में बदला गया है. केवल खंजरेब के जरिये काराकोरम राजमार्ग पर ध्यान केंद्रित करके रणनीतिक विशेषज्ञों ने आमतौर पर इस सड़क मार्ग को अनदेखा ही किया है.
सीपीईसी खेल का नया मैदान
चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे (सीपीईसी) के साथ चीनियों के पाकिस्तान के इलाके में कब्जा जमाने की कहानी जारी है, क्योंकि स्थानीय लोगों ने ‘विशेष परियोजनाओं’ के लिए अपनी हजारों एकड़ भूमि के अधिग्रहण, आजीविका पर संकट और गंभीर पर्यावरणीय क्षति होने की शिकायत की है.
इसमें से कुछ भी तब तक नहीं थमेगा जब तक कि बीजिंग को कहीं और, संभवत: दक्षिण चीन सागर में, किसी चुनौती का सामना न करना पड़े. चूंकि अधिकांश देश ‘साम्राज्य’ के निरंतर विस्तार के खिलाफ हैं, ऐसे में चीन के अंदर और बाहर, दोनों में ध्रुवीकरण शुरू होगा. हालांकि, अंतर्निहित सबक यह है: एक गंभीर चुनौती बीजिंग को भले ही क्षेत्रीय विस्तार पर विराम के लिए बाध्य कर दे लेकिन लंबे समय में दशकों से धीमी गति से जारी विस्तारवाद थमेगा नहीं.
भारत कोई और ‘अगला बड़ा कदम’ उठाने से पहले इसे निरंतर खतरे के तौर पर अच्छी तरह पहचानेगा और उसके अनुरूप ही अपनी दीर्घकालिक रक्षा और विदेश नीति तैयार करेगा. इस पर सीमित ध्यान देना, जो शायद जीवंत लोकतंत्र में अपरिहार्य है, समय-समय पर महंगा साबित हुआ है. बेहतर है इस खतरे को हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाए. लेकिन हम इसके लिए चलने वाली एक लंबी और कठिन कवायद पर ही भरोसा कर सकते हैं.
(लेखक राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय की पूर्व निदेशक हैं. विचार निजी हैं.)
(इस लेख को अंग्रेजी में पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)