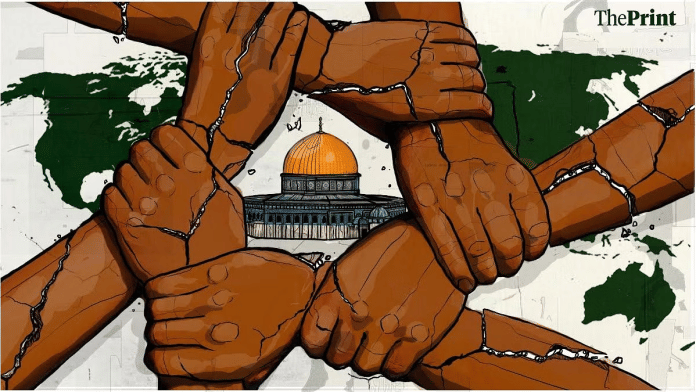इस सप्ताह इस कॉलम में जो मुद्दा उठाने की कोशिश की जा रही है वह गाज़ा में इज़रायली सेना के मौत और विध्वंस के तांडव के संदर्भ में उपयुक्तता की कसौटी पर शायद खरी न उतरे. लेकिन इस मुद्दे को जल्दी-से-जल्दी उठाए जाने की जरूरत है. यह इस कॉलम में अक्तूबर 2020 में कही गई बातों को और आगे बढ़ाती है.
सबसे पहले हम गाज़ा के मामले में सैद्धांतिक पहलू को लें, क्योंकि वहां जो कुछ हो रहा है उस पर बहुत बहस नहीं हो रही है. वहां बदले की, सामूहिक सज़ा देने की क्रूरतम कार्रवाई हो रही है, और यह कार्रवाई एक संप्रभुता संपन्न सत्ता कर रही है जिसके पास पूरे मध्य-पूर्व में सबसे शक्तिशाली सेना है.
हमास ने 7 अक्टूबर को जो किया वह इज़रायलियों और यहूदियों के खिलाफ व्यापक पैमाने पर नफरत में किया गया अपराध (‘हेट क्राइम’) था. लेकिन इज़रायल दुष्ट, आतंकवादी हमास से बदला लेने और उसे सज़ा देने की कार्रवाई जिस पैमाने पर और जिस मनमाने ढंग से कर रहा है वह भी गाज़ा के फिलस्तीनियों और व्यापक अर्थ में मुसलमानों के खिलाफ मुंहतोड़ कार्रवाई और ‘हेट क्राइम’ जैसा ही है. और अब तो इसका उल्टा नतीजा भी सामने आने लगा है. यह इज़रायल के दोस्तों को शर्मसार कर रहा है और उसके आलोचकों को एकजुट कर रहा है.
अमेरिका के अलावा, इज़रायल के लगभग सारे अहम दोस्त देशों ने आवाज़ उठाई है और वे कुल मिलाकर एक तरह की बात कह रहे हैं. उन्होंने संयुक्त राष्ट्र महासभा में युद्ध विराम की मांग करने वाले मतदान में वोट देने से परहेज किया. उनमें भारत भी शामिल है, जो आज इज़रायल और उसके नेता नेतन्याहू के सबसे करीबी दोस्तों में है. लेकिन नेतन्याहू के इज़रायल को इस सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता.
सवाल यह है कि इज़रायल को अगर इस्लामी जगत की ओर से एकजुट चुनौती का सामना करना पड़ता तब क्या वह इतना ही बेपरवाह होता? अगर इस्लामी जगत वास्तव में एक राजनीतिक, अंतरराष्ट्रीय शक्ति होती तो उसमें दुनिया की मौजूदा आबादी का एक एक चौथाई हिस्सा यानी करीब 2 अरब लोग शामिल होते. इसके मुक़ाबले यहूदियों की आबादी मात्र 0.2 फीसदी यानी 1.6 करोड़ है.
क्या मुसलमान कुल मिलाकर गरीब हैं और यहूदी अमीर, इसलिए उनकी ताकत में असंतुलन स्वाभाविक है?
दुनिया की आबादी में मुसलमानों का हिस्सा करीब 25 फीसदी है और दुनिया की जीडीपी में उनका हिस्सा करीब 23 फीसदी है. इसलिए उन्हें नगण्य ताकत नहीं माना जा सकता. और यहूदियों का हिस्सा क्या है? वे दुनियाभर में फैले हुए हैं. और हालांकि वे कई वित्तीय संस्थानों का नेतृत्व कर रहे हैं लेकिन वे खुद को एक राष्ट्र या एक ताकत के रूप में नहीं देखते. न ही वे रहस्यमय तरीके से दुनिया को अपनी मुट्ठी में रखे हुए हैं, जैसा कि कुछ लोग मानते हैं.
वे इज़रायल के यहूदियों से खुद को जोड़ते तो हैं लेकिन आज भी, पश्चिम के कई बड़े शहरों और कैंपसों में— जो दुनिया की दौलत के केंद्र हैं या जहां बड़ी-बड़ी लेन-देन होती हैं— अच्छी-ख़ासी संख्या में यहूदियों ने सड़कों पर आकर इज़रायली हमलों का विरोध किया है. ऐसा हमने किसी मुस्लिम समूह को करते नहीं देखा है.
जिन देशों में मुसलमान बहुमत में हैं उनमें भी जिन्होंने निंदा की है उनकी संख्या उंगलियों पर गिनी जा सकती है. उनमें एक मिस्र है जिसके नेता सीसी के एक बयान को पश्चिमी दुनिया में काफी उद्धृत किया गया और उसका खंडन नहीं किया गया, इसके अलावा यूएई और एक-दो और देश भी हैं.
जरा गौर कीजिए. दुनिया की एक चौथाई आबादी, दुनिया की अर्थव्यवस्था में लगभग इतनी ही भागीदारी, दुनिया में तेल के भंडार का बड़ा हिस्सा, परमाणु शक्ति (पाकिस्तान) समेत काफी मजबूत सैन्य शक्ति और यहूदियों की आबादी से 150 गुना ज्यादा की आबादी वाली ताकत इज़रायल को रोकने में विफल रही है. इज़रायल उसे मनमर्जी रगड़ने में सफल दिख रहा है. यह मैं काफी सावधानी बरतते हुए लिख रहा हूं.
यह भी पढ़ें: इज़रायल गुस्से में है, नेतन्याहू गाज़ा को मिट्टी में मिलाने को तैयार हैं, पर फौजी ताकत की भी कुछ सीमाएं हैं
तब, इस्लामी दुनिया की, जिसे ‘उम्मा’ के नाम से जाना जाता है, क्या ताकत है? शब्दकोश में ‘उम्मा’ का यह अर्थ बताया गया है— ‘मजहब से एक सूत्र में बंधा मुस्लिम समुदाय’, यानी यह कि दुनियाभर के मुसलमान अपनी आस्था के कारण एक अखिल-राष्ट्रीय सत्ता से बंधे हैं. इसके बाद और भी सवाल उठते हैं कि क्या इस्लामी दुनिया जैसी कोई चीज है भी? क्या कोई आस्था, कोई भी आस्था राष्ट्रीय सीमाओं या राष्ट्रीय भावना से ऊंची हो सकती है?
जब हम यह मानने लगे थे कि अब्राहम समझौते के बाद मध्य-पूर्व अमन और सुलह की गहरी नींद में सोने लगा है, तभी वहां फिर से आग सुलगाकर हमास ने वहां के कई विरोधाभासों, और इस्लामी दुनिया से जुड़े सवालों को उभार दिया है.
इस्लाम इसलिए सबसे अलग है कि उसके सिवा दूसरी कोई आस्था अपने भक्तों की निष्ठा, प्रेरणा और प्रतिबद्धता के मामले में खुद को अखिल-राष्ट्रीय सत्ता के रूप में नहीं देखती. ईसाई धर्म में ऐसे किसी ‘उम्मा’ का सपना नहीं देखा जाता. संख्याबल में तीसरे सबसे बड़े, हिंदू धर्म में आपस में चाहे जितनी बहस चलती हो, लेकिन वह सिर्फ इस सवाल पर होती है कि उसका देश भारत ‘हिंदू राष्ट्र’ है या नहीं. यहूदियों का अपना एक ही देश है.
सियासी इस्लाम में सबसे गहरा विरोधाभास (आस्था, और उसकी प्रथाओं तथा रीति-रिवाजों से अलग) इस मान्यता के कारण है कि धार्मिक निष्ठा को राष्ट्रवाद से ऊंचा दर्जा दिया जाना चाहिए. इसके परिणामस्वरूप जन्म लेती है ‘उम्मा’ नामक कपोल कल्पना.
दुनियाभर में मुसलमानों ने पहचान पर आधारित कई अखिल-राष्ट्रीय संगठन बनाए हैं. उनमें सबसे प्रमुख है ‘ओआइसी’ (ऑर्गनाइज़ेशन ऑफ इस्लामिक को-ऑपरेशन), जिसके सदस्य देशों की संख्या 57 है, और पांच देश ‘ऑब्जर्वर’ हैं. वैश्विक जीडीपी में इन देशों का कुल हिस्सा करीब 23 फीसदी का है. किसी साझा इस्लामी मकसद के लिए, एक समूह के तौर पर उनकी उपलब्धियां सिफर हैं.
अफ्रीका और एशिया में अरब लीग और कुछ दूसरे क्षेत्रीय संगठन हैं लेकिन किसी को किसी अखिल इस्लाम मसले पर किसी गिनती में नहीं लिया जाता. लेकिन किसी एर्दोगन या महातिर या ईरानियों को ज्यादा गंभीरता से लिया जाता है.
‘गल्फ को-ऑपरेशन काउंसिल’ (जीसीसी) ही मुस्लिम मुल्कों का एकमात्र प्रभावशाली अखिल-राष्ट्रीय संगठन है, और इस्लामी मुल्कों के इन क्लबों में पश्चिम से सबसे ज्यादा दोस्ती उसकी ही है. इसके दो अहम सदस्य अब्राहम समझौते में शामिल हुए और तीसरा भी शामिल होने जा रहा था कि हमास ने हमला कर दिया. उसके मुक़ाबले में कोई है तो वह है इस्लामी राष्ट्र ईरान.
क़तर हालांकि जीसीसी का सदस्य है, लेकिन भौगोलिक और राजनीतिक दृष्टि से परिधि पर ही स्थित है, और ईरान, अमेरिका तथा पश्चिम जगत के धुर विरोधी तथा राष्ट्रीयता विहीन मुस्लिम ब्रदरहुड तथा हमास जैसे गिरोहों के साथ अपने गहरे रिश्ते को निभाने में लगा है. सीधे-सीधे कहा जाए तो क़तर बस क़तर बनने में ही लगा है.
अगर हम तथाकथित इस्लामी दुनिया के संघर्षों के इतिहास पर नज़र डालें तो पाएंगे कि पिछले 50 वर्षों से वह अपने भीतर ही संघर्षों में उलझा रहा है. हम 1973 को कट-ऑफ वर्ष मानते हैं, क्योंकि उस साल ही कुछ मुस्लिम देशों ने मिलकर एक गैर-मुस्लिम साझा शत्रु के खिलाफ संघर्ष किया था. मिस्र और सीरिया ने योम किप्पुर युद्ध में इज़रायल से मुक़ाबला किया था. वैसे, कहा जा सकता है कि बाथवादी, कथित समाजवादी तानाशाही देश सोवियत संघ के नेतृत्व में ये दोनों देश वास्तव में इस्लामी ताक़तें नहीं थीं. तेल उत्पादक मुस्लिम देश तेल की कीमत बढ़ाने के लिए इस युद्ध में एकजुट हुए थे. यह और बात है कि इस युद्ध ने इज़रायल या उसके सहयोगी अमेरिका को ज्यादा रणनीतिक नुकसान नहीं पहुंचाया लेकिन उन्हें व्यापारिक लाभ जरूर पहुंचाया.
दूसरी ओर, इस ‘दुनिया’ के भीतर हुए सशस्त्र संघर्षों पर नजर डालिए. गाज़ा में महिलाओं और बच्चों समेत मारे गए हजारों मुस्लिम नागरिक से भी ज्यादा हैं. इसके बरअक्स अमेरिका समर्थित सऊदी सेना और यमन के हौदियों के बीच हुए युद्ध को देखिए. ब्रिटेन स्थित ‘केंपेन अगेन्स्ट आर्म्स ट्रेड’ (caat.org.uk) का आंकड़ा बताता है कि इस युद्ध में 3.77 लाख लोग मारे गए, जिनमें डेढ़ लाख की मौत तो युद्ध लड़ते हुए हुई.
सुडान में जारी गृहयुद्ध में पिछले एक दशक में करीब तीन लाख लोग मारे जा चुके हैं. इनके अलावा, इससे पहले उसके दरफुर सूबे में करीब दो लाख लोगों के मारे जाने का आंकड़ा दर्ज किया जा चुका है. सीरिया में गृहयुद्ध में करीब चार लाख मुसलमान मारे जा चुके हैं.
पिछले एक दशक में मुस्लिम दुनिया में 10 लाख से ज्यादा मुसलमान मुसलमानों के हाथों ही मारे गए हैं. इनमें से अमेरिकियों और रूसियों (सीरिया की असद हुकूमत की खातिर) द्वारा इन दोनों युद्धों में से प्रत्येक में मारे गए पांच से सात हजार तक लोगों को बाद कर सकते हैं.
हमें आठ साल चले ईरान-इराक युद्ध, अफगानिस्तान-पाकिस्तान युद्ध, मुजाहिदीन से तालिबान और तालिबान से मुजाहिदीन तक का इतिहास मालूम है. मुस्लिम ‘दुनिया’ के सारे संकट के लिए पश्चिम को दोष देने का फैशन भले रहा हो, हकीकत यही है कि सद्दाम हुसैन के इराक ने ही पहले कुवैत पर धावा किया था, इस्लामी ताकतों ने ही अमेरिका से गुहार लगाई थी कि वह आकर उसे मुक्त कराए. उस युद्ध की खबरें दे रहे पत्रकार दल में एक क्रूर चुटकुला चलता था— सऊदी और सहयोगी मुस्लिम देशों की सेनाओं (पाकिस्तान के कुछ तत्वों समेत) का गान क्या हो? ‘बढ़े चलो ईसाई सैनिक!’
200 करोड़ की आबादी वाला यह ताकतवर समुदाय अपनी ताकत से कम ज़ोर से हमला करता है, तो इसकी एक मुख्य वजह यह है कि वह खुद कई विरोधाभासों और आपसी संघर्षों से जूझता रहता है. उनमें सबसे आत्मघाती यह है कि वह इस हकीकत को कबूल करने में विफल रहा है कि राष्ट्रवाद, और प्रायः विचारधारा भी मजहब की सीमा-पार निष्ठाओं और साझेपन से कहीं ज्यादा मजबूत भावनाएं होती हैं. आस्था पर आधारित एकता के इस धोखे का एक बार फिर पर्दाफाश इस तथ्य से हो गया है कि मुस्लिम दुनिया गाज़ा युद्ध में इज़रायल की कार्रवाइयों पर लगाम लगाने में विफल रही है. नेतन्याहू हो या कोई भी इज़रायली नेता हो, वह हमेशा इस सुरक्षित पूर्वानुमान के आधार पर कार्रवाई करता है.
(संपादनः ऋषभ राज)
(नेशनल इंट्रेस्ट को अंग्रेज़ी में पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें.)
यह भी पढ़ें: क्रिकेट, क्लब और देश— खेल के मैदान पर राष्ट्रवाद की होड़ क्यों नरम पड़ रही है