आम राय तो यही है कि तीन राज्यों में भाजपा की सरकारें जिन आर्थिक मसलों के कारण चुनाव हार गईं वे थे- किसानों का असंतोष, और बेरोज़गारी. बेशक दोनों मुद्दे आपस में जुड़े हैं. अगर युवाओं को दफ्तरों और कारखानों में नौकरी मिल जाए तो उन्हें अपना परिवार चलाने लायक आमदनी होने लगेगी और गैरफायदेमंद खेतीबाड़ी करने कम ही लोग जाएंगे. लेकिन कारखानों में नौकरी बमुश्किल मिलती है, और दफ्तरों में अंग्रेज़ी भाषी ऊंची जातियों का एकाधिकार है.
अगर आप गांव छोड़कर शहर आ जाएं तो वहां का जीवन और कठिन है. शहर में आकर गांववाले कंस्ट्रक्सन साइट पर मज़दूरी करने लगते हैं. उनमें से अनुभवी और हुनरमंद लोग राजमिस्तरी, फिटर, बढ़ई और एलेक्ट्रिशियन का काम करने लगते हैं. कई तो बेहद मामूली तनख्वाह पर पहरेदार या ड्राइवर का काम करने लगते हैं. उनकी पत्नियां गांव में रह जाती हैं या शहर में घरेलू नौकरानी का काम पकड़ लेती हैं. पुरुष एक कमरे वाली खोलियों में रहने लगते हैं, बस भाड़ा ज़्यादा होने के कारण पैदल चलकर काम पर जाते हैं, और परिवार को पैसे भेजने के लिए अपने ऊपर बहुत कम खर्च करते हैं.
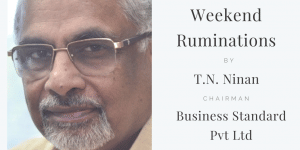
कभी-कभी वे अपने मालिक से या आपस में मिलकर शुरू की गई किट्टी से उधार लेते हैं ताकि परिवार में शादी के लिए पैसे जुटाने के वास्ते ज़मीन बंधक रखकर लिये गए कर्ज़ का भुगतान कर सकें या फिर शहर की किसी झुग्गी बस्ती में एकाध कमरा बनवा सकें. यह कमरा भी किस्तों में बनता है— पहले मिट्टी की दीवार की जगह ईंट की दीवार बनती है, फिर दो साल बाद एस्बेस्टस या टिन की छत की जगह पक्की छत बनती है, और बहुत बाद में कायदे का फर्श बन पाता है. यह सब होने में एक दशक तक बीत जाता है, जबकि कर्ज़ का मासिक किस्तों में भुगतान चलता रहता है. इतनी कवायद के बावजूद जमा पूंजी गांव में नहीं बल्कि शहर में ही इकट्ठा हो पाती है.
यह भी पढ़ें: मोदी जी , वाजपेयी सरकार की आर्थिक गलतियों को न दोहराएं
इनमें से कुछ ऐसे भाग्यशाली भी होते हैं, जो अपने बच्चों को ऐसी शिक्षा या हुनर सिखा पाते हैं कि वह एक-दो सीढ़ी ऊपर के रोज़गार की तलाश कर सके, मसलन कार मेकेनिक, होटल के हाउसकीपिंग स्टाफ या डेलीवरी ब्वाय या किसी के गोफर जैसे काम की. लड़कियां दुकान के काउंटर के पीछे खड़ी होकर काम कर सकती हैं या बूटिक आदि में. इन सबसे ज़्यादा की आकांक्षा निराशा को जन्म देती है क्योंकि वे बढ़िया अंग्रेज़ी नहीं बोल सकते.
वे प्रायः अपने मालिकों की दया पर निर्भर रहते हैं. न तो उन्हें रोज़गार की सुरक्षा हासिल होती है, न मेडिकल सुरक्षा. सरकार ने जो न्यूनतम वेतन तय किया है वह प्रायः सपना ही बना रहता है. उनका जीवन, जैसा कि हॉब्स कह गए हैं, ‘एकाकी, बदहाल, क्रूर और प्रायः छोटा’ होता है. इसलिए कोई भी सरकारी नौकरी किसी खुले बाज़ार के रोज़गार से बेहतर है क्योंकि उसमें वेतन अच्छा है, आप तंत्र के हिस्से हैं, और आपके लिए पेंशन भी है. लेकिन सरकार ने भी गड़बड़ शुरू कर दी है. वह ठेके पर काम करवाने लगी है या अस्थायी कर्मचारी रख रही है, जो वर्षों तक अस्थायी ही बने रहते हैं.
यह भी पढ़ें: चीन पर लगाम कसना कितना मुमकिन है?
इस कड़वी सच्चाई में फंसकर आप उम्मीद से भरकर उस नेता का मुंह ताकने लगते हैं, जो सब कुछ बदल डालने के वादे करता है— हर साल एक करोड़ नई नौकरियों देने का, जिसके लिए किसी नियोक्ता से परिचय बताने या किसी के पैर छूने की ज़रूरत नहीं होगी; उन सब भ्रष्ट लोगों को सज़ा देने का, जिन्होंने इस तरह की व्यवस्था बना रखी है. लेकिन पांच साल बाद वह कड़वी सच्चाई लगभग जस की तस कायम है. अब अगर कोई नौकरी में आरक्षण, खासकर जाति के आधार पर, के लिए आंदोलन शुरू करता है, तो आप इस उम्मीद में रैली या जुलूस में शामिल होते है कि कुछ तो बदलाव आएगा. अगर कोई पार्टी आपका कर्ज़ माफ करने का वादा करती है, तो उसे आपका वोट मिलता है. लेकिन आपके पास अभी भी गैरफायदेमंद खेत है और इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि फसल की अच्छी कीमत मिलेगी. और आरक्षण के बावजूद नौकरियां नदारद हैं.
बर्ट्रेण्ड रसेल ने कहा है कि अधिकतर लोग चुपचाप निराशा का जीवन जीते हैं. लेकिन युवा लोग तो हार नहीं मानना चाहते. तो फिर, कैथरीन बू ने जिसे ‘अंडर-सिटी’ कहा है, जिसके लिए ‘ओवर-सिटी’ वाली सुविधाएं और खुशियां एक न पार हो सकने वाली खाई के पार रहती हैं, उस ‘अंडर-सिटी’ में रहते हुए आप क्या करेंगे? सामूहिक पहचान आपके जीवन को ज़्यादा अर्थपूर्ण बना सकती है. सो, आप राजनीति की दुनिया की परिधि में दाखिल होते हैं.
शायद आप उस गिरोह में शामिल हो जाते हैं, जो मवेशियों के व्यापारियों की टोह में लगा रहता है, क्योंकि इसे धार्मिक स्वीकृति भी हासिल है और जब्त की गई मवेशी से पैसे बनाने की सुविधा भी, और किसी को पीट कर अपनी भड़ास निकालने का सुख भी. हम उन लोगों पर दोष मढ़ सकते हैं, लेकिन हमारी राजनीति उन्हें क्या दे रही है? इसलिए हमारे पल्ले जो हासिल होता है उसे स्वामीनाथन अय्यर ने ‘नई दिल्ली की आम सहमति’ कहा है, और वह है— सबसिडी और अनुदान की रेवड़ी, इस उम्मीद में इनसे वोट खरीदे जा सकेंगे और लोगों को शांत रखा जा सकेगा. कठोर सच यही है कि भारत की राजनीतिक अर्थनीति के पास दर्दनिवारक गोलियां तो हैं, सही इलाज़ नहीं.
‘बिज़नेस स्टैंडर्ड’ के साथ विशेष व्यवस्था के अंतर्गत
इस लेख को अंग्रेजी में पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें.

