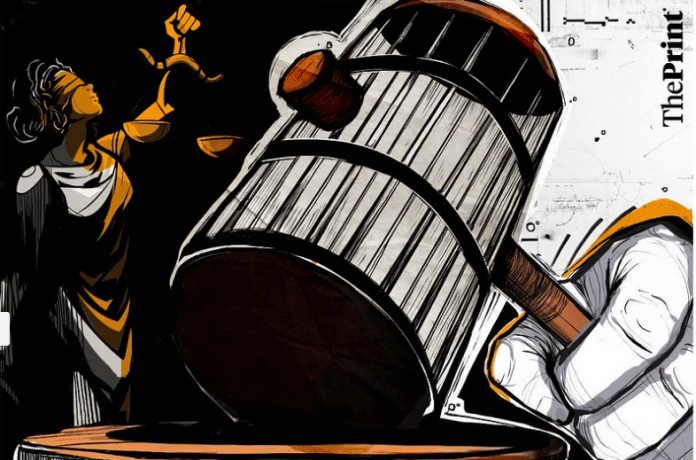बहस के लिए एक मुद्दा पेश है—पिछले करीब 15 वर्षों में ट्रायल कोर्ट (निचली अदालतों) से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक हमारी न्यायपालिका ने बेशक तरक्की की है, अगर आप उसे तरक्की मानें. इस बीच वह सुधारवादी संस्था से दंड देने वाली संस्था में तब्दील हो गई है.
ऐसा हम इस तथ्य के आधार पर कह रहे हैं कि 2022 में भारत की निचली अदालतों ने 165 व्यक्तियों को फांसी की सज़ा सुनाई है, जो वर्ष 2000 के बाद से एक साल में ऐसी सबसे बड़ी संख्या है. इसे मिलाकर फांसी की सज़ा पाने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या 539 हो गई है. अपूर्वा मंधानी की शोधपरक मगर चिंताजनक रिपोर्ट बताती है कि 17 वर्षों में यह सबसे बड़ी संख्या है. हम जानते हैं कि इनमें से ज़्यादातर की यह सज़ा कम कर दी जाएगी और कुछ को बरी कर दिया जाएगा. 2000 के बाद से कुल आठ सज़ायाफ़्ताओं को फांसी दी गई है.इनमें से चार ‘निर्भया बलात्कार एवं हत्याकांड’ के अपराधी थे. आखिर क्या वजह है कि हमारी निचली अदालतें यह अंतिम न्यायिक कदम उठा रही हैं?
अब निचली अदालत से हम देश की उच्चतम अदालत पर आते हैं. फांसी की सज़ा में बढ़ोतरी की इस लहर को इसके सबसे ताज़ा फैसले के संदर्भ में देखें, जिसमें उसने 2011 में ‘यूएपीए’ नाम के भयानक कानून पर अपने फैसले को लगभग बेमानी कर दिया है. जस्टिस एम.आर. शाह, जस्टिस सी.टी. रविकुमार और जस्टिस संजय करोल की तीन सदस्यीय बेंच ने सुप्रीम कोर्ट के पिछले तीन फैसलों को पलट दिया जिन्होंने इस सिद्धांत की पुष्टि की थी कि किसी प्रतिबंधित संगठन की सदस्यता को ही यूएपीए के तहत अपराध नहीं माना जाएगा, कि इस कानून के तहत किसी ऐसे सदस्य पर तभी आरोप लगाया जाएगा जब उसने प्रतिबंधित संगठन की किसी गतिविधि में सक्रिय भागीदारी की हो.
ताजा फैसले ने इस सिद्धांत को पूरी तरह कमजोर कर दिया है और पुलिस तथा जांच एजेंसियों को यह अधिकार दे दिया है कि किसी को किसी प्रतिबंधित संगठन से जुड़े होने के शक पर भी गिरफ्तार कर सकती हैं. और जब किसी व्यक्ति को सदस्यता के महज संदेह पर ही गिरफ्तार कर लिया जाता है तो इसके बाद उसके खिलाफ यूएपीए कानून पूरी तरह से लागू किया जा सकता है. यह कानून इतना सख़्त है कि यह खुद को बेकसूर साबित करने का जिम्मा आरोपी व्यक्ति पर डाल देता है और उसके लिए जमानत हासिल करना लगभग असंभव बना देता है. यह केवल जुड़ाव के शक पर ही किसी को दोषी बना देता है.
निर्दोष साबित करने की ज़िम्मेदारी आरोपी पर डाल देने का अर्थ इस सिद्धांत को बेमानी बना देना है कि ‘जब तक आप दोषी सिद्ध नहीं किए जाते तब तक आप निर्दोष हैं’. यह इसके बिलकुल उलट है— आपके ऊपर आरोप लगाकर आपको दोषी बता दिया गया, अब आप तभी निर्दोष माने जाएंगे जब आप जजों को यह नहीं विश्वास दिला देते कि आप निर्दोष हैं.
अफसोस की बात है कि यह कोई अकेला मामला नहीं है. पिछले कई वर्षों में हम उच्चतम अदालत को इसी दिशा में बढ़ते देख रहे हैं. कई क़ानूनों को, खासकर यूएपीए जैसे कुछ सख्त क़ानूनों को प्रतिवादी के लिए न्यायोचित बनाने की जगह अपेक्षा के विपरीत और सख्त बनाया गया है.
या कम-से-कम उदारवादी अपेक्षा के विपरीत, जबकि उच्चतम अदालत उदारवादी सिद्धांतों की, जिसे वर्तमान मुख्य न्यायाधीश ने सही ही ‘ध्रुवतारा’ (सबसे चमकता सितारा) कहा है, पक्षधर होने का दम भरती है. यूएपीए मामले पर ताजा फैसले के साथ-साथ, ‘एफसीआरए’ (विदेश से प्राप्त चंदे के नियमन से संबंधित) और ‘पीएमएलए’ (मनी लॉन्डरिंग रोकने से संबंधित) नाम के कानूनों को सत्तातंत्र के पक्ष में और अधिक सख्त बनाने के जो फैसले इसी अदालत के जाने-माने जजों ने दिए हैं वे इस सैद्धांतिक नजरिए से किस तरह मेल खाते हैं?
यह भी पढ़ेंः पूर्वोत्तर में सफलता बीजेपी की ही नहीं, भारत की भी कामयाबी की कहानी है
हम कुछ खास उदाहरणों पर भी नज़र डाल सकते हैं.
दिल्ली हाइकोर्ट ने यूएपीए के मामले में 2021 में स्वाधीनता को कड़ा झटका दिया. सीएए (नये नागरिकता कानून) के खिलाफ दिल्ली में हुए आंदोलन के मामले में देवांगना कालिता, नताशा नरवाल और आसिफ इक़बाल तन्हा को जमानत देते हुए जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल और जस्टिस अनूप जे. भंभानी ने फैसला दिया था कि यूएपीए को केवल उन्हीं मामलों में लागू किया जा सकता है जिन्हें बिलकुल आतंकवादी कार्रवाई के रूप में परिभाषित किया जाता हो. इस बेंच ने ‘आतंकवादी कार्रवाई’ नामक मुहावरे के लापरवाह इस्तेमाल के खिलाफ चेतावनी दी, और कहा था कि इसकी परिभाषा व्यापक और अस्पष्ट है.
इस फैसले के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया लेकिन गनीमत है कि उसने जमानत रद्द नहीं की मगर फैसले को स्थगित कर दिया. इसका नतीजा यह हुआ कि इस फैसले को आगे ऐसे मामलों पर लागू नहीं किया जाएगा. जुलाई 2022 में, जस्टिस ए.एम. खानविलकर की अध्यक्षता वाली दो जजों की बेंच ने तब एक नया ही न्यायिक सिद्धांत तय कर दिया जब उसने दंतेवाड़ा में आदिवासियों की के संहार की सीबीआइ जांच की मांग करने वाले एक याचिकाकर्ता पर जुर्माना ठोक दिया. उस याचिकाकर्ता का कहना था कि ये हत्याएं गैर-कानूनी हैं. अदालत ने पुलिस का यह तर्क मान लिया कि ये हत्याएं नक्सलियों द्वारा की की गईं. उसने याचिकाकर्ता हिमांशु कुमार पर न केवल जुर्माना ठोका बल्कि केंद्र सरकार की इस मांग की यह मांग भी मान ली कि उसकी एजेंसियों को उलटे याचिकाकर्ताओं की ही जांच करने की अनुमति दी जाए. अदालत ने यह भी कहा कि ‘जांच केवल इस बात की ही नहीं की जाए कि झूठे सबूत पेश किए गए बल्कि उनके खिलाफ आपराधिक साजिश समेत आइपीसी के तहत किसी दूसरे अपराध का आरोप भी लगाया जाए’.
हम और पीछे का भी उदाहरण ले सकते हैं. 2016 में, जस्टिस रंजन गोगोई (जब वे मुख्य न्यायाधीश नहीं थे) की अध्यक्षता वाली एक बेंच ने एक काबिले गौर आदेश सुनाया जिसने कम-से-कम एक महत्वपूर्ण दृष्टि से सरकारी और निजी बैंकों के बीच फर्क को खत्म कर दिया था. जस्टिस पी.सी. पंत के साथ जस्टिस गोगोई ने भ्रष्टाचार रोकथाम कानून (पीसीए) के तहत सरकारी कर्मचारी की परिभाषा का विस्तार कर दिया.
उसने कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक के लाइसेंस के तहत काम कर रहे निजी बैंक के कर्मचारी को सरकारी कर्मचारी माना जाएगा. इस प्रकार, उन्होंने तब तक जिन्हें शुद्ध रूप से निजी व्यवसाय माना जा रहा था उन्हें सरकार और सीबीआई के दायरे में ला दिया. यूएपीए मामले में जमानत देने के दिल्ली हाइकोर्ट के आदेश की तरह जब-तब हम अदालतों की ओर से ताजा बयार भी महसूस करते रहे हैं. उदाहरण के लिए, राजस्थान हाइकोर्ट के जस्टिस पंकज भण्डारी और जस्टिस समीर जैन की बेंच ने इस हफ्ते ही एक ऐसा फैसला सुनाया जिसने इस कॉलम के लिए इस सप्ताह मुद्दा दे दिया.
इस बेंच ने उन चार आरोपियों को फांसी के तख्ते पर जाने से बचा लिया जिन्हें मई 2008 में जयपुर में 71 लोगों की जान लेने और कई लोगों को घायल करने वाले सीरियल बम धमाकों में सज़ा सुनाई गई थी. वे चारों 15 साल से फांसी दिए जाने का इंतजार कर रहे थे. उन सबको दिल्ली में बाटला हाउस मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया गया था और शक था कि वे ‘इंडियन मुजाहिदीन’ नाम के एक गुट के साथ थे जिसने जयपुर बमकांड करने का दावा किया था. जजों ने उन्हें माफी देते हुए अपने आदेश में कहा कि ‘यह संस्थागत विफलता का उदाहरण है जिसके कारण जांच ढीली/कमजोर/घटिया हुई.’
इन चारों के साथ हुई नाइंसाफी ने जजों के जमीर को झकझोर दिया और उन्होंने पुलिस के मशहूर पूर्व आला अधिकारी प्रकाश सिंह के मामले में सुप्रीम कोर्ट के 2006 के फैसले का हवाला दिया. पुलिस सुधारों के लिए मुहिम चला रहे प्रकाश सिंह ने इस तरह की लापरवाही और नाइंसाफी से निबटने के लिए ‘पुलिस कन्प्लेंट्स ऑथरिटी’ (पीसीए) के गठन की जरूरत पर ज़ोर दिया था. राजस्थान हाइकोर्ट का यह फैसला झकझोर देने वाला है. इसकी तारीफ करते हुए उस कानून को याद करना जरूरी है जिसने उन पुलिसवालों को ज्यादती करके न केवल बच निकलने बल्कि इन चारों को निचली अदालत से सजा दिलवाने में भी मदद की.
जैसा कि हम पहले बता चुके हैं, आश्चर्य नहीं कि यह यूएपीए कानून ही है जिसमें वादी को नहीं बल्कि आरोपी पर ही खुद को निर्दोष साबित करने की ज़िम्मेदारी डाली गई है. और इसी कानून को सुप्रीम कोर्ट ने मजबूत बनाने का काम अभी-अभी किया है. दो परस्पर विरोधी आदेश एक ही सप्ताह में आए हैं— एक, राजस्थान हाइकोर्ट का आदेश है जिसमें इस भयानक कानून के खतरों को उजागर किया गया है; और दूसरा, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है जिसमें इस कानून को और मजबूत किया गया है.
यह भी पढ़ेंः खालिस्तान की मांग करता अमृतपाल क्यों सिर उठा रहा है और सरकार क्यों सरेंडर कर रही है?
भारतीय न्यायपालिका के एक रुझान को समझना और उसे पुष्ट करने के लिए प्रमाणों को तलाशना हमेशा से एक चुनौती रही है. इसकी एक वजह यह है कि टॉप जजों, खासकर भारत के मुख्य न्यायाधीशों का कार्यकाल छोटा होता है. यह सिविल और सैन्य सेवाओं के शीर्ष पदों या चुनाव आयोग, सीएजी, सेबी, कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया सीसीआई जैसे दूसरे संस्थानों के निश्चित कार्यकाल वाले प्रमुख पदों के मामलों के विपरीत है.
दूसरे, चूंकि वे अपनी नियुक्तियां खुद करते हैं इसलिए आप इसे निर्वाचित सरकारों या विचारधारा पर आधारित सरकारों में होने वाले परिवर्तनों से (जैसे अमेरिका में होता है) नहीं जोड़ सकते. तीसरी वजह यह है कि हमारे सिविल अधिकारियों की तरह हमारे जजों का केरियर एक स्पष्ट दिशा में नहीं चलता और न ही उन्हें मतदाताओं या समर्थकों के द्वारा बार-बार आकलन से नहीं गुजरना पड़ता. उनका आकलन और मूल्यांकन सिर्फ उनके द्वारा किए जाने वाले फैसलों से ही किया जा सकता है. न सार्वजनिक भाषणों के आधार पर और न सूक्तियों के आधार पर. ताजा प्रमाण यह है कि वे सुधारवादी सिद्धांत की जगह दंड देने के सिद्धांत की ओर साफ तौर पर मुड़ गए हैं.
(यह कॉलम लिखने में मदद के लिए लेखक अपनी सहकर्मी भद्रा सिन्हा का आभारी है)
व्यक्त विचार निजी हैं.
(इस लेख को अंग्रेजी में पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)
यह भी पढ़ेंः भारत का दोस्त कौन, दुश्मन कौन? मोदी सरकार अपनी बनाई अमेरिका-चीन-रूस-पाकिस्तान की जलेबी में उलझी