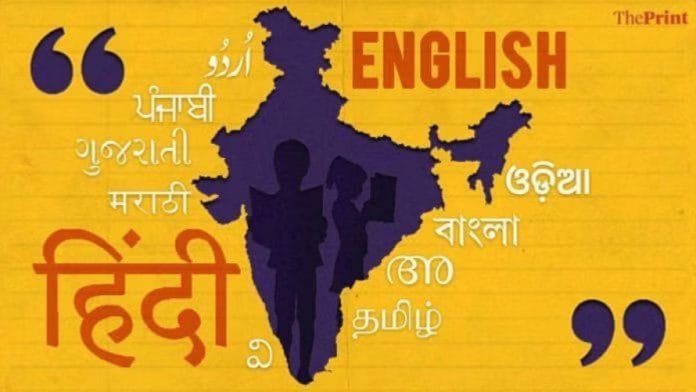भारतीय बुद्धिजीवी—खासकर हिंदू—लगातार किसी न किसी बहस में उलझे रहते हैं, लेकिन किसी समस्या को हल करने की फिक्र नहीं करते. कई मुद्दों पर तो दशकों से वही पुराने तर्क दोहराए जा रहे हैं, जबकि हालात ज्यों के त्यों बने हुए हैं या और भी बिगड़ते जा रहे हैं. भारत की भाषा नीति भी ऐसा ही एक मुद्दा है.
अभी ज़्यादातर बहसें ठाकरे भाइयों की आलोचना पर केंद्रित हैं. कुछ हफ्ते पहले तक निशाना तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम. के. स्टालिन थे. इस बीच भारत की भाषा नीति को लेकर गंभीरता से सोचने की ज़रूरत किसी ने नहीं समझी कि इसका मकसद क्या था और असल में क्या हासिल हुआ.
ठाकरे भाई तो राजनीति में नए और एक राज्य तक सीमित नेता हैं. मगर उनकी मौजूदगी से पहले के दौर का क्या? सच यह है कि आज़ाद भारत की भाषा नीति शुरू से ही बिना दिशा वाली नाव की तरह रही है. नीतियों के घोषित उद्देश्यों और असली नतीजों का कभी मेल नहीं रहा. कागज़ों पर हिंदी ‘राजभाषा’ है, लेकिन असल में अंग्रेज़ी का वर्चस्व हर क्षेत्र में लगातार बढ़ता गया है. यह किसी गैर-हिंदी नेता की वजह से नहीं हुआ, बल्कि आज़ादी के बाद से चली आ रही अधूरी और कमजोर नीतियों का नतीजा है.
नीति निर्माताओं की गलती
सच्चाई यह है कि हिंदी समेत सभी भारतीय भाषाओं को धीरे-धीरे अंग्रेज़ी से जो नुकसान हुआ है, उसकी वजह न तो तमिल राजनीति है और न ही मराठी राजनीति. इस सबसे ज़रूरी सच पर बहुत कम लोगों का ध्यान जाता है. संविधान बनने के समय से अब तक भाषा से जुड़े हर बड़े फैसले हिंदी भाषी नेताओं के नेतृत्व में ही लिए गए हैं, लेकिन वह एक भी ऐसी ठोस नीति नहीं बना सके, जिससे उनकी मंशा पूरी हो पाती. हैरानी की बात यह है कि इन नीतियों का कभी यह जांचा ही नहीं गया कि असल में उनके नतीजे क्या निकले.
दिलचस्प बात यह भी है कि अंग्रेज़ों के शासनकाल में भारतीय भाषाएं, जिनमें हिंदी भी शामिल है, खूब फली-फूली थीं. उस दौर में कई मशहूर कवि, लेखक, विद्वान, विचारक और वैज्ञानिक सामने आए, जिन्होंने अलग-अलग भारतीय भाषाओं में काम किया. आज़ादी के बाद यह सिलसिला पहले धीमा हुआ और फिर उल्टा चलने लगा. आज मौजूद सभी आंकड़े यही दिखाते हैं. दरअसल, भारतीय भाषाओं के गिरते स्तर की जड़ आज़ाद भारत की भाषा नीति में ही है. शुरुआत से ही ये नीतियां उलझी हुई और भ्रमित करने वाली रही हैं. किसी एक नेता या पार्टी को दोष देना बेकार है. पूरा राजनीतिक और बौद्धिक वर्ग इस गड़बड़ी का जिम्मेदार भी है और उसी का शिकार भी. सबसे बड़ी बात यह है कि न तो उनमें इसे सुधारने की काबिलियत है, न ही कोई ईमानदार कोशिश दिखती है.
जैसे खाने का असली स्वाद उसे चखने से ही पता चलता है, वैसे ही किसी नीति का असली असर उसके नतीजों से ही मापा जाता है. आज भारत के छोटे-छोटे शहरों तक में अंग्रेज़ी ही तरक्की की भाषा बन चुकी है—चाहे वह अच्छी पढ़ाई हो, नौकरी हो या कारोबार. जो लोग अंग्रेज़ी नहीं जानते, वे कर्मचारी या प्रशासनिक कामों तक ही सीमित रह जाते हैं, लेकिन अगर कोई व्यक्ति अपनी सोचने-समझने और रचनात्मक क्षमता को बढ़ाना चाहता है, जो हर इंसान की बुनियादी ख्वाहिश होती है, तो अंग्रेज़ी के बिना वह एक दीवार से टकरा जाता है. इसके उलट, जो व्यक्ति अंग्रेज़ी में धाराप्रवाह है और अगर वह किसी भारतीय भाषा में एक वाक्य भी न लिख सके, इससे करियर में कोई रुकावट नहीं आती. ऐसी स्थिति दुनिया के किसी विकसित देश में नहीं है, जहां अपनी मातृभाषा का ज्ञान तरक्की के लिए बेमतलब हो.
असल में, भारत की असली सरकारी भाषा अंग्रेज़ी है. हिंदी को ‘राजभाषा’ कहना ज़्यादातर राजनीतिक वजहों से किया जाता है और यह एक महंगा तमाशा बन चुका है. हिंदी को मिला यही दिखावटी (और बेकार) सम्मान तमिल, मराठी और दूसरी भाषाओं के नेताओं को अक्सर नाराज़ करता है, जब हिंदी थोपने की बात आती है. इस तरह हिंदी एक अजीब और अनुचित दोहरी परेशानी का शिकार बन जाती है—एक तरफ दिखावटी सम्मान, दूसरी तरफ विरोध और अपमान.
इसके मुकाबले, ब्रिटिश राज की भाषा नीति कहीं ज़्यादा साफ और व्यवहारिक थी. अंग्रेज़ों ने अंग्रेज़ी को सिर्फ शासन की भाषा रखा—वह भी केवल अपने प्रशासनिक कामकाज के लिए। शिक्षा और संस्कृति के बड़े क्षेत्र पूरी तरह समाज के हाथ में छोड़ दिए गए, जहां सरकार का कोई सीधा दखल नहीं था. हर क्षेत्र में स्थानीय भाषाओं के जानकारों ने अपने-अपने इलाके के लिए पाठ्यक्रम और पढ़ाई की किताबें तय कीं. अंग्रेज़ों ने कभी भी कोई केंद्रीय ‘शिक्षा नीति’ नहीं बनाई, न ही पूरे देश के लिए एक जैसे पाठ्यक्रम या किताबें लागू कीं. (आलोचक बार-बार मैकॉले के 1835 वाले नोट का हवाला देते हैं, लेकिन यह भूल जाते हैं कि वह सिर्फ एक असहमति जताने वाला दस्तावेज़ था, कोई आधिकारिक नीति नहीं। कोई यह सवाल नहीं उठाता कि उसके बाद के 112 सालों में क्या हुआ!)
असल में, उस दौर में शिक्षा, साहित्य और सांस्कृतिक गतिविधियों की ज़िम्मेदारी समाज के हाथ में थी. समाज के प्रयासों को ज्यादा आज़ादी मिली थी. इसी वजह से ब्रिटिश शासन के समय भारतीय भाषाएं साहित्य और सांस्कृतिक गतिविधियों में खूब फली-फूलीं क्योंकि यह क्षेत्र सच में समाज के नियंत्रण में था, सरकार के नहीं.
लेकिन आज़ादी के बाद हालात बदलने लगे. समाजवादी सोच वाली सरकार ने धीरे-धीरे समाज के कई क्षेत्रों को अपने दायरे में ले लिया.
1947 के बाद बनाई गई नीतियों का नतीजा यह हुआ कि हिंदी एक उपेक्षित पटरानी बनकर रह गई—जिसे राजा (सरकार) भी नहीं पूछता, लेकिन दूसरी रानियां (अन्य भाषाएं) रोज़ ताना मारती हैं, नाराज़ होती हैं, मज़ाक उड़ाती हैं. अब इस बेचारी पटरानी के पास भी कोई रास्ता नहीं है, बस चुपचाप सब सहने के अलावा. क्या ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसे इस झूठे ‘मुख्य रानी’ (राजभाषा) के ताज से आज़ाद कर दिया जाए और सभी रानियों के बीच एक समान दर्जा दे दिया जाए? कम से कम तब तो बाकी भाषाएं उसे अपनापन और बहनापा दे सकेंगी.
इसलिए ईमानदारी और भलाई इसी में है कि हिंदी को इस झूठे ‘राजभाषा’ के सम्मान से मुक्त कर दिया जाए. धीरे-धीरे, हिंदी खुद अपनी सही जगह पा लेगी. फिर उसे गैर-हिंदी नेताओं और बुद्धिजीवियों के निशाने पर भी नहीं रहना पड़ेगा और शायद वह वही अपनापन दोबारा पा सकेगी, जो उसे ब्रिटिश दौर में मिला था.
अंग्रेज़ी और हिंदी के बीच की खाई
याद रखने वाली बात है कि अंग्रेज़ी शासन के समय, हिंदी को राष्ट्रीय कामकाज की भाषा बनाने की कोशिशें ज़्यादातर गैर-हिंदी नेताओं और बुद्धिजीवियों ने ही की थीं—जैसे एम. के. गांधी, सी. राजगोपालाचारी, के. एम. मुंशी, रवींद्रनाथ ठाकुर और अन्य. वे हिंदी की ताकत और उपयोगिता को समझते थे. मगर उस वक्त हिंदी, तमिल या कन्नड़ जैसी बाकी भारतीय भाषाओं की तरह बस एक भाषा थी. अंग्रेज़ी ही अकेली प्रशासनिक भाषा थी. वर्तमान ज़मीनी हकीकत के लिहाज़ से भी यही बेहतर होगा कि हिंदी को बाकी भारतीय भाषाओं के साथ बराबरी का दर्जा दिया जाए.
यह कदम व्यावहारिक भी होगा और देशहित में भी. अंग्रेज़ी अब भी प्रशासन, शिक्षा और उद्योग-धंधों में बेधड़क हावी है. यह असर सरकार की तमाम घोषणाओं में भी दिखता है. आप खुद देखिए 1963 और 1976 के आधिकारिक भाषा कानून और नियम, फिर 1986, 2007 और 2011 के संशोधन भी यही दिखाते हैं कि हिंदी को असली प्रशासनिक भाषा बनाने में कोई खास प्रगति नहीं हुई. पिछले सात दशकों में अंग्रेज़ी और हिंदी के बीच की खाई लगातार बढ़ती गई है.
अगर हिंदी को बाकी भारतीय भाषाओं के साथ बराबरी पर रखा जाए, तो उस झूठी ‘राजभाषा’ की छवि बनाए रखने में बर्बाद हो रही भारी-भरकम रकम, समय और ऊर्जा की भी बचत होगी. हर जागरूक कर्मचारी या छात्र अच्छी तरह जानता है कि किसी भी सरकारी दस्तावेज़, नियम, आदेश या किताब को सचमुच समझना हो, तो अंग्रेज़ी संस्करण ही देखना पड़ता है. हिंदी अनुवाद अक्सर इतने उलझे हुए या गलत होते हैं कि समझने की बजाय और कन्फ्यूजन बढ़ाते हैं. असल में, ये अनुवाद इतनी लापरवाही से किए जाते हैं क्योंकि किसी को उनकी परवाह ही नहीं होती—यह सब बस रस्म निभाने जैसा होता है. (यह बात और है कि दुनिया के बाकी देशों में शानदार अनुवाद रोज़मर्रा में तमाम भाषाओं में होते रहते हैं.)
आज हालात यह हैं कि पढ़ाई-लिखाई, गंभीर शोध और उच्च गुणवत्ता वाली किताबें—सभी कुछ सिर्फ अंग्रेज़ी में ही उपलब्ध हैं. दूसरी तरफ, एक भी ऐसी हिंदी साहित्यिक पत्रिका नहीं बची है, जिसे पूरे देश में पढ़ा जाता हो या जिसकी कोई बड़ी पहचान हो, जबकि ब्रिटिश राज के समय और आज़ादी के कुछ दशक बाद तक कई हिंदी पत्रिकाएं राष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रिय थीं और प्रभावशाली मानी जाती थीं. अब वे सभी गायब हो चुकी हैं, जबकि हिंदी भाषी लोगों की संख्या, उनकी शिक्षा और आमदनी तीनों काफी बढ़ चुकी हैं.
यह एक सीधी-सी बात साबित करता है जिस चीज़ की मांग कम होती है या खत्म हो जाती है, उसका उत्पादन और कारोबार भी खत्म हो जाता है. शिक्षा, विचार और संस्कृति के क्षेत्र में यह बदलाव कभी भी बिना सरकार की मदद वाली नीतियों के संभव नहीं होता.
इसलिए बेहतर यही है कि केंद्र सरकार की भाषा नीति को साफ-साफ बदल दिया जाए—‘अंग्रेज़ी भी चलेगी’ की जगह अब सीधे ‘सिर्फ अंग्रेज़ी’ कर दी जाए. यह ज़्यादा ईमानदार और सच के करीब होगा. साथ ही, सभी राज्यों को पूरी ताकत से यह प्रोत्साहन दिया जाए कि वे अपने-अपने कामकाज पूरी तरह अपनी क्षेत्रीय भाषा में करें. राज्यों के बीच या केंद्र-राज्य के बीच जो भी संवाद हो, वह आपसी सहमति और सुविधा से तय हो—किसी एक भाषा को थोप कर नहीं.
ऐसी नीति लागू करना उतना मुश्किल नहीं जितना लोग सोचते हैं—यह तो उस ज़रूरी ऑपरेशन जैसा है, जो घाव को ठीक करने के लिए किया जाता है. इलाज के वक्त थोड़ी तकलीफ होती है, लेकिन बाद में मरीज पूरी तरह ठीक हो जाता है. अगर सच में भारतीय भाषाओं की फिक्र है, तो हर राज्य को ठान लेना चाहिए कि वह अपने पूरे कामकाज, यहां तक कि पूरी शिक्षा भी (जैसा कि छोटे यूरोपीय देश आइसलैंड तक करते हैं) अपनी भाषा में ही करेगा. इससे न सिर्फ लाखों-करोड़ों प्रतिभाशाली छात्रों को फायदा होगा, बल्कि हिंदी को लेकर चलने वाली राजनीति और कड़वाहट भी खत्म होगी. जब हर भाषा को बराबरी का दर्जा मिलेगा, तो स्वाभाविक तौर पर सभी नागरिकों में भारतीय भाषाओं के प्रति समान अपनापन और सम्मान बढ़ेगा. यही असली एकता को मज़बूत करेगा और सही मायनों में संघीय व्यवस्था को ताकत देगा.
(लेखक हिंदी के स्तंभकार और राजनीति विज्ञान के प्रोफेसर हैं. व्यक्त किए गए विचार निजी हैं)
(इस लेख को अंग्रेज़ी में पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)
यह भी पढ़ें: लोकतंत्र की असली परीक्षा: भारत को पहले ‘नेक चुनाव’ चाहिए, ‘एक चुनाव’ नहीं