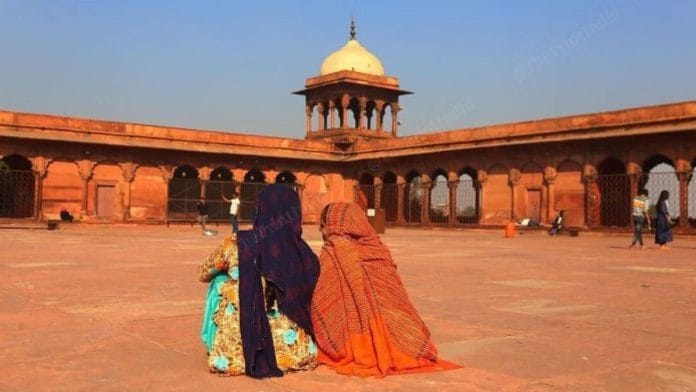पश्चिम एशिया प्रायः उबलता रहा है और वहां होने वाली उथल-पुथल भारतीय मुसलमानों को बुरी तरह परेशान करती रही है. अंतरराष्ट्रीय मामलों, खासकर मुस्लिम मुल्कों के मामलों के प्रति उनका रवैया उनकी राष्ट्रीय पहचान और राष्ट्रीय हितों से ज्यादा उनकी अपनी मजहबी पहचान और सीमा पार के प्रति वफादारी से तय होता रहा है.
पांच सौ साल पहले, 1526 में मुगलिया हुकूमत की स्थापना के बाद से भारत के मुगल बादशाहों ने सल्तनत काल की प्रथा से अलग हटते हुए किसी विदेशी सत्ता के प्रति वफादारी से इनकार कर दिया था. सल्तनत काल के सुलतान अब्बासी खिलाफत के आधिपत्य को स्वीकार करते थे. 1258 में हलाकू खान के नेतृत्व में मंगोल सेना ने बगदाद पर कब्ज़ा कर लिया था तब यह खिलाफत काहिरा में स्थानांतरित हो गई थी और 1527 तक वहीं टिकी रही. बाद में यह तुर्की के उस्मानी साम्राज्य के अधीन चली गई. इस्लाम के सियासी शब्दकोश में सुलतान का मतलब है खिलाफत का स्वायत्त शासक. मुगलों ने तुर्की में नए उस्मानी साम्राज्य को मान्यता नहीं दी और खुद को सुलतान नहीं बल्कि बादशाह कहने लगे.
भारत जब तक मुस्लिम शासकों के अधीन रहा तब तक इससे वास्तव में कोई फर्क नहीं पड़ा कि खिलाफत को मान्यता दी जाती है या नहीं, लेकिन 1857 में जब बाकी मुगल हुकूमत का भी खात्मा हो गया तब मुस्लिम शासक वर्ग खुद को बेसहारा महसूस करने लगा. अपनी दिशाहीन धार्मिक-राजनीति का वैचारिक आधार तलाशते हुए वह उस्मानी साम्राज्य के धार्मिक संस्थान से जुड़ गया. मुस्लिम शासक वर्ग ने अपना विदेशी चरित्र इस तरह बनाए रखा था कि भारत के बाहर एक नए अधिपति से जुड़ने में उसे कोई दिक्कत नहीं हुई, बल्कि इस स्वाभाविक प्रतिक्रिया को एक सांयोगिक कदम मान लिया गया.
तुर्की के प्रति नई उपजी सहानुभूति की पहली हलचल 1877-78 के रूस-तुर्क युद्ध के दौरान उभरी थी. नवस्थापित अलीगढ़ के मोहम्डन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज ने, जिसे अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का पूर्ववर्ती माना जाता है, तुर्क पोशाक को अपनी वर्दी बनाया जिसमें लाल टोपी और काला फुंदना प्रमुखता से प्रदर्शित होता था. ओटोमन साम्राज्य से जुड़ाव की यह प्रवृत्ति खिलाफत आंदोलन के दौरान और गहरी हो गई. इसने मुस्लिम मानस में भारतीय राष्ट्रवाद को अल-इस्लामिया (‘पैन इस्लामिज़्म’) के मुकाबले हमेशा के लिए गौण बना दिया और भारतीय विदेश नीति को मुसलमानों की सीमा पार की वफादारी के प्रति काफी हद तक संवेदनशील बना दिया.
भारतीय राष्ट्रवाद बनाम अल-इस्लामिया
भारत के मुस्लिम शासक वर्ग ने अपनी ऐसी पहचान बनाई जिसके चलते उन्हें देसी से ज्यादा विदेशी हम-मजहब लोगों से जुड़ने में आसानी हुई. इस तरह, भारत में जब राष्ट्रीय आंदोलन शुरू हुए तो वे अल-इस्लामिया की ओर मुड़ गए. वैसे, यह सच है कि सर सैयद अहमद खान अल-इस्लामिया के विचार के प्रति संशय रखते थे और घुमंतू उपदेशक जमालुद्दीन अफगानी (1838-97) के उपदेशों का विरोध करते थे, लेकिन सर सैयद ब्रिटिश सरकार के वफादार थे और भारतीय राष्ट्रवाद का विरोध करते थे, इसलिए अल-इस्लामिया के प्रति उनका विरोध उसके ब्रिटिश विरोधी स्वर के कारण था.
आज जिसे ‘ग्लोबल इस्लाम’ या ‘उम्मा’ कहा जाता है, उसे 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी के शुरू में पैन इस्लामिज़्म कहा जाता था. वैसे तो इसका शाब्दिक अर्थ यह है कि यह वह विचारधारा है जिसे पूरा इस्लामी संसार मानता है और उसमें समाहित है, लेकिन वास्तव में यह भारतीय मुसलमानों के राजनीतिक रुख को ज़ाहिर करता था. ये भारतीय मुसलमान रहते तो भारत में थे, लेकिन अपना वजूद वैश्विक मुस्लिम समुदाय में ढूंढते थे. वह पैदा तो भारत में हुए लेकिन थे कहीं और के, मुस्लिम संसार के मामलात उन्हें भावनात्मक और मानसिक स्तर पर सबसे ज्यादा गहराई से प्रभावित करते थे. उनकी सियासत भारत में हो रही घटनाओं के मुक़ाबले तुर्की और अरब जगत में हो रही घटनाओं से ज्यादा तय होती थी. उल्लेखनीय बात यह है कि ब्रिटिश राज के खिलाफ मुसलमानों का सबसे तगड़ा विरोध स्वराज की खातिर नहीं हुआ बल्कि इस बात को लेकर हुआ कि तुर्की में उस्मानी खिलाफत की गद्दी बचेगी या नहीं. इसके बारे में ज्यादा चर्चा आगे करेंगे.
अल-इस्लामिया की शुरुआत एक भावनात्मक और राजनीतिक मुद्दे के रूप में हुई लेकिन अग्रणी भारतीय राष्ट्रवादी नेताओं में शुमार हुए मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के लेखन ने इसे सुविचारित विचारधारा का स्वरूप प्रदान किया. 1912-13 के बाल्कन युद्ध और उस्मानी साम्राज्य को मिले झटकों ने भारतीय मुसलमानों को काफी निराश कर दिया. आज़ाद ने भारतीय मुसलमानों को अंग्रेजों के खिलाफ बगावत करने के लिए 1912 में उर्दू पत्रिका ‘अल हिलाल’ शुरू की. माना जाता था कि तुर्की की हार में अंग्रेजों का हाथ था. सरकार ने 1914 में इस पत्रिका को जबरन बंद करवा दिया. 1915 में आज़ाद ने ‘अल-बलाग़’ साप्ताहिक शुरू किया, जिसे भी जल्दी ही बंद करवा दिया गया.
इन दो पत्रिकाओं ने अल-इस्लामिया को भारतीय मुसलमानों की एक विचारधारा और एक राजनीतिक आंदोलन के रूप में स्थापित कर दिया, जो खिलाफत आंदोलन के रूप में अपने चरम उत्कर्ष तक पहुंचा. इसने अलगाववाद को एक धार्मिक पंथ के रूप में ऐसा संस्थात्मक रूप दे दिया कि देश का बंटवारा अपरिहार्य हो गया.
उम्मा का फरेब
खिलाफत आंदोलन भारतीय मुसलमानों का सबसे मजबूत अल इस्लामिया उपक्रम था, वह एक ऐसा विचित्र आंदोलन था जो भारतीय राजनीति को हमेशा प्रभावित करता रहा. यह विचित्र इसलिए था कि भारतीय मुसलमान तो तुर्की के उस्मानी खिलाफत की गद्दी बचाना चाहते थे, लेकिन खुद तुर्की के मुसलमान यह नहीं चाहते थे. 1924 में उसे खत्म कर दिया गया.
भारतीय मुसलमान चाहते थे कि अरब प्रायदीप, जिसमें इस्लाम के तमाम धर्म स्थल स्थित हैं, तुर्की के नियंत्रण में ही रहें, लेकिन अरब लोग उससे अपनी आज़ादी चाहते थे, जो उन्होंने प्रथम विश्वयुद्ध के दौरान सफल आंदोलन के जरिए अंततः हासिल कर ली.
भारतीय मुसलमान अपनी ही दुनिया में जी रहे थे. उन्हें यह मालूम नहीं था कि तुर्क और अरब लोग क्या चाहते थे और जब देर से उनका सामना हकीकत से हुआ तब उन्हें अपनी विचित्र कोशिशों से ज्यादा सदमा इन दोनों समुदायों के ‘गैर-इस्लामिक’ आचरण से पहुंचा. उन्होंने तुर्कों से गुजारिश की कि वे खिलाफत को खत्म न करें, अरबों से कहा कि वे उस्मानी साम्राज्य से अलग न हों, लेकिन भारतीय मुसलमान यह कबूल नहीं कर पाए कि वे जिस इस्लामी एकता का पीछा कर रहे थे वह महज़ ख्वाब था.
आश्चर्य की बात है कि वे अपनी मूर्खता, अपने गलत सोच और गलत आकलन को नहीं समझ पाए और ज़ाहिर तौर पर गलत होते हुए भी उसी धोखे में आगे बढ़ते गए. क्या वे यह सोच रहे थे कि एक आदर्श का पीछा करते हुए वे कोई गलती नहीं कर रहे थे? या कहीं गहराई से वे यह जानते थे कि खिलाफत आंदोलन तुर्कों के समर्थन में उतना नहीं था जितना भारत में मुस्लिम ताकत के प्रदर्शन के लिए था? महात्मा गांधी ने मुसलमानों को अपने साथ ले चलने के मकसद से खिलाफत के मसले को अपनाया मगर वे इस सामूहिक मानसिकता में निहित पेच को समझने में विफल रहे.
दोहरी पहचान का मुगालता
खिलाफत आंदोलन के जाने-माने नेता मोहम्मद अली (1878-1931) ने भारतीय मुसलमानों की दोहरी पहचान की व्याख्या करते हुए कहा था कि उनकी एक पहचान तो भारतीय की है और एक पहचान मुसलमान की है और ये दोनों पहचान न तो समान दायरे वाली है और न एक-दूसरे से मेल खाने वाली हैं, वे बस हाशिये पर आपस में थोड़ा सा मिलती हैं. अली ने 1930 में लंदन में हुए गोलमेज़ सम्मेलन में यह व्याख्या प्रस्तुत करते हुए कहा था: “मैं समान आकार वाले दो वृतों का हूं, लेकिन इन दोनों वृतों का केंद्र एक नहीं है. एक केंद्र है भारत और दूसरा केंद्र है मुस्लिम संसार…हम भारतीय मुसलमान दोनों वृतों के हैं. हर एक वृत में 30 करोड़ लोग हैं और हम किसी वृत को छोड़ नहीं सकते.”
हैरानी की बात है कि अली की व्याख्या में जो मुस्लिम वृत है वह भारतीय वृत के बाहर है. मुस्लिम वृत भारतीय वृत के अंदर क्यों नहीं हो सकता और दोनों वृतों का केंद्र एक क्यों नहीं हो सकता? क्या दूसरे समुदाय, गैर-हिंदू समुदाय भी, भारतीय वृत में नहीं हैं? क्या उन्हें विदेशी हम-मजहबों के वृत का सहारा लिये बिना इस भारतीय वृत में अपने आध्यात्मिक और भौतिक विकास की पूरी गुंजाइश नहीं दिखती? क्या दुनिया के और किसी देश में कोई दूसरा धार्मिक समुदाय अपनी पहचान को अपने दूसरे देसी समुदायों से ज्यादा किसी विदेशी हम-मजहबों से जोड़ता है? अली की व्याख्या के अनुसार, मुस्लिम वृत फैल कर भारत में पहुंचा और उसने इस देश को इस्लामी प्रभुत्व का हिस्सा बनाया. इसलिए भारतीय मुसलमान प्राथमिक रूप से भारतीय नहीं हैं बल्कि भारत में ग्लोबल उम्मा के नुमाइंदे हैं.
लेकिन जैसा कि मैं पहले कह चुका हूं, अल-इस्लामिया दुनिया भर के मुसलमानों के साथ भारतीय मुसलमानों के आदर्श जुड़ाव का कम और साथी भारतीयों से उनके कटाव का ज्यादा प्रतिनिधित्व करता है. यह सांप्रदायिक अलगाववाद को रेखांकित करने वाला विशेषण ही है. अवधारणा और कार्रवाई, दोनों मामले में अल-इस्लामिया का अर्थ है — राष्ट्रवाद-विरोध. अल-इस्लामिया ने किस तरह भारतीय राष्ट्रवाद की जगह ले ली इसका सबसे प्रतीकात्मक उदाहरण है अल्लामा इक़बाल की कविता: सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा, हम बुलबुले हैं इसके, ये गुल्सितां हमारा… बाद में ‘तराना-ए-मिल्ली’ कविता में उन्होंने लिखा : चीन-ओ-अरब हमारा, हिंदोस्तां हमारा; मुस्लिम हैं हम, वतन है सारा जहां हमारा.
विदेश नीति में तुष्टीकरण की राजनीति
अगर भारतीय मुसलमान ग्लोबल उम्मा से केवल मुसलमान के रूप में नहीं बल्कि भारतीय के रूप में जुड़ते तो राष्ट्रीय हित को वे अपने विमर्श में सबसे ऊपर रखते, लेकिन उम्मा के प्रति उनके मोह ने उन्हें अपनी फिक्र न करके भारतीय हितों को दूसरों के हितों के मुकाबले गौण बनने पर मजबूर किया. खिलाफत की रक्षा के लिए शुरू हुए आंदोलन ने अगले सौ साल के लिए भारतीय विदेश नीति का खाका तय कर दिया.
जब भी किसी मुस्लिम मुल्क का मामला सामने आता, हमारी विदेश नीति खुद-ब-खुद उम्मा समर्थक रुख अपना लेती. जो ज़ाहिर तौर पर विकासशील देशों के साथ एकजुटता का सैद्धांतिक आग्रह था वह दरअसल भारतीय मुसलमानों की भावनाओं के तुष्टीकरण का कदम होता था. इसका सबसे प्रकट उदाहरण है फिलस्तीन में अरब-यहूदी समस्या पर गांधी का रुख. अपने यहूदी ‘आत्मीय’ मित्र हरमन कालेनबाख (1871-1945) के, जिन्होंने उन्हें दक्षिण अफ्रीका में ‘तोल्स्तोय फार्म’ स्थापित करने के लिए 1100 एकड़ जमीन दान में दी थी, निरंतर अनुरोधों के बावजूद गांधी ने यहूदियों के नजरिए पर गौर करने से मना कर दिया था.
‘हरिजन’ के 26 नवंबर 1938 के अंक में गांधी ने इस मुद्दे पर एक लेख लिखा था, जो फिलस्तीनी मुद्दे पर पर भारत की नीति के लिए पत्थर की लकीर बन गई. यही नहीं, इसने मुस्लिम मुल्कों के मामले में भारतीय विदेश नीति के सीमाएं तय कर दी. उन्होंने अपने विचारों को नैतिकता की कसौटी पर कसते हुए कहा कि यह एक रणनीतिक फैसला था क्योंकि वे मुसलमानों को राष्ट्रीय आंदोलन के लक्ष्य से जोड़ना चाहते थे. लेकिन उनकी उम्मीदें पूरी नहीं हुईं.
एकतरफा मुहब्बत
भारत तो सभी अंतरराष्ट्रीय संघर्षों में हमेशा अरब समर्थक और मुस्लिम समर्थक रुख अपनाता था, लेकिन इन मुल्कों ने पाकिस्तान से हमें हो रही समस्याओं को लेकर शायद ही कभी हमारा पक्ष लिया और कश्मीर मसले पर तो वे पाकिस्तान की ज़बान में ही बोलते रहे हैं. वास्तव में वे फिलस्तीन और कश्मीर मसले को एक ही तराजू पर तौलते हैं और इज़रायल की तरह भारत को भी अपना दुश्मन मानते हैं.
भारत अपने यहां के मुस्लिम अल्पसंख्यकों को खुश रखने के लिए मुस्लिम समर्थक कूटनीति चलाता रहा है, जबकि मुस्लिम मुल्कों के भारत विरोधी रुख पर भारतीय मुसलमानों में आक्रोश पैदा होना चाहिए, उन्हें इस व्यवस्था में कोई खामी नहीं दिखती कि भारत इन मुल्कों से कोई उम्मीद रखे बिना उनका पक्ष लेता रहे. वे तुष्ट अल्पसंख्यक के रूप में इसे अपना अधिकार मानते हैं कि भारत इस्लाम की खिदमत करता रहे.
भारतीय मुसलमानों से अरबों की नफरत
लेकिन दिलचस्प बात यह है कि मुस्लिम मुल्क भारतीय मुसलमानों की कोई परवाह भी नहीं करते. वह उन्हें पक्का मुसलमान भी नहीं मानते और उनमें हिंदी और हिंदू के बीच अर्थगत भेद करने की सलाहियत भी नहीं है.
मानो इतनी उदासीनता काफी नहीं थी, तो उन्होंने भारत को 57 मुल्कों वाले ताकतवर संगठन ‘ऑर्गनाइज़ेशन ऑफ इस्लामिक को-ऑपरेशन (ओआईसी)’ में सीट की पेशकश भी नहीं की. भारत में पूरी दुनिया के 11 फीसदी यानी 20 करोड़ मुसलमान रहते हैं और वह सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाला तीसरा बड़ा देश है. भारत के बिना ओआईसी का यह दावा खोखला ही रहेगा कि वह “मुस्लिम संसार की सामूहिक आवाज़” है और “अंतरराष्ट्रीय शांति एवं समरसता की भावना के साथ मुस्लिम संसार के हितों की रक्षा” के लिए काम करता है.
दो वृत या केवल एक?
दुनिया में हर दस मुसलमान में एक मुसलमान भारतीय है. फिर भी उन्हें ओआईसी में सीट नहीं मिली है. हैरानी की बात यह है कि दुनिया की सबसे प्रातिनिधिक संस्था में प्रतिनिधित्व से इनकार किए जाने पर भी भारतीय मुसलमानों को कोई गुस्सा नहीं आता, जबकि आना चाहिए था, खासकर इसलिए किए वे खुद को ग्लोबल उम्मा का हिस्सा मानते हैं. यह स्थिति तब और दिलचस्प हो जाती है जब हम भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के खिलाफ भारतीय मुसलमानों के इन आरोपों पर गौर करते हैं कि उन्हें उनकी आबादी के अनुपात में भारतीय संसद और विधानसभाओं में प्रतिनिधित्व देने की राह आसान नहीं बनाई जा रही है. ऐसे में, वे जिन दो वृतों में होने के दावे करते हैं उनमें से एक वृत में अपने प्रतिनिधित्व से वंचित किए जाने से इतने बेफिक्र कैसे हो सकते हैं? निश्चित ही इसमें कोई गड़बड़ी है और उन्हें वृतों की अपनी प्रिय अवधारणा पर पुनर्विचार करना चाहिए.
अब, मुस्लिम संसार में इज्जत हासिल करने का एक ही उपाय है भारतीय मुसलमानों के पास: भारतीय बनिए और अपने मुसलमानत्व को भारतीयता के अंदर दाखिल कीजिए. आप दो नहीं, एक ही वृत में हैं; और भारतीय होने के सिवाय आपका कोई भविष्य नहीं है.
(इब्न खल्दुन भारती इस्लाम के छात्र हैं और इस्लामी इतिहास को भारतीय नज़रिए से देखते हैं. उनका एक्स हैंडल @IbnKhaldunIndic है. व्यक्त किए गए विचार निजी हैं.)
संपादक का नोट: हम लेखक को अच्छी तरह से जानते हैं और छद्म नामों की अनुमति तभी देते हैं जब हम ऐसा करते हैं.
(इस लेख को अंग्रेज़ी में पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें.)
यह भी पढ़ें: अब वक्त है कि बकरीद के रूप को बदला जाए—भारत के गरीबों को अब मांस नहीं, लैपटॉप और AC चाहिए