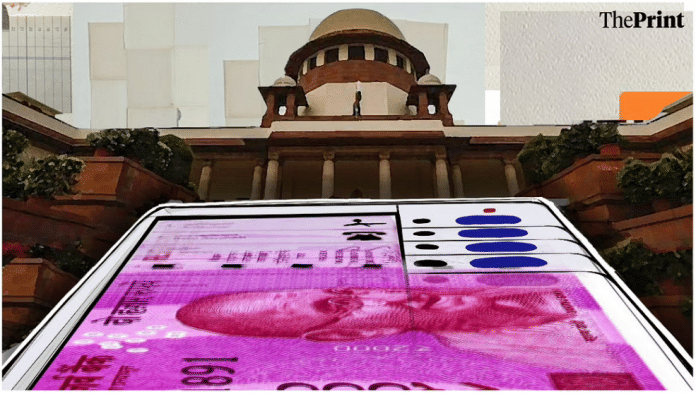सुप्रीम कोर्ट को भारत में चुनावी फंडिंग की दूषित व्यवस्था को दुरुस्त करने का एक और मौका मिला है. यह उसके लिए भूल सुधार करने का भी मौका है.
राजनीति में जो भी भ्रष्टाचार है उसकी जड़ चुनावी फंडिंग ही है. यह 1952 में हुए पहले आम चुनाव से ही शुरू हो गया था. भारत की तीन पीढ़ियों के सबसे बुद्धिमान लोग भी इसे 65 वर्षों में दुरुस्त न कर पाए. अंततः, इसे 1 अप्रैल 2017 को केंद्रीय बजट लागू होते ही वैध बना दिया गया. इसके बाद के पांच वर्षों में एक नयी राष्ट्रीय सरकार और दो दर्जन राज्य सरकारें चुनी गईं, गिराई गईं, फिर से चुनी गईं लेकिन यह व्यवस्था जस की तस बनी रही.
मोदी सरकार द्वारा लागू की गई गुमनाम चुनावी बॉन्ड की व्यवस्था को बहुत पहले दी गई चुनौती पर सुनवाई के लिए अब सुप्रीम कोर्ट ने 19 सितंबर की तारीख तय की है (वैसे इसे औपचारिक रूप से रोस्टर में शामिल नहीं किया गया है इसलिए अभी इंतजार कीजिए). उम्मीद की जाए कि देश को अंततः इस मौके का लाभ मिलेगा. सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में अप्रैल के शुरू में मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई के नेतृत्व में तीन सदस्यीय बेंच का गठन किया था, जिसमें जस्टिस दीपक गुप्ता और जस्टिस संजीव खन्ना भी शामिल किए गए थे. इस बेंच ने एक अंतरिम आदेश जारी किया था, जो अफसोस कि इतना लचर था कि इसके बारे में कहा जा सकता है कि अलेक्ज़ेंडर पोप ने मानो इसी के लिए यह वाक्य लिखा था— ‘चोट पहुंचाने को राजी तो हूं मगर हमला करने से घबराता हूं.’
वैसे, कभी भी सर्वोच्च अदालत पर सवाल उठाने में शब्दों का बहुत सावधानी से चुनाव करना जरूरी है, खासकर इस मामले में. इसकी वजह यह है कि कोर्ट के अंतरिम आदेश से, जो उसे इस मामले पर जल्दी ही विस्तार से विचार करने का मौका देता, ऐसा लगा कि उसने मामले को अनिश्चित काल के लिए लटका दिया हो. यह ‘अनिश्चित काल’ करीब साढ़े तीन साल का हो गया है और इस बीच तीन मुख्य न्यायाधीश अपना कार्यकाल पूरा कर चुके हैं. संभावना यही लगती है कि जब तक इस पर सुनवाई गति पकड़ेगी तब तक हम पांचवें मुख्य न्यायाधीश के दौर में पहुंच चुके होंगे.
यह भी पढ़ें: कर्तव्य पथ पर मोदी से मत पूछिए वे आपके लिए क्या करेंगे, खुद से पूछिए कि आप उनके भारत के लिए क्या करेंगे
अदालतों में अंतहीन तारीखों के सिलसिले से हम पहले ही त्रस्त हो चुके हैं. इसने फिल्मों को भी मसाला जुटाया है. इस सिलसिले के हम इतने आदी हो चुके हैं कि यह हमारी संस्कृति में शामिल हो गया है, यहां तक कि हमारे आला जज भी कुछ हाईकोर्टों की सुस्ती पर तंज़ कसने के लिए ‘दामिनी’ फिल्म के सनी देओल का ‘तारीख पे तारीख’ वाला मशहूर डायलॉग इस्तेमाल करने लगे हैं.
वैसे, यह मामला सामान्य से ज्यादा देरी का शिकार हुआ है. पूरी विनम्रता और पूरे सम्मान के साथ मैं यह कहना चाहता हूं कि ऐसा लगता है मानो यह जोखिम से बचने का मामला बन गया है, कि इसमें बहुत घालमेल है इसे बाद में देखा जाएगा. वैसे भी, इस अंतरिम आदेश से एक दिन पहले, 2019 के आम चुनाव में कई राज्यों में पहले चरण का मतदान हो चुका था. इस आदेश में बेंच ने कहा था कि पारदर्शिता होनी चाहिए. और उसने हमें पारदर्शिता दी भी. हुआ सिर्फ इतना कि पारदर्शिता सीलबंद लिफाफे में मिली.
बेंच ने कहा कि हरेक पार्टी को इन गुमनाम चुनावी बॉन्डों के जरिए मिले चंदे का विस्तृत ब्यौरा चुनाव आयोग को 30 मई 2019 तक देना होगा. इन ब्यौरों का खुलासा करना है या नहीं, करना है तो कैसे और कब करना है, यह फैसला चुनाव आयोग पर छोड़ दिया गया. यानी बेंच ने गेंद को बगल के मैदान यानी चुनाव आयोग के पाले में डाल दी. और चुनाव आयोग उन ब्यौरों को दबा कर बैठ गया. जो काम करने से सर्वोच्च अदालत के जज डर गए वह काम सेवानिवृत्त हो चुके लोकसेवक करेंगे, यह उम्मीद करना मूर्खता ही होगी.
‘डर गए’ शब्द कठोर हैं, लेकिन मैंने केवल एक प्रचलित मुहावरे का ही प्रयोग किया है. इसे हम दूसरी तरह से भी, चीन के ताकतवर नेता रहे तंग श्याओपिंग के शब्दों में भी कह सकते हैं. 1988 में, बीजिंग में राजीव गांधी के साथ शिखर बैठक में श्याओपिंग ने सीमा विवाद को परे रखने पर ज़ोर देने के लिए खास चीनी मिज़ाज में कहा था कि ‘हमारी पीढ़ी में शायद इतनी बुद्धिमानी नहीं थी कि सीमा विवाद जैसे जटिल मसले को सुलझा पाती, इसलिए हम इसे ज्यादा बुद्धिमान भावी पीढ़ी के भरोसे छोड़ कर जिस मामले में आगे बढ़ सकते हैं, बढ़ें.’
यह मान लेना ज्यादा उपयुक्त लगता है कि अप्रैल 2019 में उक्त बेंच ने कुछ ऐसे ही ख्याल से अंतरिम आदेश जारी किया था. अब सवाल यह है कि क्या वैसे बुद्धिमान जजों की पीढ़ी सामने आ गई है?
दिवंगत अरुण जेटली ने 2017-18 के बजट में इन चुनावी बॉन्डों की घोषणा करते हुए यही कहा था कि यह एक आंशिक सुधार ही है. उन्होंने कहा था कि चुनावी चंदे से काले धन को खत्म करने की दिशा में यह सिर्फ पहला कदम है. यह उचित बात लग रही थी क्योंकि तब तक यही हो रहा था कि अमीर लोग, अच्छे या उतने अच्छे नहीं कॉर्पोरेट, जमीन-जायदाद के बड़े खिलाड़ी, खनन के खुदा, अपराधी, तस्कर, ठग, यानी कोई भी उन राजनीतिक दलों और नेताओं को बोरी भरकर नकदी दे रहा था जिन्हें वह पसंद करता था या उन्हें आगे बढ़ाना चाहता था. लेकिन अब वे भारतीय स्टेट बैंक से चुनावी बॉन्ड खरीद सकते हैं, बेशक केवल सफ़ेद पैसे से.
उन्हें सफ़ेद पैसे से ही खरीदने का प्रोत्साहन इसलिए भी मिलता है कि इन बॉन्डों के जरिए राजनीतिक चंदा देने पर टैक्स में छूट मिलती है. इसने राजनीतिक खेमे को भी उसी सफ़ेद दायरे में शामिल होने का मौका दिया क्योंकि उसे जो चंदा मिलता है वह टैक्स-मुक्त है. लेकिन अगर यह पारदर्शिता की ओर पहला कदम था, तो अगला तार्किक कदम न उठाने ने रोग के इस उपचार को रोग से भी बदतर बना दिया.
इसका हिसाब कुछ इस तरह है. दानकर्ता—आम तौर पर कोई कॉर्पोरेट—स्टेट बैंक जाकर बियरर चेक या बॉन्ड के जरिए उसकी रकम के बराबर मूल्य का चुनावी बॉन्ड खरीदता है और अपनी पसंद की पार्टी को सौंप देता है. वह पार्टी उस बॉन्ड को निर्धारित बैंक खाते जमा कर देती है. दानकर्ता को किसी को यह बताने की जरूरत नहीं है कि उसने बॉन्ड किसे सौंपा, और दान पाने वाले को भी यह खुलासा करने की जरूरत नहीं है कि उसे पैसा कहां से मिला.
इस तरह, पहले कदम ने चुनावी फंडिंग को काले से सफ़ेद पैसे के दायरे में तो ला दिया लेकिन दूसरे कदम ने उस पर गुमनामी का पर्दा डाल दिया. सो, मामला वही रहा कि दो हितबद्ध पक्षों के बीच पूरे अंधेरे में पैसे का लेन-देन हुआ लेकिन मतदाता नहीं जान पाएगा कि किसने किसको कितने पैसे दिए. या किसी नागरिक अथवा किसी संस्था को यह पता नहीं लग पाएगा कि कोई फैसला ऐसे किसी भुगतान से प्रभावित होकर तो नहीं किया गया. गुमनाम चंदा वैसे भी यह संदेह पैदा करता है कि कहीं यह घूस तो नहीं है. यानी हालात पहले के मुक़ाबले बदतर ही हुए. पूरी तरह वैध चुनावी भ्रष्टाचार!
इसे और गहराई से जांचें. मतदाता या नागरिक को यह पता नहीं चलता कि किसने किसको पैसे दिए और क्या कोई फैसला इस दान के प्रभाव में तो नहीं किया गया. उदाहरण के लिए, किसे मालूम कि किसी सेक्टर (मान लीजिए कि इस्पात) को अचानक शुल्कों में भारी वृद्धि करने की छूट क्यों दे दी गई, जबकि इस संदेह को दूर करने का कोई उपाय नहीं है कि इस गुटबंद उद्योग ने इन चुनावी बॉन्डों की भारी खरीद की होगी.
इसके अलावा, बाहर के किसी शख्स को तो कुछ मालूम नहीं हुआ, जबकि ‘सिस्टम’ को सब मालूम है. आखिर, सरकारी बैंक को तो पता ही है कि बॉन्ड किसने खरीदे, या किस राजनीतिक दल ने कितना पैसा जमा किया. इसके बाद तो सिर्फ बॉन्ड के नंबरों का मेल करना रह जाता है. इस तरह, ‘सिस्टम’ जिसके कब्जे में है वह आसानी से पता लगा सकता है कि कौन दोस्त है और कौन दुश्मन. यानी सरकार न केवल यह तय कर सकती है कि किसे लाभ पहुंचाना है बल्कि यह भी कि किसे सजा देनी है.
सो, अब आपको समझ में आ गया होगा कि चुनावी भ्रष्टाचार के खिलाफ 65 साल से जारी लड़ाई में 1 अप्रैल 2019 को कैसे हार मिली, और नए चुनावी बॉन्डों ने ‘सिस्टम’ की सफाई करने की जगह भ्रष्टाचार को किस तरह वैध बना दिया.
सियासी तबके से हम जो उम्मीदें रखते हैं उनके मद्देनजर किसी ने यह नहीं सोचा होगा कि भाजपा सरकार चुनाव सुधार करने के अपने वादे पूरे करेगी लेकिन असली निराशा सुप्रीम कोर्ट से हुई है जिसने मामले को बहुत गरम मान कर इसे अगली-ज्यादा-बुद्धिमान-पीढ़ी के सुपुर्द करने जैसा फैसला किया.
इसके बाद पांच साल से ज्यादा बीत चुके हैं. भारत की चुनावी फंडिंग की व्यवस्था इस संदिग्ध किस्म के ‘सुधार’ से पहले के दौर में जैसी थी उसके मुक़ाबले अब और ज्यादा दूषित हो चुकी है. क्या भारत अपनी इस सबसे सम्मानित संस्था से उम्मीद कर सकता है कि वह स्पष्टता बहाल करके भूल सुधार करेगी?
(इस लेख को अंग्रेजी में पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)
यह भी पढ़ें: क्यों सोनिया-राहुल की कांग्रेस ने पतन की जो दौड़ 2004 में शुरू की थी उसे अब जीतने वाली है