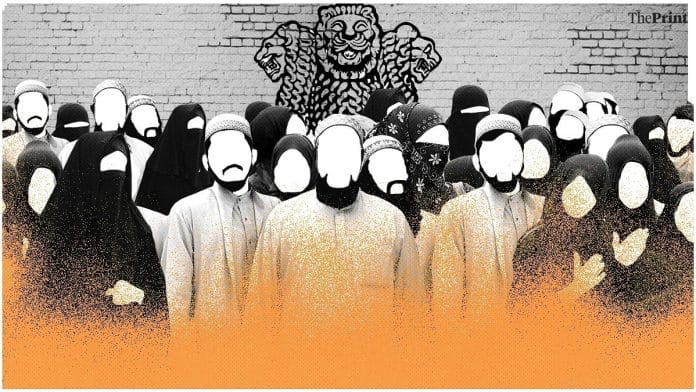गुजरात सरकार ने राज्य के लिए समान नागरिक संहिता (यूसीसी) का मसौदा तैयार करने के लिए जस्टिस रंजना देसाई की अध्यक्षता में एक समिति गठित की है. इससे पहले, उत्तराखंड भारत में यूसीसी अपनाने वाला पहला राज्य बना. यह कहना कि यूसीसी एक विवादास्पद मुद्दा है, एक मामूली बात होगी. यह हमारे विभाजित समय के सबसे राजनीतिक रूप से संवेदनशील मुद्दों में से एक है.
हमारा समाज स्वतंत्रता के सात दशकों बाद और कई सकारात्मक कानूनों के बावजूद अब भी पितृसत्तात्मक और स्त्री विरोधी बना हुआ है.
नेहरू, आंबेडकर और कुछ प्रमुख महिला स्वतंत्रता सेनानियों ने महिलाओं की समानता के लिए एक धर्मनिरपेक्ष पारिवारिक कानून या यूसीसी का प्रस्ताव रखा था. उन्हें लगा कि संविधान में लैंगिक समानता की गारंटी होने के बावजूद, महिलाओं के साथ भेदभाव बना रहेगा.
एक उम्मीद की किरण
1940 और 1950 के दशक का भारत एक अलग जगह थी. धर्म के आधार पर माने जाने वाले सांस्कृतिक नियम और प्रथाएं व्यापक रूप से फैली हुई थीं. हिंदुओं और मुसलमानों में बाल विवाह और बहुविवाह आम बात थी. महिलाओं के पास संपत्ति नहीं थी. केवल पुरुष वारिसों को ही पैतृक घरों और व्यवसायों का मालिक माना जाता था. विधवाओं का बहिष्कार और दहेज प्रथा बहुत प्रचलित थी. लैंगिक न्याय जैसे विचार लगभग अस्तित्वहीन थे. पारिवारिक कानूनों में सुधार सरकार में मौजूद कुछ प्रबुद्ध लोगों के लिए एक बहुत कठिन कार्य प्रतीत हो रहा था. एक समान नागरिक संहिता (UCC) का हर पृष्ठभूमि के नेताओं ने तीव्र विरोध किया. संविधान सभा के अधिकांश सदस्यों ने इसे भारतीय सभ्यता और प्राचीन विरासत के लिए खतरे के रूप में देखा. नेहरू को इस विचार को छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा और आंबेडकर ने इस निर्णय से असहमति जताते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया.
संविधान के राज्य नीति के निदेशक सिद्धांतों में यूसीसी को अनुच्छेद 44 के रूप में शामिल किया गया.
लेकिन एक सकारात्मक पहलू भी था. नेहरू के नेतृत्व वाली सरकार ने 1950 के दशक में हिंदू कोड बिल के माध्यम से बड़े पैमाने पर सुधार किया. 1955 के हिंदू विवाह अधिनियम के कारण, विवाह अब “सात जन्मों का बंधन” नहीं रहा. एक हिंदू पत्नी और पति दोनों को समान रूप से तलाक का अधिकार मिला. हिंदू महिलाओं को संपत्ति में कानूनी अधिकार और परिवार से जुड़े अन्य अधिकार प्राप्त हुए. दशकों में, ईसाइयों ने भी अपने पारिवारिक कानूनों में सुधार किया, जिससे महिलाओं को न्याय मिल सका.
हालांकि, रूढ़िवादी धर्मगुरुओं के विरोध के कारण, मुस्लिम पारिवारिक कानून को न तो एक साफ-सुथरे कानून के रूप में लिखा जा सका और न ही उसमें कोई बदलाव किया गया. मुसलमानों पर मुस्लिम पर्सनल लॉ (शरीयत) आवेदन अधिनियम, 1937 लागू होता है, जो अत्यंत अपर्याप्त है. यह केवल यह कहता है कि मुसलमानों को शरीयत के अनुसार चलाया जाएगा, लेकिन इसका कोई संहिताबद्ध रूप नहीं है. पुरुष प्रधान धार्मिक व्यवस्था में इसकी सही और गलत, दोनों तरह की व्याख्याएं खूब की जाती हैं.
नतीजतन, मुस्लिम महिलाएं पारिवारिक मामलों में भेदभाव का सामना करती हैं. वे बाल विवाह, एकतरफा तलाक, बहुविवाह, बच्चों की अभिरक्षा और संरक्षकता से इनकार, संपत्ति में हिस्सेदारी से वंचित होना, मुताह या अस्थायी विवाह, हलाला आदि जैसी प्रथाओं का खामियाजा भुगतती हैं. यह तब होता है जब क़ुरान ने उन्हें सहमति, मेहर, संपत्ति में हिस्सा और न्यायसंगत तलाक जैसे कई अधिकार दिए हैं. मोरक्को, ट्यूनीशिया, तुर्की और इंडोनेशिया जैसे कई मुस्लिम बहुल देशों में भारत की तुलना में अधिक लैंगिक समानता वाले कानून हैं. दुर्भाग्यवश, मुस्लिम महिलाओं को न तो मुसलमान होने के नाते और न ही एक धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र में नागरिक होने के नाते उनके अधिकार मिलते हैं.
विरोधाभास
यूसीसी के मूल उद्देश्य—लैंगिक न्याय और समानता—को धार्मिक विभाजन और नफरत के माहौल में भुला दिया गया है. बीजेपी 1985 से अपने चुनावी घोषणा पत्र में यूसीसी लागू करने का वादा करती आ रही है. शाह बानो केस ने कई मतदाताओं की नजर में इस वादे को और भी वैधता प्रदान की. यूसीसी के प्रति मुस्लिम धर्मगुरुओं का कट्टर विरोध आज बीजेपी के लिए एक राजनीतिक लाभ बन गया है. लेकिन खुद पार्टी का लैंगिक समानता पर रिकॉर्ड बहुत संतोषजनक नहीं है.
उत्तराखंड यूसीसी में बाल विवाह और बहुविवाह पर रोक जैसी विशेषताएं तो हैं, लेकिन इसमें लिव-इन रिलेशनशिप पर कठोर प्रावधान भी शामिल हैं. यह कानून संविधान द्वारा नागरिकों को दिए गए स्वतंत्रता, स्वायत्तता और गोपनीयता के अधिकार को छीन लेता है. इसकी मंशा तब साफ हो गई जब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यूसीसी को अपनाते समय कहा कि यह कानून यह सुनिश्चित करेगा कि “कोई आफताब हमारी बेटियों या बहनों के साथ श्रद्धा वाकर जैसी बर्बरता न करे.”
इसके अलावा, कुछ अन्य अस्वीकार्य कदम भी उठाए गए हैं, जैसे कि महिला पहलवानों का यौन शोषण करने के आरोपी भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष बृज भूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी न करना, बिलकिस बानो के बलात्कारियों को समय से पहले रिहा करना, और बलात्कारी राजनेताओं व धार्मिक गुरुओं के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई न करना.
भारत एक बहुसांस्कृतिक और बहु-धार्मिक देश होने के साथ-साथ एक धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र भी है. भारतीय समाज शायद अभी तक धर्मनिरपेक्ष पारिवारिक कानूनों के लिए तैयार न हो, लेकिन आज भारतीय महिलाएं अपने अधिकारों के प्रति पहले से कहीं अधिक जागरूक हैं. इस अहम मुद्दे का राजनीतिकरण होना निराशाजनक है और हमारे नेतृत्व के बारे में एक खराब तस्वीर पेश करता है.
सबसे पहले, मैं सरकार में यूसीसी को आगे बढ़ाने वालों से कुछ सवाल पूछना चाहती हूं. लैंगिक न्यायसंगत कानून राष्ट्रीय प्राथमिकता होनी चाहिए, फिर यह राज्य-स्तरीय प्रयोग क्यों? आदिवासियों को इससे बाहर क्यों रखा जा रहा है? आदिवासी महिलाओं को भी उतना ही न्याय चाहिए जितना मुस्लिम महिलाओं को. पुरुष और महिला के अलावा दूसरी लैंगिक पहचानों का क्या होगा? ट्रांसजेंडर लोगों को भी न्याय का अधिकार है. सरकार यह दावा नहीं कर सकती कि वह यूसीसी लाकर लैंगिक न्याय की अनिवार्यता का पालन कर रही है, जबकि वह विवाह में बलात्कार के मुद्दे पर न्याय देने से इनकार कर रही है. विवाह की संस्था को बनाए रखने का यह जुनून क्यों, जब इसकी कीमत महिलाओं की भारी पीड़ा और हिंसा से चुकानी पड़ रही है? ये विरोधाभास कई भारतीयों के लिए विश्वसनीय नहीं हैं. इसके अलावा, सरकार को ज्यादा बातचीत और सलाह-मशविरा करने की जरूरत है. बहुसंख्यक वर्चस्व और अहंकार की भाषा कोई फायदा नहीं देगी. लक्ष्य लैंगिक न्याय है, न कि “मुसलमानों को सबक सिखाना.”
विपक्षी दलों को भारतीय मुसलमानों की बदलती स्थिति को समझने की जरूरत है. उन्हें यह स्वीकार करना चाहिए कि आम मुसलमान महिलाओं के साथ न्याय करना चाहते हैं. इसका प्रमाण तीन तलाक के खिलाफ महिलाओं के नेतृत्व में हुआ आंदोलन था. कुछ राजनीतिक स्वार्थ रखने वाले लोग न तो मुसलमानों के प्रवक्ता हैं और न ही रूढ़िवादी उलेमा.
आखिर में, सभी को यह समझना चाहिए कि यूसीसी का एक रूप पहले से ही मौजूद है—स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के रूप में. इस कानून को मजबूत करने के लिए 30 दिन की पूर्व सार्वजनिक सूचना जैसी समस्याग्रस्त धाराओं को हटाया जा सकता है और इसमें विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, गोद लेने से जुड़े सभी पहलुओं को शामिल किया जा सकता है. इसे प्राथमिकता के आधार पर लोकप्रिय बनाया जाना चाहिए. प्रधानमंत्री मोदी अपने अगले मन की बात में भारतीयों को इस कानून के तहत विवाह करने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं. कुछ वर्षों के बाद, इस संशोधित और बेहतर कानून को सभी के लिए अनिवार्य बनाया जा सकता है.
जकिया सोमन महिला अधिकार कार्यकर्ता और भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन की संस्थापक सदस्य हैं। व्यक्त विचार निजी हैं.
(इस लेख को अंग्रेज़ी में पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)
यह भी पढ़ें: भारत को हफ्ते में 90 घंटे काम वाली नहीं बल्कि चार दिन काम की फ्रांस वाली व्यवस्था चाहिए