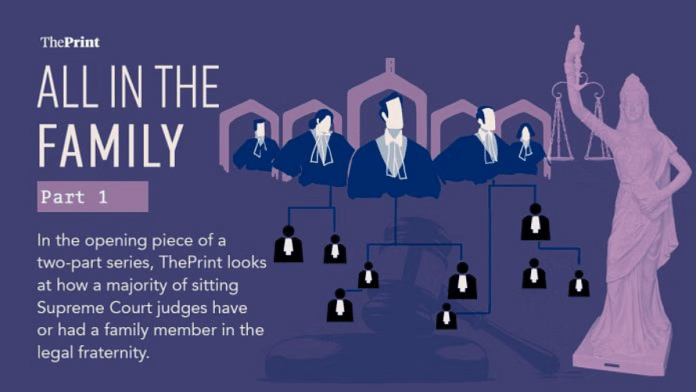नई दिल्ली: दिप्रिंट की एक जांच में पाया गया है कि सुप्रीम कोर्ट के कम से कम 30 प्रतिशत मौजूदा जज पूर्व जजों के रिश्तेदार हैं और अन्य 30 प्रतिशत के माता-पिता या दादा-दादी वकील रहे हैं.
वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में 33 जज हैं, जिनमें भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) संजीव खन्ना भी शामिल हैं.
33 जजों में से कम से कम 10 पूर्व जजों के करीबी रिश्तेदार हैं, जबकि इतने ही न्यायाधीशों के पिता वकील थे. यह जानकारी सार्वजनिक रूप से उपलब्ध संसाधनों और संबंधित उच्च न्यायालयों से प्राप्त की गई है, जहां से जजों को पदोन्नत किया गया, साथ ही सुप्रीम कोर्ट के स्रोतों से भी.
सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस एम. बी. लोकुर इस निष्कर्ष से हैरान नहीं हैं. उन्होंने दिप्रिंट से कहा, “विरासत हर जगह है — मेडिकल, बिजनेस, राजनीति, बॉलीवुड, सिविल सेवा सभी जगह. प्रतिशत अलग-अलग हो सकता है, लेकिन यह मौजूद है.”
वरिष्ठ अधिवक्ता इंदिरा जयसिंह ने कहा, “इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है”. उनका कहना है कि विशेषाधिकार से विशेषाधिकार पैदा होता है, जिसे अब आम तौर पर “विरासत” या “वंशीय उत्तराधिकार” कहा जाता है. हालांकि, उनका कहना है कि न्यायनिर्णयन एक “सार्वजनिक सेवा है, न कि कोई व्यावसायिक उद्यम, इसलिए ऐसा कभी नहीं होना चाहिए था.”
जांच से कानूनी समुदाय के भीतर अंतर्संबंधों के जटिल जाल का भी पता चलता है — एक ऐसा नेटवर्क जो पीढ़ियों और अदालतों में फैला हुआ है.
उदाहरण के लिए सुप्रीम कोर्ट के जज मनोज मिश्रा का मामला ले लीजिए. उनके दादा और पिता दोनों ही इलाहाबाद हाई कोर्ट में प्रमुख वकील थे, जबकि उनके भाई अपुल मिश्रा भी वकील हैं. जस्टिस मिश्रा की पत्नी अभिलाषा मिश्रा वकील राजीव लोचन शुक्ला की चाची हैं, जिन्हें अब सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में पदोन्नति के लिए अनुशंसित किया है. राजीव लोचन शुक्ला इलाहाबाद हाई कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश दिवंगत जस्टिस एम.एन. शुक्ला के पोते हैं.
जस्टिस मिश्रा के दो बेटे रघुवंश और देवांश मिश्रा वकालत कर रहे हैं. अपुल मिश्रा के बेटे देववृत मिश्रा भी वकील हैं. रघुवंश की शादी इलाहाबाद हाई कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस विपिन सिन्हा की बेटी कल्पना सिन्हा से हुई है, जो खुद भी एक विरासत लेकर आए हैं.
न्यायमूर्ति विपिन सिन्हा के पिता न्यायमूर्ति जगमोहनलाल सिन्हा थे, जिन्होंने 1975 में इलाहाबाद हाई कोर्ट का वह फैसला सुनाया था, जिसमें तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के चुनाव को अमान्य घोषित कर दिया गया था. न्यायमूर्ति विपिन सिन्हा के भाई की शादी छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा की बहन से हुई है. दूसरे भाई इलाहाबाद में वरिष्ठ अधिवक्ता हैं.
इसलिए भारतीय न्यायपालिका की जड़ें अक्सर कानूनी पेशे में मजबूती से जमी होती हैं, जिसमें ब्लैक रोब और हथौड़ा अक्सर पीढ़ियों से चला आ रहा है.
हालांकि, न्यायमूर्ति लोकुर का मानना है कि कानूनी या न्यायिक परिवार में पैदा होने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए फायदे के साथ-साथ नुकसान भी हैं. उन्होंने दिप्रिंट से कहा, “एक उत्तराधिकारी को उस माहौल के कारण बढ़त मिलती है जिसमें वह बड़ा हुआ है. मुझे लगता है कि इससे फर्क पड़ता है. दूसरी ओर, उत्तराधिकारी पर सफल होने का दबाव होता है और सभी सफल नहीं होते.”
न्यायमूर्ति लोकुर के अनुसार, कॉलेजियम प्रणाली में कुछ बदलाव लाने की ज़रूरत है, जिसमें “सरकार का रवैया भी शामिल है”.
उन्होंने दिप्रिंट से कहा, “सरकार को मनमाने आधार पर सक्षम वकीलों की नियुक्ति को रोकना या विलंबित नहीं करना चाहिए. सरकार द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला पॉकेट वीटो सबसे दुर्भाग्यपूर्ण है. सरकार कॉलेजियम प्रणाली में एक प्रमुख खिलाड़ी है, और कॉलेजियम प्रणाली की आलोचना करने से पहले उसे अपने घर को भी व्यवस्थित करना चाहिए.”
वरिष्ठ अधिवक्ता वृंदा ग्रोवर का कहना है कि दिप्रिंट के निष्कर्ष “इस बात की पुष्टि करते हैं कि कॉलेजियम द्वारा की गई न्यायिक नियुक्तियां ‘कानूनी अभिजात वर्ग’ के एक छोटे समूह से ही की जाती हैं और इससे यथास्थिति बनी रहती है.”
वरिष्ठ अधिवक्ता दुष्यंत दवे का मानना है कि पेशे में यह पैटर्न काफी बड़ा है. दवे ने दिप्रिंट से कहा, “यह एक तथ्य है और कोई भी इस बारे में नहीं सोच सकता कि इसे कैसे रोका जा सकता है. यह एक व्यवसायी के बेटे के व्यवसायी बनने, एक डॉक्टर के बेटे के डॉक्टर बनने, एक वकील के बेटे के वकील बनने और फिर जज बनने जैसा है.”
हालांकि, उनका कहना है कि मौजूदा नियुक्ति प्रक्रिया “काफी गंभीर रूप से दोषपूर्ण है और इसलिए, यह मौजूदा या पिछले न्यायाधीशों के रिश्तेदारों तक ही सीमित हो जाती है.”
उन्होंने आगे कहा, “इसलिए, इसे व्यापक आधार पर होना चाहिए ताकि अन्य वकील जो समान रूप से अच्छे हैं, या बेहतर नहीं हैं, उन्हें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बनने का मौका मिल सके.”
संभावित सुधारों के बारे में दवे को नहीं लगता कि कॉलेजियम प्रणाली में कोई सुधार किया जा सकता है, क्योंकि “यह व्यक्तिगत पसंद और नापसंद, व्यक्तिगत अहंकार और पक्षपात से गंभीर रूप से ग्रस्त है”.
उन्होंने कहा, “आप जितनी भी मानवीय कमियां सोच सकते हैं, वह सभी कॉलेजियम में शामिल जजों में हैं, इसलिए वह सही फैसला लेने में सक्षम नहीं हैं. कॉलेजियम प्रणाली को एक ज़्यादा प्रभावी संस्था द्वारा प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए, जो इन कमियों से बचते हुए न्यायपालिका की स्वतंत्रता की रक्षा कर सके.”
जैसे माता-पिता, वैसे बच्चे
यह सर्वविदित है कि सीजेआई खन्ना के चाचा सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश एच.आर. खन्ना थे, जिन्हें 1976 में ए.डी.एम. जबलपुर मामले में एकमात्र असहमतिपूर्ण फैसला लिखने के लिए जाना जाता है — जिसमें आपातकाल के दौरान भी व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण के लिए तर्क दिया गया था.
न्यायमूर्ति एच.आर. खन्ना को तत्कालीन इंदिरा गांधी सरकार ने पद से हटा दिया था, जिसने न्यायमूर्ति एम.एच. बेग को अगला सी.जे.आई. घोषित किया था. न्यायमूर्ति संजीव खन्ना के पिता डी.आर. खन्ना भी दिल्ली हाई कोर्ट के न्यायाधीश थे.

वरिष्ठ अधिवक्ता सौरभ कृपाल इस बात से सहमत हैं कि ऐसे रिश्तेदार होने से जो न्यायाधीश या वरिष्ठ वकील भी हो सकते हैं, सिस्टम में नौकरी के लिए घुसना दूसरों की तुलना में बहुत आसान हो जाता है.
पूर्व सीजेआई न्यायमूर्ति बी. एन. कृपाल के बेटे कृपाल का कहना है कि ये आंकड़े टॉप वकील या टॉप न्यायाधीश के बच्चे होने के साथ मिलने वाले सामान्य विशेषाधिकार को दर्शाते हैं.
उन्होंने दिप्रिंट से कहा, “मुझे लगता है कि यह सिर्फ ‘चाचा न्यायाधीशों’ द्वारा अपने बच्चों या दोस्तों को आगे बढ़ाने का मामला नहीं है. मुझे लगता है कि यह सिस्टम के भीतर मौजूद एक प्रणालीगत पूर्वाग्रह का मामला है, जो न केवल उच्च न्यायपालिका के न्यायाधीशों में, बल्कि संभवतः कानून के हर स्तर पर दिखाई देता है और इसमें समस्या है.”
न्यायमूर्ति कृपाल ने नवंबर 1979 से दिल्ली हाई कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में भी काम किया था. उन्हें 1993 में गुजरात हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया. उन्होंने 2002 में सीजेआई के रूप में सेवा देने से पहले सितंबर 1995 में सुप्रीम कोर्ट में अपना रास्ता बनाया.

पूर्व कानून मंत्री वीरप्पा मोइली ने कहा कि 2010 में उन्होंने प्रधानमंत्री, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों और अन्य पूर्व न्यायाधीशों के साथ-साथ कई कानूनी विद्वानों के साथ न्यायपालिका के बारे में दो दिवसीय परामर्श किया था.
उन्होंने दिप्रिंट से कहा, “चर्चा के बाद यह बात सामने आई कि राज्यों के साथ-साथ राष्ट्रीय स्तर पर कॉलेजियम के गठन में तत्काल सुधार की ज़रूरत है…सभी सहमत थे कि नियुक्तियों में कमियां और पक्षपात हुआ है…योग्य लोगों को नहीं लाया जा रहा है. यहां लैंगिक पक्षपात है, जातिगत पक्षपात भी है.”
जयसिंह भी मानती हैं कि अपने वर्तमान स्वरूप में न्यायिक प्रणाली “न्यायपालिका में अन्य सभी हाशिए पर पड़े समुदायों की तुलना में उच्च जाति के प्रतिनिधित्व को जन्म देती है”.
उन्होंने दिप्रिंट से कहा, “न्यायाधीशों के कुछ रिश्तेदारों के लिए, इस प्रणाली के बहुत फायदे हैं. हमारे यहां ‘अंकल जज’ की परिघटना है, वैसे ‘आंटी जज’ की नहीं.”
ग्रोवर का कहना है कि न्यायपालिका को जिन मुद्दों पर फैसले लेने के लिए कहा जाता है, उनकी व्यापकता और गहराई को देखते हुए, “यह ज़रूरी है कि उच्च न्यायपालिका न केवल क्षेत्रीय विविधता को प्रतिबिंबित करे, बल्कि इससे भी महत्वपूर्ण रूप से दृष्टिकोण और अनुभवों की बहुलता को प्रतिबिंबित करे”.
उदाहरण के तौर पर, वे बताती हैं कि न्यायिक नियुक्तियों के लिए कानून के विभिन्न कानूनी क्षेत्रों में विशेषज्ञता पर ध्यान दिया जाता है, लेकिन लिंग, धर्म, जाति और आदिवासियों से संबंधित मुद्दों में, “नियुक्तियां वास्तविक होने के बजाय प्रतीकात्मक होती हैं”.
ग्रोवर ने जोर देकर कहा, “नियुक्तियों के मानदंड अत्यंत संकीर्ण हैं और गणतंत्र की जटिलता का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं.”
अपवाद
हालांकि, शीर्ष अदालत के सभी न्यायाधीश कानूनी पेशे से जुड़े नहीं हैं. दिप्रिंट को कम से कम चार ऐसे न्यायाधीश मिले जिनके माता-पिता सिविल सेवक, राज्यपाल और यहां तक कि कवि भी रहे हैं.

विरासत को आगे बढ़ाना
अपने खुद के अनुभव को याद करते हुए कृपाल ने कहा कि जब उन्हें नौकरी चाहिए थी, तो उन्होंने अपने पिता से एक वरिष्ठ वकील को फोन करवाया, जिसके साथ वे काम करना चाहते थे.
उन्होंने दिप्रिंट को बताया, “तथ्य यह है कि मैंने ऑक्सफोर्ड से दो बार पहला स्थान हासिल किया, मैंने कैम्ब्रिज में अपनी यूनिवर्सिटी में टॉप किया था, मैं सेंट स्टीफंस कॉलेज में मेरिट लिस्ट में था — इनमें से किसी भी चीज़ से किसी व्यक्ति को नौकरी पर रखने में कोई फर्क नहीं पड़ता. इसलिए मेरी शैक्षणिक योग्यताएं वह कारण नहीं हैं जिसके कारण मुझे वह नौकरी मिली, भले ही मेरे पास वह हो…मैं बस भाग्यशाली था.”
उन्होंने कहा कि उस समय उनके पिता एक न्यायाधीश थे, यह स्पष्ट रूप से समझा जाने वाला प्रस्ताव था कि एक न्यायाधीश का बच्चा उस अदालत में प्रैक्टिस नहीं करेगा जहां माता-पिता मौजूद हैं. कृपाल ने कहा, यह “दुख की बात है कि अब ऐसा कुछ नहीं हो रहा है जो अब उतना हो रहा है जितना होना चाहिए”.
“इसलिए जब मेरे पिता सुप्रीम कोर्ट में थे, तो मैं सुप्रीम कोर्ट में घुस भी नहीं सकता था.”
दरअसल, कृपाल ने बताया कि जब उनके पिता सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बने, तो उन्होंने तीन साल के लिए वकालत छोड़ दी. “2000 से 2003 तक, जब वे शीर्ष न्यायाधीश थे, मैं जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र के साथ काम कर रहा था. इसलिए, मैंने यह सुनिश्चित करने के लिए देश छोड़ दिया कि ईमानदारी बनी रहे और कोई किसी पर उंगली न उठा सके.”
हालांकि, ऐसा लगता है कि अब ऐसा नहीं है. वर्तमान में, सुप्रीम कोर्ट के कम से कम 60 प्रतिशत न्यायाधीशों के बच्चों ने कानून की पढ़ाई की है, जिनमें से कुछ दिल्ली और देश भर की विभिन्न अदालतों में प्रैक्टिस कर रहे हैं, यह जानकारी सुप्रीम कोर्ट और विभिन्न हाई कोर्ट के सूत्रों से मिली है, जहां ये बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं.
पद्मेश मिश्रा के मामले में हाल के दिनों में उनकी वंशावली ने सुर्खियां बटोरी हैं. पिछले साल, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश प्रशांत कुमार मिश्रा के बेटे पद्मेश को राजस्थान का अतिरिक्त महाधिवक्ता (एएजी) बनाया गया था. उनकी नियुक्ति राज्य की मुकदमेबाज़ी नीति में संशोधन के साथ हुई थी, जिसके तहत राज्य सरकार को 10 साल के अनुभव के मानदंड का पालन किए बिना किसी को भी पद पर नियुक्त करने की अनुमति दी गई थी.
मिश्रा की नियुक्ति के साथ-साथ मुकदमेबाज़ी नीति में जोड़े गए खंड को भी चुनौती दी गई थी. हालांकि, राजस्थान हाई कोर्ट की एकल न्यायाधीश पीठ ने इस चुनौती को खारिज कर दिया, लेकिन अब इस आदेश को चुनौती देने वाली अपील हाई कोर्ट की दो न्यायाधीशों वाली पीठ के समक्ष दायर की गई है.

जयसिंह का कहना है कि किसी भी जज ने इस समस्या को हल करने की कोशिश नहीं की है, जहां न्यायाधीशों के बेटे और बेटियां उसी कोर्ट में पेश होते हैं जिसमें उनके पिता न्यायाधीश हैं, “इस झूठे तर्क पर कि वह अपने पिता से दूर रहते हैं”.
न्यायाधीश या वकील के परिवार से संबंधित होने के साथ आने वाले विशेषाधिकार को स्वीकार करते हुए, कृपाल उन धारणाओं की ओर इशारा करते हैं जो न्यायाधीश के बेटे या बेटी को न्यायालय में ले जा सकती हैं, जो उनके लिए “नुकसानदायक” हो सकता है.
किरपाल “नुकसान” के बारे में एक-दो बातें जानते हैं. 2017 में, उनका नाम पहली बार HC कॉलेजियम द्वारा 2017 में दिल्ली हाई कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में पदोन्नति के लिए प्रस्तावित किया गया था. तब से उनकी उम्मीदवारी सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम और सरकार के बीच विवाद का विषय रही है — बाद में उनके साथी के स्विस नागरिक होने और “उनके अंतरंग संबंध” और “उनके यौन अभिविन्यास” के बारे में खुलेपन पर आपत्ति जताई गई.
उन्होंने कहा कि कानूनी हलकों में यह धारणा है कि उनके नाम की सिफारिश सिर्फ इसलिए की गई क्योंकि जस्टिस डी. वाई. चंद्रचूड़ के पिता वाई. वी. चंद्रचूड़ ने अपने पिता को जज नियुक्त किया था. किरपाल ने दिप्रिंट से कहा, “बेशक, इसमें से कुछ भी सच नहीं है, क्योंकि जब मेरे पिता को नियुक्त किया गया था, तब कोई कॉलेजियम सिस्टम नहीं था, लेकिन लोगों के लिए यह मायने नहीं रखता. वह किसी व्यक्ति की किसी भी उपलब्धि को अपने आप ही कमतर आंकते हैं और उसे नीचा दिखाते हैं, क्योंकि वह बस कहेंगे कि आप एक जज के बच्चे हैं.”
1990 के दशक में सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के ज़रिए कॉलेजियम सिस्टम लाए जाने से पहले, कॉलेजियम सिस्टम की स्थापना से पहले के वर्षों में न्यायिक नियुक्तियों में कार्यपालिका का प्राथमिक अधिकार था. इसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश के साथ “परामर्श” करके मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्तियां की जाती थीं.
यह भी पढ़ें: नियामगिरी से कश्मीर तक: परिवारवालों को राहुल गांधी की संवेदनाओं से कांग्रेस को क्या कुछ हासिल हुआ
‘घर में झांकना’
न्यायिक नियुक्तियों में मौजूदा खामियों पर आम सहमति होने के बावजूद, न्यायपालिका में अधिक विविधता लाने के मुद्दे पर कानूनी बिरादरी के बीच अलग-अलग राय है.
वरिष्ठ अधिवक्ता विकास सिंह कहते हैं कि कॉलेजियम प्रणाली के साथ उनकी शिकायत यह रही है कि वह “घर में झांकते रहे हैं”.
सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष ने दिप्रिंट से कहा, “मैं यह नहीं कह रहा हूं कि उनके बच्चे पदोन्नति के हकदार नहीं हैं, लेकिन पदोन्नति की प्रक्रिया में, आप केवल उन लोगों को देखते हैं जिन्हें आप जानते हैं या जिनके बारे में आपने सुना है…यही कारण है कि कॉलेजियम प्रणाली विश्वसनीयता खो रही है. इस अंदरूनी नज़र के कारण, स्वतः ही पूर्वाग्रह और पक्षपात आ जाते हैं.”
सिंह नियुक्ति की मौजूदा प्रणाली को फिर से बनाने पर जोर देते हैं, जिसमें विशिष्ट मानदंड बताए गए हैं कि कौन न्यायाधीश बन सकता है.
जयसिंह का मानना है कि कॉलेजियम में सुधार या पुनर्गठन ज़रूरी है. उन्होंने दिप्रिंट से कहा, “न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाने चाहिए और व्यक्ति के बारे में सार्वजनिक रूप से विचार किया जाना चाहिए.”
ग्रोवर के अनुसार, वे राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (एनजेएसी) जैसे विकल्प के बजाय कॉलेजियम प्रणाली का समर्थन करती हैं, लेकिन वे एक चेतावनी भी देती हैं: “अगर कॉलेजियम प्रणाली को प्रासंगिक बने रहना है और जनता का विश्वास बनाए रखना है तो उसे न्यायिक नियुक्तियों में शामिल मानदंडों और विचारों को फिर से परिभाषित करना होगा. अब वक्त आ गया है कि न्यायिक नियुक्तियों को संवैधानिक सिद्धांतों और लक्ष्यों के साथ जोड़ा जाए, जिसमें विशेषाधिकार को खत्म करना और उच्च न्यायपालिका की संरचना को लोकतांत्रिक बनाना शामिल है.”
हालांकि, किरपाल इन आंकड़ों को कानूनी पेशे में प्रवेश स्तर पर बहिष्कार की समस्या के रूप में देखते हैं. वे बताते हैं, “जब कोई वरिष्ठ व्यक्ति प्रवेश स्तर के व्यक्ति को केवल 20,000 रुपये या 15,000 रुपये का भुगतान करता है, तो यह भी एक समस्या है. हमारे सामने जो मूल समस्या है, वह कानूनी पेशे में अभिजात्यवाद है और यह समझने की इस प्रक्रिया से दूर नहीं हो सकता कि शीर्ष पर क्या हो रहा है.” योग्य वकील वकीलों को बेहतर पहुंच और अवसर प्रदान करना उनका सुझाव है. “यह बहुत हद तक पुराने लोगों का नेटवर्क है कि आप शीर्ष वरिष्ठों या अच्छे वरिष्ठों के चैंबर में कैसे स्थान पाते हैं.”
जबकि कॉलेजियम प्रणाली के अधिकांश आलोचक राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (एनजेएसी) की तर्ज पर एक विकल्प का सुझाव देने में जल्दी करते हैं, किरपाल को नहीं लगता कि इससे अधिक समावेशी न्यायपालिका की गारंटी होगी.
उन्होंने ज़ोर दिया, “यह भारत की समस्या है. हर बार जब कोई राजनेता सत्ता में आता है, तो यह एक वंशानुगत घटना बन जाती है. न्यायाधीशों के साथ भी यही होगा. हमें हल निकालना होगा और इसका एकमात्र जवाब वकीलों का एक असाधारण समूह प्राप्त करना है.”
(इस रिपोर्ट को अंग्रेज़ी में पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)
(यह दिप्रिंट की दो पार्ट की सीरीज़ की पहली रिपोर्ट है.)
यह भी पढ़ें: ED ने 1,000 करोड़ के FEMA उल्लंघन की जांच में ‘एम्पुरान’ के सह-निर्माता की कंपनी पर मारा छापा