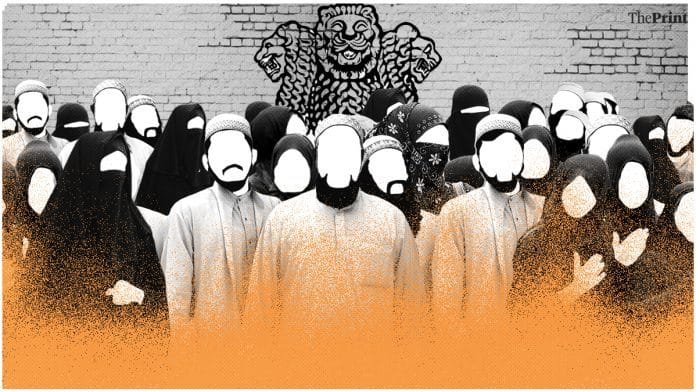इस्लाम में जातियां और उसमें विभाजन होने की बात उसके कुछ कर्मकांडों और प्रथाओं से खूब जगजाहिर होती है. कुफू के बारे में बात हो या फिर जुमे की नमाज से पहले पढ़े जाने वाले खुतबे की, हर किसी की अवधारणाएं अलग-अलग हैं. ये और कई अन्य प्रथाएं मुस्लिम समाज के एक खास वर्ग-अशराफ- के पक्ष में झुकी हुई हैं. पसमांदाओं के खिलाफ अंतर्निहित भेदभाव को समझने के लिए हम उन्हें एक-एक करके देखते हैं.
कुफ़ु का सिद्धान्त
कुफ़ु का शाब्दिक अर्थ बराबरी, समान और मेल के होता है. इस्लाम में कूफ़ु का मतलब होता है कि शादी विवाह के लिए कौन-कौन एक समान या एक मेल या एक बराबर के हैं. कुफु के लिए कई शर्तें हैं. यहां तक कि अशराफ उलेमाओं में भी इस बात को लेकर मतभेद हैं. जहां कुछ तीन बिंदु तो मानते हैं वहीं कुछ चार, पांच या सात को भी मानते हैं. लेकिन लगभग सभी के नज़दीक नसब/नस्ल/जाति का बिंदु ज़रूर मिलता है.
जिसमें स्पष्ट रूप से वर्णन किया गया है कि अमुक जाति की कन्या अमुक नस्ल/जाति के वर के लिए बराबर है (कूफ़ु है) और अमुक के लिए बराबर नही है, अर्थात नस्लीय/जातिगत विभेद को पूर्णतः मान्यता प्रदान की गई है और अंतरजातीय विवाह को इस्लाम विरोधी और ऐसे सम्पन्न विवाह को अमान्य करार दिया गया है.
इस्लामी विधि के चार बड़े सर्वमान्य मसलको (सम्प्रदायों) में से तीन मसलक इसकी मान्यता देते हैं जबकि इमाम मालिक द्वारा संपादित मसलक जाति आधारित कूफ़ु का विरोध करता है और विवाह के लिए धार्मिक कर्तव्य परायणता को वरीयता देता है.
यह भी पढ़ें: नस्लीय भेदभाव को अच्छे से समझते थे पैगम्बर मोहम्मद, इसलिए इसे खत्म करने की पूरी कोशिश की
जुमा का ख़ुत्बा
शुक्रवार (जुमा) को प्रार्थना (नमाज़/ सला) से पहले दिया जाने वाला उपदेश जुमे का ख़ुत्बा (उपदेश) कहलाता है. जुमे के ख़ुत्बे को लेकर अशराफ उलेमा में विरोधाभास देखने को मिलता है, लेकिन नस्लीय/जातीय श्रेष्ठता लगभग सभी फिरके और मसलको (सम्प्रदायों) के ख़ुत्बे में पाया जाता है. इस ख़ुत्बे में भी एक विशेष जनजाति क़ुरैश के लोगों और फिर उसमें भी क़ुरैश की उप जनजाति बनू फातिमा (मुहम्मद की सबसे छोटी बेटी फातिमा के वंशज; फातमी सैयद, सैयदों में सब से पवित्र और उच्च माने जाते हैं) के लोगो का ही गुणगान होता है, विशेषतया फातिमा और उनके बेटे हसन और हुसैन लगभग सभी ख़ुत्बो में कॉमन है, कुछ ख़ुत्बे में पहले चारो खलीफाओं और मुहम्मद(स०) के चाचाओं का वर्णन भी मिलता है.
यहां यह बात ध्यान देने की है कि जुमे की नमाज़ सर्वप्रथम एक अंसारी सहाबी (मुहम्मद के साथी) असद बिन जरारा (र०) ने प्रारम्भ किया था लेकिन किसी भी मसलक/फ़िरके के ख़ुत्बे में उनका नाम नहीं लिया जाता है.
दूसरी एक और बात गौर करने की है कि ना तो मुहम्मद (स०) की किसी दूसरी बेटियों का नाम और ना ही उनकी किसी सन्तान का नाम किसी भी प्रकार के ख़ुत्बे में दर्ज है. यहां तक कि अंसार सहाबा (ओवेस और खजरज जनजाति के मुहम्मद के साथियों) का भी वर्णन नहीं होता है जिनका इस्लाम के लिए दिए गए बलिदान से किसी को इनकार नहीं है.
दरूद व सलाम
प्रत्येक नमाज़ (प्रार्थना) में पढ़ा जाने वाला दरूद (एक प्रकार का अरबी भाषा मे लिखा गया मंत्र) में भी इब्राहिम और उसके आल ( सन्तानों) और मुहम्मद और उसके आल (सन्तानों) के लिए शांति की प्रार्थना की गई है. अशराफ उलेमा दरूद से क़ुरैश और सैयद जाति (मुहम्मद के वंशज) के उच्च होने की दलील लाते है और कहते है कि सैयदों के लिए तो पूरी दुनिया के मुसलमान हर नमाज़ में दुआ करते हैं.
जबकि कुछ पसमांदा उलेमा ने इस्लाम के जातिवादी रहित चरित्र की रक्षा करते हुए इस दरूद की व्याख्या करते हुए ‘आल’ शब्द का अनुवाद सन्तान से ना करके इब्राहिम और मुहम्मद के मानने वाले सारे मुसलमानो से किया है और दलील के रूप में क़ुरआन की उस पंक्तियों का उद्धरण करते है जिसमें आल शब्द का अर्थ सन्तान के अर्थ में ना होकर उसके मानने वाले और अनुयायी से है.
फ़िरक़ा/मसलक
अशराफ ने फ़िरके बनाया ही अपनी सरदारी और वर्चस्व को मेन्टेन रखने के लिए. जिस अशराफ को उक्त फिर्के में सरदारी नही मिली उसने तुरंत एक नया फ़िरक़ा गढ़ लिया और उसका सरदार बन बैठा और यह सरदारी, भगवान के दर्जे तक की होती है कि फिर्के के अशराफ संस्थापक हर तरह के सवाल जवाब से मुक्त और तमाम इंसानी कमी कोताही से पाक समझा जाता है और उस पर सवाल उठाने वाले और अलोचना करने वालों को इस्लाम से बाहर का (काफिर/कुफ्र का फतवा देकर) रास्ता दिखा दिया जाता है. दूसरे पसमांदा अपने मानने के जज़्बे के साथ सभी फिर्को का इतना मज़बूत सिपाही बन जाता है कि अपनी जान तक देने को तैयार रहता है इसीलिए आपसी फिरको की लड़ाई में खून सिर्फ पसमांदा का बहता है और वर्चस्व अशराफ की मैंटेन रहता है.
यही अशराफ फिर्के को लेकर स्वयं इतना लिबरल (उदार) और नस्ल/जाति को लेकर इतना कट्टर होता है कि एक फिर्के का अशराफ दूसरे फिर्के के अशराफ से रिश्ता करने में ज़रा भी नही हिचकिचाता ( जिसे स्वयं काफिर घोषित किये हुए है) जबकि पसमांदा के मन-मस्तिष्क में फिरकापरस्ती का ऐसा वायरस पेवस्त किये हुए हैं कि एक ही जाति का पसमांदा उसी जाति के दूसरे मसलक/फिर्के के मानने वाले पसमांदा से शादी विवाह का रिश्ता नही रखता. (क्योंकि दूसरे फिर्के वाले को पहले फिर्के के अशराफ मौलवी ने काफिर घोषित कर रखा है, और काफिर से वैवाहिक सम्बन्ध को वर्जित/हराम करार दे रखा है).
एक दृष्टिकोण यह भी है कि अशराफ उलेमा द्वारा आसिम बिहारी के आंदोलन को कमज़ोर करने और पसमांदा की एकता को तोड़ने के लिए इस्लामी मसलक/ फिर्के का खेल खेला गया और इस्लाम की कई एक व्याख्या करते हुए देवबन्दी, बरेलवी, अहले हदीस आदि नामों से फिर्के और मसलक बनाये गए जिसका नेतृत्व आजतक अशराफ उलेमा ने अपने पास रखा.
अशराफ का पक्ष
अशराफ द्वारा नस्लवाद/जातिवाद के पक्ष में यह तर्क दिया जाता है कि जातियां कभी भी ख़त्म नहीं हो सकती क्योंकि क़ुरान में है कि जातियां पहचान के लिए बनाई गईं हैं.
अधिकतर अशराफ उलेमा का यह अक़ीदा (आस्था) है कि वंश/जाति पर गर्व करना यद्यपि हराम (वर्जित) है, लेकिन इसका मतलब यह नही कि वंश/जाति की श्रेष्ठता कोई चीज़ ही नही और यह एक ईश्वरी उपहार (नेमत) है.
मुहम्मद (स०) के कथनों (हदीसो) के परस्पर विरोधाभास का लाभ उठाकर अशराफ उनके दोनों कथनो का प्रयोग समय और स्थितियों के अनुरूप अपने हित के अनुसार करता है. एक अजीब बात है कि जो इस्लामी विद्वान नस्लवादी/जातिवादी हदीसो को गढ़ा(बनाया) हुआ हदीस मानते है उन्होंने भी कभी उन हदीसों को हदीस की किताबों से बाहर नहीं निकाला है. बल्कि आज भी ऐसी सभी हदीसें सुरक्षित रखे गए हैं.
पसमांदा पक्ष
पसमांदा आंदोलन से जुड़े कुछ पसमांदा कार्यकर्ता क़ुरान की नस्लवादी/जातिवादी व्याख्या और मुहम्मद के नस्लवादी/जातिवादी कथनों को अशराफ द्वारा गढ़ा/ तोड़ मरोड़ किया हुआ मानते हैं. और वो क़ुरान और मुहम्मद(स०) के अन्य नस्लवादी/जातिवाद विरोधी कथनों (हडीसों) को सत्य मानकर मुहम्मद(स०) के आखिरी उद्बोधन जिसमें नस्लवाद/ जातिवाद का प्रबल विरोध है, को पसमांदा आंदोलन का नीति पत्र मानते हैं.
यह भी पढ़ें: कैसे अशराफ उलेमा पैगंबर के आखिरी भाषण में भ्रम की स्थिति का इस्तेमाल जातिवाद फैलाने के लिए कर रहे
उपसंहार
आलेख के अब तक के सभी भागों के विवरण से ये साफ पता चलता है कि इस्लाम में नस्लवाद/जातिवाद का कांसेप्ट भले ही क़ुरान में और मुहम्मद (स०) के चरित्र में ना रहा हो और उन्होंने अपने जीवन काल और सुधारवादी कार्यक्रम में जातिवाद/नस्लपरस्ती का विरोध किया हो लेकिन उनके जाने के बाद से ही ये इब्लीसवादी/शैतानी प्रवृति इस्लाम का हिस्सा रहा है.
आज भी मुस्लिम समुदाय के सभी राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय मामले में नस्लीय/जातीय अस्मिता और श्रेष्ठता को वरीयता दिया जाता है इसीलिए एक खास जनजाति/नस्ल/कबिले (कुरैश-सैयद, शेख) के ही लोग सभी संस्थाओ और संगठनों एवं देश/ राज्य के मालिक/अधिकारी हैं. शादी विवाह के लिए इस्लामी फ़िक़्ह(विधि) में “कूफ़ु” का सिद्धान्त नस्लीय/जातीय बन्धन को मान्यता देता है.
इस्लाम में सैद्धान्तिक रूप से जातिवाद है कि नही यह एक इल्मी बहस तो हो सकती है लेकिन जहाँ तक सामाजिक परिवर्तन और सामाजिक न्याय का सवाल है यह बात कही जा सकती है कि इस समय संसार मे जो इस्लाम प्रचलित है वो पूरी तरह से नस्लवाद/जातिवाद की कैद में है. प्रोफेसर शफीउल्लाह अनीस अपनी कविता के माध्यम से इसी बात को कुछ यूँ बयान करते हैं.
इस्लाम दो है
एक जो आसमान में है
और एक वह जो ज़मीन पर
हक़ीक़त क्या है
मैं क्या जानूं
खून आसमान में तो नहीं बहता
गाली आसमान में नहीं पड़ती
ज़ाति का फ़र्क़
नस्ल का भेद
यह सब क्या तिलिस्म है?
फरेब है?
माना के आसमानी इस्लाम में यह सब नहीं
क्या इसी बात से तसल्ली कर लूं मैं
माना के आसमानी इस्लाम में यह सब नहीं
मगर मैं आसमान में नहीं रहता
मेरी हक़ीक़त यहीं है
इसी ज़मीन पर
जिस इस्लाम के पहले खलीफा की नियुक्ति नस्ल के आधार पर होती है, उसका पारितोषिक नस्ल और क्षेत्र के आधार पर तय होता है, तीसरे खलीफा की हत्या नस्ल के आधार पर होती और जुम्मे का ख़ुत्बे में एक नस्ल/जनजाति विशेष की महत्ता का बखान हो, शादी विवाह के लिए जातीय बंधन हो, वो इस्लाम कैसे नस्लवाद/जातिवाद रहित होने का दावा कर सकता है.
पुरुषोत्तम अग्रवाल अपने लेख ‘मुस्लिम राजनीति में नया मोड़’ में लिखते हैं कि सच्चाई यह है कि इस्लाम का उदय तो हुआ सभी अनुयायियों की बराबरी और उनके आपसी भाईचारे के ईश्वरी सिद्धान्त मानते हुए, लेकिन जैसे जैसे इस्लाम मध्यकालीन सामंती सत्ता तन्त्रो से जुड़ता गया वैसे-वैसे सिद्धान्त और व्यवहार में खाई बढ़ती चली गयी. सिद्धान्त भाईचारे का ही रहा, व्यवहार सामंती समाज मे स्वीकृत जन्मजात ऊंच नीच के अनुकूल होता गया, सुल्तानों का इस्लाम पैग़म्बर के इस्लाम से जुदा हो गया.’ (दैनिक सहारा नई दिल्ली, 23.09.1996)
कुल मिला के यह कहा जा सकता है कि इस्लाम दो तरह का है एक अशराफ का इस्लाम और दूसरा पसमांदा का इस्लाम. पसमांदा ऊंच नीच रहित मुहम्मद (स०) के सैद्धान्तिक इस्लाम की वकालत करता है वहीं अशराफ अपने द्वारा व्याखित इस्लाम को ही इस्लाम मानता है और उसे ही पसमांदा पर थोपे हुए है. और विडम्बना यह है कि अशराफ का इस्लाम ही समाज में मान्य और प्रचलित है.
(यह दिप्रिंट-इस्लाम डिवाइडेड में चार-भाग की श्रृंखला का ये आखिरी भाग है)
(लेखक, अनुवादक स्तंभकार मीडिया पैनलिस्ट सामाजिक कार्यकर्ता और पेशे से चिकित्सक हैं. व्यक्त विचार निजी हैं)
यह भी पढ़ें: क्या वाकई इस्लाम में समता का सिद्धांत है? क्योंकि खलीफ़ा बनने का अधिकार सिर्फ कुरैश को है