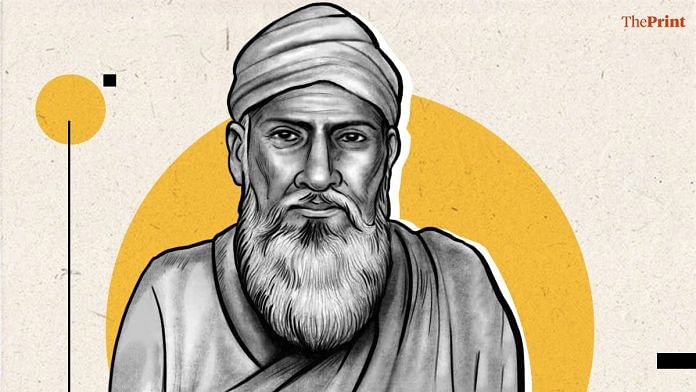अठारह सौ सत्तावन में लड़े गये देश के पहले स्वतंत्रता संग्राम के अवध के सबसे बड़े नायक मौलवी अहमदउल्ला शाह का आज 164वां शहादत दिवस है. उनका यह शहादत दिवस इस अर्थ में बहुत खास है कि इस बार हमारे पास उन्हें याद करने के दो अतिरिक्त बड़े कारण हैं. पहला यह कि देश में राजनीतिक कारणों से पैदा की जा रही साम्प्रदायिक घृणा के बीच नई पीढ़ी का यह जानना पहले से ज्यादा जरूरी हो चला है कि उस संग्राम को हिन्दुओं व मुसलमानों ने कंधे से कंधा मिलाकर लड़ा था और अंग्रेज लाख जतन करके भी उनकी एकता को खंडित नहीं कर पाये थे.
दूसरा कारण यह कि अयोध्या के रामजन्मभूमि-बाबरी मस्जिद विवाद के सुप्रीम कोर्ट के नौ नवम्बर, 2019 फैसले के मुताबिक मुस्लिम पक्ष को जो पांच एकड़ भूमि प्रदान की गई है, उस पर निर्माणाधीन मस्जिद को इन्हीं मौलवी अहमदउल्ला शाह का नाम दिया गया है. दरअसल, मस्जिद निर्माण के लिए बने ट्रस्ट ने मस्जिद के साथ जोड़ने के लिए किसी ऐसी शख्सियत का नाम तलाशना शुरू किया, जो इस विवाद के कारण हिन्दुओं-मुसलमानों के बीच पैदा हुई दूरियों के बरक्स दोनों के बीच सद्भाव व सौमनस्य का वायस बन सके तो उसे मौलवी से बेहतर कोई नाम मिला ही नहीं. इसलिए उसने अपनी मस्जिद को ‘मौलवी अहमद उल्लाह शाह मस्जिद’ कहना ही पसन्द किया.
रोटी और कमल
दरअसल, 1857 में मौलवी ने अपनी संगठन शक्ति को शंकरपुर (रायबरेली) के राणा वेणीमाधो सिंह की रणशक्ति के साथ मिलाकर हिन्दू मुस्लिम एकता की बेल को इतना सींचा था कि उसमें सब कुछ साझा हो गया था. जानकारों के अनुसार मौलवी देश के पहले ऐसे शख्स थे, जिनके द्वारा बांटे गये बगावत के पर्चे में अंग्रेजों को काफिर कहा गया था.
उन दिनों छावनी-छावनी और शहर-शहर साधु-फकीरों, सिपाहियों व चैकीदारों के जरिये रोटी व कमल का जो फेरा लगता था, वह भी मौलवी की ही सूझ थी. किसी गांव या शहर में बागियों की तरफ से जो रोटियां आती थीं, उन्हें खाकर वैसी ही दूसरी ताजा रोटियां बनवाकर दूसरे गांवों या शहरों को रवाना कर दी जाती थीं. रोटियां खाने वालों के निकट इसका अर्थ होता था कि हम भी गदर में शामिल हो गये हैं. इस शामिल होने में जाति व धर्म का कोई भेदभाव नहीं था.
यह भी पढ़ें: ‘खून के धब्बे धुलेंगे कितनी बरसातों के बाद’- राजनीतिक सत्ता में बैठे हुक्मरानों को फैज़ से डर क्यों
हम जानते हैं कि 1857 में इस संग्राम की शुरुआत 31 मई को होनी थी, मगर मेरठ के सिपाहियों का खून दस मई को ही उबाल खा गया, जिससे अंग्रेज संभल गये और संग्राम की योजना थोड़ी गड़बड़ा गई. फिर भी वह शुरू हुआ तो अवध में लगा कि अब अंग्रेजी राज का कोई नामलेवा नहीं बचेगा. जानना दिलचस्प है कि तब आमने-सामने की कई लड़ाईयां हारने के बाद अंग्रेज मौलवी को ‘फौलादी शेर’ कहने लगे थे. अवध की पुरानी राजधानी फैजाबाद (अब अयोध्या) को मुख्य कर्मभूमि बनाने के कारण ‘फैजाबादी’ शब्द मौलवी के नाम से ऐसा जुड़ गया था कि कई इतिहासकारों ने उन्हें फैजाबाद का ही कोई पदच्युत तालुकेदार या जमीनदार समझ लिया है. वे जब भी किसी अभियान पर निकलते, उनके आगे-आगे डंका अथवा नक्कारा बजता रहता था. इसलिए कुछ लोग उन्हें नक्कारशाह व डंकाशाह भी कहते हैं.
अब, कुछ लोग उनकी वंशावली की तलाश में भी ‘बेचैन’ हो रहे हैं, लेकिन कहते हैं कि मौलवी को आत्मप्रचार में कतई कोई दिलचस्पी नहीं थी. वे एक सूफी संत की इस शिक्षा को अपने जीवन का उद्देश्य बताते थे कि सीने में सांस रहते नाइंसाफी को मंजूर नहीं करना है. इसी के तहत अंग्रेजों की नाइंसाफी से लड़ने के लिए फरवरी, 1857 में, जब स्वतंत्रता संग्राम की सुगबुगाहट तक नहीं थी, उन्होंने फैजाबाद (अब अयोध्या) में अपना सशस्त्र जमावड़ा शुरू किया तो सशंकित अंग्रेजों ने उनसे अपने हथियार सौंप देने को कहा. इससे इनकार कर देने पर उन्हें कई प्रलोभन दिये गये. फिर भी वे नहीं माने तो उनकी गिरफ्तारी के आदेश दे दिये गये. अवध की पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार करने से मनाकर दिया तो अंग्रेजी फौज आयी, जिसने 19 फरवरी, 1857 को उन्हें न सिर्फ पकड़ लिया, बल्कि जंजीरों में बांधकर फैजाबाद शहर में घुमाया. बाद में मुकदमे का नाटक कर उन्हें फांसी की सजा सुना दी गयी.
लेकिन आठ जून, 1857 को बागी देसी फौज ने जेल पर हमला करके वहां बंद मौलवी को छुड़ाकर अपना चीफ चुन लिया. उसने उसकी आमद में तोपें भी दागीं. भरपूर जश्न के बाद मौलवी ने इस फौज की कमान संभाल ली और फैजाबाद को आजाद कराने के बाद राजा मान सिंह को उसका शासक बनाया. गौरतलब है कि मान सिंह को शासक बनाना भी उनके हिन्दू-मुस्लिम एकता के प्रयत्नों के ही तहत था.
फैजाबाद का मोर्चा जीतने के बाद मौलवी ने तत्कालीन आगरा व अवध प्रांत में घूमघूम कर क्रांति की ज्वाला जगायी. कई इतिहासकारों ने लिखा है कि लखनऊ नगर के अन्दर क्रांति के सबसे योग्य नेता मौलवी ही थे. होम्स ने मौलवी को ‘उत्तर भारत में अंग्रेजों का सबसे जबरदस्त शत्रु’ बताया है. अंग्रेजों के दुर्भाग्य से उनका यह शत्रु पूरी तरह जनता का आदमी था, लेकिन इसी कारण कई रईसों, राजाओं और नवाबों को उनकी आज्ञाओं का पालन करने में हिच होती थी.
परास्त होना तो जैसे मौलवी ने सीखा ही नहीं था. कई बार बागियों को पीछे हटना पड़ा तो मौलवी ने उन्हें छापामार लड़ाई की रणनीति प्रदान की. अंग्रेज आमने-सामने की लड़ाइयों में भी उतने आतंकित नहीं हुए थे, जितने इन छापामार मुकाबलों से हुए. 15 जनवरी, 1858 को गोली से घायल होने के बावजूद मौलवी का मनोबल नहीं टूटा और 21 मार्च, 1858 को लखनऊ के पतन के बाद भी उन्होंने शहर के केन्द्र में अंग्रेजों सेना से दो-दो हाथ किये. वहां से निकले तो अंग्रेज छः मील तक पीछा करके भी उनके पास नहीं फटक सके.
यह भी पढ़ें: जब तक जनता ‘राजनीतिक उपभोक्ता’ बनी रहेगी, उसे ऐसे ही महंगाई झेलनी पड़ेगी!
मौलवी के सिर की कीमत 50,000 रुपये
स्वतंत्रता संग्राम के पूरी तरह विफल हो जाने के बाद भी मौलवी शाहजहांपुर को अपनी गतिविधियों का केन्द्र बनाकर अंग्रेजों की नाक में दम करते रहे. अंग्रेजों ने उन्हें पकड़ने और मार देने की कई साजिशें रचीं मगर सबमें असफल रहे. बाद में उन्होंने उनके सिर की कीमत रखी पचास हजार रुपये. पचास हजार रुपये आज के नहीं, 1858 के.
इन्हीं रुपयों के लालच में शाहजहांपुर जिले की पुवायां रियासत के विश्वासघाती राजा जगन्नाथ सिंह के भाई बलदेव सिंह ने 15 जून, 1858 को तब धोखे से गोली चलाकर मौलवी की जान ले ली, जब वे अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष में मदद मांगने उसकी गढ़ी पर गये थे. उसने मौलवी का सिर कटवाकर रूमाल में लिपटवाया और शाहजहांपुर के कलेक्टर को सौंपकर मुंहमांगी कीमत वसूल ली.
कलेक्टर ने उस सिर को शाहजहांपुर कोतवाली के फाटक पर लटकाकर प्रदर्शित किया ताकि जो लोग उसे देखें, आगे सिर उठाने की जुर्रत न करें. मगर कुछ देशभक्तों ने जान पर खेलकर मौलवी का सिर वहां से उतार लिया और पास के लोधीपुर गांव के एक छोर पर पूरी श्रद्धा व सम्मान के साथ दफन कर दिया. वहीं दूर खेतों के बीच आज भी मौलवी की मजार है. अवध में लोग उन्हें याद करते हुए कहते हैं कि उनके बाद उनके जैसा हिन्दू-मुस्लिम एकता का पैरोकार दूसरा कोई नहीं हुआ.
(कृष्ण प्रताप सिंह फैज़ाबाद स्थित जनमोर्चा अखबार के स्थानीय संपादक और वरिष्ठ पत्रकार हैं. व्यक्त विचार निजी हैं)
यह भी पढ़ें: ‘आखिरी शब दीद के काबिल थी ‘बिस्मिल’ की तड़प!’, काश, अपनी जिन्दगी में हम वो मंजर देखते!