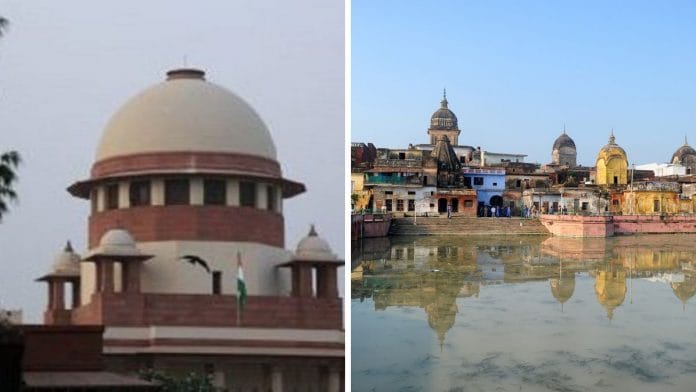गत सोलह अक्टूबर को देश के सबसे बड़े न्यायालय ने देश के सबसे संवेदनशील रामजन्मभूमि-बाबरी मस्जिद विवाद की सुनवाई पूरी की तो वह उसके इतिहास की दूसरी सबसे लंबी चलने वाली सुनवाई बन चुकी थी. वह चल रही थी तो न्यायालय ने खुद के मध्यस्थता पैनल के नाकाम रहने के बावजूद पक्षकारों को आपसी सुलह-समझौते के प्रयास जारी रखने की छूट दे रखी थी. अलबत्ता, उनके प्रयासों के लिए सुनवाई रोकना गवारा नहीं था.
अब सुनवाई खत्म हो जाने के बाद भी पक्षों के बीच दावेदारी छोड़ने व सुलह-समझौते के प्रस्तावों को लेकर आ रही खबरें यह जताने के लिए पर्याप्त हैं कि विवाद के ऊंट को इस या उस करवट बैठाने के लिए परदे के आगे-पीछे अभी भी बहुत कुछ चल रहा है.
ऐसे में न्यायालय द्वारा सुरक्षित फैसले के, जिसके 17 नवंबर से पूर्व ही सुना दिये जाने की उम्मीद है, इंतजार में बहुत संयम और समझदारी बरतने की जरूरत है. हम लम्बे अरसे से ऐसी सरकारों के दौर में हैं, जो ऐसे संयमों व समझदारियों पर अपने राजनीतिक फायदों वाली कार्रवाइयों को तरजीह देती हैं. ऐसा नहीं होता तो न अयोध्या का सर्वथा स्थानीय स्तर का यह विवाद समय के साथ विकराल होकर देश और उसकी व्यवस्था के लिए नासूर में बदलता और न उसकी हैसियत इतनी बढ़ती कि वह आधुनिक भारत के इतिहास का ऐसा पृष्ठ बन जाये जो देश के सामाजिक, राजनीतिक व धार्मिक माहौल के साथ उसकी बुनियादी लिखावट तक को बदल डाले.
यह भी पढ़ें : हर बार ‘चुनावी मुद्दा’ बनकर रह जाने वाली अयोध्या अब नई सुबह चाहती है : ग्राउंड रिपोर्ट
अयोध्या का अतीत गवाह है कि वोटों के लिए धार्मिक व साम्प्रदायिक ध्रुवीकरण की कोशिशों में कोई सीमा न मानने वाली राजनीति 1986 में इस विवाद के खात्मे के लिए उसके नागरिकों में हुई सर्वसम्मति के आड़े नहीं आती तो हम इसकी आड़ में ‘हिंदू-मुस्लिम भाई-भाई’ और ‘ईश्वर-अल्ला तेरो नाम’ जैसी सदियों के अनुभवों से बनी सामाजिक मान्यताओं को लगातार संकटग्रस्त देखने को अभिशप्त नहीं होते. आज की तारीख में किसे नहीं मालूम कि धर्मों और सम्प्रदायों का इस्तेमाल करने वाली राजनीति ने ही इस धर्मप्रधान कहलाने वाले देश में कट्टरता के ऐसे बीज बोये कि धर्म शब्द ही संदिग्ध लगने लगा. इतना ही नहीं, इस बहुलवादी देश में एक धर्म को दूसरे के खिलाफ खड़ा करने और बहुसंख्यक व अल्पसंख्यक जैसे विभाजनों को बढ़ाने वालों के मनसूबे भी फूलने-फलने लगे. धर्म को सबको साथ लेकर चलने का नाम बताने वालों को किनारे लगा दिया गया, सो अलग.
इन हालात में विवाद के न्यायिक फैसले को लेकर उत्सुकता बेहद स्वाभाविक है, लेकिन हमें नागरिकों के तौर पर उसके राजनीतिक व सामाजिक असर को लेकर भी सचेत रहने की जरूरत है. अच्छी बात यह है कि अयोध्या ने इसे लेकर हमेशा ही असीम धैर्य का परिचय दिया है. छह दिसम्बर, 1992 की ध्वंस को ही धर्म बना देने वाली कोशिशों को लेकर भी उसने आपा नहीं खोया.
इस बार एक अच्छी बात यह भी हुई है कि अयोध्या पुलिस फैसले के बाद अमन चैन बनाये रखने को लेकर समय रहते सचेत हो गई है. उसके आला अधिकारी जिले के कस्बों व गांवों में चैपालों व गोष्ठियों में लोगों को समझा रहे हैं कि देश में कोई अदालत सर्वोच्च न्यायालय से बड़ी नहीं है. इसलिए उसका फैसला कुछ भी और किसी के भी पक्ष या विपक्ष में हो, सभी को उसका सम्मान करना है. वे यह हिदायतें भी दे रहे हैं कि इस सिलसिले में किसी भी शरारत को कतई बर्दाश्त नहीं किया जायेगा. इस सिलसिले में पुलिस की एक बड़ी सुविधा यह है कि जो जमातें कभी यह कहती थीं कि यह कानूनी नहीं, आस्था का विवाद है और इस कारण अदालतें इसका फैसला ही नहीं कर सकतीं, वे भी सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को मानने की बात कह रही हैं. विवाद के पक्षकार तो खैर उसे न्यायालय ले ही इसीलिए गये हैं कि वह उसका निपटारा कर दे.
लेकिन इस विवाद में सिर्फ अयोध्या ही कसौटी पर नहीं है. शेष देश से भी, जो पहले ही ऐसे मामलों के दूध से जला हुआ है, छाछ को भी फूंक-फूंक कर पीने की अपेक्षा है. इस तथ्य के मद्देनजर और भी कि छह दिसम्बर 1992 को विवादित स्थल पर खड़े सैकड़ों साल पुराने ऐतिहासिक ढांचे को योजनाबद्ध अभियान चलाकर तोड़ डालने वालों को अभी तक दंड नहीं मिल पाया है. इस ढांचे के ध्वंस के कारण हमारा देश दुनिया में कितना बदनाम हुआ, पिछड़ा और हमारे समाज के भीतर की दरारें कितनी गहरी हो गईं, इसे इस फैसले की घड़ी में भी याद रखना आवश्यक है.
यह भी पढ़ें : अयोध्या में एहतियात के नाम पर धारा 144 से जनाक्रोश बढ़ रहा है, प्रशासन की पोल भी खुल रही है
इस कारण और भी कि विवाद के फैसले पर देश की ही नहीं, दुनिया भर की नजर रहेगी. वह न सिर्फ चुपचाप देखेगी, बल्कि अपने इतिहास में दर्ज करेगी कि भारत के बहुभाषी बहुधर्मी समाज ने इस फैसले को किस तरह ग्रहण किया. सोचिये जरा कि इसके बावजूद हमने संयम नहीं बरता तो इस इतिहास में हमें कहां, कितनी और कैसी जगह मिल पायेगी? यकीनन, सर्वोच्च न्यायालय के फैसले की इस घड़ी में हमारे सामने अपने भावी इतिहास की फिक्र करने का वक्त आ खड़ा हुआ है. यह जताने का भी कि तमाम असहमतियों के बावजूद हम अपनी संवैधानिक संस्थाओं और उनके फैसलों का कितना सम्मान करते हैं.
(लेखक जनमोर्चा अख़बार के स्थानीय संपादक हैं, यह लेख उनका निजी विचार है)