मोदी-भाजपा को 2019 में मात देनी है तो यह ताकतवर नेताओं को उनके गढ़ों में हराकर ही दी जा सकती है क्योंकि चुनावी विश्लेषण के लिहाज से यही तर्कपूर्ण दिखता है, चाहे विचारधारात्मक विरोध का तक़ाज़ा कुछ भी हो.
‘मसखरा राजकुमार’, ‘चौकीदार चोर है’, ‘पक्षी की बीट’…. इस तरह के जुमलों के कारण राजनीतिक विमर्श के गर्त में पहुंच जाने को लेकर हम भले ही खीझ उठते हों, सचाई यह है कि राजनीति के इस मैदान में एक दुर्लभ मगर अपेक्षित मिलनसारिता का मंज़र उभर आया है. तेलुगु देशम पार्टी और कांग्रेस के बीच गठजोड़ और मुस्कराती तस्वीरें इसकी एक मिसाल हैं.
कट्टर दुश्मन एक-दूसरे से गले मिल रहे हैं. पुराने दोस्त नौका विहार कर रहे हैं, और खिलवाड़ के नए उपाय तलाश रहे हैं. अगर राजनीति का मंच अब कुंवारों की मधुशाला जैसा दिख रहा है, तब कल्पना कर सकते हैं कि 2019 का चुनाव किस तरह का होगा.
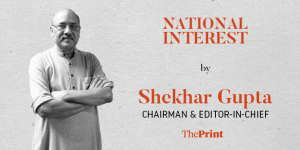
भारत का राजनीतिक इतिहास बताता है कि शक्तिशाक्ली नेता को, खासकर वह जो बहुमत से लैस हो उसे चुनौती देने वाला कभी भी नहीं हरा सका है— फिलहाल तो ऐसा नहीं लग रहा. ऐसे नेता को हराने की ताकत सिर्फ खुद उसके अपने ही हाथ में होती है, जैसा कि 1977 में इंदिरा गांधी के उदाहरण से स्पष्ट है. उस समय लोग उनके किसी प्रतिद्वंद्वी को वोट नहीं दे रहे थे. दक्षिण भारत को छोड़ दें तो लोगों ने इमरजेंसी की ज़्यादतियों के वास्ते उन्हें सज़ा देने के लिए उनके खिलाफ वोट दिया था.
अगर इंदिरा गांधी ने 1977 में खुद को हराया, तो यही काम 1989 में राजीव गांधी ने किया. वीपी सिंह ने हिंदी पट्टी में चुनाव अभियान तो चलाया मगर वे न तो प्रधानमंत्री पद के स्पष्ट दावेदार थे और न ही राजीव को टक्कर देते दिख रहे थे. शाह बानो से लेकर बोफोर्स और अयोध्या तक राजीव के तमाम गलत कदमों के कारण ही उनकी पार्टी के सबसे प्रतिबद्ध वोट बैंक ने भी उनका साथ छोड़ दिया था.
2004 में अटल बिहारी वाजपेयी काफी लोकप्रिय नेता थे, हालांकि उन्हें बहुमत नहीं हासिल था. उनके खिलाफ कोई एकजुट विपक्ष खड़ा नहीं था, न ही उनकी गद्दी को चुनौती देने वाला कोई था. मगर वे अपनी पार्टी के अहंकार की वजह से हारे, जिसने वक्त से काफी पहले ही अपनी जीत घोषित कर दी थी.
यह भी पढ़ें: डोभाल जी, डरिए मत, गठबंधन की कमज़ोर सरकारों ने ज़्यादा मज़बूत फ़ैसले लिए
उसने चुनाव समय से पहले करवाया, ‘शाइनिंग इंडिया’ जैसे बड़बोले दावे कर डाले, सहयोगियों को गंवा दिया, और दूसरों (मसलन चंद्रबाबू नायडू) का सफाया करवा दिया क्योंकि वे 2002 के गुजरात दंगों पर ठोस जवाब नहीं दे पाए. इस लिहाज से देखें तो वाजपेयी ने भी खुद को हराया. 1977-2004 के बीच के ये तीन चुनाव हमें यह सबक सिखाते हैं कि तथाकथित ‘टीना’ (यानी दूसरा कोई विकल्प न होना) एक भयावह हकीकत है, लेकिन एकमात्र हकीकत नहीं.
भारतीय मतदाता की यह अनूठी परपीड़क बहादुरी क्या है, जो कभी-कभी एक ताकतवर नेता को भी उखाड़ फेंकने का फैसला कर लेती है, जबकि उसके सामने कोई विकल्प भी उपलब्ध नहीं होता? इसे सरकार विरोधी आक्रोश भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि हाल के दशकों में गठबंधन सरकारों ने भी लगातार दूसरी बार चुनाव जीता है (1999 में वाजपेयी ने, 2009 में मनमोहन सिंह ने). इसकी एक व्याख्या यह हो सकती है कि मतदाता तब भी ‘टीना’ से प्रभावित हो सकते हैं जब भले ही वे असंतुष्ट या नाराज़ हों. लेकिन अगर वे नाराज़ हो गए, तो वे चालू सरकार को निकाल बाहर करना चाहते हैं. इसके बाद सत्ता में कौन आ रहा है, इससे उन्हें फर्क नहीं पड़ता.
हमारा सवाल यह है कि क्या मोदी सरकार इस कगार पर पहुंच गई है?
इस सवाल का जवाब हम पंडितों से पूछने की बजाय जनमत सर्वेक्षणों के आंकड़ों में ढूढ़ेंगे. ‘इंडिया टुडे’ समेत इन सभी पर्याप्त गंभीर सर्वेक्षणों से एक समान किस्म की प्रवृत्ति उभरती है—कि मोदी सरकार की लोकप्रियता लगातार घट रही है, लेकिन इसकी गति बहुत धीमी है. इसके पक्ष में आंकड़े विपक्ष के आंकड़ों से काफी मजबूत हैं. इसलिए आप फिलहाल इस संभावना को नकार सकते हैं कि 1977, 1989 या 2004 कि तरह उसके खिलाफ ‘बहिष्कार वोट’ पड़ने वाले हैं. इसलिए उसे दूसरी बार सरकार बनाने का मौका मिल सकता है. संभव है कि उसे स्पष्ट बहुमत न मिले और सरकार भाजपा के नेतृत्व वाले गठबंधन की बने.
इस स्थिति में बदलाव केवल एक उपाय से तो निश्चित ही नहीं आएगा, लेकिन दो उपायों से आ सकता है. राहुल गांधी से लेकर मायावती तक किसी को भी प्रधानमंत्री पद के अगले उम्मीदवार के रूप में पेश किया जाए, तो इस उपाय से मोदी को हराया नहीं जा सकता. बल्कि यह उनकी जीत की गारंटी बन जाएगी. वे इसे दो उम्मीदवारों कि सीधी टक्कर वाला, राष्ट्रपति पद का चुनाव बना देंगे. कोई भी विपक्षी नेता उनसे सीधी टक्कर लेने की स्थिति में नहीं है. इसके साथ ही यह भी सच है कि महागठबंधन हमेशा की तरह एक ख्वाब ही बना हुआ है. बिना एक नेता के महागठबंधन नामुमकिन है.
मोदी को हराने के लिए दो उपाय किए जा सकते हैं. सर्वेक्षणों से यह तो साफ है कि उनकी लोकप्रियता बढ़ नहीं रही है, जैसी कि 2008-09 में यूपीए की बढ़ रही थी. बल्कि उनकी लोकप्रियता धीरे-धीरे घट ही रही है. क्या विपक्ष अगले छह महीनों में इस असंतोष को आक्रोश में तब्दील कर सकता है? यह किया जा सकता है, लेकिन नामुमकिन लगता है. राफेल अभी भी बोफोर्स नहीं बन पाया है, हालांकि मोदी सरकार के कुछ मंत्री इस पर जो प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं वे वैसी ही हैं जैसी तब राजीव गांधी की थीं.
मुद्दे किसानों और पेट्रोल आदि की कीमतों के भी हैं, लेकिन महंगाई (खासकर खाद्य पदार्थों की) में मामूली इजाफा इन मसलों के प्रति गुस्से को ज्यादा भड़कने नहीं दे रही. आज कोई जयप्रकाश नारायण या वीपी सिंह नहीं हैं जो इसे एक कटु चुनाव में तब्दील कर सके.
राहुल गांधी अभी यह कर पाने में सफल नहीं हो रहे हैं. वे अनिल अंबानी समेत, कॉरपोरेट के साथ भाजपा की मिलीभगत के आरोपों के बूते जो मुहिम चला रहे हैं वह पर्याप्त ज़ोर इसलिए नहीं पकड़ पा रहा है क्योंकि कांग्रेस खुद कॉरपोरेट, खासकर अंबानी घराने से नज़दीकियों के लिए मशहूर रही है. इसलिए हम फिलहाल तो ‘बहिष्कार वोट’ की संभावना को खारिज कर सकते हैं.
दूसरी रणनीति यह हो सकती है कि एक जनरल के नेतृत्व वाली विपक्षी सेना के साथ एक राष्ट्रीय चुनाव के मोर्चे पर मोदी से न लड़कर कई छोटे-छोटे, राज्य स्तरीय (क्षेत्रीय नहीं) मोर्चों पर ताकतवर स्थानीय नेताओं से लड़ा जाए. इसके लिए ऐसे सीमित स्थानीय गठजोड़ किए जाएं, जो विचारधारात्मक विरोधों को परे रखकर चुनावी तर्कों को तरजीह देते हों. तेलंगाना में चंद्रबाबू नायडु और राहुल गांधी यही कर रहे हैं, और आंध्र प्रदेश में भी इसे आगे बढ़ाने कि संभावना है.
याद रहे कि शिरोमणि अकाली दल के अलावा टीडीपी ही भारत में सबसे प्रबल कांग्रेस-विरोधी पार्टी रही है. 2013 में नायडू ने सोनिया गांधी पर आरोप लगाया था कि उन्होंने आंध्र प्रदेश का विभाजन केवल अपने बेटे राहुल को प्रधानमंत्री बनाने की (कुत्सित) मंशा से किया था. लेकिन आज वे उन्हीं से गले मिलते हुए फोटो खिंचवा रहे हैं. साझा दुश्मन के डर से बड़ी कोई चीज़ नहीं है, जो दो दुश्मनों को भी एक कर दे.
यह भी पढ़ें: भारतीयों और उनके भगवान के बीच पुजारी नहीं बन सकता है सुप्रीम कोर्ट
आंध्र या तेलंगाना में भाजपा कोई बड़ी ताकत नहीं है लेकिन 42 सीटों वाले दो राज्यों में बिना किसी सहयोगी के उसे घाटा तो होगा ही. भाजपा के लिए इसे आंध्र बनाम भाजपा की बजाय मोदी बनाम राहुल मुक़ाबला बनाने में मुश्किल पेश आएगी. तमिलनाडु में भाजपा फिलहाल कमजोर स्थिति में है, वहां उसकी भूलचूक वाली सहयोगी अन्नाद्रमुक आलोकप्रिय है. वैसे, अभी वहां स्थिति स्पष्ट नहीं हुई है. सो, क्षेत्रीय गठबंधन की अगली रस्साकशी तमिलनाडु में होने वाली है. आप इस संभावना से इनकार नहीं कर सकते कि भाजपा वहां अन्नाद्रमुक को खारिज करके फिर से द्रमुक को अपने पाले में खींच ले.
हम पहले ही कह चुके हैं कि यह अपेक्षित राजनीतिक मिलनसारिता का मौसम है. अगर टीडीपी और कांग्रेस, सपा और बसपा सरीखे पक्के दुश्मन करीब आ सकते हैं तो अतीत में सहयोगी रह चुकीं द्रमुक और भाजपा को करीब आने से कौन रोक सकता है. लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो भाजपा से कई छोटी, राज्य स्तरीय लड़ाइयां लड़ने की कांग्रेस/विपक्ष की रणनीति को ताकत मिलेगी.
महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल सरीखे बड़े राज्यों की राजनीति पहले से ही काफी सुनिश्चित है. कर्नाटक के बारे में आप कभी पक्के तौर पर कुछ नहीं कह सकते इसलिए वहां खेल खुला है. हिंदी हृदयप्रदेश में सपा-बसपा समझौता अभी पक्का नहीं हुआ है लेकिन यह तार्किक और संभावित लगता है. मध्य प्रदेश और राजस्थान में भाजपा-कांग्रेस में सीधी टक्कर है लेकिन वहां मैदान में बसपा या दूसरे छोटे स्थानीय दलों के कूदने से फर्क पड़ सकता है.
कांग्रेस और भाजपा, दोनों ही इन सहयोगियों का छोटा-मोटा लाभ लेने की कोशिश करेंगी. जैसे कि हरियाणा, छतीसगढ़, झारखंड, असम में, जहां भाजपा के नेतृत्व में गठबंधन सरकारें चल रही हैं. असम में भाजपा राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर (एनआरसी) के आधार पर पहचाने गए ‘विदेशियों’ में हिंदुओं तथा मुसलमानों के बीच जो भेदभाव करना चाहती है, उससे प्रफुल्ल महंत की एजीपी खीज रही है. पंजाब में भाजपा घाटे में रहेगी क्योंकि वहां मुक़ाबला कांग्रेस बनाम अकाली ही होगा, न कि कांग्रेस बनाम मोदी. क्या दिल्ली और पंजाब में कांग्रेस-आप साझीदारी मुमकिन है? इसकी उम्मीद नहीं दिखती, लेकिन अगर टीडीपी-कांग्रेस मेल हो सकता है तो फिर क्या कहा जा सकता है?
सो, लगता है कि राजनीति इसी करवट मुड़ने जा रही है. महागठबंधन न हो, मगर राज्यों के स्तर पर कई गठबंधन हो सकते हैं. इनके बूते विपक्ष लोकप्रिय स्थानीय नेताओं के खिलाफ भाजपा को कई छोटी-छोटी लड़ाइयों में उलझा सकता है. मोदी-शाह की रणनीति विपक्ष को ऐसी छूट लेने से रोकने की होगी और लड़ाई को मोदी बनाम राहुल की सीधी टक्कर की ओर मोड़ देने की होगी. 2019 का कुछ ऐसा ही परिदृश्य उभरता दिख रहा है. विपक्ष ने आंध्र-तेलंगाना में पहली चाल चल दी है.
(इस लेख को अंग्रेजी में पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें.)

