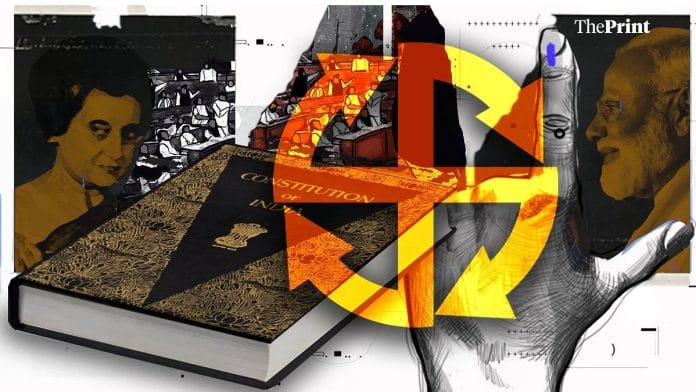यह कहना भ्रामक ही होगा कि आज के बाद 22 जनवरी को हमारे राष्ट्रीय कैलेंडर की सबसे महत्वपूर्ण तारीखों में नहीं गिना जाएगा. दुनिया के सबसे प्राचीन धर्म के लिए एक नये बड़े उत्सव का आविष्कार नरेंद्र मोदी की वाकई एक उपलब्धि है. लेकिन इसके साथ कुछ राजनीतिक सवालों पर विचार करना भी लाजिमी है.
क्या 22 जनवरी हमारी संवैधानिक धर्मनिरपेक्षता के लिए अंतिम मोड़ बनकर रह जाएगी? मोदी-शाह की भाजपा ने अयोध्या नाम की शिला पर जो वैचारिक ऐलान दर्ज कर दिया है, क्या उसका जवाब संभव है? क्या मोदी को चुनौती देने वालों का कोई भविष्य है?
अगर इन सारे सवालों के सामने घुटने टेक दिए जाते हैं तो बेहतर है कि हम यह बहस यहीं बंद कर दें. लेकिन जरूरत इस बात की है कि हम ऐसा न करें, क्योंकि ऐसा करना बेतुके ढंग से यह मान लेना होगा कि भारत में अब प्रतिस्पर्द्धी राजनीति की संभावना खत्म हो गई है. राजनीति किसी भी समाज में बंद नहीं होती. अगर यह अयोध्या के रामराज्य में भी नहीं बंद नहीं हुई थी, तो 21वीं सदी के लोकतंत्र में भी बंद नहीं होगी, चाहे यह आपके नजरिए से कितनी भी दोषपूर्ण क्यों न लगती हो.
अयोध्या समारोह का सबसे अप्रत्याशित परिणाम यह दिखाता है कि मोदी सरकार और भाजपा की विचारधारा को चुनौती देने वालों में से अधिकतर ने मानो बड़ी आसानी से हार मान ली है. कई लोगों को डर है कि गणतंत्र मर चुका है; कम-से-कम उस गणतंत्र का अस्तित्व तो खत्म हो गया जिसमें हम पले-बढ़े, जिसका निर्माण उन संस्थापकों ने किया था जिन्हें हम पूजते रहे हैं. इसमें कुछ सच्चाई हो सकती है लेकिन लोकतंत्र का यह स्वभाव है कि निर्वाचित नेता अपना चरित्र और चाल बदल सकते हैं. आप उनसे असहमत हैं तो इसका मतलब यह नहीं है कि वह मर गया. यह गणतंत्र इंदिरा गांधी की इमरजेंसी की अग्निपरीक्षा से गुजर चुका है.
उन्होंने जिन राजनीतिक शक्तियों को 21 महीने तक जेल में बंद रखा उन्होंने इस गणतंत्र को पुनर्स्थापित करने का संकल्प दिखाया. उनके ही कुछ वारिस आज उसके बुनियादी सिद्धांतों को बदलने और अलग तरह से परिभाषित करने की कोशिश कर रहे हैं. उन्हें चुनौती दी जा सकती है, जैसे 1970 के दशक में श्रीमती गांधी को दी गई थी.
आज जरूरत सिर्फ इस बात की है कि चुनौती देने वालों को केवल शुद्ध संकल्प से ज्यादा का प्रदर्शन करना पड़ेगा. वे भाजपा के विजय संघर्ष से सबक सीख सकते हैं. यह दर्शाता है कि एक शक्तिशाली राजनीतिक ताकत को किस तरह परास्त किया जा सकता है, और दूसरी ताकत अप्रत्याशित रूप से किस तरह उभर सकती है.
गौर कीजिए कि भाजपा के आंकड़े किस तरह बदलते गए हैं. इस पार्टी की स्थापना 1980 में हुई, जबकि उस साल जनवरी में हुए चुनाव ने श्रीमती गांधी को फिर से सत्ता में बैठा दिया था. यह पार्टी पुरानी जनसंघ का नया अवतार थी और पूरी तरह आरएसएस की विचारधारा का प्रतिनिधित्व करती थी. अपने पहले लोकसभा चुनाव में, 1984 में वह महज दो सीटें जीत पाई. इसके बाद 1989 में उसकी सीटें बढ़कर 85, 1991 में 120, 1996 में 161, 1998 में 182, और 1999 में भी 182 हो गईं. इनमें से अंतिम दो नतीजों ने उसे अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में छह साल के लिए सत्ता में बैठाया.
इस पूरे दौर में सबसे उल्लेखनीय बात यह रही कि उसने अपनी मूल विचारधारा को लेकर लचीलेपन का किस तरह परिचय दिया. इस नयी पार्टी के संस्थापकों में सत्ता और विचारधारा के बीच संतुलन साधने का कौशल था. आपके दिल को सबसे प्रिय जो बड़े वैचारिक मुद्दे हैं उनके लिए भी समय आएगा! मुमकिन है कि आपकी पीढ़ी नियति से किए गए वादे (नेहरू के प्रशंसक माफ करें) को न पूरा कर पाए, लेकिन आपके बच्चे पूरा करेंगे.
कितने धैर्य और संकल्प की जरूरत है, यह भी आप भाजपा से सीख सकते हैं. 1989 में वह 85 सीटें जीती थी और तब वह राष्ट्रीय गठबंधन में अपना हिस्सा मांग सकती थी, लेकिन उसने नहीं मांगा. बल्कि उसने वी.पी. सिंह के जनता दल को बाहर से समर्थन दिया, जबकि उसका सबसे कट्टर वैचारिक शत्रु (हम जानबूझकर प्रतिद्वंद्वी शब्द के बदले शत्रु शब्द का प्रयोग कर रहे हैं) वाम मोर्चा भी उस सरकार को समर्थन दे रहा था.
शत्रु से हाथ मिलाने में कोई शर्म नहीं की उसने. उसके पीछे मकसद था. एक तो कांग्रेस को कमजोर करने के लिए उसे सत्ता से दूर रखना था; दूसरे, यह रणनीति थी कि अस्थिर तीसरा मोर्चा जनता को यह एहसास कराएगा कि सत्ता एक राष्ट्रीय पार्टी के हाथ में ही होनी चाहिए. और जरूरी नहीं कि वह राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस ही हो, अब एक विकल्प प्रस्तुत है. और तीसरे, उसे मंदिर की मुहिम खड़ी करने के लिए समय चाहिए था.
2004 में भाजपा एक दशक के लिए सत्ता से बाहर हो गई, लेकिन उसकी सीटों का आंकड़ा सैकड़े के अंक से नीचे नहीं गया. सत्ता के छह वर्षों और प्रभावी सरकार ने उसका आधार बना दिया था. सत्ता से वनवास खत्म होने तक उसने नयी प्रतिभाओं और नरेंद्र मोदी के रूप में नये नेतृत्व का निर्माण कर लिया था.
मोदी का किस तरह उत्कर्ष हुआ और वे किस तरह इंदिरा गांधी के बराबर माने जाने वाले राजनीतिक पुरोधा बन गए? 1990 के दशक में वे गुजरात में आरएसएस के एक गुमनाम-से प्रचारक थे. वे अपनी वरिष्ठता, पारिवारिक विरासत या आलाकमान के किसी आदेश के बूते शिखर तक नहीं पहुंचे. उन्होंने भाजपा के अंदर संघर्ष किया, जिसे भारतीय राजनीति में अमेरिकी राजनीति की ‘प्राइमरी’ वाली प्रक्रिया के समान माना जा सकता है. मोदी ने पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं, पूर्व तथा वर्तमान पार्टी अध्यक्षों और दूसरे राष्ट्रीय दिग्गजों को पीछे छोड़ दिया. पार्टी ने, उसके कार्यकर्ताओं ने 2004 और 2009 में पराजित हुए नेताओं को खारिज कर दिया. अब जरा यह देखिए कि 2014 के बाद से भाजपा के प्रतिद्वंद्वियों ने क्या किया.
मजबूत संवैधानिक लोकतंत्र में क्रांतियां रातोंरात नहीं हो जातीं. इसमें कभी-कभी पीढ़ियां गुजर जाती हैं. 1984 की दो सीटों वाली बदहाली से 2014 के बहुमत तक पहुंचने में भाजपा को तीन दशक की कड़ी मेहनत, धैर्य, और कुछ बलिदान देने की जरूरत पड़ी.
उसके नेताओं ने तब हाथ नहीं खड़े कर दिए थे जब उनकी पार्टी का अस्तित्व लगभग समाप्त हो गया था और श्रीमती गांधी ने 529 सीटों के लिए हुए चुनाव में 353 सीटों का विशाल बहुमत हासिल कर लिया था. तब अगर भाजपा के नेता यह कहते कि यह गणतंत्र का अंत है, तो वे आज 22 जनवरी के बाद हताश हुए मोदी के आलोचकों के मुक़ाबले ज्यादा सही होते. खास तौर से इसलिए भी कि जनवरी 1980 में वे यह सोच सकते थे कि अभी-अभी तो उन्होंने इस गणतंत्र को इमरजेंसी के चंगुल से मुक्त कराया था और मतदाताओं ने उनकी उपलब्धि पर इतनी जल्दी पानी फेर दिया! और, भारत के लोग अगर श्रीमती गांधी को माफ करते हुए उन्हें इतनी जल्दी सत्ता में वापस बैठाने को तैयार थे, तो क्या वे वास्तव में इस लोकतंत्र के हक़दार थे?
यह कहना कि गणतंत्र मर चुका है और इसके साथ उसका उदारवाद भी खत्म हो चुका है, और कुछ नहीं बल्कि गुस्से में जाहिर की गई हताशा, पराजयवादी सोच ही है. यह वैसा ही है जैसे 1970 के दशक की हिंदी फिल्मों में बाप अपने बिगड़ैल बेटे से यह कहता था कि ‘तुम मेरे लिए मर चुके हो’.
लोकतांत्रिक राजनीति हमेशा विचारों, विचारधाराओं की लड़ाई होती है. संवैधानिक गणतंत्र कभी मरता नहीं; राजनीतिक नेता, पार्टियां, विचार आदि ही मरा करते हैं. उदाहरण के लिए, स्वतंत्र पार्टी का ‘लिबर्टेरियन’ (इच्छास्वातंत्र्य) का विचार कहां लुप्त हो गया? 1967 के चुनाव में इस पार्टी को जनसंघ की 35 सीटों के मुक़ाबले 44 सीटें मिली थीं, और वह इंदिरा गांधी की कांग्रेस पार्टी के बाद दूसरी सबसे बड़ी पार्टी थी.
हताशा का दूसरा रूप यह डर है कि मोदी को वर्तमान संविधान को रद्द करके नया संविधान लिख डालने, भारत में राष्ट्रपति शासन वाली व्यवस्था लागू करने, और खुद को आजीवन राष्ट्रपति घोषित करने का अधिकार मिल गया है; कि यह आखिरी चुनाव होगा, आदि-आदि. वे ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे. उन्हें जो अधिकार चाहिए वह सब उन्हें इसी संविधान, इसी संसद और इन्हीं चुनावों से हासिल हो सकता है, तो वे इस ‘सिस्टम’ को क्यों बदलेंगे जो उनके लिए शानदार तरीके से काम कर रही है? इसी सिस्टम, संविधान और सियासत में उनके प्रतिद्वंद्वियों को उन्हें हराने के राजनीतिक, बौद्धिक, और नैतिक हथियार खोजने पड़ेंगे. मोदी ने इस गणतंत्र को जिस दिशा में मोड़ दिया है उसे वे अगर पसंद नहीं करते तो उन्हें इसे सही दिशा देनी होगी.
(संपादनः शिव पाण्डेय)
(इस लेख को अंग्रेज़ी में पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें.)
यह भी पढे़ंः गाज़ा से पाकिस्तान तक उथल-पुथल के बीच सियासी इस्लाम मजबूत और कमज़ोर दोनों, आपकी नज़र की मर्ज़ी