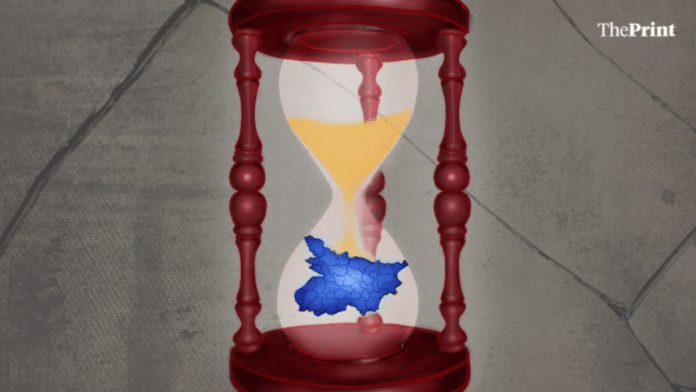अपनी 18वीं विधानसभा के गठन के लिए मतदान कर रहा बिहार इस बात पर गर्व करता रहा है कि दुनिया में सबसे पहले लोकतंत्र का जन्म उसी की सरजमीं पर हुआ, और इसीलिए प्रधानमंत्री आज यह कह पा रहे हैं कि भारत लोकतंत्र की जननी है.
आपको बिहार के वैशाली जिले में पहुंचाने वाले हाइवे के किनारे लगा एक साइनबोर्ड भी यह घोषणा करता दिखेगा : ‘विश्व के प्रथम गणतंत्र में आपका स्वागत है’. यह कोई लोककथा नहीं है. इसके कई ऐतिहासिक साक्ष्य मौजूद हैं: कई शिलालेख, कई शोधग्रंथ इसकी पुष्टि करते हैं. अपनी जानकारियों को ताजा करने के लिए आप पटना के शानदार संग्रहालय भी जा सकते हैं.
लोकतंत्र यानी ऐसे गणतंत्र का विचार जिसमें हर एक व्यक्ति को बोलने और चुनने की आजादी हो. यह भारत को बिहार की ओर से, और दुनिया को भारत की ओर से सबसे बड़ी देन है. लेकिन इससे एक सवाल उभरता है कि बिहार के लिए लोकतंत्र कितना अच्छा साबित हुआ है? जनता के लोकतंत्र का उसे क्या लाभ मिला है?
उसके समाज, उसकी जनता और अर्थव्यवस्था की जो हालत है उससे तो यही लगता है कि उसे कुछ भी हासिल नहीं हुआ है. वहां कोई उद्योग नहीं है, टैक्स के रूप में कोई आय नहीं है, गुजारे भर की खेती के सिवाय वहां कोई आर्थिक गतिविधि नहीं है. उसकी प्रति व्यक्ति आय का आंकड़ा देश में सबसे छोटा है और हमारे सबसे धनी राज्य के इस आंकड़े के 20 प्रतिशत के बराबर है. और यह अंतर बढ़ता ही जा रहा है. इस राज्य की सबसे उत्पादक गतिविधि श्रम का निर्यात है— वह भी बेहतर आर्थिक स्थिति वाले राज्यों में ज़्यादातर ऐसे रोजगारों के लिए, जिनसे न्यूनतम कमाई होती हो.
बिहार की दुरावस्था से उपजी खीझ, और एक और जातीय जनगणना से उभरी उम्मीद में मैंने 7 अक्तूबर 2023 को अपने इस कॉलम में लिखा था: ‘बिहार आज जो सोच रहा है उसे वह दो दिन पहले सोचा करता था’. आज जब वहां चुनाव हो रहा है, आजाद भारत की उसकी तीसरी पीढ़ी नये सोच में बदले उस पुराने सोच की कीमत अदा कर रही है. वह जातिवाद, पहचान, सामाजिक समीकरणों, और सबसे निचले पायदन पर होने के बावजूद संतुष्ट नजर आती है.
हम यह देख सकते हैं कि आखिर किसी को कोई चिंता क्यों नहीं है. बिहार बाकियों से, अपने पड़ोसी राज्यों से भी इतना पीछे छूट गया है कि उसके मतदाता अपनी आज की स्थिति की तुलना सिर्फ अपनी पिछली स्थिति से करते हैं: क्या मैं अपने अभिभावकों से बेहतर स्थिति में हूं ? इस सवाल का जवाब प्रायः हां में होता है. क्या हमारे बच्चे बेहतर स्थिति में होंगे? हकीकत को देखें तो उम्मीद का जवाब अक्सर ‘हां’ ही होता है. यह सोच आकांक्षाओं के पैमाने को डरावने रूप से निचले स्तर पर लाकर छोड़ देता है.
बिहार के मतदाताओं की पीढ़ी-दर-पीढ़ी न्यूनतम अपेक्षाओं को लेकर जीती और संघर्ष करती रही है. सामंती और ऊंची जातियों के अत्याचारों से सुरक्षा मिलती रहे, तीन जून का खाना मिलता रहे, कानून-व्यवस्था की बुनियादी हालत ठीक रहे, बिजली और सड़क आदि की सुविधाएं मिलती रहें, इतना काफी है. लेकिन 2025 के भारत में अगर आपका सपना बस यही है तो यह दुखद है. यही वजह है कि ‘रेवड़ी’ बांटने की निंदा करने वाले नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार आज उन्हीं सपनों को पूरा करने की राजनीतिक पेशकश कर रहे हैं. उनके प्रतिद्वंद्वी बेशक राज्य के 2.76 करोड़ परिवारों के एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी देने का वादा कर रहे हैं. यह कोई क्रूर मज़ाक नहीं है. यह नीतीश कुमार के 20 साल के शासन के बाद के बिहार की चिंताजनक सच्चाई है.
यह खास तौर से उस राज्य के लिए चिंताजनक है जिसकी राजनीतिक संस्कृति की जड़ें गहरी, जीवंत और साहसपूर्ण हैं. लेकिन इसे इस तरह देखिए. बिहार न होता तो गांधी गांधी न होते. वे 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे और उन्होंने चंपारण में जबरन नील की खेती करवाने वाले अंग्रेज़ ठेकेदारों के खिलाफ अपने सत्याग्रह से देश और दुनिया का ध्यान आकर्षित किया. उस इलाके में आज भी भारत के सबसे गरीब राज्य के कुछ सबसे गरीब जिले मौजूद हैं. वहां लोग आज भी कितने गरीब, कितने उदासीन और अभावग्रस्त हैं, यह देखना हो तो उस क्षेत्र का दौरा कीजिए. तब आप कल्पना कर सकेंगे कि 1915 में ये लोग कितनी दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था में जी रहे होंगे. फिर भी उन्होंने गांधी को गले लगा लिया था. निर्धनतम बिहार उनका पहला राजनीतिक साथी बना था.
जयप्रकाश नारायण (जेपी) संयोग से बिहारी थे, लेकिन बिहार के लोगों में राजनीतिक जागरूकता और हिम्मत न होती तो क्या वे लोकनायक कहे जाते? उनके आंदोलन को बिहार के लोगों की ताकत हासिल थी और उसने पूरे भारत को इतने नाटकीय रूप से प्रभावित किया था कि इंदिरा गांधी ने घबराकर इमरजेंसी लगा दी थी जिसके चलते 1977 में वे चुनाव हार गईं. गांधी के बाद 20वीं सदी के भारत में जेपी सबसे बड़ी नैतिक शक्ति के रूप में उभरे और उन्होंने थोड़े समय के लिए राजनीतिक उपलब्धि भी हासिल की. बिहार ने कांग्रेस पार्टी को राष्ट्रीय स्तर पर जिस पतन की ओर धकेला उससे वह कभी उबर नहीं सकी.
अगर महात्मा गांधी और जयप्रकाश नारायण के उत्कर्ष का श्रेय बिहार और उसके लोगों को जाता है, तो हम 1960 वाले दशक में उभरे कर्पूरी ठाकुर की भी बात करें. तब तक इस राज्य को एक पूर्व-निर्धारित विकल्प के रूप में ऊंची जाति के निर्वाचित मुख्यमंत्री मिलते रहे थे. समस्तीपुर के एक साधारण नाई परिवार से उभरे कर्पूरी ठाकुर ने इसे चलन को चुनौती दी और इसे बदल डाला. और यह केवल बिहार के लिए नहीं हुआ. उन्होंने निचली मानी जाने वाली जातियों के सशक्तीकरण के लिए सामाजिक न्याय के आंदोलन को जन्म दे दिया, जो छह दशक बाद आज भी जारी है.
कर्पूरी ठाकुर ने उन सामाजिक समीकरणों के निर्माण में प्रमुख भूमिका निभाई जिन्होंने कांग्रेस को पहली बार 1967 में कई राज्यों में बहुमत से वंचित कर दिया. बिहार की संयुक्त विधायक दल की सरकार, जिसमें वे शिक्षा तथा दूसरे मंत्रालयों की ज़िम्मेदारी के साथ उप-मुख्यमंत्री बने, ज्यादा दिनों तक नहीं चल सकी, लेकिन उन्होंने उस नयी राजनीति की नींव डाल दी जिसे मंडलवादी राजनीति कहा जाता है. इसने कांग्रेस (जिसे नब्बे के दशक के शुरू में नरम हिंदुत्व की ओर झुकते देखा गया था) और भाजपा के जवाब में एक धर्मनिरपेक्ष विकल्प प्रस्तुत किया.
तब तक कांग्रेस को सबको समेटने वाली एक ऐसी छतरी के रूप में देखा जाता था, जो जनसंघ (जिसे इंदिरा गांधी हिंदुओं की नहीं बल्कि बनियों को पार्टी कहा करती थीं) को हंसी में उड़ा सकती थी. कर्पूरी ठाकुर और बिहार की जनता ने भारत में पहली बार कांग्रेस विरोधी और अंततः भाजपा विरोधी सामाजिक गठबंधन का निर्माण कर दिया था. यह और बात है कि यह अंततः बिखर गया, इसका हर घटक दो राष्ट्रीय गठबंधनों में से किसी-न-किसी एक से जुड़ गया. कर्पूरी ठाकुर के निधन के 37 साल बाद आज भी कांग्रेस और भाजपा, दोनों को उनकी विरासत के रूप में मिले किसी एक गठबंधन की सवारी करनी पड़ती है. इसलिए आप समझ सकते हैं कि मोदी सरकार ने उन्हें मरणोपरांत भारतरत्न से क्यों सम्मानित किया.
लिच्छवी काल के लोकतंत्र से लेकर कर्पूरी ठाकुर के सामाजिक न्याय, जेपी की संपूर्ण क्रांति, निचले वर्गों के सशस्त्र वामपंथी (मार्क्सवादी-लेनिनवादी) आंदोलनों और उसके जवाब में सामंती ऊंची जातियों की रणवीर सेना तक बिहार की जमीन भारत में कहीं की जमीन के मुक़ाबले क्रांतियों के लिए ज्यादा उपजाऊ रही है. इसके बावजूद बिहार इतना पीछे क्यों रह गया? कौन-सा अभिशाप उसका पीछा कर रहा है? उसकी क्रांतियां अपनी ही संतानों को क्यों अपना ग्रास बनाती रही हैं?
राजनीतिक सिद्धांत बघारना इस राज्य का एक बड़ा शगल रहा है. हम इसे ‘पंडिताई’ कहने से परहेज कर रहे हैं क्योंकि इससे जातिवादी संकेत उभरते हैं. बिहार के लोगों में राजनीतिक जागरूकता, जुनून और बहसबाजी एक उद्योग का स्तर हासिल कर चुकी है. शायद यही वहां वास्तविक उद्योग की भारी कमी की भरपाई कर रही है. मैं यह हल्के रूप में नहीं कह रहा हूं. राजनीति का स्थायी जुनून देश के बाकी हिस्सों के मुक़ाबले बिहार के विनाश की मूल वजह है. पहचान की राजनीति कहीं भी हो वह पीछे की ओर ले जाती है, लेकिन बिहार में यह आत्मघाती जुनून का रूप ले चुकी है.
इस राज्य को शांघाई तो छोड़िए, गुजरात या कर्नाटक बनाने का भी वादा कोई नहीं कर रहा है. हर किसी की पीढ़ीगत शिकायतें हैं, और हर किसी का कोई नेता है जो इन शिकायतों को दूर करने का वादा कर रहा है. और जब हर कोई एक ही वादा कर रहा हो, तब आगे निकलने की उम्मीद वही करेगा जो ज्यादा पैसे फेंकेगा. जिस प्रदेश ने दुनिया को लोकतंत्र, भारत को उसका महात्मा और लोकनायक, और सामाजिक न्याय का आंदोलन दिया वह न्यूनतम अपेक्षाओं की राजनीति का अभिशाप भोग रहा है. यह राष्ट्रीय दुर्भाग्य ही है.
(नेशनल इंट्रेस्ट को अंग्रेज़ी में पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)
यह भी पढ़ें: जब भारत जंग में पाकिस्तान को वॉकओवर नहीं देता, तो क्रिकेट में क्यों दें?