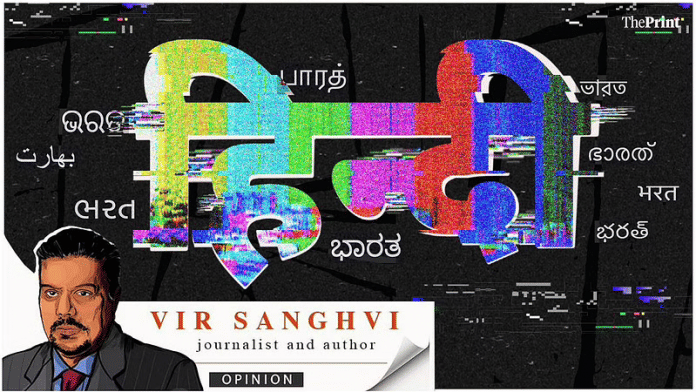भारत की विविधतापूर्ण और बहुलतावादी परंपराओं को कमजोर करने के लिए इन दिनों जितनी तरह के झूठ फैलाए जा रहे हैं उनमें इस दावे से ज्यादा घातक दूसरा कोई दावा नहीं होगा कि हिंदी भारत की राष्ट्रीय भाषा है. न यह आज है और न यह कभी रही है. यकीन न हो तो संविधान को देख लीजिए.
वास्तव में, भारत की कोई राष्ट्रीय भाषा है ही नहीं. यह संविधान सभा में हुई बहस (जो अक्सर बेहद तीखी भी हो जाया करती थी) का निष्कर्ष है. 1946 में, संयुक्त प्रांत (आज के उत्तर प्रदेश) से इस सभा के एक सदस्य आर.वी. धुलेकर ने एक घोषणा की थी, जिसके इन शब्दों की प्रतिध्वनि वर्तमान समय में फिर से उठ रही है कि ‘जो लोग हिंदुस्तानी नहीं जानते उन्हें भारत में रहने का कोई अधिकार नहीं है… बेहतर है वे यहां से चले जाएं.’
तब धुलेकर कोई आज के कंगना रनौत नहीं थे, सो जवाहरलाल नेहरू ने जब उन्हें समझाया-बुझाया तो वे शांत हो गए थे. लेकिन अकेले वही यह मांग नहीं कर रहे थे. संविधान सभा के कई सदस्य भी ऐसे मुद्दे उठा रहे थे जो आगे के वर्षों में बार-बार उभरने वाले थे— क्या कारों के नंबर प्लेट रोमन लिपि में हों या देवनागरी में? क्या केंद्र सरकार को राज्यों से हिंदी में पत्राचार करना चाहिए?
यह भी पढ़ें: हिंदी यूं ही लोकप्रिय नहीं, काफी सरकारी जोर-आजमाइश हुई है
हिंदी को थोपना कभी सरकारी एजेंडा नहीं रहा
नेहरू और गांधीजी, दोनों हिंदुस्तानी को (जो कि हिंदी से काफी मिलती-जुलती है मगर ‘आकाशवाणी’ वाली संस्कृतनिष्ठ हिंदी नहीं है) राष्ट्रीय भाषा बनाना चाहते थे लेकिन इसके खिलाफ दक्षिण भारत से उठी तेज आपत्तियों के आगे दोनों ने कदम खींच लिये. उदाहरण के लिए, टी.टी. कृष्णमाचारी ने, जो बाद में मद्रास से कैबिनेट मंत्री बने, ‘हिंदी साम्राज्यवाद’ की बात उठाई और चिंता प्रकट की कि दक्षिण के लोग गुलाम बन जाएंगे.
अंतिम समझौता यह हुआ कि कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं होगी और इसके बदले हिंदी के साथ अंग्रेजी भी सरकारी संवाद की राजभाषा बना दी गई.
मामला यहीं पर सुलझ जाना चाहिए था लेकिन एक खामी रह गई. संविधान ने कहा कि अंग्रेजी को सरकारी भाषा के तौर पर प्रयोग करने की समीक्षा 15 साल बाद की जाए. यह समीक्षा 1965 में की गई. तब तक भावनाएं और उभर आई थीं. भाजपा के पूर्ववर्ती जनसंघ ने मांग उठाई कि हिंदी को पूरे भारत में लागू किया जाए और उसे पढ़ाया भी जाए. हिंदी पट्टी में सिमटे जनसंघ के वोटरों की यह लोकप्रिय मांग थी और इन बहसों के कारण ही अटल बिहारी वाजपेयी राष्ट्रीय स्तर पर चमके थे.
लेकिन गैर-हिंदी राज्यों के नेताओं की ओर से जवाबी मुहिम चलाई गई. मैसूर, बंगाल, आंध्र और तमिलनाडु के कांग्रेसी नेताओं ने हिंदी थोपे जाने का विरोध किया. यह कांग्रेस के केंद्रीय नेताओं के रुख के विपरीत था. नेहरू 1950 में हिंदुस्तानी को लागू करना चाहते थे, तो प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री भी हिंदी को चाहते थे. शास्त्री अपना फैसला लागू करने की स्थिति में थे मगर पूरे दक्षिण भारत में हिंसक दंगे और विरोध शुरू हो गए.
आखिर में यह फैसला किया गया कि यथास्थिति बनाए रखी जाए और हिंदी पर ज़ोर न दिया जाए. यह स्थिति आज तक बनी हुई है.
1960 के दशक में भाषा को लेकर हुए दंगों के शांत होने के बाद तमाम समझदार नेता इस नतीजे पर पहुंचे कि हिंदी तो सरकारी हुक्मनामे के बिना भी फैलेगी. उसे दक्षिण वालों या बंगालियों पर जबरन थोपने की कोई जरूरत नहीं है.
इसकी कुछ तो वजह यह थी कि हिंदी पट्टी के लोग पूरे भारत में आवाजाही कर रहे हैं और अपनी भाषा लेकर जा रहे हैं. इसकी कुछ वजह यह भी थी कि भारत की लोकप्रिय संस्कृति में हिंदी वाला तत्व मजबूत है.
यह भी पढ़ें: ट्विटर एक शोरशराबे वाले मंच से ज्यादा कुछ नहीं, बीजेपी ये अच्छे से जानती है लेकिन पत्रकार नहीं
लोकप्रिय संस्कृति में हिंदी
मुंबईया फिल्म उद्योग को ही ले लीजिए. इसके ज्यादातर अगुआ उन राज्यों से आए जहां हिंदी मातृभाषा नहीं है, चाहे वे राज कपूर हों या राजेश खन्ना, यश चोपड़ा, ऋषिकेश मुखर्जी, बिमल राय, गुरुदत्त, वी. शांताराम, रमेश सिप्पी, गुलज़ार, के. आसिफ, देवानंद, नादियाडवाला परिवार, वैजयंतीमाला, स्मिता पाटिल, धर्मेंद्र, हेमा मालिनी, रेखा, श्रीदेवी, जया प्रदा, एकता कपूर, फराह खान, शर्मिला टैगोर, तब्बू, साहिर लुधियानवी, सुनील दत्त. यह सूची अनंत है. यहां तक कि अमिताभ बच्चन, जिन्हें यूपी वाले अपना बताते हैं, आधा पंजाबी हैं.
लेकिन मुंबईया फिल्म उद्योग ने इन सितारों के मूल को परे रखकर हिंदुस्तानी में फिल्में बनाई. इसने हिंदी और हिंदुस्तानी के विस्तार में जितनी मदद की उतनी शायद किसी बात ने नहीं की होगी. बाद में टेलीविज़न ने फिल्म उद्योग का ही अनुकरण किया.
भारत ने अंततः जिस भाषा नीति को अपनाया वह भारत की ही तरह पच्चीकारी वाली थी. अमेरिका सबको पिघलाकर एक सांचे में ढालता है. वहां प्रवासी चाहे जहां से आएं, उन्हें अंग्रेजी पढ़कर ‘अमेरिकन’ बन जाना पड़ता है.
लेकिन भारत में हमने पिघलाकर एक सांचे में ढालने वाली सोच को खारिज कर दिया. हरेक एक जैसा बन जाए या एक ही भाषा बोले, ऐसा कोई दबाव नहीं डाला गया. हर कोई अपनी मूल पहचान बनाए रखकर भारतीय हो सकता है. आप केवल तमिल बोलते हों या केवल बांगला बोलते हों, कोई किसी से कम भारतीय नहीं माना जाएगा. यही हमारी भाषा नीति का केंद्रीय तत्व बना. संकीर्ण भाषायी कसौटी के मुताबिक भारतीयता को परिभाषित नहीं किया जाता है.
इस मॉडल ने भारत को एकजुट बनाए रखा है. इसके विपरीत, पाकिस्तान ने जब अपने पूर्वी भाग के बांग्लाभाषी लोगों पर उर्दू थोपने की कोशिश की तो उसके ऊपर सांस्कृतिक दमन का आरोप लगा और इसने अंततः अलगाववादी भावना को जन्म दिया जिसके चलते पाकिस्तान टूट गया और बांग्लादेश बना.
भारत ने चूंकि हरेक भाषा को पनपने का मौका दिया और हिंदी चूंकि धीरे-धीरे अहिंदी भाषी राज्यों में निरंतर पैठ बना रही है इसलिए 1960 वाले भाषायी दंगों की पुनरावृत्ति नहीं हुई. लेकिन अब अचानक हिंदी थोपने की मांग क्यों उभर रही है?
मामला हिंदी बनाम अंग्रेजी का होता तो बात समझी जा सकती थी. भाजपा और उसके जनाधार में अंग्रेजी विरोधी भावना मजबूत है. लेकिन इस बार मामला हिंदी बनाम सभी भाषाओं का है.
यह भी पढ़ें: इंदिरा की तरह हैं मोदी- कांग्रेस को इतिहास से सबक लेना चाहिए, सोनिया और प्रशांत किशोर ला सकते हैं बदलाव
भाजपा भी हिंदी थोपने के खिलाफ थी
जबकि विवाद का भारतीय (और कामयाब) समाधान हो चुका है तब भाजपा उस झगड़े को फिर क्यों उभारना चाहती है? 1960 के दशक में हिंदी समर्थक अभियान से चमके वाजपेयी ने भी बाद में इससे हाथ खींच लिये थे क्योंकि उन्हें समझ में आ गया था कि हिंदी को जबरन लादने का उग्र विवाद पैदा करने से ज्यादा प्रभावी उपाय यह है कि हिंदी को धीरे-धीरे खुद ही अपना विस्तार करने दिया जाए.
इस मसले को फिर से उभारने की कोशिशों ने मुझे वाकई हैरत में डाल दिया है. वर्षों तक जनसंघ और भाजपा, कांग्रेस के इस कटाक्ष का विरोध करती रही है कि वह ‘हिंदी पट्टी के बनियों की पार्टी’ है. भाजपा के नये अवतार ने इस दावे का निर्णायक जवाब दे दिया है और उसने दिखा दिया है कि उसकी राष्ट्रीय महत्वाकांक्षाओं की सीमा हिंदी पट्टी से कहीं आगे तक फैल चुकी है.
तो जनसंघ वाले दौर के, जब उसका जनाधार हिंदी पट्टी में ही सिमटा हुआ था- पुराने पड़ चुके मंच को वह फिर क्यों सजाने पर आमादा है? इससे उसे हिंदी पट्टी में कोई फायदा नहीं होने वाला क्योंकि वह इसमें जहां तक आगे बढ़ चुकी है उससे आगे नहीं जा सकती. लेकिन यह हिंदी पट्टी के बाहर के उन क्षेत्रों के मतदाताओं को नाराज करेगा, जहां वह अपना प्रभाव बढ़ाना चाहती है और यह साबित करना चाहती है कि वह केवल हिंदी क्षेत्र की पार्टी नहीं है.
अगर इसके पीछे कोई कुटिल चाल नहीं है जिसे मैं नहीं समझ पाया हूं, तो मेरा अनुमान यही है कि अमित शाह के मुंह से पुराना ‘संघी’ नारा फिसल गया जिसके पीछे शायद कोई राष्ट्रीय बहस शुरू करने की मंशा न रही हो. उनके आज्ञाकारी समर्थकों ने तोते की तरह उसे दोहरा दिया.
लेकिन इस बहस के नतीजे जब जाहिर हो रहे हैं तब भाजपा को इसे खामोशी से दफना देने की पहल करनी चाहिए. आप उन लोगों पर हिंदी नहीं थोप सकते जो यह मानने को तैयार नहीं हैं कि हिंदी उनकी भाषा से श्रेष्ठ है. ऐसा करके आप न केवल भारत के बहुलतावादी और विविधतावादी सोच को चोट पहुंचाते हैं, बल्कि आप नरेंद्र मोदी की भाजपा को हिंदी पट्टी वाले एजेंडा की क्षेत्रीय पार्टी में तब्दील कर देते हैं.
मोदी इतने चतुर तो हैं ही कि वे इस धारणा को मजबूत नहीं होने देंगे.
(वीर सांघवी भारतीय प्रिंट और टीवी पत्रकार, लेखक और टॉक शो होस्ट हैं. उनका ट्विटर हैंडल @virsanghvi है. व्यक्त विचार निजी हैं)
(इस लेख को अंग्रेज़ी में पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)
यह भी पढ़ें: हिजाब, हलाल, नवरात्रि के बहाने मोदी का भारत मुसलमानों को नहीं बल्कि हिंदुओं दे रहा है संदेश