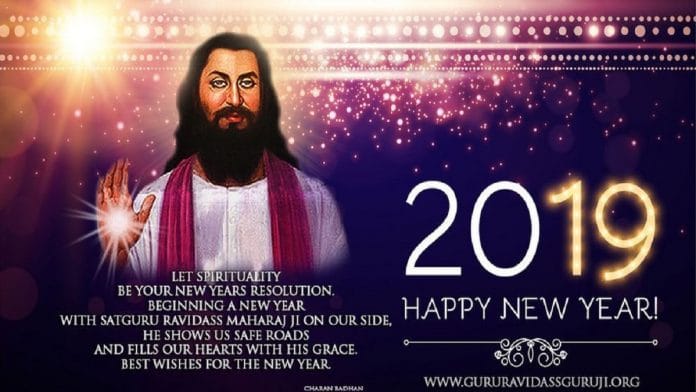डॉ. आंबेडकर ने अपनी किताब प्राचीन भारत में क्रांति और प्रतिक्रांति में लिखा है कि भारत का इतिहास क्रांति और प्रतिक्रांतियों का इतिहास है. यहां निरंतर ब्राह्मणवाद और दलित-बहुजन परंपरा के बीच संघर्ष चलता रहा है. प्राचीनकाल में बुद्ध ने ब्राह्मणवाद को चुनौती दी. मध्यकाल में उत्तर भारत में कबीर और रैदास ने ब्राह्मणवाद को चुनौती दी. रैदास ने जन्म के आधार पर श्रेष्ठता की अवधारणा को पूरी तरह खारिज कर दिया-
रैदास बाभन मत पूजिए जो होवे गुन हीन,
पूजिए चरन चंडाल के जो हो गुन परवीन.
एक ओर ब्राह्मणवादी परंपरा परजीवी, निठल्ली परंपरा रही है. द्विज जातियां दलित-बहुजनों के श्रम पर पलती रही हैं. वहीं, दलित-बहुजन परंपरा श्रम संस्कृति की वाहक रही है. रैदास स्वयं भी श्रम करके जीवन-यापन करते थे. वे चर्मकार का काम करते थे और श्रम करके जीने को सबसे बड़ा मूल्य मानते हैं. घर-बार छोड़कर वन जाने या सन्यास लेने
को ढोंग-पाखण्ड मानते हैं—
नेक कमाई जउ करइ गृह तजि बन नहिं जाय.
रैदास अभिमानी परजीवी ब्राह्मण की तुलना में श्रमिक को ज्यादा महत्व देते हैं-
धरम करम जाने नहीं, मन मह जाति अभिमान,
ऐ सोउ ब्राह्मण सो भलो रविदास श्रमिकहु जान.
बुद्ध की तरह रैदास ने भी ऊंच-नीच अवधारणा और पैमाने को पूरी तरह उलट दिया. वे कहते हैं कि जन्म के आधार पर कोई नीच नहीं होता है, बल्कि वह व्यक्ति नीच होता है, जिसके हृदय में संवेदना और करुणा नहीं है-
दया धर्म जिन्ह में नहीं, हद्य पाप को कीच,
रविदास जिन्हहि जानि हो महा पातकी नीच.
उनका मानना है कि व्यक्ति का आदर और सम्मान उसके कर्म के आधार पर करना चाहिए, जन्म के आधार पर कोई पूज्यनीय नहीं होता है. बुद्ध, कबीर, फुले, आंबेडकर और पेरियार की तरह रैदास भी साफ कहते हैं कि कोई ऊंच या नीच अपने मानवीय कर्मों से होता है, जन्म के आधार पर नहीं. वे लिखते हैं—
रैदास जन्म के कारने होत न कोई नीच,
नर कूं नीच कर डारि है, ओछे करम की नीच.
आंबेडकर की तरह रैदास का भी कहना है कि जाति एक ऐसा रोग है, जिसने भारतीयों की मनुष्यता का नाश कर दिया है. जाति इंसान को इंसान नहीं रहने देती. उसे ऊंच-नीच में बांट देती है. एक जाति का आदमी दूसरे जाति के आदमी को अपने ही तरह का इंसान मानने की जगह ऊंच या नीच मानता है. रैदास का कहना है कि जब तक जाति का खात्मा नहीं होता, तब तक लोगों में इंसानियत जन्म नहीं ले सकती-
जात-पात के फेर मह उरझि रहे सब लोग,
मानुषता को खात है, रैदास जात का रोग.
वे यह भी कहते हैं कि जाति एक ऐसी बाधा है, जो आदमी को आदमी से जुड़ने नहीं देती है. वे कहते हैं एक मनुष्य दूसरे मनुष्य से तब तक नहीं जुड़ सकता, जब तक जाति का खात्मा नहीं हो जाता—
रैदास ना मानुष जुड़े सके जब लौं जाय न जात
दलित-बहुजन परंपरा के अन्य कवियों की तरह रैदास भी हिंदू-मुस्लिम के बीच कोई भेद नहीं करते. वे दोनों के पाखण्ड को उजागर करते हैं. वे साफ शब्दों में कहते हैं कि न मुझे मंदिर से कोई मतलब है, न मस्जिद से, क्योंकि दोनों में ईश्वर का वास नहीं है—
मस्जिद सो कुछ घिन नहीं मन्दिर सो नहीं प्यार,
दोउ अल्ला हरि नहीं कह रविदास उचार.
रैदास मंदिर-मस्जिद से अपने को दूर रखते हैं, लेकिन हिंदू-मुस्लिम दोनों से प्रेम करते हैं—
मुसलमान से दोस्ती, हिन्दुवन से कर प्रीत,
रविदास ज्योति सभ हरि की, सभ हैं अपने मीत.
रैदास बार-बार इस बात पर जोर देते हैं कि हिंदुओं और मुसलमानों में कोई भेद नहीं है. जिन तत्वों से हिंदू बने हैं, उन्हीं तत्वों से मुसलमान. दोनों के जन्म का तरीका भी एक ही है—
हिन्दू तुरूक महि नाहि कछु भेदा दुई आयो इक द्वार,
प्राण पिण्ड लौह मास एकहि रविदास विचार.
ब्राह्मणवादी द्विज परंपरा के विपरीत दलित-बहुजन परंपरा के कवि श्रम की संस्कृति में विश्वास करते हैं. उनका मानना था कि हर व्यक्ति को श्रम करके ही खाना खाने का अधिकार है—
रविदास श्रम कर खाइए है, जो-लौ-पार बसाय.
नेक कमाई जौ करई कबह न निष्फल जाय.
रैदास एक ऐसे समाज की कल्पना करते हैं, जहां संपत्ति पर निजी मालिकाना नहीं होगा, समाज अमीर और गरीब में बंटा नहीं होगा, कोई दोयम दर्जे का नागरिक नहीं होगा और न ही वहां कोई छूत-अछूत होगा. अपने इस समाज को उन्होंने बेगमपुरा, बिना गम यानी बिना दुख का शहर, नाम दिया है-
बेगमपुरा सहर को नाउ, दुखु-अंदोहु नहीं तिहि ठाउ.
ना तसवीस खिराजु न मालु, खउफु न खता न तरसु जुवालु.
अब मोहि खूब बतन गह पाई, ऊहां खैरि सदा मेरे भाई.
काइमु-दाइमु सदा पातिसाही, दोम न सोम एक सो आही.
आबादानु सदा मसहूर, ऊहाँ गनी बसहि मामूर.
तिउ तिउ सैल करहि जिउ भावै, महरम महल न को अटकावै.
कह ‘रविदास’ खालस चमारा, जो हम सहरी सु मीतु हमारा
हिंदी के द्विज आलोचकों ने रैदास को सगुणमार्गी और सनातन धर्म का संत ठहराने की कोशिश किया और उन्हें वेदों-पुराणों का समर्थक बताने की कोशिश की. जबकि सच्चाई यह है कि उन्होंने चारों वेदों को खारिज किया है-
चारो वेद किया खंडौति, ताकौ विप्र करे डंडौति
दलित-बहुजन परंपरा के अन्य कवियों की तरह रैदास के मन में भी अपनी जाति और पेशे को लेकर कोई हीनताबोध का भाव नहीं है. वे यह कहते हैं—
ऐसी मेरी जाति विख्यात चमार.
ऐसा माना जाता है कि संत रैदास का जन्म 1398 में हुआ था और उनकी मृत्यु 1518 में हुई. उनका जन्म काशी (बनारस) में चर्मकार परिवार में हुआ था. इन संत कवियों के काव्य का आधार बौद्ध धम्म की मानवीय करुणा और समता की विचारधारा रही है. साहित्यकार कंवल भारती के शब्दों में, ‘संत काव्य का वास्तविक आधार बौद्ध धर्म है. बौद्ध धर्म के पतन के बाद जो बुद्ध वचन परंपरा से जन-जीवन में संचित थे, संत काव्य में उन्हीं की अभिव्यंजना हुई है. इसका सबसे प्रबल प्रमाण यह है कि संतों का साहित्य जीवन की स्वीकृति का साहित्य है, उसमें पीड़ित जन का आक्रोश और आवेश, सुखी समाज की आकांक्षा, और शोषक श्रेणी के प्रपंचों पर आघात है, और सबसे बढ़कर समता, स्वतंत्रता और बंधुत्व की स्पष्ट अभिव्यक्ति है.’
(यह लेख 19 फरवरी को प्रकाशित किया जा चुका है)
(लेखक हिंदी साहित्य में पीएचडी हैं और फ़ॉरवर्ड प्रेस हिंदी के संपादक हैं.)