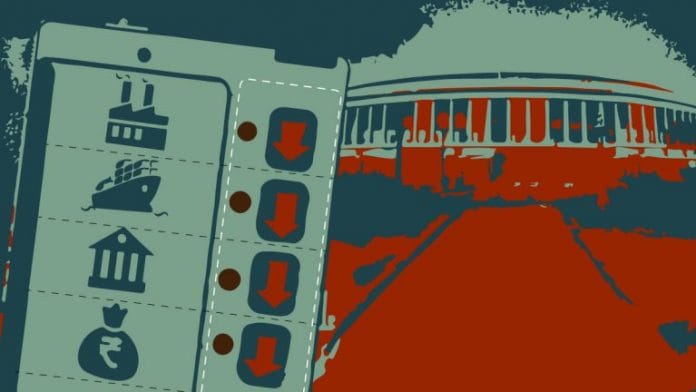चुनाव प्रचार से उड़ी धूल जब बैठ जाएगी और नई सरकार बागडोर संभाल लेगी तब उसे आर्थिक मंदी का सामना करना पड़ेगा. ध्यान देने वाली बात यह है कि मुद्दा यह नहीं होगा कि वृद्धि दर फिर से 7 प्रतिशत के आंकड़े को कब छूएगी या इसके ऊपर कब जाएगी, बल्कि यह होगा कि यह 6.5 प्रतिशत के इर्द-गिर्द कब तक घूमती रहेगी. पहली बात तो यह है कि हम यह मान कर न चलें कि पहले जो था उस स्तर पर वापसी स्वतः हो जाएगी; दूसरी बात यह कि जीडीपी के आंकड़ें की विश्वसनीयता तार-तार हो चुकी है. इसलिए ध्यान वास्तविक आंकड़ों पर दिया जाए जिनसे छेड़छाड़ नहीं हो सकती. ये आंकड़े परेशान करने वाली कहानी कहते हैं.
व्यापारिक वस्तुओं का निर्यात लगभग पिछले पांच वर्षों से सुस्त है. यह घरेलू मैन्युफैक्चरिंग की नाकामी को दर्शाता है, और इसने अर्थव्यवस्था को अंतर्मुखी बना दिया है. टैक्स से आय में पहले तो उछाल दिखी, फिर यह गिर गई है. जीएसटी के मद में जो आमद है उससे साफ है कि व्यापार में उछाल नहीं है. उपभोग के आंकड़े कई क्षेत्रों में गिरावट दर्शाते हैं, जिससे कॉर्पोरेट बिक्री और मुनाफे प्रभावित हो रहे हैं. कर्ज के भारी बोझ के कारण बैलेंसशीटों पर दबाव कायम है. तमाम उद्यमी कर्ज का बोझ घटाने की जुगत में भिड़े हैं. इनमें से कुछ तो हाथ खड़े करते हुए बेच कर बाहर निकल रहे हैं, खासकर विदेशी निवेशकों को बेच कर, और बाकी खुद को दिवालिया घोषित कर रहे हैं.
यह भी पढ़ें: अगर मोदी की सत्ता में वापसी नहीं होती तो उसका ज़िम्मेदार विपक्ष नहीं वो खुद होंगे
इस्पात, सीमेंट, बिजली के ‘कोर सेक्टर’ के उत्पादन आंकड़े किसी उछाल के संकेत नहीं दे रहे हैं. भारतीय अर्थव्यवस्था पर नज़र रखने के लिए केंद्र ने जिन कॉर्पोरेट प्रोजेक्टों को चुना था वे भी लंबे समय से सुस्त पड़े हैं. प्रोजेक्टों के लिए सरकारी कोश से मदद में कटौती हो गई है (या पिछले कामों के लिए भुगतान नहीं किए गए हैं) क्योंकि राजस्व में कमी आ गई है. पूंजी की आमद के कारण बाहरी खाता संतोषजनक है लेकिन चालू खाते का घाटा परेशान करने वाला है.
वित्त क्षेत्र घिसटता आ रहा है. क्रेडिट की आमद तो सुधरी है मगर बैंक अभी भी मुश्किल में हैं. सरकारी बैंकों ने अंतिम तिमाही तक 52,000 करोड़ से ज्यादा के खराब कर्ज जारी किए हैं, जो पिछले आंकड़े का लगभग दोगुना है. उधार देने वाली अगली जमात गैर-बैंकिंग वित्त कंपनियों की है, जिनमें अपनी बैलेंस शीट में छिपे राज के कारण आत्मविश्वास की कमी है और उन्हें लिक्विडिटी की समस्या का सामना करना पड़ रहा है.
इस तरह की बहुआयामी, चौतरफा मंदी का सामना कोई सरकार कैसे करे? वह आर्थिक कारोबार को मजबूती देने के लिए मौद्रिक तथा वित्तीय कदम उठाती है. लेकिन रिज़र्व बैंक ने ब्याज दरों में जो कटौती की वह बाज़ार में वास्तविक दरों में परिलक्षित नहीं हुई है. जहां तक वित्तीय नीति की बात है, घाटा इतना बड़ा है कि सरकार वित्तीय अनुशासन न लागू करे तो करों में छूट देना नामुमकिन है. अगर वह ऐसा करती है तो सरकारी उधार इतना बढ़ जाएगा कि मौद्रिक नीति के लिए बड़ी समस्या पैदा हो जाएगी. तीसरा समाधान यह है कि भारतीय माल को विदेश में सस्ता करने और प्रतिस्पर्धा में लाने के लिए रुपये का अवमूल्यन किया जाए. इससे भारत को ग्लोबल खिलाड़ियों के लिए आकर्षक बनाया जा सकता है. लेकिन किसी भी सरकार ने इस रास्ते पर कदम रखने के बारे में नहीं सोचा.
यह भी पढ़ें : चुनावी वादों को निभाने के बजाए, नई सरकार को अर्थव्यवस्था के मामले में ठंडे दिमाग से काम लेना होगा
असली खतरा यह है कि पिछले आर्थिक सुधारों ने जो गति प्रदान की थी वह टूट न जाए, इसलिए सिस्टम को ज्यादा प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए नए ढांचागत सुधार करने होंगे. पिछले 15 वर्षों में ऐसे सुधार नहीं किए गए हैं इसलिए एजेंडा जस का तस है— जमीन, श्रम और पूंजी के मामले में सुधार करने होंगे. इसका अर्थ है कि अहम कानूनों में बदलाव, सरकारी कंपनियों को कड़े बजट प्रावधानों से बांधना (एअर इंडिया सरीखों को उबारने की कोशिश से परहेज). राजनीतिक लिहाज से यह असंभव-सा है, क्योंकि इससे कामगारों और किसानों को परेशानी होगी, जो पहले से ही दबाव में माने जा रहे हैं.
तथ्यों और तर्कों से एक ही निष्कर्ष निकलता है कि देश को सुस्त वृद्धि के लिए तैयार रहना होगा. यह पहले से स्पष्ट है, लेकिन इसे जीडीपी और बेरोजगारी के आंकड़ों से खिलवाड़ करके (और प्रतिकूल पड़ने वाले को दबा करके) छिपा दिया जाता है. मनमोहन सिंह सरकार के जाने के साथ आर्थिक वृद्धि दर 7 प्रतिशत के आंकड़े से नीचे होती गई. आज सरकारी आंकड़ा भी इसे 7 प्रतिशत से नीचे दिखा रहा है. चूंकि यह दर युवाओं को रोजगार देने के लिए पर्याप्त नहीं है इसलिए इसका राजनीतिक और सामाजिक असर होगा और कमजोर अर्थव्यवस्था लोकलुभावनवाद के लिए उर्वर ज़मीन तैयार करेगी.
(इस खबर को अंग्रेजी में पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)