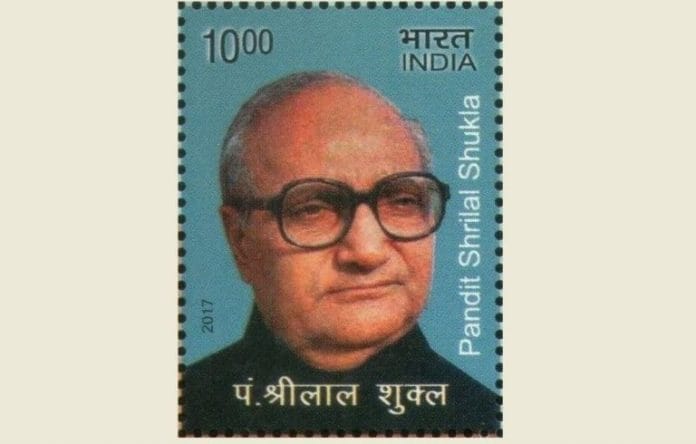हिंदी साहित्य में ‘राग दरबारी’ एक अप्रतिम रचना है, जो अपने प्रकाशित होने के 50 साल बाद भी भारतीय ब्यूरोक्रेसी और ‘पंचायती राज की पॉलिटिक्स’ पर करारा व्यंग्य करती है. 50 साल बाद भी हमें गांवों से आने वाली कहानियां ऐसी ही नज़र आती हैं. हमारी कल्पना में अब भी राग दरबारी गांवों की राजनीति का पर्याय है. हमें इस उपन्यास के पात्रों और घटनाओं पर हंसी आती है, इनके परिणामों पर तिरस्कार की भावना आती है. पर पढ़ते हुए हम उन प्रताड़नाओं को महसूस नहीं कर पाते जो उपन्यास में लगातार बने रहने वाले पात्र लंगड़ के साथ हुआ था. हमें उससे सहानुभूति तो होती है पर ये भी लगता है कि हम कहीं न कहीं वैद्य जी, रुप्पन बाबू या रंगनाथ के शहरी या ग्रामीण अभिजात्य वर्ग से हैं. अगर ‘हमें’ की जगह ‘मुझे’ कर दिया जाए तो बात ज़्यादा क्लियर हो सकती है. यहीं पर ये बात उठाई जा सकती है कि अगर किसी दलित व्यक्ति ने राग दरबारी लिखी होती तो उसका रूप कैसा होता? क्या ये व्यंग्य रचना हो पाती?
इसके परिप्रेक्ष्य में राग दरबारी का एक उद्धरण कुछ यूं ले सकते हैं-
‘चमरही’ गांव के एक मुहल्ले का नाम था, जिसमें चमार रहते थे. चमार एक जाति का नाम था, जिसे अछूत माना जाता था. अछूत एक प्रकार के दुपाये का नाम है जिसे लोग संविधान लागू होने से पहले छूते नहीं थे. संविधान एक कविता का नाम है, जिसके अनुच्छेद 17 में छुआछूत खत्म कर दी गई है, क्योंकि इस देश के लोग कविता के सहारे नहीं, बल्कि धर्म के सहारे रहते हैं और क्योंकि छुआछूत इस देश के लोगों का धर्म है, इसलिये शिवपाल गंज में भी दूसरे गांवों की तरह अछूतों के अलग अलग मुहल्ले थे और उनमें सबमें प्रमुख मुहल्ला चमरही था…’
अगर दलित लेखन को देखें तो प्रोफेसर तुलसी राम के आत्मकथात्मक उपन्यास ‘मुर्दहिया’ से एक उद्धरण इस प्रकार है-
‘मुर्दहिया’ हमारे गांव धरमपुर (आजमगढ़) की बहुउद्देशीय कर्मस्थली था. चरवाही से लेकर हरवाही तक के सारे रास्ते वहीं से गुज़रते थे. इतना ही नहीं, स्कूल हो या दुकान, बाजार हो या मंदिर, यहां तक कि मज़दूरी के लिए कलकत्ता वाली रेलगाड़ी पकड़ना हो, तो भी मुर्दहिया से ही गुजरना पड़ता था. हमारे गांव की ‘जियो-पॉलिटिक्स’ यानि ‘भू-राजनीति’ में दलितों के लिए मुर्दहिया एक सामरिक केन्द्र जैसी थी. जीवन से लेकर मरन तक की सारी गतिविधियां मुर्दहिया समेट लेती थी. सबसे रोचक तथ्य यह है कि मानव और पशु में कोई फर्क नहीं करती थी. वह दोनों की मुक्तिदाता थी. विशेष रूप से मरे हुए पशुओं के मांसपिंड पर जूझते सैकड़ों गिद्धों के साथ कुत्ते और सियार मुर्दहिया को एक कला-स्थली के रूप में बदल देते थे. रात के समय इन्हीं सियारों की ‘हुआं-हुआं’ वाली आवाज़ उसकी निर्जनता को भंग कर देती थी. हमारी दलित बस्ती के अनगिनत दलित हज़ारों दुख-दर्द अपने अंदर लिए मुर्दहिया में दफन हो गए थे. यदि उनमें से किसी की भी आत्मकथा लिखी जाती, उसका शीर्षक ‘मुर्दहिया’ ही होता.
राग दरबारी पढ़ते हुए छुआछूत के प्रति जुगुप्सा नहीं होती, हंसी आती है. पर मुर्दहिया का उद्धरण पढ़ के क्रोध और ग्लानि होती है.
राग दरबारी के एक प्रमुख पात्र (संभवतः दलित) सनीचर की राजनीतिक चेतना कुछ यूं बढ़ती है-
‘जैसे भारतीयों की बुद्धि अंग्रेज़ी की खिड़की से झांककर संसार का हालचाल देती है, वैसे ही सनीचर की बुद्धि रंगनाथ की खिड़की से झांकती हुई दिल्ली का हालचाल लेने लगी’.
रंगनाथ शहर से आये हुए कथित उच्च जाति के युवा प्रतीत होते हैं. वहीं तुलसी राम अपने सगे चाचा और जेदी चाचा का ज़िक्र करते हुए बताते हैं कि उनकी वजह से उन्हें कम्युनिज़्म, विदेशी पॉलिटिक्स, प्रतिरोध इत्यादि की समझ आई. एक तरह से वो उनको अपना गुरू मानते हैं. राग दरबारी में सनीचर की चेतना के बारे में पढ़ते हुए लगता है कि कोई उच्च जाति का इंसान ही दलित समाज में ये चेतना जगा सकता है. पर मुर्दहिया पढ़ते हुए लगता है कि राजनीतिक चेतना तो किसी एक शब्द से भी जग सकती है.
राग दरबारी का पात्र लंगड़ एक नकल यानी पेपर की एक फोटोकॉपी लेने के लिए कचहरी के चक्कर काटते काटते प्राण त्याग देता है. उसकी पीड़ा समझ में आती है, पर महसूस नहीं हो पाती. लगता है कि ऐसा ही होता है, हम इसमें क्या कर सकते हैं. पर जब मुर्दहिया में हम अध्यापकों द्वारा जातिसूचक शब्द इस्तेमाल होते देखते हैं, तो क्रोध आता है, इस व्यवस्था को बदलने का जी चाहता है. सनीचर के प्रति छोटे पहलवान या रंगनाथ या रुप्पन बाबू का नजरिया देखकर हंसी ही आती है. पर एक दलित के प्रति जातिसूचक शब्द या उसकी आंख की कमी को उसके व्यक्तित्व का पर्याय बना देना मर्मांतक पीड़ा देता है.
यहां यह साबित करने की कोशिश नहीं है कि राग दरबारी एक ‘जातिवादी’ उपन्यास है या फिर किसी ‘ब्राह्मण’ द्वारा लिखा हुआ उपन्यास है. बस ये समझने की कोशिश की जा रही है कि 1967 में लिखे राग दरबारी में आजादी के 17 वर्षों का जो खाका खींचा गया वो 50 साल बाद बदला क्यों नहीं. जिस समय वो उपन्यास आया था, वो एक करारा व्यंग्य था. अगर देश में बदलाव आता तो एक व्यंग्यात्मक उपन्यास एक दलित की तरफ से भी आ सकता था. ये एक कमाल की बात है कि आज़ादी के 70 साल बाद भी एक दलित व्यक्ति का कथन करारा व्यंग्य नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें हंसने जैसा कुछ है ही नहीं. सनातन पीड़ा की द्योतक ये कहानी हंसी में कैसे तब्दील हो सकती है?
ऑस्कर वाइल्ड ने अपने उपन्यास द पिक्चर ऑफ डोरियन ग्रे में तत्कालीन विक्टोरियन समाज पर कटाक्ष किया था. पर वो कटाक्ष भी अभिजात्य वर्ग के लिए ही था. ऑस्कर वाइल्ड उस अभिजात्य वर्ग की प्रताड़ना से खुद नहीं बच सके. बड़प्पन की झूठी शान बघारते उस समाज ने ऑस्कर वाइल्ड की इहलीला ही समाप्त कर दी. अगर ऑस्कर वाइल्ड ने अपने गे होने की कहानी को लिखा होता तो शायद वो विक्टोरियन समाज को ज़्यादा तोड़ता. यहां भी ऑस्कर वाइल्ड को सलाह देने की हिमाकत नहीं की जा रही, बस सामाजिक प्रताड़ना से लड़ने में लेखन की तैयारी को समझने की कोशिश की जा रही है.
2016 में बुकर पुरस्कार से सम्मानित कृति द सेलआउट के लेखक पॉल बेट्टी अश्वेत समुदाय के हैं और उन्होंने ये उपन्यास व्यंग्यात्मक शैली में लिखा है. ज्ञात हो कि अमेरिका में श्वेत और अश्वेत का अंतर अभी भी बहुत ज़्यादा है. पर पॉल बेट्टी का ये व्यंग्यात्मक लेखन और इसे मिला पुरस्कार ये दर्शाता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अश्वेतों के संघर्ष को समझा जा रहा है. पर भारतीय दलित लेखन की अंतर्राष्ट्रीय अनुपस्थिति हतप्रभ करने वाली है, समझ नहीं आ रहा कि कोई इसे समझने का प्रयास कर भी रहा है कि नहीं. ये फिक्शन की ही बात हो रही है. हालांकि, अरविंद अडिगा की बुकर सम्मानित कृति द वाइट टाइगर एक तरीके से जातिवादी व्यवस्था से पीड़ित व्यक्ति की ही कहानी है. पर अपने समग्र रूप में वो एक व्यक्ति की कहानी हो जाती है. अइन रैंड के उपन्यास द फाउंटेनहेड के पात्र गेल विनांड की तरह, जिसकी सफलता में उसके कुकर्म समेत उसकी पीड़ा भी छुप जाती है.
रुप्पन बाबू के शब्दों में पूरे देश में शिवपालगंज फैला हुआ है. पर अपने समाज को देखें तो पता लगता है कि पूरे देश में मुर्दहिया फैली हुई है. और ये बात मज़ाक या व्यंग्य की नहीं है. वैद्य जी के शब्दों में- दिल्लगी मत करो! गम्भीर बात को हंसी में मत उड़ाओ.
क्योंकि मलखान सिंह अपनी कविता सुनो ब्राह्मण में लिखते हैं-
सुनो ब्राह्मण ! हमारी दासता का सफर / तुम्हारे जन्म से शुरू होता है /और इसका अंत भी / तुम्हारे अंत के साथ होगा.
(लेखक पूर्व पत्रकार हैं, @abhishapt ट्विटर हैंडल है)