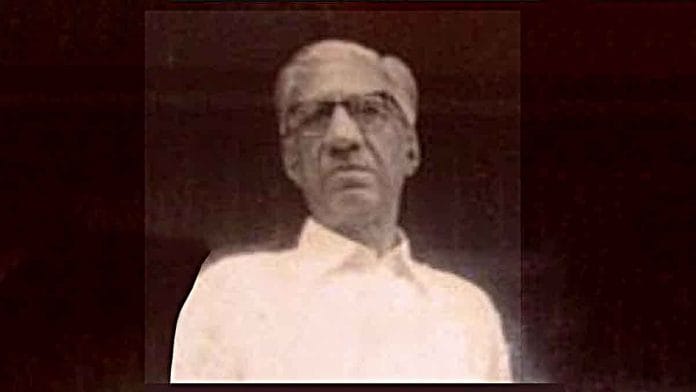पढ़कर कुछ याद आया आपको? तो बताइये, किसने रचा यह गीत? नहीं याद कर पा रहे? कोई बात नहीं. अपनी सर्जना के सौ साल पूरे करने की ओर बढ़ रहा कोई गीत अपने रचयिता को एकदम से बिसरा दिये जाने के बावजूद आम लोगों के जेहन में इस तरह ताजा बना रहे, तो इसमें भी रचयिता की हार नहीं जीत ही होती है.
यों, इस गीत के रचनाकार की एक कहानी का नाम भी हार-जीत से जुड़ा है-‘हार की जीत’! हां-हां, वही बाबा भारती, उनके घोड़े सुल्तान और डाकू खड़ग सिंह वाली, जिसमें बाबा के जान से भी प्यारे सुल्तान को उनसे छीन लेने की फिराक में अपाहिज का भेष धरकर रास्ते में बैठा डाकू खड़ग सिंह छल करके अपने मकसद में कामयाब हो जाता है, तो बाबा उससे कहते हैं-घोड़ा ले जाओ. मगर मेरी एक प्रार्थना सुनते जाओ. किसी से कहना नहीं कि तुमने इस तरह मुझसे मेरा घोड़ा छीना. वरना लोग दीन-दुखियों व अशक्तों पर भरोसा करना छोड़ देंगे.
जीत के नशे में खड़ग सिंह उस वक्त तो उन्हें कोई उत्तर दिये बिना चला जाता है लेकिन बाद में यह सोच-सोचकर ग्लानिग्रस्त हो जाता है कि एक बाबा भारती हैं, जिन्हें मुझ जैसे डकैत का शिकार होते वक्त भी अपनी नहीं दीनों व दुखियारों का भरोसा टूटने की चिंता थी और एक मैं हूं कि किसी का भरोसा टूटे या दिल, मेरी बला से! ग्लानि बर्दाश्त से बाहर हो जाती है तो वह रात के अंधेरे में सुल्तान को चुपके से बाबा के उसी अस्तबल में बांध जाता है, जहां बाबा ने सुल्तान को पहली बार उसे दिखाया था!
बुरे से बुरे व्यक्ति के भीतर भी भलाई के तत्व होने और किसी न किसी दिन उनके जीत जाने के अदम्य विश्वास से भरी इस कालजयी कहानी को इसमें समाहित अनूठे आदर्शवाद के लिए अलग से रेखांकित किया जाता है.
आपको जानकर ताज्जुब होगा कि यह अपने रचनाकार की पहली ही कहानी थी, जो 1920 में अपने समय की सर्वश्रेष्ठ पत्रिका ‘सरस्वती’ में छपी। ऐसा कम ही होता है कि किसी रचनाकार की पहली ही कहानी, और कहानी ही क्यों, उसके पात्र भी अजर-अमर हो जायें! यहां तक कि लोग उनकी कल्पना करने वाले कथाकार को भले ही भूल जायें, उन्हें न भुला पायें! लेकिन ‘हार की जीत’ के साथ कुछ ऐसा ही हुआ और उसके प्रकाशन के बाद से अब तक देश की कई पीढ़ियां धोखा देने वाले को बाबा भारती की आंख से देखती आयी हैं.
आप पढ़ना चाहें तो यह कहानी महात्मा गांधी अन्तरराष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय की कवियों व लेखकों से सम्बन्धित वेवसाइट पर, नहीं तो 2014 में नेशनल बुक ट्रस्ट द्वारा स्मिता चतुर्वेदी के सम्पादन में प्रकाशित ‘सुदर्शन’ नाम की पुस्तक में उपलब्ध है.
अरे, आप तो समझ गये! जी हां, उन रचनाकार का नाम था सुदर्शन, जिन्होंने इसके अलावा ‘अंधकार’, ‘गुरुमंत्र’, ‘दिल्ली का अंतिम दीपक’, ‘परिवर्तन’, ‘राजा’, ‘सच का सौदा’, ‘अठन्नी का चोर’, ‘तीर्थयात्रा’, ‘पत्थरों का सौदागर’, ‘पृथ्वीवल्लभ’ और साइकिल की सवारी जैसी अमर कहानियां लिखीं.
1896 में अविभाजित भारत के स्यालकोट में, जो अब पाकिस्तान में है, पैदा हुए सुदर्शन अपने चार भाई बहनों में दूसरे थे. उनका माता-पिता का दिया नाम बदरीनाथ भट्ट था और छुटपन में ही दोनों को खो देने के बाद उन्होंने ढेरों तकलीफें भोगीं. स्यालकोट में ही जैसे-तैसे बी.ए. करने के बाद वे रोजगार की तलाश में लाहौर चले गये, जहां से उर्दू का एक अपने समय का बड़ा ही लोकप्रिय अखबार निकाला.
इसी बीच बटाला गुरुदासपुर की एक कन्या से उनका विवाह हुआ और कुछ मित्रों के खराब बरताव के कारण वे 1932 में लाहौर छोड़कर कलकत्ता चले गये, जहां उन दिनों चल रही टाकीजों में अच्छे लेखकों की बहुत मांग थी. लेकिन वहां भी उनका मन रमा नहीं और 1938 में वे मुम्बई जा पहुंचे.
जाहिर है कि मुंशी प्रेमचंद और उपेन्द्रनाथ ‘अश्क’ की तरह वे भी उर्दू से हिन्दी में आये और प्रेमचंद की ही तरह उनकी भाषा भी सहज, स्वाभाविक और मुहावरेदार है. अपने समय के दूसरे सुधारवादी सर्जकों की तरह उनके लेखन का लक्ष्य भी समाज व राष्ट्र का पुनर्निर्माण कर उन्हें गुलामी की गन्दगियों व कमजोरियों से मुक्ति दिलाकर सुदृढ़ बनाना था. उनकी गणना प्रेमचंद संस्थान के विश्वम्भरनाथ कौशिक, राजा राधिकारमण प्रसाद सिंह और भगवतीचरण वाजपेयी जैसे रचनाकारों के साथ की जाती थी. लाहौर की उर्दू पत्रिका ‘हजार दास्तां’ में उनकी कहानियां प्रायः प्रकाशित होती थीं। उनकी कई पुस्तकें मुम्बई के हिन्दी ग्रंथ रत्नाकर कार्यालय से भी छपीं.
1945 में महात्मा गांधी द्वारा प्रस्तावित अखिल भारतीय हिन्दुस्तानी प्रचारसभा, वर्धा की साहित्य परिषद के वे सम्मानित सदस्य थे. गांधी जी के ही अनुरोध पर उन्होंने ‘सबकी बोली’ नाम से हिन्दी की एक पुस्तिका लिखी थी जो बहुत दिनों तक कक्षा चार के बच्चों को पढ़ाई जाती रही.
कहानियों के अलावा सुदर्शन फिल्म निर्माण के क्षेत्र में भी सक्रिय रहे। दशक भर लम्बे फिल्मी कैरियर में उन्होंने कई फिल्मों की पटकथाएं और गीत भी लिखे. 1934 में आयी उनकी पहली फिल्म का नाम ‘रामायण’ था, जबकि 1935 की ‘धूप-छांव’ में उनका रचा एक बड़ा ही मनहर गीत था-मन की आंखें खोल, बाबा! मन की आंखें खोल! 1952 में प्रदर्शित ‘रानी’ उनकी आखिरी फिल्म थी. ‘तेरी गठरी में’, जिसका जिक्र शुरू में कर आये हैं, संभवतः किसी फिल्म का हिस्सा नहीं है, फिर भी लोकप्रियता में अपना सानी नहीं रखता.
एक ऐसा भी वक्त था, जब आम चुनावों के दौरान देश की विभिन्न राजनीतिक पार्टियां इस गीत को अपने विरोधियों को इंगित करने और मतदाताओं को उनसे सावधान रहने को कहने के लिए इस्तेमाल किया करती थीं। 1941 में आयी सोहराब मोदी की लोकप्रिय फिल्म ‘सिकन्दर’ की सफलता का एक बड़ा आधार सुदर्शन की लिखी उत्कृष्ट पटकथा ही बताई जाती है। 1935 में उन्होंने ‘कुंवारी या विधवा’ नाम की एक फिल्म का निर्देशन भी किया। 1950 में फिल्म लेखक संघ गठित किया गया तो उन्हें उसका पहला उपाध्यक्ष बनाया गया था.
लेकिन आगे चलकर वे हिन्दी वालों की विस्मरण की आत्मघाती प्रवृत्ति के ऐसे शिकार हुए कि अब उनके बारे में ज्यादा जानकारियां उपलब्ध ही नहीं है. 1967 में 16 दिसम्बर को 72 वर्ष की उम्र में उनका देहांत हुआ तो वे अपने पीछे चार बेटे व एक पुत्री छोड़ गये थे. क्या हिन्दी की श्री-वृद्धि के लिए किया गया उनका योगदान इतना तुच्छ था कि उनकी कतई खोज-खबर न ली जाये? सोचें तो डाकू खड़ग सिंह जैसी ही आत्मग्लानि होती है.