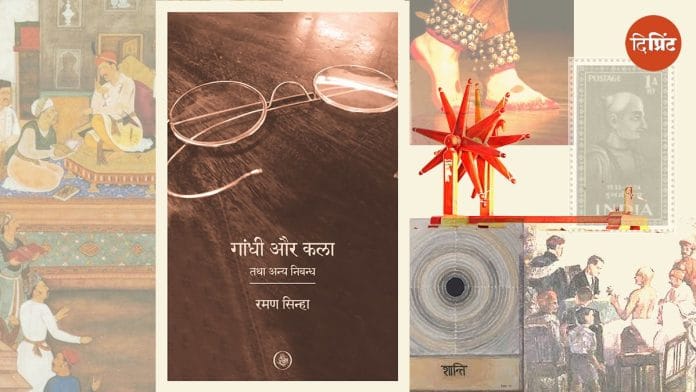(किताब को राजकमल प्रकाशन ने छापा है जिसका अंश प्रकाशन की अनुमति से छापा जा रहा है.)
…मेरे बारे में इतने सारे अन्धविश्वास व्याप्त हैं कि अब मेरे लिए उन लोगों से आगे निकलना लगभग असम्भव हो गया है जो उन्हें फैला रहे हैं. नतीजतन, तब मेरे दोस्तों की प्रतिक्रिया लगभग हमेशा एक मुस्कान होती है जब मैं दावा करता हूं कि मैं खुद एक कलाकार हूं.
उपर्युक्त उद्धरण में गांधी जी ने दिलीप कुमार राय से जो बात कही, वह आज भी सच है. मुस्कान के रूप में प्रतिक्रिया अभी तक बदली नहीं है क्योंकि हम शायद ही कला के सम्बन्ध में बात करते हुए कभी गांधी जी को याद करते हैं, उनको एक कलाकार के रूप में देखना तो दूर की बात है. हालांकि, उन पर कई तरह से चर्चा की जा सकती है; उदाहरण के लिए हम गांधीवादी सौन्दर्यशास्त्र पर बात कर सकते हैं; हम यह भी जानने की कोशिश कर सकते हैं कि गांधी सौन्दर्य और कला के बारे में क्या सोचते थे, साहित्य, चित्रकला, संगीत आदि के बारे में उनकी क्या राय थी; हम फिल्म, नाटक, चित्रकला, संगीत, मूर्तिकला, साहित्य के उन कार्यों का भी विश्लेषण कर सकते हैं जिनमें गांधी या गांधीवाद विषय रहा है; साहित्यकार और अनुवादक के रूप में भी गांधी ध्यान देने योग्य हैं क्योंकि उनका लेखन गुजराती और अंग्रेज़ी में करीब सौ खंडों में व्याप्त है.
गांधीवादी सौन्दर्यशास्त्र : सत्याग्रह का सौन्दर्यशास्त्र
सत्य ही सौन्दर्य है.
दिनांक 23.03.1921 के ‘यंग इंडिया’ में गांधी जी ने लिखा कि सत्याग्रह का शाब्दिक अर्थ है सत्य पर आग्रह अर्थात सत्य-बल. सत्य आत्मा या अन्तरात्मा है. इसलिए, इसे आत्म-शक्ति के रूप में जाना जाता है. किसी अन्य स्थान पर उन्होंने घोषणा की कि “मैं सत्य में या सत्य के माध्यम से सुन्दरता देखता और पाता हूँ. सभी सत्य, केवल सच्चे विचार ही नहीं, बल्कि सच्चे चेहरे, सच्चे चित्र, या गीत, अत्यधिक सुन्दर हैं…सत्य स्वयं को ऐसे रूपों में प्रकट कर सकता है जो हो सकता है कि बाहरी रूप से बिलकुल भी सुन्दर न हों.
सुकरात, हमें बताया गया है कि वे अपने युग के सबसे सच्चे व्यक्ति थे, लेकिन कहा जाता है कि उनकी शक्ल-सूरत ग्रीस में सबसे बदसूरत थी. मेरे विचार से, वे सुन्दर थे क्योंकि उनका सारा जीवन सत्य के लिए प्रयासरत था और आपको याद होगा कि उनका बाहरी रूप फिडियस को उनके सत्य की सुन्दरता को सराहने से नहीं रोक पाया, हालाँकि एक कलाकार के रूप में वह बाह्य सौन्दर्य को देखने का भी आदी था.” यहां गांधी अन्तर्वस्तु (कंटेंट) और रूप (फॉर्म) के द्विभाजन पर ज़ोर देते हैं और अन्तर्वस्तु का पक्ष लेते हैं.
बाद में वे रूप को अनैतिकता के साथ भी जोड़कर देखने लगते हैं और लिखते हैं, “ऑस्कर वाइल्ड को ले लो. मैं उनके बारे में बात कर सकता हूं, क्योंकि मैं उस समय इंग्लैंड में था जब उनकी बहुत चर्चा हो रही थी…वाइल्ड ने सर्वोच्च कला को केवल बाहरी रूपों में ही देखा इसलिए,अनैतिकता का सौन्दर्यीकरण करने में सफल रहे.” अनैतिकता के सौन्दर्यीकरण की स्वाभाविक परिणति यह सूत्र है, ‘कला, कला के लिए’ और गांधी जी इसका कड़ा विरोध करते हैं, वे लिखते हैं, “जो लोग ‘कला के लिए कला’ को आगे बढ़ाने का दावा करते हैं, वे अपना दावा पूरा करने में असमर्थ हैं…कला केवल एक साधन हो सकती है, उस साध्य का, जिसे हम सबको अवश्य प्राप्त करना चाहिए.”
गांधी के इस कथन पर कि ‘सत्य ही ईश्वर है’, रोम्या रोलां ने टिप्पणी की थी कि “मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि इसमें ईश्वर की एक महत्त्वपूर्ण विशेषता आनन्द का अभाव है और इस पर मैं ज़ोर देता हूं कि मैं आनन्द के बिना किसी ईश्वर को नहीं पहचानता.” गांधी ने इसका उत्तर देते हुए कहा कि वह कला और सत्य के बीच अन्तर नहीं करते. मैं ‘कला के लिए कला’ के सूत्र के खिलाफ हूं. मेरे लिए सभी कलाएँ सत्य पर आधारित होनी चाहिए. मैं सुन्दर चीज़ों को अस्वीकार करता हूं, अगर वे सत्य व्यक्त करने के बजाय असत्य व्यक्त करती हों…कला में सत्य प्राप्त करने के लिए मैं बाहरी चीज़ों के हू-ब-हू अनुकरण की अपेक्षा नहीं करता हूं. केवल जीवित चीज़ें ही आत्मा को जीवित आनन्द देती हैं और आत्मा को ऊपर उठा सकती हैं.”
यहां ऐसा लगता है कि गांधी, प्लेटो और अरस्तू के अनुकरण सिद्धान्त से सम्भवत: अवगत थे और निश्चित रूप से वे अरस्तू के पक्ष में थे, जिन्होंने प्लेटो के विपरीत अनुकरण की ऐसी अवधारणा परिकल्पित की थी, जो यथातथ्य सत्याभास से परे है, लेकिन वे इस तथ्य के प्रति भी गहराई से सचेत थे जैसा कि उन्होंने कहीं और लिखा है कि “सत्य और असत्य अक्सर साथ-साथ रहते हैं; अच्छाई और बुराई अक्सर एक साथ पाई जाती है. एक कलाकार में भी, चीज़ों की सही धारणा के साथ ग़लत परिप्रेक्ष्य का होना, विरल नहीं है. वास्तव में सुन्दर रचनाएं तब जन्म लेती हैं जब सही अवबोध काम कर रहा होता है. यदि ऐसे क्षण जीवन में दुर्लभ हैं, तो वे कला में भी दुर्लभ हैं.”
यह एक सत्याग्रही की एक दुर्लभ अन्तर्दृष्टि है, जिसके लिए जीवन और कला दो अलग-अलग वस्तुएं नहीं थीं, बल्कि जैसा कि एक बार उन्होंने कहा था, “मेरे लिए निश्चय ही सबसे महान कलाकार वह है जो श्रेष्ठ जीवन जीता है.” यह हमें यूनानी सिद्धान्तकार लोंजाइनस के कथन की याद दिलाता है कि महान लेखन महान दिमाग़ की प्रतिध्वनि होता है. निश्चित रूप से यह निर्वैयक्तिकता के आधुनिकतावादी सिद्धान्त के खिलाफ है जहां जीवन और कला को एक नहीं माना जाता है, लेकिन गांधी ज़ोर देकर कहते हैं कि “हम लोग इस विश्वास के आदी हो गए हैं कि कला निजी जीवन की शुद्धता से स्वतंत्र होती है. मैं अपने तमाम अनुभव के बल पर कह सकता हूं कि इससे ज़्यादा झूठी बात और कुछ नहीं हो सकती. अब जबकि मैं अपने सांसारिक जीवन के अन्त के करीब पहुंच गया हूं, मैं कह सकता हूँ कि जीवन की पवित्रता ही सर्वोच्च और सच्ची कला है. सुसंस्कृत स्वर से बढ़िया संगीत उत्पन्न करने की कला बहुतेरे प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन शुद्ध जीवन के सामंजस्य से वैसे संगीत को उत्पन्न करने की कला विरले ही प्राप्त कर पाते हैं.”
संक्षेप में, सच्चिदानन्द का भी यही अर्थ है. गांधी ने रोम्या रोलाँ को इस शब्द का अर्थ यह कहकर समझाया कि सत का अर्थ है सत्य, चित्त का अर्थ है जीवित और वास्तविक ज्ञान जो सच्चे अवबोध से रहित न हो तथा आनन्द का अर्थ है पारलौकिक आनन्द. इस अवधारणा में सत्य आनन्द से अविभाज्य है.
जो उपयोगी है, वह सुन्दर है
जो उपयोगी है क्या वह सुन्दर है? गांधी ने एक बार टिप्पणी की थी, “आप सब्ज़ियों में रंग की सुन्दरता क्यों नहीं देख सकते?” और फिर एक और जगह उन्होंने ज़ोर देकर कहा था कि “उपयोगिता से रहित सौन्दर्य अकल्पनीय है.” उनके लिए कला में उपयोगिता का अर्थ था, मनुष्य को “नैतिकता के मार्ग पर एक क़दम और आगे ले जाना और उसे उन्नत दृष्टि प्रदान करना.”
प्रकृति के रूप में कला
आम तौर पर कला की चर्चा या तो प्रकृति या संस्कृति के सन्दर्भ में की जाती है. प्रकृति प्रदत्त है जबकि संस्कृति का निर्माण होता है. अगर हम कला को प्रकृति के रूप में देखते हैं तो हम इसका एक प्राकृतिक वस्तु के रूप में मूल्यांकन करना चाहते हैं जबकि संस्कृति के रूप में कला को एक कलाकृति के रूप में देखा जाता है. गांधी कला को प्राय: प्रकृति के रूप में देखते हैं, यही कारण है कि वे कहते हैं, “मेरे लिए कला को वास्तव में महान होने के लिए उसकी भी अपील प्रकृति की सुन्दरता की तरह, सार्वभौमिक होनी चाहिए…प्रस्तुति में सरल और प्रकृति की भाषा की तरह अपनी अभिव्यक्ति में प्रत्यक्ष.” कोई आश्चर्य नहीं कि जब उनसे पूछा गया कि वे विशेषज्ञता के इतने ख़िलाफ़ क्यों हैं, तो उन्होंने एक जवाबी सवाल किया, “आप उस स्पष्ट तथ्य को क्यों नहीं देखना चाहते कि प्रकृति जो सभी वास्तविक कलाओं की अन्तिम प्रेरणा है, वह कभी सीमा नहीं बाँधती. वह कभी भी कुछ इस तरह का विशेष स्वरूप नहीं बनाती कि केवल कुछ सुसंस्कृत लोग ही उसका आनन्द ले सकें, बाकी विशाल बहुमत को ठंड में ठिठुरता ही छोड़ दे.”
एक दूसरी जगह वे सवाल करते हैं कि “क्या कोई ऐसे चित्र की परिकल्पना कर सकता है जो प्रेरणा देने के मामले में नक्षत्र खचित आकाश, राजसी समुद्र, और विशाल पर्वतों से तुलनीय हो? क्या किसी चित्रकार के रंग की उगते भोर के सिन्दूर या ढलते दिन के स्वर्ण रंग से तुलना हो सकती है? नहीं, मेरे दोस्त, मुझे प्रकृति के अलावा और किसी से प्रेरणा नहीं चाहिए. उसने अभी तक मुझे कभी निराश नहीं किया है; वह मुझे विस्मित करती है, रहस्यपूर्ण बनाती है, मुझे परमानन्द का अनुभव कराती है. मुझे मनुष्य की बचकानी रंग-योजनाओं की क्या आवश्यकता है?”
यहां गांधी हमें प्लेटो के अनुकरण के रूप में कला के विचार की याद दिलाते हैं.19 लेकिन जब संगीत की बात आती है तो गांधी की प्रतिक्रिया अलग होती है, वे कहते हैं, “मेरे लिए संगीत ऐसी चीज़ है जिससे ख़ुशी और प्रेरणा मिलती है. मुझे अच्छी तरह याद है, जब मैं दक्षिण अफ़्रीका के एक अस्पताल में बीमार पड़ा था, कितना आनन्द, शान्ति और आराम मुझे संगीत से मिलता था. मेरे सविनय अवज्ञा अभियान की बढ़ती सफलता के लिए धन्यवाद कहें कि उन दिनों कुछ लोगों ने मेरे पैर तोड़ने की कोशिश की थी और मैं उन्हीं चोटों से उबर रहा था. मेरे अनुरोध पर, मेरे एक मित्र की बेटी, अक्सर मेरे लिए प्रसिद्ध भजन, ‘लीड काइंडली लाइट’ गाती थी और यह उपचार एक बाम की तरह काम करता था! मैं अब भी इस गीत को कृतज्ञता के साथ याद करता हूं.”
आश्चर्य नहीं कि संगीत और प्रार्थना उनकी सुव्यवस्थित दैनिकी और योजना के अभिन्न अंग थे जिन्हें उन्होंने अपनी विदेश यात्राओं के व्यस्त कार्यक्रम में भी कभी नहीं छोड़ा. यहाँ दृष्टव्य है लुई फिशर की वह रिपोर्ट जो दिसम्बर 1931 में लन्दन के गोलमेज़ सम्मेलन से लौटने के बाद स्विट्ज़रलैंड में रोम्या रोलाँ के साथ गांधी के प्रवास की है, वे लिखते हैं, “पिछली शाम गांधी ने रोलाँ को बीथोवेन बजाने को कहा. रोलाँ ने पाँचवीं सिम्फनी का ‘एंडांटे’ (विलम्बित) प्रस्तुत किया और अपनी पसन्द से ग्लुक का ‘एलिसियन फ़ील्ड्स’ भी.
पांचवीं सिम्फनी का विषय प्राय: भाग्य के साथ मनुष्य का संघर्ष, भाग्य के साथ मनुष्य का सामंजस्य, मनुष्य का भाईचारा माना जाता है. दूसरा आन्दोलन, एंडांटे, मधुर है और कोमल गीतात्मक भावनाओं से संवलित है, प्रशान्त उदात्तता और आशावाद से भरा हुआ है. रोलाँ ने इसे इसलिए चुना क्योंकि यह गांधी के व्यक्तित्व की उनकी अवधारणा के क़रीब था. यह कोमल और प्रेम से पूर्ण है. ग्लुक की रचना में स्वर्गदूतों को बांसुरी की धुन पर गाते हुए लगभग सुना जा सकता है. यह दिव्य संगीत है, पवित्रता और स्पष्टता से भरा हुआ. इस पर गीता को बाँधा जा सकता है.”
इस घटना को रोलाँ ने ख़ुद अपनी डायरी में नोट किया था कि गांधी चाहते थे कि वह विशेष रूप से बीथोवेन बजाएँ और जब उन्होंने ऐसा किया और उन्हें इस पर टिप्पणी करने के लिए कहा गया तो उन्होंने नटखट की तरह हँसते हुए कहा, “जब आप इसे अच्छा कह रहे हैं तो यह ज़रूर अच्छा ही होगा.” वैसे गांधी कई बार यह निवेदन कर चुके थे कि वह उस कला और साहित्य को पसन्द करते हैं जो लाखों लोगों से बात कर सके.
निश्चित रूप से, गांधी कला में ‘अभिव्यक्ति’ के बजाय सम्प्रेषण पर ज़ोर देते थे. ईसा मसीह के जीवन पर डीन फरार की पुस्तक का हवाला देते हुए उन्होंने लिखा है कि लेखक ने अंग्रेज़ी भाषा में लिखित यीशु के बारे में सब कुछ पढ़ा, और फिर वह फ़िलिस्तीन गया, ‘बाइबिल’ में वर्णित हर उस जगह और स्थान को ढूँढ़ा जिसे वह पहचान सकता था, और फिर उसने प्रार्थना और विश्वास के साथ इंग्लैंड की सामान्य जनता के लिए एक ऐसी भाषा में पुस्तक लिखी जिसे सभी समझ सकते थे. यह डॉ. जॉनसन की शैली में नहीं बल्कि डिकेंस की आसान शैली में थी.
क्या हम लोगों के पास फर्रार जैसे आदमी हैं जो गाँव के लोगों के लिए महान साहित्य तैयार करें? हमारे साहित्यकार कालिदास और भवभूति और अंग्रेज़ी लेखकों पर ध्यान देंगे और उससे प्रेरित साहित्य हमें देंगे. मैं चाहता हूं कि वे गांवों में जाएं, उनका अध्ययन करें और हमें कुछ जीवनदायी तत्त्व प्रदान करें…हमें वैसी कला और साहित्य की ज़रूरत है जो लाखों लोगों से बात कर सके. गांधी हमेशा यह मानते रहे कि चूँकि हमें प्रकृति के मनोरम दृश्य का आनन्द लेने के लिए दुभाषिए की आवश्यकता नहीं पड़ती है—सूर्योदय के रंग औ रोगन या सूर्यास्त के प्रशान्त वातावरण या वसन्त की ठंडी हवाएं हमें बिना किसी सहायता के सीधे सम्प्रेषित होती हैं, इसलिए वे पूछते हैं कि किसी कलात्मक कृति को समझने के लिए हमें किसी कलाकार की क्यों ज़रूरत होनी चाहिए?
इसे सीधे मुझसे ही क्यों नहीं बोलना चाहिए? मैंने वेटिकन कला-संग्रह में क्रूस पर मसीह की एक मूर्ति देखी, जिसने मेरा ध्यान तत्काल खींचा और मुझे मंत्रमुग्ध कर दिया. मैंने इसे पांच साल पहले देखा था लेकिन यह अभी भी मेरे समक्ष उपस्थित है. मैसूर के बेलूर के एक प्राचीन मन्दिर में मैंने पत्थर की एक छोटी सी मूर्ति देखी जिसने मुझसे बात की और मैंने बिना किसी मदद के उसे समझ लिया. यह एक अर्ध-नग्न औरत की मूर्ति थी, जो अपने कपड़ों की सिलवटों से ख़ुद को उस कामदेव के बाण से बचाने के लिए संघर्ष कर रही थी, जो आख़िरकार हारकर उसके पैरों तले बिच्छू के रूप में घायल पड़ा था. मैं मूर्ति में उस पीड़ा को देख सकता था—बिच्छू के डंक की पीड़ा.
प्रकृति जैसी कला और इसकी आसान सम्प्रेषण क्षमता के गांधीवादी प्रस्ताव को हम एक ऐसे उदाहरण के प्रतिपक्ष में रखकर विचार कर सकते हैं जिसे रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने गांधी के साथ एक बहस में उद्धृत किया था, वे लिखते हैं, “मैं एक वीणावादक की तलाश में हूँ. मैंने उसे पूर्व में ढूंढ़ा और मैंने पश्चिम में भी उसे ढूँढ़ने की कोशिश की है, लेकिन मेरी खोज का वह आदमी नहीं मिला. वे सभी विशेषज्ञ हैं, वे तार में गूंज पैदा कर सकते हैं, वे भारी क़ीमतों की मांग करते हैं, लेकिन उनके अद्भुत प्रदर्शन मेरे दिल को छू नहीं पाते.
अन्तत: मैं एक ऐसे व्यक्ति से मिला, जिसके पहले ही सुर ने भीतर की मेरी सभी दमित भावनाओं को तिरोहित कर दिया. उसमें आनन्द की अग्नि-शक्ति थी जो अपने स्पर्श से अन्य सभी हृदयों को प्रफुल्लित कर सकती है. मेरे लिए उनकी अपील तत्काल थी और मैं उन्हें उस्ताद के रूप में प्रणाम करता हूँ. फिर मैं एक वीणा बनाना चाहता था. इसके लिए सभी प्रकार की सामग्री और एक अलग तरह के विज्ञान की आवश्यकता थी. मेरे पास साधनों की कमी देखकर मेरे उस्ताद को दया आनी चाहिए थी और उन्हें कहना चाहिए था: ‘कोई बात नहीं, मेरे बेटे तुम एक अच्छी वीणा के लिए महँगी कारीगरी और समय में वक़्त गँवाने के बजाय लकड़ी के किसी टुकड़े पर कसे हुए किसी साधारण तार पर अभ्यास करो. कुछ समय में ही तुम पाओगे कि वह वीणा जितना ही अच्छा है.’ क्या सचमुच वह वैसा (वीणा जैसा) होगा? मुझे भय है कि ऐसा नहीं होगा.”
गांधी और गांधीवाद को वर्षों से विभिन्न कला-रूपों में—फ़िल्म, रंगमंच, संगीत, चित्रकला, मूर्तिकला, साहित्य और यहां तक कि पैरोडी और कंप्यूटर गेम में भी निरन्तर विवेचित-विश्लेषित किया गया है. किसी भी दृष्टि से देखें यह वैविध्यपूर्ण और विशाल काम है जिसे एक लेख में समेटना सम्भव नहीं, इसलिए चयनधर्मी होना ही एकमात्र रास्ता हो सकता है. सबसे पहले हम साहित्य से शुरुआत करते हैं.
(गांधी और कला तथा अन्य निबंध के लेखक रमण सिन्हा हैं.)