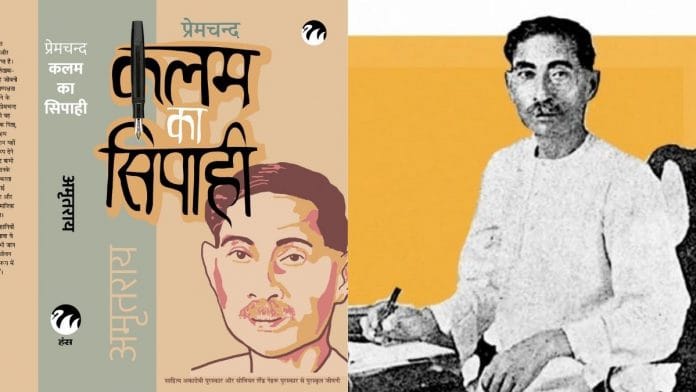छुट्टियां जैसे-तैसे ख़त्म हुईं और नवाब फिर कानपुर पहुंच गया और फिर वही दोस्तों की महफ़िलें, क़हक़हे और चहचहे शुरू हुए जिनके लिए उसका दिल तड़पता था.
लेकिन वह सब महफ़िलें, शेर-ओ-शायरी के चर्चे, बेफ़िक्र कुंआरी जिन्दगी की मस्तियां जहां एक तरफ़ उसकी जिन्दगी के सूनेपन को भरती थीं वहीं दूसरी तरफ़ उसे और भी बढ़ा देती थीं. अपना अकेलापन अब उसे खलने लगा था. तबीयत बहुत रंगीन न सही, मगर जवान तो थी. आख़िर कब तक वह इसी तरह अपनी जिन्दगी की लढ़ियां ठेलेगा? पच्चीस साल का तो हुआ, घर बसाने की अब और कौन-सी उम्र आएगी? या तो फिर उसका ख़याल ही छोड़ दिया जाए, जो कि नवाब के लिए मुमकिन न था. तबीयत ही उसने वैसी न पाई थी. वह घरेलू ढंग का आदमी था और उसकी तमाम परेशानियों के बावजूद उसी में ख़ुश रह सकता था. कुंआरेपन की मस्त, बेफ़िक्र, ग़ैर-जिम्मेदार जिन्दगी के अपने मज़े हैं लेकिन वह मज़े नवाब के लिए न थे. और फिर पन्द्रह-सोलह साल की उम्र से जिस लड़के के गले में गिरस्ती का जुआ पड़ गया हो, वह दूसरा कुछ सोच भी तो नहीं सकता….जब तक कि इकबारगी बग़ावत पर न आमादा हो जाए. मगर बग़ावत भी कैसे करे, पहले से भी तो कुछ जिम्मेदारियां चली आ रही हैं, मां की, उनके बच्चे की— उनसे कैसे मुंह फेर ले? होते हैं, ऐसे भी लोग होते हैं, बहुत होते हैं, जो दूसरों की चिन्ता नहीं करते, बस अपनी ख़ुशी, अपना आराम देखते हैं. मगर नवाब उनमें से न था, न प्रकृति से और न इतने वर्षों के अभ्यास से.
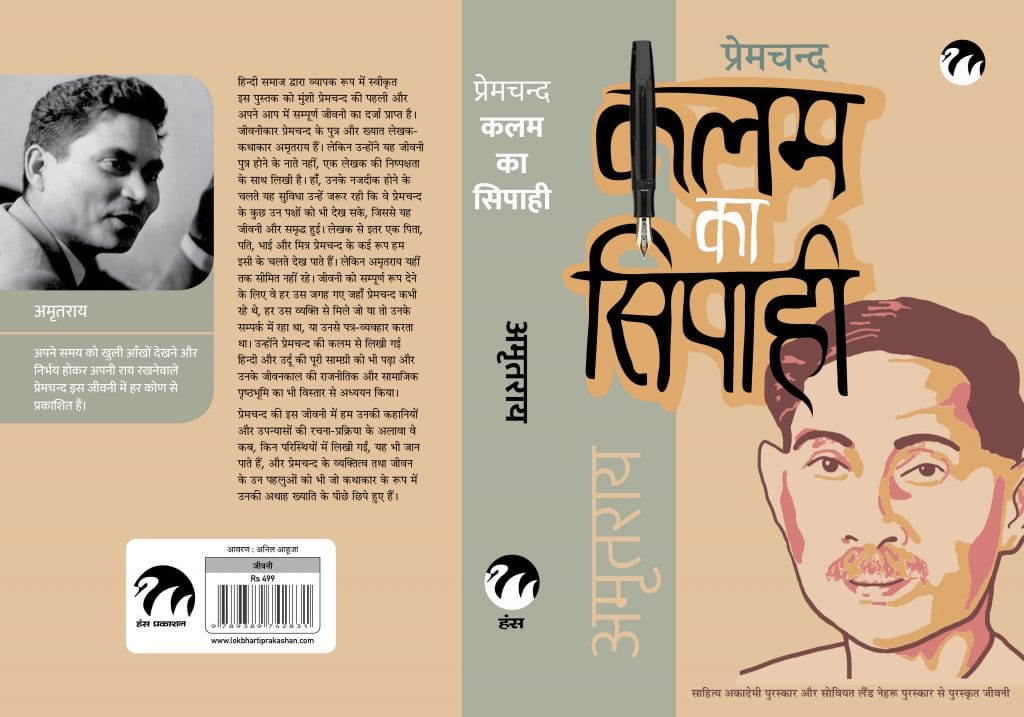
लिहाज़ा जब यह सब खटराग रहना ही है तो इसका सुख भी कुछ क्यों न उठाया जाए. वह तो शादी बुरी हुई, बिलकुल नाकाम रही, बड़ा दुख दिया उसने. लेकिन अब तो ख़ैर उससे नाता टूट गया. अच्छा ही हुआ. मन थोड़ा हल्का था, मगर कुछ था जो करक रहा था.
कायस्थों में लड़कियों की कुछ कमी न थी, और नवाब उस वक़्त एक हंसमुख, जिन्दादिल, स्वस्थ और सुन्दर, खाता-कमाता नौजवान था. चाची शादी करने के लिए पीछे पड़ी थीं और जेब से कुछ खर्चे बग़ैर एक हसीन और बाशऊर बीवी मिली जाती थी. नौजवान नवाब उसके सपने भी देखने लगा था. लेकिन फिर आदमी का विवेक भी तो है. कैसे रचा ले वह उस तरह का ब्याह! ऐसी बड़ी-बड़ी बातें अभी उसने अपनी किताब में लिखीं और जब अपनी बारी आई तो भूल जाए उन सब बातों को? नहीं, उसके लिए तो यही उचित है कि अगर उसे दुबारा शादी करनी ही हो तो किसी विधवा लड़की से करे, वह ख़ुद कहां का कुंआरा है! न रहा हो उससे सम्बन्ध तो क्या, ब्याह तो हुआ. यही सब बातें सलाह करने की थीं.
आख़िरकार, मुंशी दयानरायन के शब्दों में, ‘शादी के बारे में बड़े सोच-विचार और बहुत कुछ बहस-मुबाहसे के बाद उन्होंने तय किया कि दूसरी शादी की जाए तो किसी विधवा ही से की जाए.’ घरवाले, ख़ासकर चाची, विधवा-विवाह के बहुत खिलाफ़ थीं. इस तरह की चीज़ घर में पहले कभी न हुई थी. बिरादरीवाले क्या कहेंगे! नाक कट जाएगी! लोग कहेंगे ज़रूर कोई ऐब है लड़के में तभी तो कुंआरी लड़की नहीं मिली बिरादरी में, वर्ना क्यों करता विधवा लड़की से ब्याह! चाची उन दिनों नवाब के साथ ही कानपुर में रह रही थीं और नवाब कुछ दिनों से, नाजुक तबीयत के, लम्बे छरहरे मुंशी नौबतराय ‘नज़र’ और एक महराजिन के साथ दयानरायन साहब के घर के पास ही मकान लेकर रह रहे थे. हर रोज़ घर में शादी का मसला छिड़ता और इसी तरह की बातें होतीं. कभी-कभी तो नवाब की तबीयत इतना ज़्यादा भिन्ना जाती कि वह शादी से बाज आने की बात सोचने लगता. लेकिन कुछ तो उम्र का तक़ाज़ा और कुछ उसकी घरेलू ढंग की तबीयत, शादी कर लेना ही उसने तय कया. लेकिन अपने इस इरादे पर वह अटल था कि विधवा ही से शादी करेगा. दूसरों की मुंहदेखी मैं नहीं कर सकता. मुझे जो बात ठीक मालूम होती है, वही मैं करूंगा, जिसे शरीक होना हो, हो, न होना हो, न हो.
तभी संयोग से एक रोज़ नवाब की नज़र किसी अख़बार में, शायद बरेली के आर्यसमाजी शंकरलाल श्रोत्रिय के पर्चे में छपे हुए एक इश्तहार पर पड़ी जिसमें लिखा था कि मौजा सलेमपुर डाकखाना कनवार ज़िला फतेहपुर के कोई मुंशी देवीप्रसाद अपनी बाल-विधवा कन्या का विवाह करना चाहते हैं और जो सज्जन चाहें इस विषय में उक्त पते पर पत्र-व्यवहार कर सकते हैं.
नवाब ने फ़ौरन उस पते पर ख़त लिखा. उसके जवाब में ख़त के साथ पच्चीस-तीस पन्ने का एक किताबचा आया. यह किताबचा अगर और किसी वजह से नहीं तो अपनी लेखन शैली के कारण एक मार्के का और बहुत दिलचस्प दस्तावेज़ है. लेकिन और भी बड़ी बात यह है कि उससे बहुत मज़े की रोशनी उस कायस्थ समाज पर पड़ती है जिसमें नवाब का जन्म हुआ, जिसके बीच वह पला-बढ़ा और जिसके माध्यम से उसने सबसे पहले हिन्दू समाज के मसलों को समझा. जिस समाज के अन्दर से यह दस्तावेज़ पैदा हुआ वही नवाबराय का पहला और बुनियादी समाज है. वही उसकी ज़बान है और वही उसके सोचने-विचारने का ढंग. बाद में उसकी निगाह भी फैली और उसका समाज भी फैला, ताहम उसकी घुट्टी में यही समाज था.
किताबचे पर उसका नाम दिया है, ‘कायस्थ बाल विधवा उद्धारक’ और उसके नीचे यह इबारत है— मूर्ख गुपनाम द्वारा लिखित जिसको मुंशी गजाधरप्रसाद नायब नाजिर दीवानी ने यूनियन प्रेस, इलाहाबाद में छपवाकर प्रकाशित किया. 1905.
गुप्त नाम से किताबचे को लिखना और एक अज़ीज़ के नाम से उसको छपवाना, यह सब कार्रवाई थी उन्हीं मुंशी देवीप्रसाद की जो अपनी बाल-विधवा कन्या शिवरानी का पुनर्विवाह करना चाहते थे. यह मुंशी देवीप्रसाद अपने गांव के एक बहुत प्रभावशाली व्यक्ति थे. पैसा तो कुछ ख़ास न था मगर इज़्ज़त बहुत थी. दिमाग़ तो वैसा ही पाया था जैसी कि कायस्थ खोपड़ी मशहूर है मगर साथ ही मिज़ाज में कुछ ठाकुरों जैसा अक्खड़पन भी था. दबंग कड़ियल आदमी थे. बहुत शरीफ़, पुराने ढंग के वज़ादार, न तो ख़ुद किसी से बेअदबी करते थे और न किसी की बेअदबी बर्दाश्त करते थे. दोस्ती की टेक निभाना भी जानते थे और दुश्मन को नेस्तनाबूद करने में भी पीछे न रहते थे. उनके तीन लड़के थे और दो लड़कियां. दोनों लड़कियों का ब्याह उन्होंने छुटपन में ही, दस-ग्यारह साल की उम्र तक पहुंचते-पहुंचते कर दिया था. किस्मत का खेल कुछ ऐसा हुआ कि छोटी लड़की शिवरानी ब्याह के तीन महीने बाद ही विधवा हो गई. न तो वह पति के घर गई और न उसने पति का मुंह देखा, मगर फिर भी वह विधवा थी और यह उनकी जिन्दगी का सबसे बड़ा ग़म था. मां-बाप दोनों अपनी इस बेटी का मुंह देखते और कलेजा थाम लेते थे. आख़िरकार बहुत पसोपेश के बाद दोनों ने अपने मन में इस बात का फ़ैसला कर लिया कि हम अपनी बेटी का ब्याह फिर से करेंगे. आज भी यह काम आसान नहीं है, पचपन बरस पहले तो वह बग़ावत से कम न था. लेकिन मुंशी देवीप्रसाद अब इस बग़ावत पर आमादा थे. अपनी बेटी का दुख उनसे देखा न जाता था. होगा समाज का विरोध, डटकर होगा— हो. जो होगा देखा जाएगा. एक बार फ़ैसला कर लेने पर पीछे क़दम हटानेवाले आदमी मुंशी देवीप्रसाद न थे. बिरादरी का एक-एक आदमी हमें छोड़ दे, तो भी यह ब्याह होगा. और चोरी-छिपे न होगा, इश्तहार बंटवाकर होगा. सब लोग जान जाएं कि मुंशी देवीप्रसाद अपनी विधवा कन्या का विवाह फिर से कर रहे हैं.
लेकिन इसके लिए ज़रूरी था कि सबसे पहले इस काम के लिए फिज़ा तैयार की जाए. मुक़दमे में कूदने के पहले अपने काग़ज़ात सब ठीक कर लेने चाहिए ताकि बाद में बग़लें न झांकनी पड़ें. इसी ख़याल से यह इश्तहारी पर्चा हिन्दी और उर्दू में तैयार किया गया और उसे काफ़ी बड़ी संख्या में छपवाकर दूर-दूर तक भेज दिया गया. जिसे एतराज करना हो, करे; आए हमसे बहस करे, या तो वह मुझे क़ायल कर दे कि मैं ग़लत काम कर रहा हूं या मैं उसे वेद-पुराण और शास्त्रों की नज़ीर देकर क़ायल कर दूंगा कि ठीक बात यही है, बाक़ी सब तो पोंगा ब्राह्मणों का खेल है.
किताबचा बिलकुल आर्यसमाजी अन्दाज़ में ओउम्तत्सत् के साथ शुरू होता है और उसी रंग में आगे बढ़ता है—
प्रार्थना पत्र खिदमत में सब भाइयों कायस्थ चित्रगुप्तवंशी के पहुंचकर सुशोभित हो, परमात्मा रोज़-ब-रोज़ तरक़्क़ी देवे.
दरख़्वास्त वास्ते सुधार करने चाल-चलन ब्योहार जो क़ाबिल सुधार करने के है कि जो न सुधार चाल-चलन करने से महापातक होता है कि सब भाइयों को मालूम है और देखते हैं शास्त्रोक्त प्रमाण व वेदाज्ञानुसार सब भाइयों के सामने इस पत्र द्वारा प्रकाशित करता हूं अपने-अपने ज्ञान बुद्धि से ध्यान देकर उनके सुधारने में दिल व जान से मुस्तैद हो जाइए.
हे मेरे प्यारे क़ौमी भाइयो कायस्थ चित्रगुप्तवंशी ज़रा ध्यान देकर सुनिए कि पद्म पुराण एक प्राचीन पुराण व मुस्तनिद किताब है जिससे साबित है कि बाबा चित्रगुप्त पुरुषा याने मूरिस आला सब भाइयों के हैं और जब से सृष्टि की रचना हुई बदर्बार महाराज धर्मराज के न्यायकारी व आमाल नेक व बद जो जैसा काम करता है, तहरीर फ़रमाया करते हैं वा उसी के मुताबिक़ सज़ा व जज़ा याने स्वर्ग व नर्क तजवीज़ फ़र्माते हैं.
उन्हीं बाबा चित्रगुप्त जी के पुण्य व प्रताप व आशीर्वाद से सब उनकी औलादें कि जिनके सन्तान व वंश में सब भाई हैं, वेदविद्या का पठन-पाठन करते रहैं, श्रेष्ठ कहलाते रहैं व वक़्त महाराज क्षत्रियों के राज्य समय में कायस्थ वंश भाई अपनी वेद विद्या व बुद्धि की लियाक़त से बड़े-बड़े ओहदों पर (न्यायाधीश) व राज्य कार्य के मंत्री व दीवान मुक़र्रर होते रहे और राज्य का इन्तिज़ाम माकूल करते रहे कि सबसे श्रेष्ठ व लायक़ समझे जाते रहे.
समय के उलट-फेर से कि ज़माना तरक़्क़ी का हमेशा किसी का एक ही तरह पर नहीं क़ायम रहा है, काल-चक्र घूमा करता है…राज्य हाथ से जाता रहा पाप कर्मों का प्रचार होता गया.
समाज का बराबर पतन होता गया और उसमें कोई सुधार इसलिए नहीं होता कि लोग बस अपने स्वार्थ के बन्दे हैं, किसी को अपने समाज के भले-बुरे की चिन्ता नहीं है और हैं तो बस लम्बी-चौड़ी बातें, कथनी कुछ और करनी कुछ—
‘जाबज़ा शहरों व क़स्बों व नामी मुक़ामात में क़ौमी सभा व कमेटी व कान्फ्रेंस वास्ते धर्म की रक्षा व क़ौमी चाल-चलन ब्यौहार व रीति रस्म के दुरुस्ती के लिए शास्त्रोक्त प्रमाण से मुक़र्रर फ़रमाया है और वहां व्याख्यान व लेक्चर धर्म सम्बन्धी दिए जाते हैं. और उस जलसा सभा में सब भाई बैठकर सुनते हैं और सत्य-सत्य कहते हैं, हां में हां गला मिलाते हैं और उन व्याख्यानों के अमल करने का न व्याख्यान देनेवालों के दिलों पर असर रहता है न व्याख्यान सुननेवाले के दिल पर असर पहुंचता है. यह तो मशहूर बात है कि जब तक कोई नसीहत याने उपदेश देनेवाला उस नसीहत व उपदेश का आमिल न होगा तब तक करनेवाला सुननेवाले के असर दिल पर नहीं पहुंचता कि अमल करे. वह यह कहता है कि ख़ुदरा फजीहत व दीगरां नसीहत करते हैं. बस हे मेरे प्यारे भाइयो जब सभा विसर्जन करके श्रोता-वक्ता भाई साहेबान बाहर तशरीफ़ लाए तो न उस व्याख्यान की सुध है न उसके ध्यान की ख़बर है…’
और आख़िरकार इस सबका वही नतीजा हुआ जो होना था, सारी शेख़ी किरकिरी हो गई, अब— ‘न वह बूट जूता है न कोट पतलून है न गुलूबन्द है न टोपी पेटारीदार दस्तार है बल्कि रय्यार है पैरों में खार है जामाज़ीस्त से बेज़ार हैं घर की हालत कहना अनुचित प्रमात्मा रक्षपाल है धिक्कार धिक्कार धिक्कार आख़ थू आख़ थू आख़ थू घमंड पर है…’
इतनी लानत-मलामत के बाद जो कि सब पेशबन्दी है, किताबचा असल बात पर आता है— हे मेरे सजातीय भाई कायस्थ चित्रगुप्तवंशी क्या आप लोग अपने-अपने प्रत्यक्ष नेत्रों से यह न देखते होंगे कि जिन कन्याओं का विवाह हो गया है और दिरागमन याने गौना नहीं हुआ पति याने शौहर उनका मर गया है तो वह बाल विधवा बेचारी नाकर्दे गुनाह अपनी-अपनी जिन्दगी किस-किस मुसीबत से काटती हैं…दूसरे वह कन्याएं कि जिनका विवाह और दिरागमन दोनों हो गया है बहुत ही थोड़े दिन के बाद पति उनके मर गए हैं. कुछ भी जिन्दगी का लुत्फ़ नहीं उठाया यहां तक कि सन्तान उत्पन्न होने की नौबत नहीं. तो उन बेचारियों की मुसीबत कहने में नहीं आ सकती है. उनका घर में रहना माइका क्या ससुराल दोनों ही जगह के सहकुटुम्बी माता व पिता व भ्राता सब पर पहाड़ का ऐसा बोझ भार सिर पर मालूम होता है. ग़रज़ कि दोनों किसिम के बाल विधवा कन्या कि जिनका विवाह मात्र हुआ है दिरागमन नहीं हुआ और शास्त्र के अनुसार उनका कन्यात्व नष्ट नहीं हुआ वह मिसिल क्वांरी कन्या के हैं….हे मेरे भाइयो जांच करने से मालूम हुआ है व देखने में आया है कि उन कन्याओं दोनों किसिम की कि कुछ तो मुसीबत खाने-पीने से कुछ सतसंग पाकर कुछ काम के वश होकर कि कामदेव बड़ा बली शैतान है मतिभ्रम कर देता है कि बड़े-बड़े मुनियों और महात्मा के हृदय में क्षोभ कर दिया है और भला इन अबलाओं की क्या गिनती है व्यभिचार करने लगती हैं याने बहुतों का कस्बी हो जाना और बहुतों का घर ही में बदचलन हो जाना व बहुतों का अन्य पुरुष विरुद्ध वर्ण याने दूसरे जात के साथ निकल जाना बहुतों के हमल-हराम रह जाना व उसका इसक़ात हमल कराना बालक का मारना वग़ैरा वग़ैरा कहां तक कहा जावै बड़े-बड़े घोर पाप होते हैं व हो गए कि सुनि अघ नर्कहु नाक सकोरी. संसार में रूसियाही बल्कि पुश्तों तक का ऐसा दाग़ धब्बा लग जाता है कि उसका मिटाना बहुत कठिन हो जाता है….
(फर्याद बाल विधवा कन्याओं की) हे मेरे सजातीय कायस्थ चित्रगुप्तवंशी आप लोग ग़ौर करके बिला पक्षपात के इंसाफ़ कीजिए कि जब किसी पुरुष की स्त्री मर जाती है तो वह पुरुष दो-दो अथवा तीन-तीन विवाह कर लेने का अधिकारी होता है और हम बाल विधवाओं ने जो पति के पास तक नहीं गई हैं और पति का मुंह तक नहीं देखा है पुनर्विवाह हमारे करने में आप लोग लज्जा व घृणा करते हो…क्या पुरुष को काम प्रबल अधिक सताता है और हम काम को जीते हुए हैं. हे भाइयो, हम स्त्रियों का नाम ही कामिनी है. वैदक शास्त्र से ज़ाहिर है कि पुरुष से दुगुण अधिक काम अग्नि स्त्री के होती है…
इसके बाद फिर ऋग्वेद, यजुर्वेद, वशिष्ठस्मृति, नारदस्मृति, प्रजापतिस्मृति, कात्यायनस्मृति, मनुस्मृति आदि शास्त्रों से प्रमाण पर प्रमाण जुटाये गए हैं कि किन-किन दशाओं में विधवा का पुनर्विवाह सम्भव है, उचित है.
नवाब ने इस इश्तहार को पढ़ा तो उसकी तबीयत फड़क उठी. इस सवाल पर ख़ुद उसके विचारों से यह चीज़ कितना मेल खाती थी! उसने फ़ौरन लड़की की फ़ोटो की फ़रमाइश की.
देहात में तसवीर उतरवाने का तब कहां चलन, मगर ख़ैर मुंशी देवीप्रसाद ने अपनी लड़की की तसवीर उतरवाकर कानपुर भेजी— सीधी-सादी, दुबली-पतली एक देहाती लड़की, बाल बिखरे हुए, माथे पर हल्का-सा घूंघट. गन्दुमी रंग जो नवाब के तपे सोने जैसे रंग के मुक़ाबले में काफ़ी दबा हुआ था, नाक-नक़्श भी बहुत मामूली, कोई ख़ास बात नहीं, जब कि नवाब यक़ीनन दस-पांच हज़ार में एक ख़ूबसूरत नौजवान था. लेकिन उसे सुन्दरी की तलाश न थी— उसके नखरे उठाने की सकत भी उसमें कहां थी! वह तो एक सीधी-सादी घरेलू लड़की चाहता था जो उसके संग तकलीफ़-आराम झेल सके. यह लड़की, जहां तक देखने में आता था, वैसी ही थी. मुंशी दयानरायन से भी शायद मशविरा हुआ और फिर नवाब ने अपनी रज़ामन्दी लिख भेजी. अब मुंशी देवीप्रसाद ने लड़के को देखने की ख़्वाहिश ज़ाहिर की और उसे फतेहपुर बुलाया. नवाब पहुंचा. ससुर ने भी दामाद को पसन्द किया. ज़्यादा अब तंग करने के लिए था भी क्या. लेन-देन की कोई बात ही न थी. शादी उसी दम तय हो गई. दोनों पक्ष समझ रहे थे कि उन्हें अपनी-अपनी बिरादरी का विरोध सहना पड़ेगा और दोनों तैयार थे.
आख़िर 1906 के फागुन में शिवरात्रि के रोज़ शादी हो गई. नवाब के साथ बारात में, एक उनके छोटे भाई महताब को छोड़कर और कोई रिश्तेदार न था, बस दो-चार दोस्त और हमजोली जिनमें मुंशी दयानरायन ख़ास थे.
(मुंशी प्रेमचंद की जीवनी के लेखक अमृत राय हैं जो उनके पुत्र थे. इस किताब को हंस प्रकाशन ने छापा है, जो अब राजकमल प्रकाशन समूह का हिस्सा है. किताब का यह अंश प्रकाशन की अनुमति से छापा जा रहा है)
यह भी पढ़ें: कैसे लीडर बन गोपी, क्रांति का तराना गाते हुए संगदिल दिलीप कुमार नया दौर लिखते हुए अमर हो गए