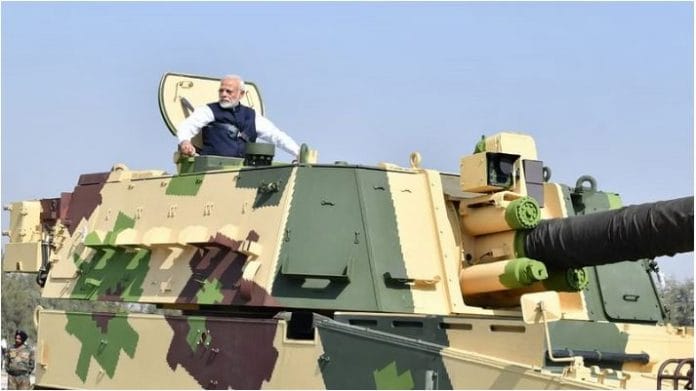राष्ट्रीय सुरक्षा की योजना बनाने वालों को भविष्य के अज्ञात और अप्रत्याशित खतरों और अवसरों से निपटने की तैयारी करने की ज़िम्मेदारी चाहे-अनचाहे लेनी ही पड़ती है. यह चुनौती संसाधन की कमी और विज्ञान और प्रौद्योगिकी में प्रगति की अबाध संभावनाओं के कारण और बढ़ जाती है. बाहर से होने वाले खतरे बेहतर जाने-पहचाने और स्वीकृत होते हैं. बगावतों आदि के रूप में उभरने वाले आंतरिक खतरे परेशान करने वाले होते हैं लेकिन सरकारें अक्सर उन पर काबू पाने की ताकत रखती हैं. लेकिन सांप्रदायिक टकराव ऐसा बारूद हैं जो लंबे समय तक अस्वीकृत और उपेक्षित रहने के कारण अक्सर फट पड़ते हैं. भारत के लिए तो यह जलती हुई चिनगारी ही रही है.
आरएसएस के सरसंघचालक मोहन भागवत ने मुस्लिम समुदाय के कुछ लोगों से हाल में मुलाक़ात की. इसके बाद वे एक मदरसे में गए ‘ऑल इंडिया मुस्लिम इमाम्स’ संगठन के मुखिया मोहम्मद इलयासी से मुलाक़ात की. भागवत की ये बैठकें शायद राष्ट्रीय स्तर पर हिन्दू-मुस्लिम संबंधों को लेकर चिंता का संकेत देती हैं. जाहिर है, दोनों पक्षों की गुप्त मंशाओं के लिए उनकी आलोचना की गई और उनके प्रयासों के बारे में यह मुगालता नहीं पाला जा सकता कि धर्म की राजनीति को लेकर उनमें कोई हृदय परिवर्तन हुआ है.
1990 के दशक के बाद से और अयोध्या में राम मंदिर को भारत में धर्म की राजनीति में प्रमुखता दिए जाने के कारण सांप्रदायिकता का पारा उफान पर रहा है. इस पारे को एक ओर भाजपा और आरएसएस व उसके समर्थकों ने और दूसरी ओर पाकिस्तान और कुछ कट्टरपंथी गुटों की शह पर काम करने वाले कुछ मुस्लिम संगठनों ने ऊपर चढ़ाने का काम किया है. इसका कुल असर यह हुआ है कि सांप्रदायिक सदभाव दूषित हुआ है और यह कुछ अलग-थलग जगहों में सीमित रहा है. लेकिन इस स्थिति की समीक्षा का वक़्त आ गया है क्योंकि हम असली खतरे को पहचान नहीं रहे हैं, जो सामान्य दृष्टि से ओझल है.
यह भी पढ़ें: म्यांमार बॉर्डर की बेहतर निगरानी और चीन के खतरे का मुकाबला करने के लिए सेना संभाले असम राइफल्स की कमान
असली खतरा क्या है
असली खतरे का अंदाजा मोहन भागवत के उस बयान से लगता है, जो उन्होंने मेघालय की जनजातीय आबादी की तरफ दिल्ली के हाथ बढ़ाने के अवसर पर दिया था— ‘पहचान के लिहाज से भारत के सभी लोग हिंदू हैं.’ ऐसा लगता है कि राजनीतिक हिंदुत्व सीमारेखाएं खींच रहा है जबकि हिंदू धर्म के दर्शन में कोई सीमारेखा नहीं खींची गई है और वह मूलतः बहुलतावादी है. सीमाएं ‘पराये’ को जन्म देती हैं, जो हिंदू धर्म को ईसाई और इस्लाम जैसे अब्राहमवादी धर्मों (Abrahamic religions) के करीब पहुंचा देती हैं लेकिन यहूदी धर्म को हमारे संदर्भ में अलग रखती हैं. इस तरह की धारणा को भारतीय सामाजिक ताने-बाने में पिरोना न केवल असंवैधानिक है बल्कि यह आंतरिक टकराव का आधार बना सकता है और राष्ट्रीय सुरक्षा तंत्र के लिए बड़ा खतरा बन सकता है.
जाहिर है, राजनीतिक हिंदुत्व यह मानता है कि धर्म के आधार पर बनी सांस्कृतिक पहचान राष्ट्रीय पहचान से बड़ी होती है. मार्के की बात यह है कि यह एक निर्वाचित सरकार की सैद्धांतिक देन है. लेकिन यह उस संवैधानिक खतरे को ढंक नहीं सकता जिससे बचाना हर उस तत्व की ज़िम्मेदारी है जिसने इसकी शपथ ली है. इस लिहाज से, अंतिम ज़िम्मेदारी सेना की है, जो सर्वोच्च संवैधानिक सत्ता राष्ट्रपति के अधीन होने के कारण इसके लिए कर्तव्यबद्ध है.
सेना की भूमिका
भारत के लोकतांत्रिक ढांचे में सेना की भूमिका का आधार उसका अ-राजनीतिक स्वरूप है. संवैधानिक ढांचे में, उसकी अंतिम निष्ठा राष्ट्रपति के प्रति है, जो कमांडर-इन-चीफ हैं. निर्वाचित सरकार कार्यपालिका के नाते सेना पर अपनी सत्ता का उपयोग राष्ट्रपति की ओर से करती है. सेना को जो अधिकार और जनादेश मिलता है वह सरकार के अधिकारों से संवैधानिक रूप से तय होता है. सिविल-मिलिटरी संबंधों के मामले में व्यापक सहमति इस बात पर है कि सेना राजनीतिक रूप से तटस्थ रहेगी और स्वैच्छिक रूप से सिविल सत्ता के अधीन रहेगी जबकि सिविल सत्ता ‘सेना की पेशागत स्वायत्तता’ को मान्यता देगी. भारत में सिविल-मिलिटरी ढांचे का अ-राजनीतिक स्वरूप पश्चिम के उदार लोकतांत्रिक देशों की सेनाओं से मिलता-जुलता है.
राजनीतिक हिंदुत्व जिस दिशा में जा रहा है उसकी दिशा बदलने के मामले में सेना कुछ नहीं कह सकती, और यह उचित भी है. लेकिन समाज की व्यापक प्रवृत्तियों और दिशा से परिचित सैन्य नेतृत्व क्या इस मसले की ओर से आंखें मूंदे रह सकता है? क्या सेना यह मान कर चल सकती है कि इस मामले में उससे कुछ करने की अपेक्षा नहीं रखी जाएगी, इसलिए इसमें वह कुछ नहीं कर सकती? दूसरी ओर, क्या सेना की पेशागत स्वायत्तता उसके नेतृत्व को यह आदेश नहीं देती कि वह सैन्य संस्थान के राष्ट्रीय मूल्यों की रक्षा करे, उन्हें मजबूत करे और घरेलू राजनीति की खतरनाक प्रवृत्तियों से उन्हें बचाए? क्या सैन्य नेतृत्व को यह नहीं चाहिए कि वह खुद संवेदनशील बने और सैनिकों को भी निरंतर संवेदनशील बनाए? अन्यथा सैन्य बल यह नहीं समझ पाएगा कि धर्म की राजनीति देश को किस दिशा में ले जा रही है. और उसे यह सब इस तरह करना है कि वह सरकार द्वारा दिए गए अधिकारों से बाहर जाकर काम करती न दिखे.
सीमाओं का सम्मान करते हुए काम करें
यह काफी कठिन और लगभग असंभव कार्य नज़र आता है. बेशक, यह दिखावा करना सबसे आसान है कि ऐसी कोई समस्या है ही नहीं, और न वह भविष्य में उभर सकती है. इसे अपने कर्तव्य का उल्लंघन भी नहीं माना जाएगा क्योंकि सेना को जानकार बनाने के उपाय न करने के दीर्घकालिक असर हो सकते हैं और इसके लिए किसी उच्च पदस्थ व्यक्ति— मसलन चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस) या सेनाओं के अध्यक्षों— को बाद में जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकेगा.
लेकिन कभी राष्ट्रीय स्तर पर लंबे समय तक गंभीर सांप्रदायिक संकट बना रहा और भारतीय सेना अगर अपने आंतरिक धार्मिक पूर्वाग्रह के कारण कानून-व्यवस्था लागू करने में विफल रही तो एक संस्थान के रूप में उसे इसके दोष से बरी नहीं किया जा सकेगा. हो सकता है, सेना में यह पूर्वाग्रह हाल में पैदा हुआ हो क्योंकि यह नागरिक समाज में भी खुल कर फैल रहा है और इसकी वजह यह है कि सैन्य नेतृत्व ने यह मान कर इस ओर से आंखें फेर ली हैं कि इससे उनका कोई मतलब नहीं है.
कई मौकों पर राजनीतिक नेतृत्व सेना के ऊंचे पदों पर नियुक्ति में अपनी ताकत का इस्तेमाल करके सीनियरिटी के सिद्धांत को हवा में उड़ाते रहे हैं. अगर इस कोशिश के साथ वह सैद्धांतिक झुकाव भी शामिल हो गया, जिसकी पैरवी भागवत ने मेघालय में की या उनकी नियुक्ति इस उम्मीद से की गई कि उनसे अपनी बात मनवाई जा सकती है, तो सांप्रदायिक विस्फोट (अगर ऐसा कुछ हुआ तब) का सामना करने की भारत की क्षमता कमजोर होगी और इसके नतीजे देश को भारी पड़ेंगे.
जैसी कि प्रचलित कहावत है, पार्टी और सरकार के बीच का अंतर खत्म होता जा रहा है. संस्थाएं जिस तरह चरमरा रही हैं, धर्म पर आधारित राज्य-व्यवस्था की ओर कदम बढ़ाने में ज्यादा देर नहीं लगेगी. इसलिए सेना को अपने अंदर झांकना होगा और अपने संस्थागत मूल्यों की रक्षा और मजबूती के उपाय करने पर ज़ोर देना होगा.
सैन्य ढांचा बिलकुल सीधा खड़ा है. उम्मीद इस बात पर टिकी है कि राष्ट्रीय सुरक्षा और मनोबल से जुड़े मसलों पर तीनों सेनाओं के शीर्ष सामूहिक पैनलों के बीच बंद कमरों में विचार-विमर्श होते हैं. इसमें सेना के दो उच्चतम स्तरों—सीडीएस/ तीनों सेनाओं के अध्यक्षों और उनसे ठीक नीचे के पदाधिकारियों, तीनों सेनाओं के कमांड फॉर्मेशनों के अध्यक्षों को शामिल किया जाना चाहिए. जो कुछ दांव पर लगा हो उसके मुताबिक, इन विमर्शों के नैतिक रूप से सफल नतीजे कर्तव्य की भावना और भारतीय संविधान के प्रति अटूट निष्ठा से तय होंगे.
इसमें शक नहीं कि सेना से जिस उच्च कर्तव्य के निर्वाह की अपेक्षा की जाती है उसका काफी अनुमान ही लगाया जा सकता है और उसके साथ आदर्शवाद बहुत जुड़ा है. अंततः, धर्म के नाम पर जो गिरावट आ रही है उसे जो बड़ी ताकत रोक सकती है वह सैन्यबल की नहीं बल्कि जनचेतना की ताकत ही हो सकती है. लेकिन इसके बहाने सेना अपने भीतर के दानवों से मुक़ाबला न करे, इसे उचित नहीं ठहराया जा सकता.
(इस लेख को अंग्रेजी में पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)
यह भी पढ़ें: महात्मा गांधी ने भारत को क्या दिया? आजादी की लड़ाई का सबसे बड़ा हथियार और संघर्ष का सबसे महान तरीका