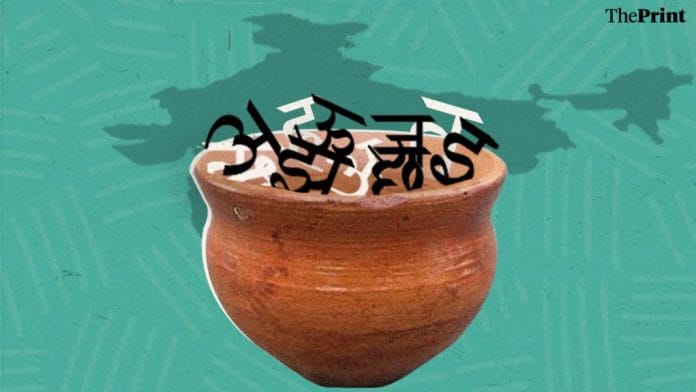अभी जब मैं हिंदी दिवस और हिन्दी के सिलसिले में आपसे बात करने की सोच रहा था, पिछले हिंदी दिवस का एक वाकया याद आ गया. कान्वेंट स्कूल में पढ़ रही मेरी नातिन को ‘हिंदी डे’ पर ‘एस्से’ लिखना था और उसके मां-बाप उसकी कोई मदद नहीं कर पा रहे थे. निराश होकर इतना ‘डिफीकल्ट एस्से’ लिखवाने के लिए अपनी टीचर पर झुंझलाती हुई-सी वह मेरे पास आई तो मैं उसको यह समझाते-समझाते परेशान हो गया था कि आजादी के दो साल बाद 1949 में 14 सितम्बर को संविधान सभा में महज एक मत के बहुमत से हिंदी को देश की राजभाषा घोषित किया गया तो क्यों उसे उसकी ‘विजय’ से ज्यादा आजादी की लड़ाई में उसके योगदान के पुरस्कार के तौर पर देखा गया था और क्यों उसके समर्थकों की खुशी का कोई पारावार नहीं था.
हां, उसे यह बताते-बताते कि इस खुशी के पीछे कोई संकीर्ण क्षेत्रवाद नहीं था क्योंकि हिंदी के उस दौर के समर्थकों में उसकी क्षेत्रीय परिधि के बाहर के अनेक अन्य भाषा-भाषी भी शामिल थे, मैं इस निष्कर्ष पर पहुंच चुका था कि यह सब समझने को लेकर वह कतई इमोशनल नहीं थी और चाहती थी कि जैसे-तैसे उसका ‘एस्से कम्प्लीट’ हो जाये बस. अलबत्ता, उसकी जिज्ञासा थी कि जब हिंदी को राजभाषा घोषित करने के चार चाल बाद तक इस दिन ‘हिंदी दिवस’ नहीं मनाया गया तो क्या जरूरत थी कि 1953 में वर्धा की राष्ट्रभाषा प्रचार समिति इसे मनाने का अनुरोध और उसे स्वीकृति दिलाने के प्रयत्न करती?
जब तक मैं उसे बताता कि तब देश के उन क्षेत्रों में राजभाषा के प्रचार-प्रसार और उन्नयन की गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिए इस दिवस की जरूरत थी, जो तब तक उसकी पहुंच से बाहर थे और इसीलिए 1975 में 10 जनवरी को नागपुर में पहला विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ तो उस दिन विश्व हिंदी दिवस भी मनाया जाने लगा, मेरा समाधान हो गया था कि इस बीच हिंदी की जड़ें कितने शातिराना ढंग से काट दी गई हैं.
यह भी पढे़ं: ऐसे ‘दोस्तों’ के रहते हिन्दी को दुश्मनों की क्या जरुरत
हिंदी दिवस के साथ कई विडम्बनाएं
इस शातिराने का ही फल है कि अब हिंदी दिवस के साथ कई विडम्बनाएं जुड़ गई हैं. अब इस दिन देश व दुनिया के भाषाई परिदृश्य में हुए भारी उलट-पलट की अनदेखी कर कभी ‘भूली-बिसरी’ हिंदी को याद किया जाता है, कभी उसके ‘पिछड़ेपन’ पर आंसू बहाये जाते हैं, कभी दर्शन, ज्ञान-विज्ञान और चिन्तन के बजाय, विज्ञापन व बाजार की ही भाषा होकर रह जाने को लेकर चिंताएं जताई जाती हैं, कभी प्रचार-प्रसार के प्रति समर्पण की झूठी-सच्ची कसमें खाई जाती हैं और कभी सरकारी दफ्तरों में हिंदी सप्ताह, पखवाड़े या माह वगैरह मनाये जाते हैं. हां, कभी ‘अपनी’ सरकार हुई तो उसकी अथक कोशिशों से प्रवासियों में अपनी जड़ों से बढ़ते जुड़ाव के कारण हिंदी का वैश्विक दबदबा बढ़ने की बात भी की जाती है. अलबत्ता, इस सवाल का जवाब गोल करते हुए कि हिंदी के बढ़ते दबदबे वाली उस दुनिया में भारत भी कहीं है या नहीं. कई बार इससे भी आगे बढ़कर नई तकनीक से हिंदी के सबलीकरण की बात भी की जाती है-इसे भुलाकर कि इस तकनीक को ही बहाना बनाकर कई जगहों से हिंदी को विदा भी कर दिया गया है.
चूंकि इन दोनों ही रवैयों का जमीनी हकीकत से मेल नहीं है, दोनों हिंदी के पांवों की बेड़ियों जैसे हैं. वे उसे आगे बढ़कर अपने रास्ते की वास्तविक चुनौतियों की ठीक से शिनाख्त तक नहीं करने देते. न ही उसकी हितचिंता से जुडे़ वास्तविक सवालों को हल होने देते हैं. मिसाल के तौर पर, उसके कई ‘शुभचिंतक’ उसके ज्ञान-विज्ञान या दार्शनिक चिंतन-मनन की भाषा न बन पाने को लेकर तो बड़ा स्यापा करते हैं लेकिन इसके कारण नहीं तलाशते. इस सवाल तक तो जाते ही नहीं कि जब हिन्दी प्रदेशों में ज्ञान-विज्ञान व दर्शन की कोई प्रतिष्ठा ही नहीं है, यहां तक कि संविधान में जरूरी बताये गये साइंटिफिक टेम्परामेंट की भी कदर नहीं, तो हिंदी उनकी भाषा होने का सपना भी क्योंकर देख सकती है?
राजनीतिक प्रवाहों की अनुकूलता व प्रतिकूलता के मद्देनजर कभी वे कहते हैं कि सरकार जान-बूझकर हिंदी के लिए कुछ नहीं करती, उसे उसकी उचित जगह दिलाने की इच्छाशक्ति नहीं दिखाती, उसके प्रति सौतेलापन बरतती है और कभी यह कि वह हिंदी की राह में भरपूर गलीचे बिछा रही है. साफ है कि कभी वे अंतिरंजनाओं से काम लेते हैं तो कभी पूर्वाग्रहों से, लेकिन कभी भी वस्तुनिष्ठ नहीं हो पाते. उन्हें यह सवाल निमकौड़ी जैसा लगता है कि आजादी के 75 साल भी हिंदी को अपनी स्थिति के लिए राज्याश्रय की मोहताज क्यों होना चाहिए? अब तक के राज्याश्रय ने सम्मानितों-पुरस्कृतों और सम्मान व पुरस्कार के आंकाक्षियों की जमात बड़ी करने के अलावा उसे क्या दिया है? क्या ‘संत को कहां सीकरी सों काम, आवत जात पनहियां टूटी, बिसरि गयो हरिनाम’ कहते और ‘नर का मनसबदार’ होने से इनकार हुए राज्याश्रय को हमेशा अपने ठेंगे पर रखने वाले भक्त कवियों ने अपने वक्त की प्रतिकूलताओं में भी इस जमात से कुछ कम हिंदी सेवा की?
नहीं. कम की होती तो हिंदी के वरिष्ठ साहित्यकार नरेश सक्सेना को उसकी आज की ‘राज्याश्रयी शाखा’ की करतूतों से क्षुब्ध होकर यह नहीं कहना पड़ता कि हिंदी का भला इसी में है कि उसको फौरन राजभाषा के पद से हटा दिया जाये? क्योंकि एक तो उसका यह पद हाथी के दांतों जैसा है, जो खाने के और होते हैं, दिखाने के और. दूसरे, इस दिखावे की बिना पर वह अन्य भारतीय भाषाओं की घृणा, दूसरे शब्दों में कहें तो सौतियाडाह, झेलती रहने को अभिशप्त हो गई है.
ऐसे में नरेश सक्सेना के इस सवाल का सामना क्यों नहीं किया जाना चाहिए कि हिंदी राजभाषा न रहे, जो वह वास्तव में अभी बन भी नहीं पायी है, तो किसी भारतीय भाषा को उसके कथित साम्राज्यवाद का भय क्यों सतायेगा? या किसी भी अन्य भाषा को राजभाषा या राष्ट्रभाषा बना दिया जाये, तो हिंदी से क्या छिन जायेगा, जब इस बिना पर उसे कभी कुछ मिला ही नहीं?
लेकिन क्या कीजिएगा, जिन्हें खुद को राष्ट्रवादी कहने वाली सरकार द्वारा अधिकतर सरकारी योजनाओं के नाम अंग्रेजी में रखने, यहां तक कि नारे भी अंग्रेजी में देने में कोई हिंदी विरोध नहीं दिखता, वे ऐसे सवालों का सामना क्योंकर कर सकते हैं? वे भी नहीं ही कर सकते, जिन्हें पत्रकारिता के हिंदी को पालने-पोषने में अप्रतिम व ऐतिहासिक योगदान के बावजूद उसके जीवन मरण के संकटों से कोई लेना-देना नहीं है. उन विश्वविद्यालयों के संकट से भी नहीं, जिनके संकेतों की गहराई शीर्षस्थ आलोचक विजय बहादुर सिंह के इस बयान से आंकी जा सकती है कि आज हिंदी में जितने भी महत्वपूर्ण काम हो रहे हैं, विश्वविद्यालयों व उच्च शिक्षा संस्थानों से बाहर हो रहे हैं? तिस पर हिंदी के पास अवतार सिंह पाश जैसे अंतिम सांस तक अपनी जनता के संघर्षों में जूझने वाले कवियों या साहित्यकारों का भी अकाल है.
अंग्रेजी रानी और वह नौकरानी बनी हुई है
अंत में एक और बात. हिंदी में ऐसे उलाहने देने की परम्परा बहुत समृद्ध है कि देश के दक्षिण के राज्यों के विरोध, नकार या अस्वीकार के कारण ही हिंदी आज तक वास्तविक राजभाषा नहीं बन पाई है, अंग्रेजी रानी और वह नौकरानी बनी हुई है. लेकिन इस पर विचार नहीं किया जाता कि आजादी के शुरुआती दशकों में हिंदी-हिंदी का शोर मचाकर उन राज्यों में यह धारणा किसने फैलाई कि हिंदी तो सच पूछिये तो अंग्रेजी का स्थान लेने की उतावली में है और वह दूसरी भारतीय भाषाओं की अंग्रेजी जैसी ही दुश्मन है.
इस बिंदु पर भी कोई नहीं ही सोचता कि उक्त धारणा को दूर करने के लिए हिंदी भाषी राज्यों में दक्षिण की भाषाओं के पठन-पाठन का त्रिभाषा फार्मूला लाया गया तो उसे किसने विफल किया? क्यों राजनीतिक विरोध के बावजूद हिंदी दक्षिण भारतीय राज्यों में धीरे-धीरे ही सही फैल रही है, लेकिन दक्षिण की भाषाओं में हिंदी भाषियों की रुचि कतई नहीं जाग रही. यों हिंदी समाज ‘अपनी’ हिंदी की कदर भी नहीं कर पा रहा और इस व्यामोह में फंसा हुआ है कि इंग्लिश मीडियम में दीक्षित उसके बच्चे हाय-बाय भी बोलें और उनका चरण स्पर्श करना भी न भूलें. सवाल है कि ऐसे व्यामोह के रहते हिंदी के आरोहों व अवरोहों का वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन कैसे मुमकिन हो और बिना उसे मुमकिन किये उसकी राह के कांटे कैसे बुहारे जायें?
(कृष्ण प्रताप सिंह फैज़ाबाद स्थित जनमोर्चा अखबार के संपादक और वरिष्ठ पत्रकार हैं. व्यक्त विचार निजी हैं)
यह भी पढे़ं: ‘खून के धब्बे धुलेंगे कितनी बरसातों के बाद’- राजनीतिक सत्ता में बैठे हुक्मरानों को फैज़ से डर क्यों