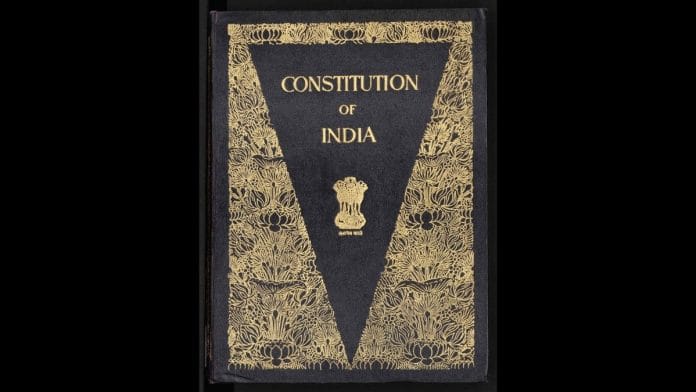समाजवाद की विचारधारा की उत्पति भारत में नहीं हुई. भारत के लिहाज से यह आयातित सामाजिक-आर्थिक दर्शन है. हालांकि आजादी के आंदोलन के अंतिम दौर में भारत में कई नेता समाजवादी दर्शन से प्रभावित रहे. यह भी सही है कि आजादी के बाद ‘समाजवाद’ को ठोक-ठेठा कर भारतीय विचारधारा के तौर पर साबित करने के खूब प्रयोग हुए.
इन्हीं प्रयोगों के तहत इसे ‘भारतीय समाजवाद’ का नाम देकर अलग-अलग ढंग से परिभाषित करने की कोशिशें भी हुईं जो अभी भी जारी हैं. मगर व्यावहारिकता की कसौटी पर वे अनेक प्रयोग असफल ही साबित हुए. मिसाल के तौर पर 1991 के आर्थिक सुधारों को कांग्रेस द्वारा समाजवाद के आकर्षण में की गयी चालीस साल की गलतियों के ‘भूल सुधार’ के तौर पर देखना चाहिए. वह एक भूल सुधार था, जिसे नरसिम्हा राव को भारत के ढहते आर्थिक ढांचे को बचाने के लिए मजबूरी में करना पड़ा. अगर आजादी के बाद समाजवाद की नीतियां सफल हुई होतीं तो 1991 के आर्थिक सुधारों की जरुरत ही नहीं पड़ती.
यह ठीक है कि हमने भूल सुधार किए, लेकिन यह भी सच है कि हमने आधे-अधूरे सुधार ही किये. हमने उस गलती को तो कुछ हदतक सुधार लिया जो पंडित नेहरु के दौर में समाजवादी नीतियों के साथ आगे बढ़ने को लेकर हुई थी, किंतु उस गलती को चिमटे से भी नहीं छुआ, जिस गलती को इंदिरा गांधी ने 1976 में आपातकाल के दौरान किया था.
य़ह भी पढ़ें: क्यों जाति-व्यवस्था से मुक्ति पाने के लिए आंबेडकर ने पंथ-परिवर्तन का रास्ता अपनाया
42 वां संविधान संशोधन और समाजवाद
समाजवाद के मोह में पंडित नेहरु और इंदिरा गांधी दोनों से गलतियां हुईं. परंतु दोनों की गलतियों में बुनियादी अंतर है. जिस समाजवाद की आर्थिक नीतियों को नेहरु ने भारत की राज्य प्रणाली में व्यवहारिक बनाने का प्रयास किया, इंदिरा गांधी ने उसे संवैधानिक जामा पहना दिया. यह अलग बात है कि जब यह सबकुछ घटित हो रहा था तब देश का लोकतंत्र बंधक था. आपातकाल लागू था. सरकार से असहमत लोग जेल में थे.
3 जनवरी 1977 को 42वां संविधान संशोधन लागू होते ही एक स्टेट के रूप में भारत गणराज्य की विचारधारा ‘समाजवादी’ हो गयी. समाजवादी राज्य बनना हमारे लोकतांत्रिक गणराज्य का आधिकारिक उद्देश्य बन गया. आज असहमतियों के बावजूद भी कोई राजनीतिक दल ‘समाजवाद’ को खारिज करने की स्थिति में नहीं रह सकता है.
भारत को ‘समाजवादी’ गणराज्य घोषित करने के साथ ही 3 जनवरी 1977 की उसी तारीख को संविधान में यह भी दर्ज हुआ कि स्टेट के रूप में भारत गणराज्य का कोई ‘पंथ’ नहीं है. एक राज्य के नाते भारत ‘पंथनिरपेक्ष’ रहेगा. आश्चर्य होता है कि परस्पर दो विरोधाभाषी शब्दों को एक साथ, एक दिन, एक समय संविधान का हिस्सा बना दिया गया.
संविधान और लोकतंत्र की भावना में विरोधाभास पैदा करने वाला वह संशोधन आज भी कायम है. यह भूल-सुधार कब होगा अथवा होगा भी या नहीं होगा, कहना कठिन है.
ऐसा नहीं है कि 42वें संशोधन के तहत जितने नए प्रावधान लागू हुए, वो सब कायम हैं. इंदिरा की हार होने के बाद 1977 में आई जनता पार्टी की सरकार ने 44वें संशोधन से 42वें संशोधन के अनेक फैसलों को पलट दिया. फिर भी उद्देशिका में हुए बदलाव नहीं पलटे. इसका कारण शायद यही रहा होगा कि जनता पार्टी सरकार में समाजवादी भी थे, राष्ट्रवादी भी थे, कांग्रेसी भी थे और कुछ यथास्थितिवादी नेता भी थे. अत: संभव है कि इस बदलाव से होने वाले संभावित टकराव की स्थिति में जनता पार्टी सरकार जाना नहीं चाहती होगी.
2019 के आंकड़ों के अनुसार देश में 2293 पंजीकृत राजनीतिक दल हैं. इनमें प्रमुख रूप से 7 राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त दल हैं तथा 59 प्रदेश स्तर पर की मान्यता वाले राजनीतिक दल हैं. क्या ये सभी दल इस बात के लिए बाध्य ही रहेंगे कि उन्हें ‘समाजवादी’ विचार के प्रति उन्हें असहमत नहीं होना है. असहमत हैं भी तो इसका विरोध नहीं कर सकते हैं? विरोध इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि ‘समाजवाद’ का विरोध संविधान की उद्देशिका का विरोध हो सकता है!
राज्यों की समस्याओं के समाधान में विफल समाजवाद
सवाल यह भी है कि ऐसे में यदि कोई राजनीतिक दल ‘समाजवाद’ के सिद्धांतों का विरोध करता हो अथवा उससे इतर अपनी अलग वैचारिक राय रखता हो तो उसे भारत में चुनकर शासन करने का अधिकार क्यों नहीं होना चाहिए?
यह प्रमाणित तथ्य है कि समाजवाद की नीतियां आधुनिक विश्व में असरहीन और अप्रासंगिक साबित हुई हैं. जिन देशों में समाजवाद का उदय हुआ, वही देश इससे बाहर निकल चुके हैं. इसके पीछे कारण यही रहा है कि बीसवीं शताब्दी के शुरूआती कालखंड में समाजवाद का आदर्शलोक सत्ता को हासिल करने उपकरण तो बना, लेकिन राज्य की समस्याओं के समाधान के स्थायी रास्ते खोजने में विफल हुआ.
दुनिया के तमाम देश जो समाजवाद के अंध उत्साह में आगे बढ़े थे, उन्हें एक समय के बाद अपने पांव रोकने पड़े. उन्हें अहसास हो गया कि वे एक अव्यवहारिक मॉडल पर जा रहे हैं, जिसका ढहना निश्चित है. जिन्होंने अपने पांव नहीं रोके उन्हें कालक्रम में चित होना पड़ा.
लगभग सभी लोकतांत्रिक देशों ने यह कमोबेस मान लिया है कि उत्पादन के साधनों पर स्वामित्व(Ownership), नियंत्रण(Control) और नियमन(Regulation) राज्य द्वारा किया जाना असंभव और अव्यवहारिक है. यह मछली को पेड़ पर चढना सिखाने की जिद पालने जैसा है. ऐसे में राज्य का दायरा सिर्फ नियमन तक सीमित हो रहा है. आज भी जिन देशों समाजवादी नीतियां लागू हैं, उनमें से अनेक देश अपने राजनीतिक मॉडल को तो समाजवाद की अलोकतांत्रिक प्रणाली से चला रहे हैं लेकिन आर्थिक नीतियों में उन्हें भी ढील देनी ही पड़ी है. भारत में तो समाजवादी धारा इस नाते भी असफल कही जायेगी क्योंकि यहां समाजवादी राजनीति ने ‘परिवारवाद’ का नया विद्रूप रूप पकड़ लिया.
समाजवाद का एक दोष यह भी है कि वह अपने मूल रूप में लोकतंत्र के साथ सामानांतर टिका नहीं रह सकता. सोवियत संघ का विभाजन इसका सबसे बड़ा उदाहरण है. लोकतंत्र की आशाएं जितनी प्रबल होती हैं, समाजवादी सत्ता की जड़ें उतनी ही कमजोर होती जाती हैं.
ऐसे में गंभीर सवाल है कि इंदिरा गांधी ने आपातकाल के आनन-फानन में अगर ‘समाजवादी’ शब्द को संविधान की उद्देशिका का हिस्सा बनाया तो उनकी मंशा क्या रही होगी ? संविधान के 42वें संशोधन के प्रावधानों को देखकर यह संदेह तो उठता ही है कि कहीं इंदिरा गांधी भारत को भी सोवियत मॉडल के तर्ज पर ‘समाजवादी लोकतंत्र’ की तरफ तो ले जाने के मंशा तो नहीं पाल बैठी थीं ? वरना उस परिस्थिति में समाजवाद को संविधान की उद्देशिका का हिस्सा बनाने का और क्या औचित्य समझ आता है ?
खैर, ‘समाजवादी’ विचारधारा की बाध्यता संविधान में रहनी चाहिए अथवा नहीं, यह एक प्रश्न है. इस प्रश्न पर और अधिक विमर्श होना चाहिए. इसपर व्यापक चर्चा होनी चाहिए. लेकिन एक सवाल यह भी कि अगर भारत के संविधान की उद्देशिका में आयातित ‘समाजवादी’ विचारधारा को जगह मिल सकती है तो क्या किसी और भी विचारधारा को भी जगह मिल सकती है ? मसलन क्या ‘राष्ट्रवादी’ शब्द भी कभी उद्देशिका का हिस्सा बन सकता है?
लेखक भाजपा के थिंकटैंक एसपीएमआरएफ में फेलो हैं. लेख में व्यक्त विचार उनके निजी हैं.
यह भी पढ़ें: कई फसलों को आवश्यक वस्तु के दायरे से निकालने के कदम पर गांधी मोदी के साथ होते तो नेहरू के विरोध में